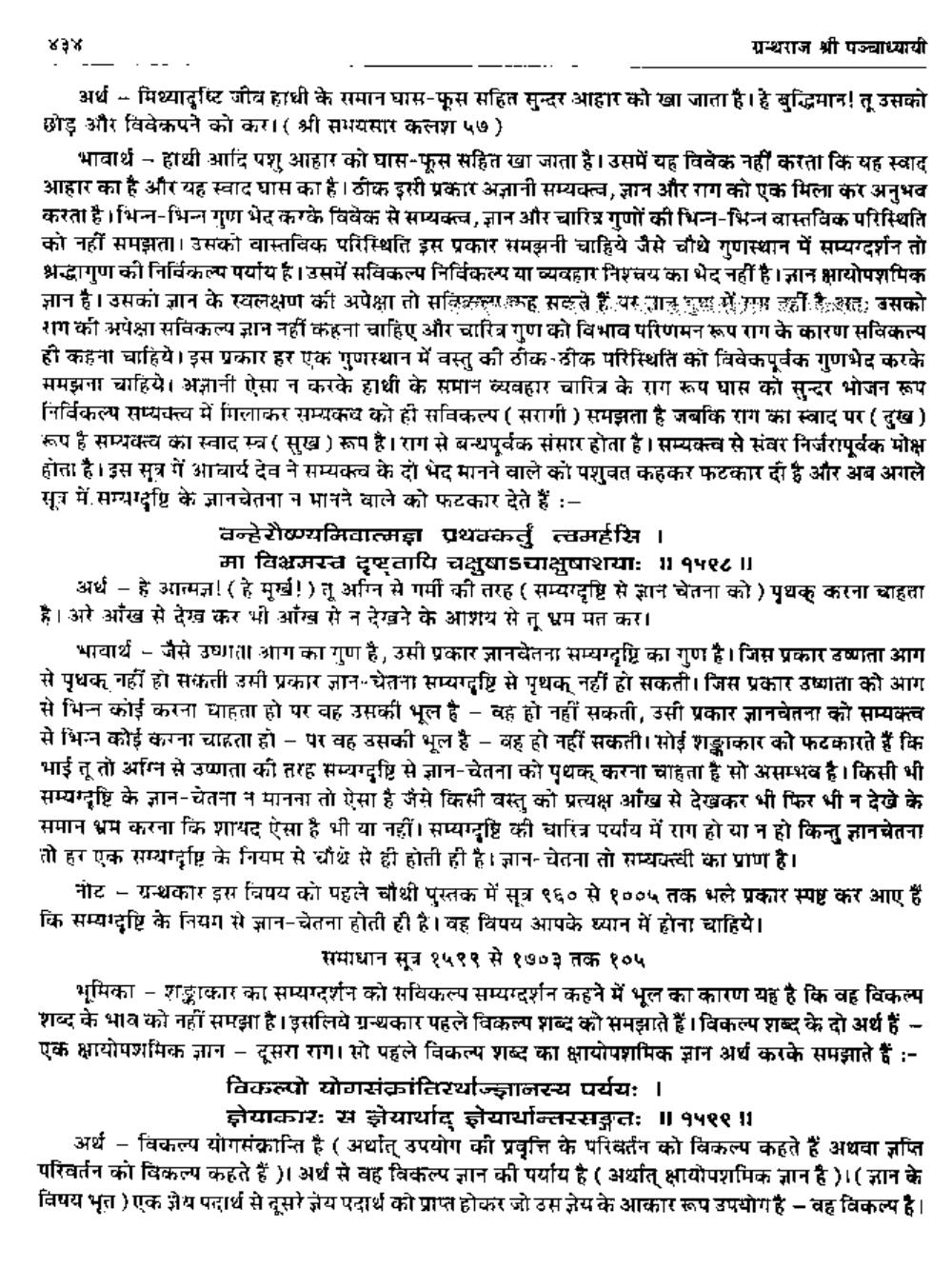________________
४३४
ग्रस्थराज श्री पञ्चाध्यायी
---"-..
-
____ अर्थ - मिथ्यादृष्टि जीव हाधी के समान घास-फूस सहित सुन्दर आहार को खा जाता है। हे बुद्धिमान! तू उसको छोड़ और विवेकपने को कर। ( श्री समयसार कलश ५७)
भावार्थ - हाथी आदि पशु आहार को घास-फूस सहित खा जाता है। उसमें यह विवेक नहीं करता कि यह स्वाद आहार का है और यह स्वाद घास का है। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी सम्यक्त्व, ज्ञान और गग को एक मिला कर अनुभव करता है। भिन्न-भिन्न गाभेद करके विवेक से सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्रगुणों की भिन्न-भिन्न वास्तविक परिस्थिति को नहीं समझता। उसको वास्तविक परिस्थिति इस प्रकार समझनी चाहिये जैसे चौथे गुणस्थान में सम्यग्दर्शन तो श्रद्धागुण की निर्विकल्प पर्याय है। उसमें सविकल्प निर्विकल्प या व्यवहार निश्चय का भेद नहीं है। ज्ञान क्षायोपशामिक ज्ञान है । उसको ज्ञान के स्वलक्षण की अपेक्षा तो सचिवमा कह सकते हैं. परवाच अपर में नहीं है. अतः उसको राग की अपेक्षा सविकल्प ज्ञान नहीं कहना चाहिए और चारित्र गुण को विभाव परिणमन रूप राग के कारण सविकल्प ही कहना चाहिये। इस प्रकार हर एक गुणस्थान में वस्तु की ठीक-ठीक परिस्थिति को विवेकपूर्वक गुणभेद करके ममझना चाहिये। अज्ञानी ऐसा न करके हाथी के समान व्यवहार चारित्र के राग रूप घास को सुन्दर भोजन रूप निर्विकल्प सम्यक्त्व में मिलाकर सम्यकप को ही सविकल्प ( सरागी) समझता है जबकि राग का स्वाद पर ( दुख) रूप है सम्यक्त्व का स्वाद स्त्र ( सुख ) रूप है। राग से बन्थपूर्वक संसार होता है। सम्यक्त्व से संवर निर्जरापूर्वक मोक्ष होता है। इस सूत्र में आचार्य देव ने सम्यक्व के दो भेद मानने वाले को पशुवत कहकर फटकार दी है और अब अगले सूत्र में सम्यग्दष्टि के ज्ञानचेतना न मानने वाले को फटकार देते हैं :
तन्हेरौष्ण्यमिवात्मज्ञ प्रथक्कर्तुं त्तमर्हसि ।
मा विभमरत्वदरतापि चक्षषाचाक्षषाशयाः ॥१५९८॥ अर्थ – हे आत्मज्ञ! (हे मूर्ख!) तू अग्नि से गर्मी की तरह ( सम्यग्दृष्टि से ज्ञान चेतना को) पृथक् करना चाहता है। अरे आँख से देख कर भी आँख से न देखने के आशय से तू धम मत कर।
भावार्थ - जैसे उघणात आग का गुण है, उसी प्रकार ज्ञानवेतना सम्यग्दृष्टि का गुण है। जिस प्रकार उष्णता आग से पृधक नहीं हो सकती उसी प्रकार ज्ञान चेतना सम्यग्दृष्टि से पृथक् नहीं हो सकती। जिस प्रकार उष्णता को आग से भिन्न कोई करना चाहता हो पर वह उसकी भूल है - वह हो नहीं सकती, उसी प्रकार ज्ञानचेतना को सम्यक्त्व से भिन्न कोई करना चाहता हो - पर वह उसकी भूल है - वह हो नहीं सकती। सोई शङ्काकार को फटकारते हैं कि भाई तू तो अग्नि से उष्णता की तरह सम्यग्दृष्टि से ज्ञान-चेतना को पृथक करना चाहता है सो असम्भव है। किसी भी सम्यग्दृष्टि के ज्ञान-चेतना न मानना तो ऐसा है जैसे किसी वस्तु को प्रत्यक्ष आंख से देखकर भी फिर भी न देखे के समान भ्रम करना कि शायद ऐसा है भी या नहीं। सप्यादष्टि की चारित्र पर्याय में राग हो या न हो किन्तु ज्ञानचेतना तो हर एक सम्यादृष्टि के नियम से चौथे रे ही होती ही है। ज्ञान-चेतना तो सम्यक्त्वी का प्राण है।
नोट - ग्रन्थकार इस विषय को पहले चौथी पुस्तक में सूत्र ९६० से १००५ तक भले प्रकार स्पष्ट कर आए हैं कि सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान-चेतना होती ही है। वह विषय आपके ध्यान में होना चाहिये।
समाधान सूत्र १५९९ से १७०३ तक १०५ भूमिका - शङ्काकार का सम्यग्दर्शन को सविकल्प सम्यग्दर्शन कहने में भूल का कारण यह है कि वह विकल्प शब्द के भाव को नहीं समझा है। इसलिये ग्रन्थकार पहले विकल्प शब्द को समझाते हैं। विकल्प शब्द के दो अर्थ हैं - एक क्षायोपथमिक ज्ञान - दूसरा रागा सो पहले विकल्प शब्द का क्षायोपशमिक ज्ञान अर्थ करके समझाते हैं :
विकल्पो योगसंक्रांतिराज्ज्ञानस्य पर्ययः ।
क्षेयाकारः स शेयार्थाद ज्ञेयार्थान्तरसङ्गतः ॥ १५९९॥ अर्थ – विकल्प योगसंक्रान्ति है ( अर्थात् उपयोग की प्रवृत्ति के परिवर्तन को विकल्प कहते हैं अथवा ज्ञप्ति परिवर्तन को विकल्प कहते हैं )। अर्थ से वह विकल्प ज्ञान की पर्याय है ( अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञान है)। (ज्ञान के विषय भृत ) एक ज्ञेय पदार्थ से दूसरे ज्ञेय पदार्थ को प्राप्त होकर जो उस ज्ञेय के आकार रूप उपयोग है - वह विकल्प है।