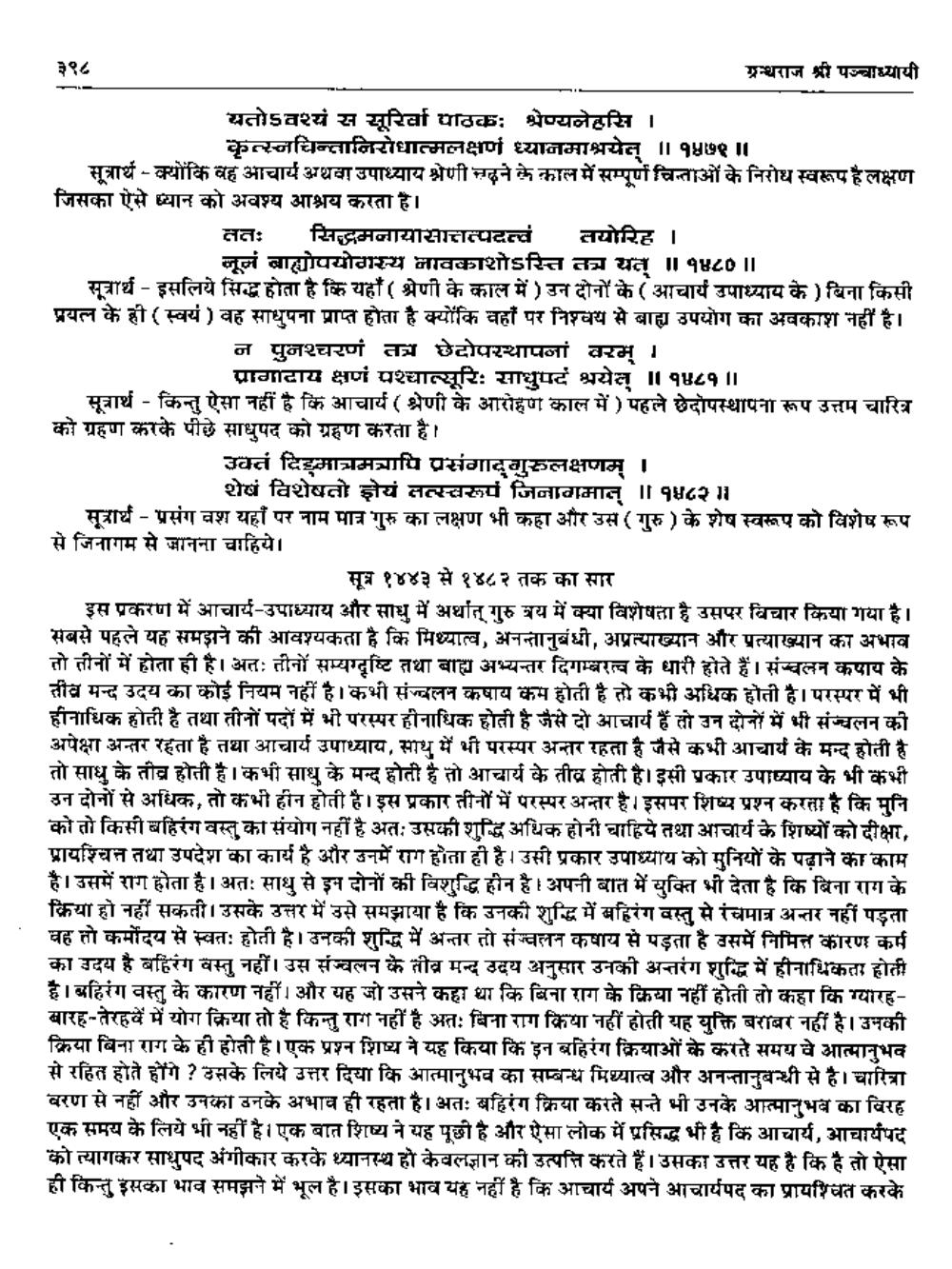________________
३९८
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
यतोऽवश्यं स सूरिर्वा पाठकः श्रेण्यनेहसि ।
कत्रनचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत ॥ १४७९।। थ - क्योंकि वह आचार्य अथवा उपाध्याय श्रेणी मढ़ने के काल में सम्पूर्ण चिन्ताओं के निरोध स्वरूप है लक्षण जिसका ऐसे ध्यान को अवश्य आश्रय करता है।
ततः सिन्द्रमनायासात्तत्परत्वं तयोरिह ।
जूनं बाह्योपयोगस्य नावकाशोऽस्ति तत्र यत् ॥ १४८० ॥ सूत्रार्थ - इसलिये सिद्ध होता है कि यहाँ( श्रेणी के काल में ) उन दोनों के (आचार्य उपाध्याय के बिना किसी प्रयत्न के ही (स्वयं ) वह साधुपना प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ पर निश्चय से बाह्य उपयोग का अवकाश नहीं है।
न पुनश्चरणं तत्र छेदोपस्थापनां वरम् ।
प्रागादाय क्षणं पश्चात्सूरिः साधुपदं श्रयेत् ॥ १४८१॥ सत्रार्थ - किन्त ऐसा नहीं है कि आचार्य (श्रेणी के आरोहण काल में पहले छेदोपस्थापना रूप उ को ग्रहण करके पीछे साधुपद को ग्रहण करता है।
उक्तं दिमात्रमत्रापि प्रसंगाद्गुरुलक्षणम् ।
शेख विशेषतो होयं तत्स्वरूयं जिनागमाल || १५८२॥ सूत्रार्थ - प्रसंग वश यहाँ पर नाम मात्र गुरु का लक्षण भी कहा और उस (गुरु) के शेष स्वरूप को विशेष रूप से जिनागम से जानना चाहिये।
सूत्र १४४३ से १४८२ तक का सार इस प्रकरण में आचार्य-उपाध्याय और साधु में अर्थात् गुरु वय में क्या विशेषता है उसपर विचार किया गया है। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अभाव तो तीनों में होता ही है। अत: तीनों सम्यग्दृष्टि तथा बाह्य अभ्यन्तर दिगम्बरत्व के धारी होते हैं। संचलन कषाय के तीव्र मन्द उदय का कोई नियम नहीं है। कभी संज्वलन कषाय कम होती है तो कभी अधिक होती है। परस्पर में भी हीनाधिक होती है तथा तीनों पदों में भी परस्पर हीनाधिक होती है जैसे दो आचार्य हैं तो उन दोनों में भी संचलन की अपेक्षा अन्तर रहता है तथा आचार्य उपाध्याय, साथ में भी परस्पर अन्तर रहता है जैसे कभी आचार्य के मन्द होती है तो साधु के तीव्र होती है। कभी साधु के मन्द होती है तो आचार्य के तीव्र होती है। इसी प्रकार उपाध्याय के भी कभी उन दोनों से अधिक, तो कभी हीन होती है। इस प्रकार तीनों में परस्पर अन्तर है। इसपर शिष्य प्रश्न करता है कि मुनि को तो किसी बहिरंग वस्तु का संयोग नहीं है अतः उसकी शुद्धि अधिक होनी चाहिये तथा आचार्य के शिष्यों को दीक्षा, प्रायश्चित्त तथा उपदेश का कार्य है और उनमें राग होता ही है। उसी प्रकार उपाध्याय को मुनियों के पढ़ाने का काम है। उसमें राग होता है। अतः साधु से इन दोनों की विशुद्धि हीन है। अपनी बात में युक्ति भी देता है कि बिना राग के क्रिया हो नहीं सकती। उसके उत्तर में उसे समझाया है कि उनकी शुद्धि में बहिरंग वस्तु से रंचमात्र अन्तर नहीं पड़ता वह तो कर्मोदय से स्वत: होती है। उनकी शुद्धि में अन्तर तो संचलन कषाय से पड़ता है उसमें निमित्त कारण कर्म का उदय है बहिरंग वस्तु नहीं। उस संचलन के तीव्र मन्द उदय अनुसार उनकी अन्तरंग शुद्धि में हीनाधिकता होती है। बहिरंग वस्तु के कारण नहीं। और यह जो उसने कहा था कि बिना राग के क्रिया नहीं होती तो कहा कि ग्यारहबारह-तेरहवें में योग क्रिया तो है किन्तु राग नहीं है अतः बिना राग क्रिया नहीं होती यह युक्ति बराबर नहीं है। उनकी क्रिया बिना राग के ही होती है। एक प्रश्न शिष्य ने यह किया कि इन बहिरंग क्रियाओं के करते समय वे आत्मानुभव से रहित होते होंगे? उसके लिये उत्तर दिया कि आत्मानुभव का सम्बन्ध मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी से है। चारित्रा वरण से नहीं और उनका उनके अभाव ही रहता है। अतः बहिरंग क्रिया करते सन्ते भी उनके आत्मानुभव का विरह एक समय के लिये भी नहीं है। एक बात शिष्य ने यह पूछी है और ऐसा लोक में प्रसिद्ध भी है कि आचार्य,आचार्यपद को त्यागकर साधुपद अंगीकार करके ध्यानस्थ हो केवलज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। उसका उत्तर यह है कि है तो ऐसा ही किन्तु इसका भाव समझने में भूल है। इसका भाव यह नहीं है कि आचार्य अपने आचार्यपद का प्रायश्चित करके