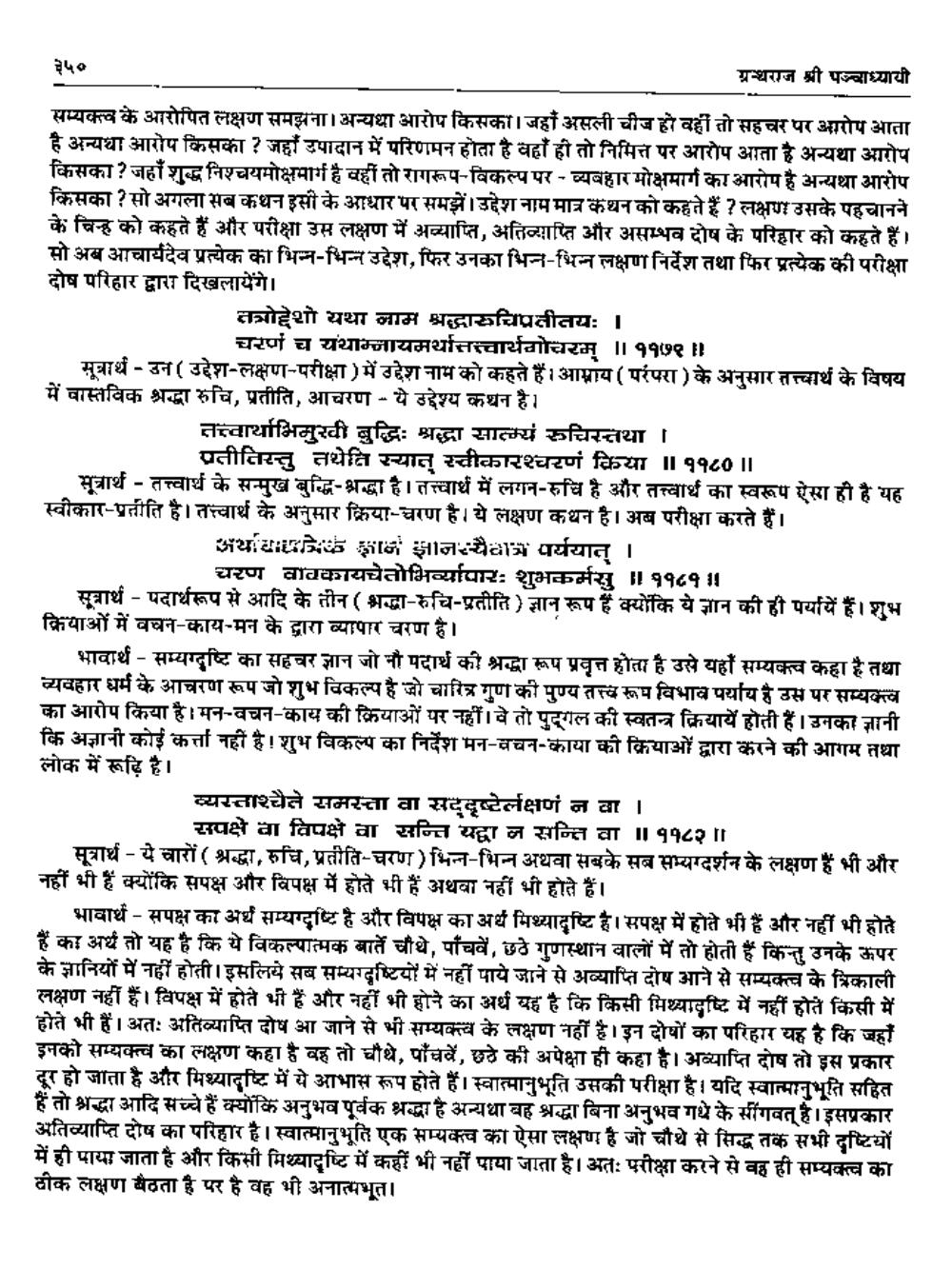________________
ग्रन्थराज श्री पञ्वाध्यायी
सम्यक्त्व के आरोपित लक्षण समझना। अन्यथा आरोप किसका। जहाँ असली चीज हो वहीं तो सहचर पर आरोप आता है अन्यथा आरोप किसका? जहाँ उपादान में परिणमन होता है वहाँ ही तो निमित्त पर आरोप आता है अन्यथा आरोप किसका? जहाँ शुद्ध निश्चयमोक्षमार्ग है वहीं तो रागरूप-विकल्प पर - व्यवहारमोक्षमार्गका आरोप है अन्यथा आरोप किसका? सो अगला सब कथन इसी के आधार पर समझें। उद्देश नाम मात्र कथन को कहते हैं ? लक्षण उसके पहचानने के चिन्ह को कहते हैं और परीक्षा उस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोष के परिहार को कहते हैं। सो अब आचार्यदेव प्रत्येक का भिन्न-भिन्न उद्देश,फिर उनका भिन्न-भिन लक्षण निर्देश तथा फिर प्रत्येक की परीक्षा दोष परिहार द्वारा दिखलायेंगे।
तत्रोद्देशो यथा नाम श्रद्धासचिप्रतीतयः ।
चरणं च यथाम्जायमर्थातत्वार्थगोचरम् ॥ ११७९॥ सत्रार्थ - उन उद्देश-लक्षण-परीक्षा) में उद्देशनामको कहते हैं। आम्राय ( परंपरा के अनसार तत्त्वार्थ में वास्तविक श्रद्धा रुचि, प्रतीति, आचरण - ये उद्देश्य कथन है।
तत्वार्थाभिमुखी बुद्धिः श्रद्धा सात्म्यं रुचिरत्तथा ।
प्रतीतिरतु तथेति स्यात् स्तीकारश्चरणं क्रिया ॥ ११८० ॥ सूत्रार्थ - तत्त्वार्थ के सन्मुख बुद्धि-श्रद्धा है। तत्त्वार्थ में लगन-रुचि है और तत्त्वार्थ का स्वरूप ऐसा ही है यह स्वीकार-प्रतीति है। तत्वार्थ के अनुसार क्रिया-चरण है। ये लक्षण कथन है। अब परीक्षा करते हैं।
अर्थाय झामझानस्यैवापर्ययात् ।
चरण वावकायचेतोभिर्व्यापारः शुभकर्मसु ॥ ११८१॥ सूत्रार्थ - पदार्थरूप से आदि के तीन ( श्रद्धा-रुचि-प्रतीति ) ज्ञान रूप हैं क्योंकि ये ज्ञान की ही पर्यायें हैं। शुभ क्रियाओं में वचन-काय-मन के द्वारा व्यापार चरण है। __भावार्थ - सम्यग्दृष्टि का सहचर ज्ञान जो नौ पदार्थ की श्रद्धा रूप प्रवृत्त होता है उसे यहाँ सम्यक्व कहा है तथा व्यवहार धर्म के आचरण रूप जो शुभ विकल्प है जो चारित्रगुण की पुण्य तत्त्वरूप विभाव पर्याय है उस पर सम्यक्त्व का आरोप किया है। मन-वचन-काय की क्रियाओं पर नहीं। वे तो पुद्गल की स्वतन्त्र क्रियायें होती हैं । उनका ज्ञानी कि अज्ञानी कोई कर्ता नहीं है। शुभ विकल्प का निर्देश मन-वचन-काया की क्रियाओं द्वारा करने की आगम तथा लोक में रूढ़ि है।
व्यरताश्चैते समस्ता वा सदृष्टेलक्षणं न वा ।
सपक्षे वा विपक्षे वा सन्ति यदा न सन्ति वा ॥ ११८२।। सूत्रार्थ - ये चारों ( श्रद्धा, रुचि, प्रतीति-चरण) भिन्न-भिन्न अथवा सबके सब सम्यग्दर्शन के लक्षण हैं भी और नहीं भी हैं क्योंकि सपक्ष और विपक्ष में होते भी हैं अथवा नहीं भी होते हैं।
भावार्थ - सपक्ष का अर्थ सम्यग्दृष्टि है और विपक्ष का अर्थ मिथ्यादृष्टि है। सपक्ष में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं का अर्थ तो यह है कि ये विकल्पात्मक बातें चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान वालों में तो होती हैं किन्तु उनके ऊपर के ज्ञानियों में नहीं होती। इसलिये सब सम्यग्दृष्टियों में नहीं पाये जाने से अव्याप्ति दोष आने से सम्यक्त्व के त्रिकाली लक्षण नहीं हैं। विपक्ष में होते भी हैं और नहीं भी होने का अर्थ यह है कि किसी मिथ्यादृष्टि में नहीं होते किसी में होते भी हैं। अतः अतिव्याप्ति दोष आ जाने से भी सम्यक्त्व के लक्षण नहीं है। इन दोषों का परिहार यह है कि जहाँ इनको सम्यक्त्व का लक्षण कहा है वह तो चौथे, पाँचवें, छठे की अपेक्षा ही कहा है। अव्याप्ति दोष तो इस प्रकार दूर हो जाता है और मिथ्यादृष्टि में ये आभास रूप होते हैं। स्वात्मानुभूति उसकी परीक्षा है। यदि स्वात्मानुभूति सहित हैं तो श्रद्धा आदि सच्चे हैं क्योंकि अनुभवपूर्वक श्रद्धा है अन्यथा बह श्रद्धा बिना अनुभव गधे के सींगवत् है। इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष का परिहार है। स्वात्मानुभूति एक सम्यक्व का ऐसा लक्षण है जो चौथे से सिद्ध तक सभी दृष्टियों में ही पाया जाता है और किसी मिथ्यादृष्टि में कहीं भी नहीं पाया जाता है। अतः परीक्षा करने से वह ही सम्यक्त्व का ठीक लक्षण बैठता है पर है वह भी अनात्मभूत।