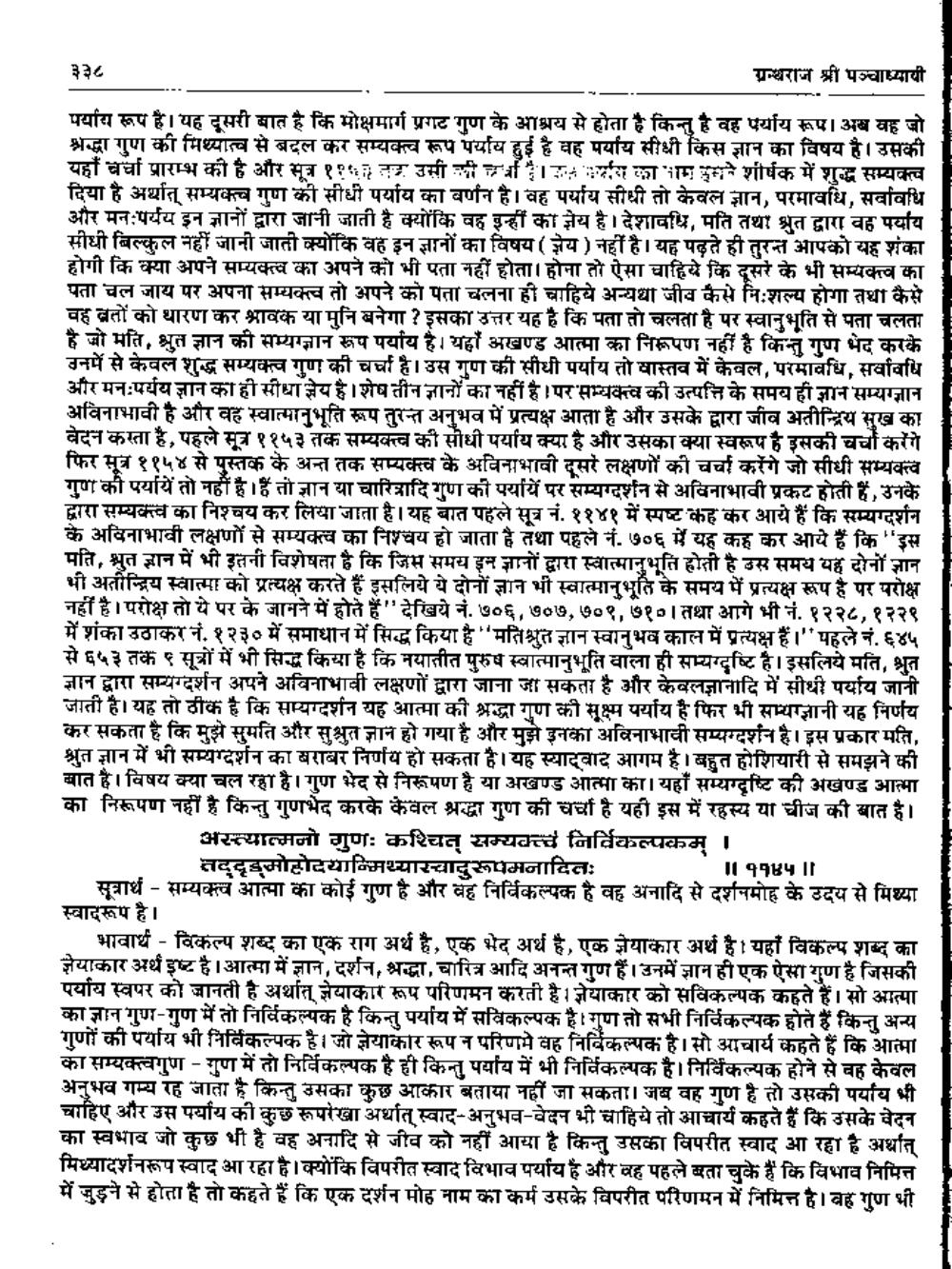________________
३३८
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
पर्याय रूप है। यह दूसरी बात है कि मोक्षमार्ग प्रगट गुण के आश्रय से होता है किन्तु है वह पर्याय रूप। अब वह जो श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व से बदल कर सम्यक्त्व रूप पर्याय हुई है वह पर्याय सीधी किस ज्ञान का विषय है। उसकी यहाँ चर्चा प्रारम्भ की है और सत्र १ तह उसी भी
नायकापाममने शीर्षक में शुद्ध सम्यक्त्व दिया है अर्थात् सम्यक्च गुण की सीधी पर्याय का वर्णन है। वह पर्याय सीधी तो केवल ज्ञान, परमावधि, सर्वावधि
और मन:पर्यय इन ज्ञानों द्वारा जानी जाती है क्योंकि वह इन्हीं का ज्ञेय है। देशावधि, मति तथा श्रुत द्वारा वह पर्याय सीधी बिल्कुल नहीं जानी जाती क्योंकि वह इन ज्ञानों का विषय (ज्ञेय) नहीं है। यह पढ़ते ही तुरन्त आपको यह शंका होगी कि क्या अपने सम्यक्त्व का अपने को भी पता नहीं होता। होना तो ऐसा चाहिये कि दूसरे के भी सम्यक्त्व का पता चल जाय पर अपना सम्यक्व तो अपने को पता चलना ही चाहिये अन्यथा जीव कैसे निःशल्य होगा तथा कैसे वह व्रतों को धारण कर श्रावक या मुनि बनेगा? इसका उत्तर यह है कि पता तो चलता है पर स्वानुभूति से पता चलता है जो मति, श्रुत ज्ञान की सम्यग्ज्ञान रूप पर्याय है। यहाँ अखण्ड आत्मा का निरूपण नहीं है किन्तु गुण भेद करके उनमें से केवल शुद्ध सम्यक्त्व गुण की चर्चा है। उस गुण की सीधी पर्याय तो वास्तव में केवल, परमावधि, सर्वावधि और मन:पर्यय ज्ञान काही सीधा ज्ञेय है। शेष तीन ज्ञानों का नहीं है। पर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान अविनाभावी है और वह स्वात्मानुभूति रूप तुरन्त अनुभव में प्रत्यक्ष आता है और उसके द्वारा जीव अतीन्द्रिय सुख का वेदन करता है, पहले सूत्र ११५३ तक सम्यक्त्व की सीधी पर्याय क्या है और उसका क्या स्वरूप है इसकी चर्चा करेंगे फिर सूत्र ११५४ से पुस्तक के अन्त तक सम्यक्त्व के अविनाभावी दूसरे लक्षणों की चर्चा करेंगे जो सीधी सम्यक्त्व गुण की पर्यायें तो नहीं है। हैं तो ज्ञान या चारित्रादि गुण की पर्यायें पर सम्यग्दर्शन से अविनाभावी प्रकट होती हैं, उनके द्वारा सम्यक्त्व का निश्चय कर लिया जाता है। यह बात पहले सूत्र नं. ११४१ में स्पष्ट कह कर आये हैं कि सम्यग्दर्शन के अविनाभावी लक्षणों से सम्यक्त्व का निश्चय हो जाता है तथा पहले नं.७०६ में यह कह कर आये हैं कि "इस मति, श्रुत ज्ञान में भी इतनी विशेषता है कि जिस समय इन ज्ञानों द्वारा स्वात्मानुभूति होती है उस समय यह दोनों ज्ञान भी अतीन्द्रिय स्वात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं इसलिये ये दोनों ज्ञान भी स्वात्मानुभूति के समय में प्रत्यक्ष रूप है पर परोक्ष नहीं है। परोक्ष तो ये पर के जानने में होते हैं"देखिये नं.७०६, ७०७,७०९,७१० । तथा आगे भी नं. १२२८,१२२९ में शंका उठाकर नं.१२३० में समाधान में सिद्ध किया है "मतिश्रुत ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष हैं।"पहले नं.६४५ से ६५३ तक ५ सूत्रों में भी सिद्ध किया है कि नयातीत पुरुष स्वात्मानुभूति वाला ही सभ्यग्दष्टि है। इसलिये मति, श्रुत ज्ञान द्वारा सम्यग्दर्शन अपने अविनाभावी लक्षणों द्वारा जाना जा सकता है और केवलज्ञानादि में सीधी पर्याय जानी जाती है। यह तो ठीक है कि सम्यग्दर्शन यह आत्मा की श्रद्धा गुण की सूक्ष्म पर्याय है फिर भी सम्यग्ज्ञानी यह निर्णय कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्रुत ज्ञान हो गया है और मुझे इनका अविनाभावी सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार मति, श्रुत ज्ञान में भी सम्यग्दर्शन का बराबर निर्णय हो सकता है। यह स्याद्वाद आगम है। बहुत होशियारी से समझने की बात है। विषय क्या चल रहा है। गुण भेद से निरूपण है या अखण्ड आत्मा का। यहाँ सम्यग्दृष्टि की अखण्ड आत्मा का निरूपण नहीं है किन्तु गुणभेद करके केवल श्रद्धा गुण की चर्चा है यही इस में रहस्य या चीज की बात है।
अस्त्यात्मनो गुणः कश्चित् सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम् । तददडमोहोदयान्मिथ्यारचादरूपमनादितः
॥ ११४५॥ सूत्रार्थ - सम्यक्त्व आत्मा का कोई गुण है और वह निर्विकल्पक है वह अनादि से दर्शनमोह के उदय से मिथ्या स्वादरूप है।
भावार्थ - विकल्प शब्द का एक राग अर्थ है, एक भेद अर्थ है, एक ज्ञेयाकार अर्थ है। यहाँ विकल्प शब्द का ज्ञेयाकार अर्थ इष्ट है।आत्मा में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि अनन्त गुण हैं। उनमें ज्ञानहीएक ऐसागुण है जिसकी पर्याय स्वपर को जानती है अर्थात् ज्ञेयाकार रूप परिणमन करती है। ज्ञेयाकार को सविकल्पक कहते हैं। सो आत्मा का ज्ञान गुण-गुण में तो निर्विकल्पक है किन्तु पर्याय में सविकल्पक है। गुण तो सभी निर्विकल्पक होते हैं किन्तु अन्य गुणों की पर्याय भी निर्विकल्पक है। जो ज्ञेयाकार रूपन परिणमे वह निर्विकल्पक है। सो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का सम्यक्त्वगुण - गुण में तो निर्विकल्पक है ही किन्तु पर्याय में भी निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक होने से वह केवल अनुभव गम्य रह जाता है किन्तु उसका कुछ आकार बताया नहीं जा सकता। जब वह गुण है तो उसकी पर्याय श्री चाहिए और उस पर्याय की कुछ रूपरेखा अर्थात् स्वाद-अनुभव-वेदन भी चाहिये तो आचार्य कहते हैं कि उसके वेदन का स्वभाव जो कुछ भी है वह अनादि से जीव को नहीं आया है किन्तु उसका विपरीत स्वाद आ रहा है अर्थात मिथ्यादर्शनरूप स्वाद आ रहा है। क्योंकि विपरीत स्वाद विभाव पर्याय है और वह पहले बता चके हैं कि विभाव निमित्त में जुड़ने से होता है तो कहते हैं कि एक दर्शन मोह नाम का कर्म उसके विपरीत परिणमन में निमित्त है। वह गुण भी