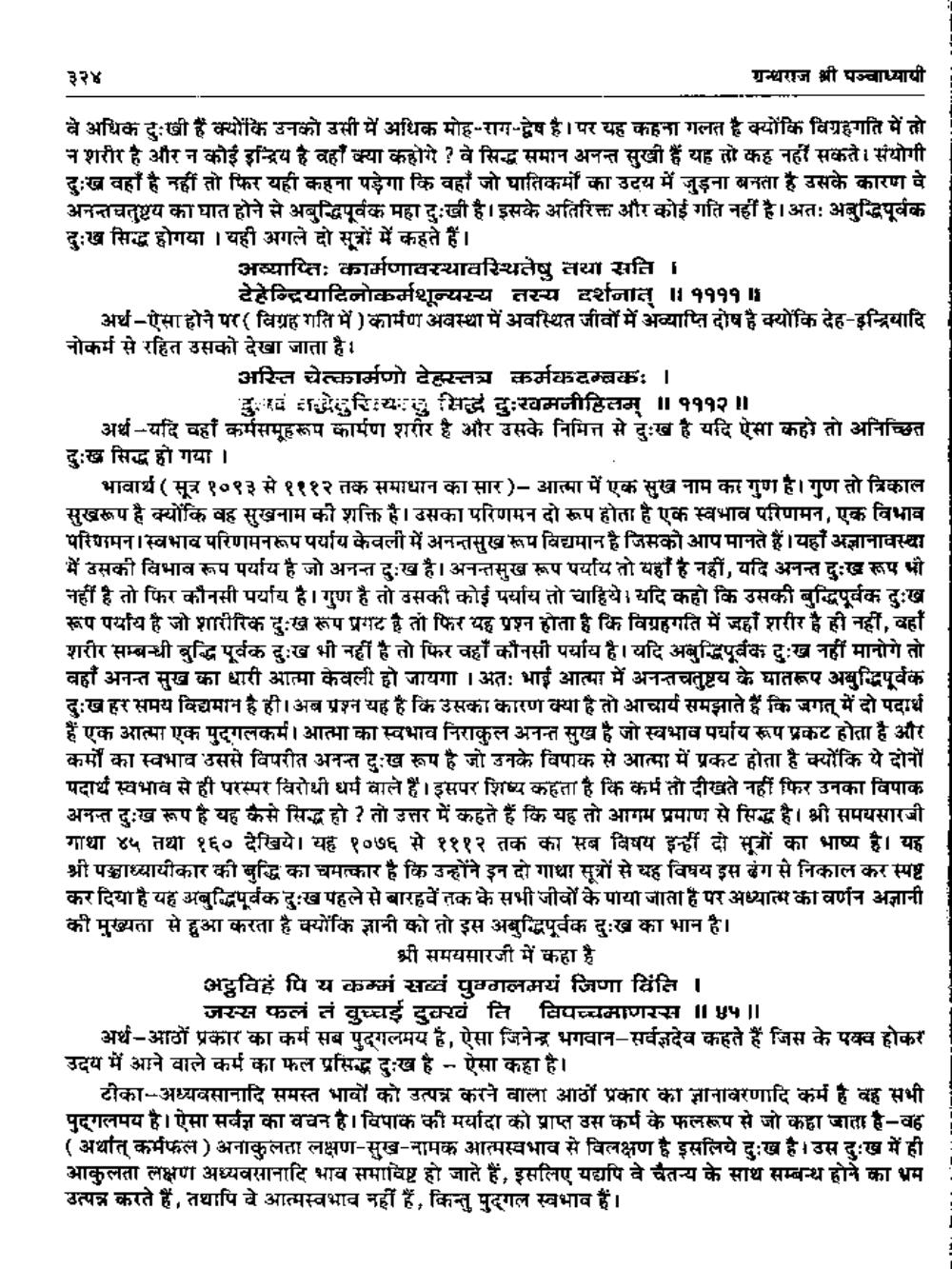________________
३२४
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
वे अधिक दुःखी हैं क्योंकि उनको उसी में अधिक मोह-राग-द्वेष है। पर यह कहना गलत है क्योंकि विग्रहगति में तो न शरीर है और न कोई इन्द्रिय है वहाँ क्या कहोगे ? वे सिद्ध समान अनन्त सुखी हैं यह तो कह नहीं सकते। संयोगी दुःख वहाँ है नहीं तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वहाँ जो घातिकर्मों का उदय में जुड़ना बनता है उसके कारण वे अनन्त चतुष्टय का घात होने से अबुद्धिपूर्वक महा दुःखी है। इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। अत: अबुद्धिपूर्वक दुःख सिद्ध होगया । यही अगले दो सूत्रों में कहते हैं।
अव्याप्तिः कार्मणावस्थावस्थितेषु तथा सति ।
टेहेन्द्रियाटिनोकर्मशून्यस्य तस्य दर्शनातु ।।११११॥ अर्थ-ऐसाहोने पर (विग्रह गति में कार्मण अवस्था में अवस्थित जीवों में अव्याप्ति दोष है क्योंकि देह-इन्द्रियादि नोकर्म से रहित उसको देखा जाता है।
अस्ति चेत्कार्मणो देहस्तत्र कर्मकटम्बकः ।
दु मेनुरिया:सुसिझे दुःरवमनीहितम् ॥ १११२ ॥ अर्थ-यदि वहाँ कर्मसमूहरूप कार्पण शरीर है और उसके निमित्त से दुःख है यदि ऐसा कहो तो अनिच्छित दुःख सिद्ध हो गया। ___ भावार्थ (सूत्र १०९३ से १११२ तक समाधान का सार)- आत्मा में एक सुख नाम कर गुण है। गुण तो त्रिकाल सुखरूप है क्योंकि वह सुखनाम की शक्ति है। उसका परिणमन दो रूप होता है एक स्वभाव परिणमन, एक विभाव परिचामनास्वभाव परिणमनरूपपर्याय केवली में अनन्तसुखरूप विद्यमान है जिसको आपमानते है।यहां अज्ञानावस्या में उसकी विभाव रूप पर्याय है जो अनन्त दुःख है। अनन्तसुख रूप पर्याय तो यहाँ है नहीं, यदि अनन्त दुःख रूप भी नहीं है तो फिर कौनसी पर्याय है। गुण है तो उसकी कोई पर्याय तो चाहिये। यदि कहो कि उसकी रूप पर्याय है जो शारीरिक दुःख रूप प्रगद है तो फिर यह प्रश्न होता है कि विग्रहगति में जहाँ शरीर है ही नहीं, वहाँ शरीर सम्बन्धी बुद्धि पूर्वक दुःख भी नहीं है तो फिर वहाँ कौनसी पर्याय है। यदि अबुद्धिपूर्वक दुःख नहीं मानोगे तो वहाँ अनन्त सुख का धारी आत्मा केवली हो जायगा । अतः भाई आत्मा में अनन्तचतुष्टय के यातरूप अबुद्धिपूर्वक दुःख हर समय विद्यमान है ही। अब प्रश्न यह है कि उसका कारण क्या है तो आचार्य समझाते हैं कि जगत् में दो पदार्थ हैं एक आत्मा एक पुद्गलकर्म। आत्मा का स्वभाव निराकुल अनन्त सुख है जो स्वभाव पर्याय रूप प्रकट होता है और कर्मों का स्वभाव उससे विपरीत अनन्त दुःख रूप है जो उनके विपाक से आत्मा में प्रकट होता है क्योंकि ये दोनों पदार्थ स्वभाव से ही परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं। इसपर शिष्य कहता है कि कर्म तो दीखते नहीं फिर उनका विपाक अनन्त दुःख रूप है यह कैसे सिद्ध हो ? तो उत्तर में कहते हैं कि यह तो आगम प्रमाण से सिद्ध है। श्री समयसारजी गाथा ४५ तथा १६० देखिये। यह १०७६ से १११२ तक का सब विषय इन्हीं दो सूत्रों का भाष्य है। यह श्री पश्चाध्यायीकार की बद्धि का चमत्कार है कि उन्होंने इन दो गाथा यह विषय इस ढंग से निकाल कर स्पष्ट कर दिया है यह अबुद्धिपूर्वक दुःख पहले से बारहवें तक के सभी जीवों के पाया जाता है पर अध्यात्म का वर्णन अज्ञानी की मुख्यता से हुआ करता है क्योंकि ज्ञानी को तो इस अबुद्धिपूर्वक दुःख का भान है।
श्री समयसारजी में कहा है अटुविहं पिय कम्मं सब्वं पुग्गलमयं जिणा विति ।
जस्स फलं तं वुच्चई दुक्रवं ति विपच्चमायरस ॥ ५५॥ अर्थ-आठों प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान-सर्वज्ञदेव कहते हैं जिस के पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुःख है - ऐसा कहा है।
टीका-अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुदगलमय है। ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फलरूप से जो कहा जाता है-वह ( अर्थात् कर्मफल)अनाकुलता लक्षण-सुख-नामक आत्मस्वभाव से विलक्षण है इसलिये दुःख है। उस दुःख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ सम्बन्ध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं. तथापि वे आत्मस्वभाव नहीं हैं, किन्तु पदगल स्वभाव हैं।