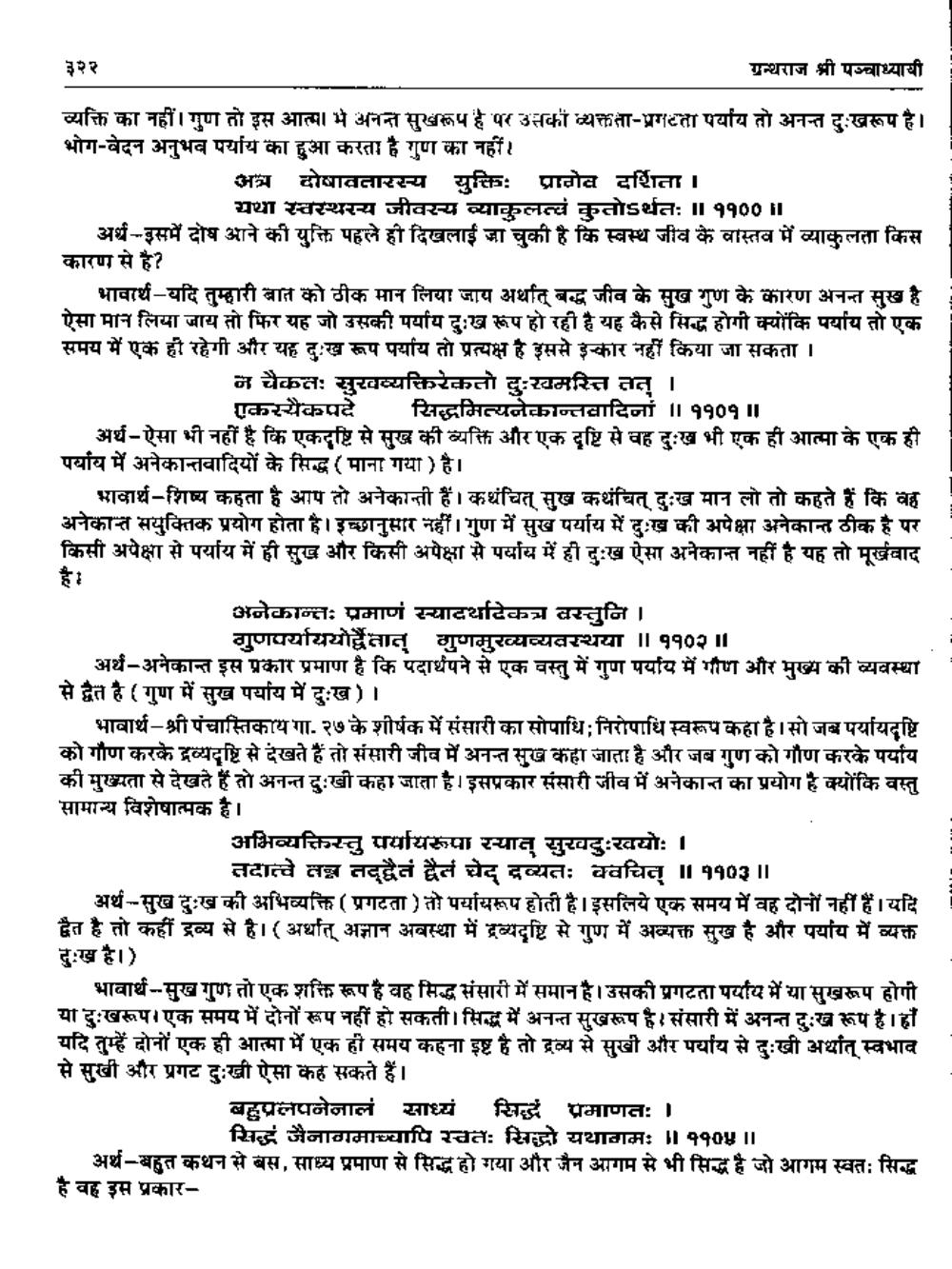________________
३२२
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
व्यक्ति का नहीं। गुण तो इस आत्मा में अनन्त सुखरूप है पर उसका व्यक्तता-प्रगटता पर्याय तो अनन्त दुःखरूप है। भोग-वेदन अनुभव पर्याय का हुआ करता है गुण का नहीं।
अत्र दोषावतारस्य युक्तिः प्रावोत दर्शिता ।
यथा स्वस्थरय जीवस्य व्याकुलत्वं कुतोऽर्थतः ॥ ११०० ।। अर्थ-इसमें दोष आने की युक्ति पहले ही दिखलाई जा चुकी है कि स्वस्थ जीव के वास्तव में व्याकुलता किस कारण से है?
भावार्थ-यदि तुम्हारी बात को ठीक मान लिया जाय अर्थात् बद्ध जीव के सुख गुण के कारण अनन्त सुख है ऐसा मान लिया जाय तो फिर यह जो उसकी पर्याय दुःख रूप हो रही है यह कैसे सिद्ध होगी क्योंकि पर्याय तो एक समय में एक ही रहेगी और यह दुःख रूप पर्याय तो प्रत्यक्ष है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ।
न चैकलः सुरवव्यक्तिरेकतो दुःखमस्ति तत् ।
एकस्यैकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवादिनां ॥ ११०१।। अर्थ-ऐसा भी नहीं है कि एकदृष्टि से सुख की व्यक्ति और एक दृष्टि से वह दुःख भी एक ही आत्मा के एक ही पर्याय में अनेकान्तवादियों के सिद्ध (माना गया ) है। ___ भावार्थ-शिष्य कहता है आप तो अनेकान्ती हैं। कथंचित् सुख कथंचित् दुःख मान लो तो कहते हैं कि वह
योग होता है। इच्छानुसार नहीं।गण में सख पर्याय में दःख की अपेक्षा अनेकान्त ठीक है पर किसी अपेक्षा से पर्याय में ही सुख और किसी अपेक्षा से पर्याय में ही दुःख ऐसा अनेकान्त नहीं है यह तो मूर्खवाद है।
अनेकान्तः प्रमाणं स्याटर्थादेकत्र वस्तुनि ।
गुणपर्याययोद्वैतात् गुणमुरव्यव्यवस्थया || ११०२ ॥ अर्थ-अनेकान्त इस प्रकार प्रमाण है कि पदार्थपने से एक वस्तु में गुण पर्याय में गौण और मुख्य की व्यवस्था से द्वैत है ( गुण में सुख पर्याय में दुःख )। ___ भावार्थ-श्री पंचास्तिकाय गा. २७ के शीर्षक में संसारी का सोपाधि; निरोपाधि स्वरूप कहा है।सो जब पर्यायदृष्टि को गौण करके द्रव्यदृष्टि से देखते हैं तो संसारी जीव में अनन्त सुख कहा जाता है और जब गुणको गौण करके पर्याय की मुख्यता से देखते हैं तो अनन्त दुःखी कहा जाता है। इसप्रकार संसारी जीव में अनेकान्त का प्रयोग है क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है।
अभिव्यक्तिस्तु पर्यायरूपा स्यात् सुरवदुःखयोः ।
तदात्वे तन तद्वैतं द्वैतं चेद् द्रव्यतः क्वचित् ॥ ११०३ ।। अर्थ-सुख दुःख की अभिव्यक्ति ( प्रगटता) तो पर्यायरूप होती है। इसलिये एक समय में वह दोनों नहीं हैं। यदि द्वैत है तो कहीं द्रव्य से है। ( अर्थात् अज्ञान अवस्था में द्रव्यदृष्टि से गुण में अव्यक्त सुख है और पर्याय में व्यक्त दुःख है।)
भावार्थ-सुख गुण तो एक शक्ति रूप है वह सिद्ध संसारी में समान है। उसकी प्रगटता पर्याय में या सुखरूप होगी या दुःखरूप। एक समय में दोनों रूप नहीं हो सकती। सिद्ध में अनन्त सुखरूप है। संसारी में अनन्त दुःख रूप है। हाँ यदि तुम्हें दोनों एक ही आत्मा में एक ही समय कहना इष्ट है तो द्रव्य से सुखी और पर्याय से दुःखी अर्थात् स्वभाव से सुखी और प्रगट दुःखी ऐसा कह सकते हैं।
बहुप्रलपनेजालं साध्यं सिद्धं प्रमाणतः ।
सिद्धं जैनागमाच्यापि स्वत: सिद्धो यथागमः ॥११०४ ॥ अर्थ-बहुत कथन से बस, साध्य प्रमाण से सिद्ध हो गया और जैन आगम से भी सिद्ध है जो आगम स्वतः सिद्ध है वह इस प्रकार