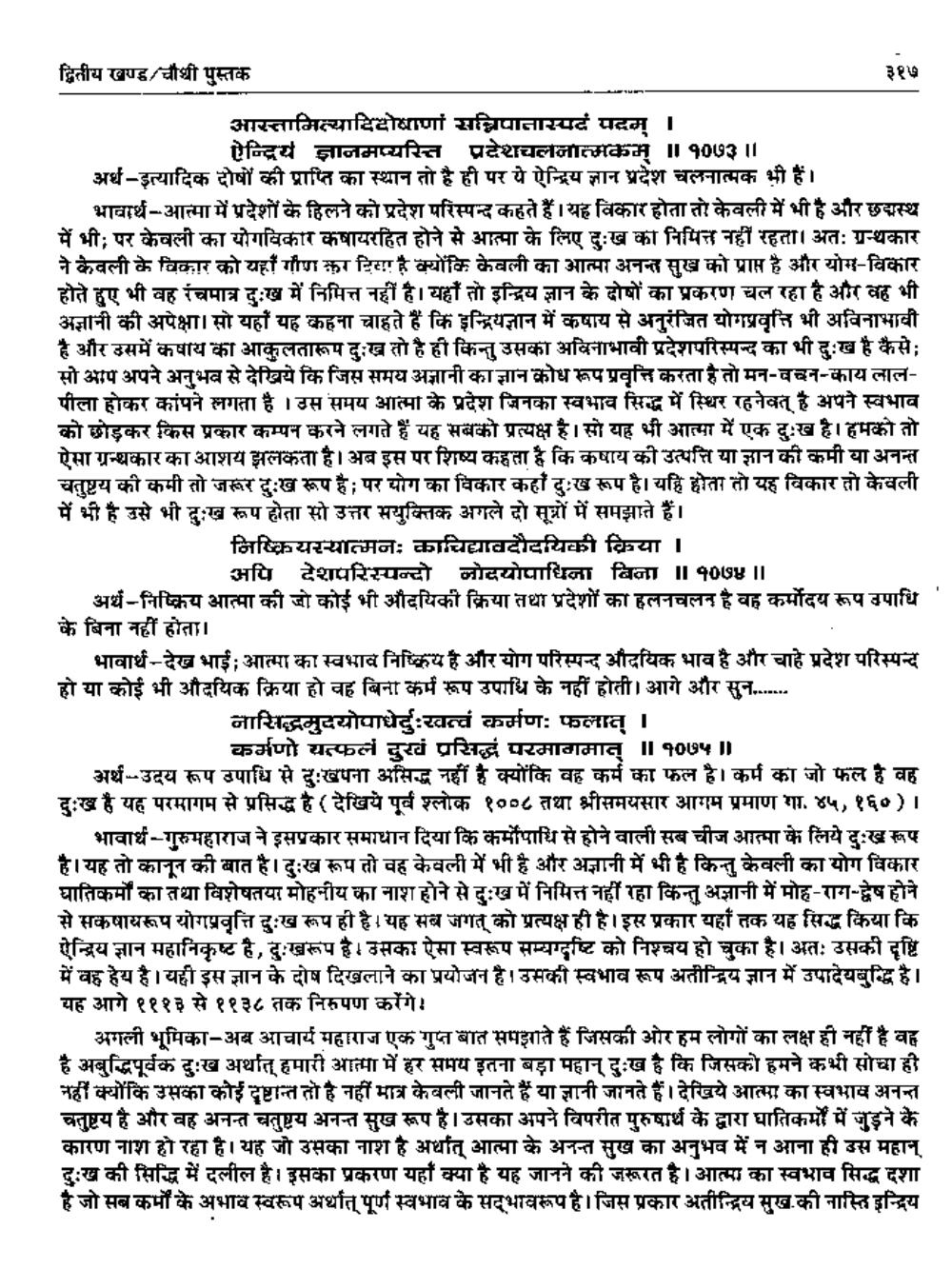________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
आस्तामित्यादिदोधाणां सन्निपातास्पदं पदम् ।
ऐन्द्रियं ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम् ॥ १०७३ ।। अर्थ-इत्यादिक दोषों की प्राप्ति का स्थान तो है ही पर ये ऐन्द्रिय ज्ञान प्रदेश चलनात्मक भी हैं।
भावार्थ-आत्मा में प्रदेशों के हिलने को प्रदेश परिस्पन्द कहते हैं। यह विकार होता तो केवली में भी है और छयस्थ में भी; पर केवली का योगविकार कषायरहित होने से आत्मा के लिए दुःख का निमित्त नहीं रहता। अतः ग्रन्थकार ने केवली के विकार को यहाँ गौण कर दिया है क्योंकि केवली का आत्मा अनन्त सख को प्राप्त है और योग-विकार होते हुए भी वह रंचमात्र दुःख में निमित्त नहीं है। यहाँ तो इन्द्रिय ज्ञान के दोषों का प्रकरण चल रहा है और वह भी अज्ञानी की अपेक्षा। सो यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इन्द्रियज्ञान में कषाय से अनुरंजित योगप्रवृत्ति भी अविनाभावी है और उसमें कषाय का आकुलतारूप दुःख तो है ही किन्तु उसका अविनाभावी प्रदेशपरिस्पन्द का भी दुःख है कैसे; सो आप अपने अनुभव से देखिये कि जिस समय अज्ञानीकाज्ञान क्रोध रूप प्रवृत्ति करता है तो मन-वचन-काय लाल
। लगता है । उस समय आत्मा के प्रदेश जिनका स्वभाव सिद्ध में स्थिर रहनेवत् है अपने स्वभाव को छोड़कर किस प्रकार कम्पन करने लगते हैं यह सबको प्रत्यक्ष है। सो यह भी आत्मा में एक दःख है। हमको तो ऐसा ग्रन्थकार का आशय झलकता है। अब इस पर शिष्य कहता है कि कषाय की उत्पत्ति या ज्ञान की कमी या अनन्त चतुष्टय की कमी तो जरूर दःख रूप है। पर योग का विकार कहाँ दःख रूप है। यहि होता तो यह विकार तो केवली में भी है उसे भी दुःख रूप होता सो उत्तर सयुक्तिक अगले दो सूत्रों में समझाते हैं।
निष्क्रियरयात्मनः काचिद्यावदौदयिकी क्रिया ।
अपि देशपरिस्पन्दो नोदयोपाधिना बिना ॥ १०७४ ॥ अर्थ-निष्क्रिय आत्मा की जो कोई भी औदयिकी क्रिया तथा प्रदेशों का हलनचलन है वह कर्मोदय रूप उपाधि ' के बिना नहीं होता।
भावार्थ-देख भाई; आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है और योग परिस्पन्द औदयिक भाव है और चाहे प्रदेश परिस्पन्द हो या कोई भी औदयिक क्रिया हो वह बिना कर्म रूप उपाधि के नहीं होती। आगे और सुन......
नासिद्भमुदयोपाधे?:रवत्वं कर्मण: फलात् ।
कर्मणो यत्फलं दुरवं प्रसिद्ध परमागमात् ॥ १०७५ ॥ अर्थ-उदय रूप उपाधि से दुःखपना असिद्ध नहीं है क्योंकि वह कर्म का फल है। कर्म का जो फल है वह दुःख है यह परमागम से प्रसिद्ध है ( देखिये पूर्व श्लोक १००८ तथा श्रीसमयसार आगम प्रमाण गा. ४५, १६०)।
भावार्थ-गुरुमहाराज ने इसप्रकार समाधान दिया कि कर्मोपाधि से होने वाली सब चीज आत्मा के लिये दुःख रूप है। यह तो कानून की बात है। दुःख रूप तो वह केवली में भी है और अज्ञानी में भी है किन्तु केवली का योग विकार घातिकर्मों का तथा विशेषतया मोहनीय का नाश होने से दुःख में निमित्त नहीं रहा किन्तु अज्ञानी में मोह-राग-द्वेष होने से सकषायरूप योगप्रवृत्ति दुःख रूप ही है। यह सब जगत् को प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध किया कि ऐन्द्रिय ज्ञान महानिकृष्ट है, दुःखरूप है। उसका ऐसा स्वरूप सम्यग्दष्टि को निश्चय हो चुका है। अतः उसकी दृष्टि में वह हेय है। यही इस ज्ञान के दोष दिखलाने का प्रयोजन है। उसकी स्वभाव रूप अतीन्द्रिय ज्ञान में उपादेयबुद्धि है। यह आगे १११३ से १९३८ तक निरूपण करेंगे।
अगली भूमिका-अब आचार्य महाराज एक गुप्त बात समझाते हैं जिसकी ओर हम लोगों का लक्ष ही नहीं है वह है अबुद्धिपूर्वक दुःख अर्थात् हमारी आत्मा में हर समय इतना बड़ा महान् दुःख है कि जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि उसका कोई दृष्टान्त तो है नहीं मात्र केवली जानते हैं या ज्ञानी जानते हैं। देखिये आत्मा का स्वभाव अनन्त चतुष्टय है और वह अनन्त चतुष्टय अनन्त सुख रूप है। उसका अपने विपरीत पुरुषार्थ के द्वारा घातिकर्मों में जुड़ने के कारण नाश हो रहा है। यह जो उसका नाश है अर्थात् आत्मा के अनन्त सुख का अनुभव में न आना ही उस महान् दुःख की सिद्धि में दलील है। इसका प्रकरण यहाँ क्या है यह जानने की जरूरत है। आत्मा का स्वभाव सिद्ध दशा है जो सब कर्मों के अभाव स्वरूप अर्थात् पूर्ण स्वभाव के सद्भावरूप है। जिस प्रकार अतीन्द्रिय सुख की नास्ति इन्द्रिय