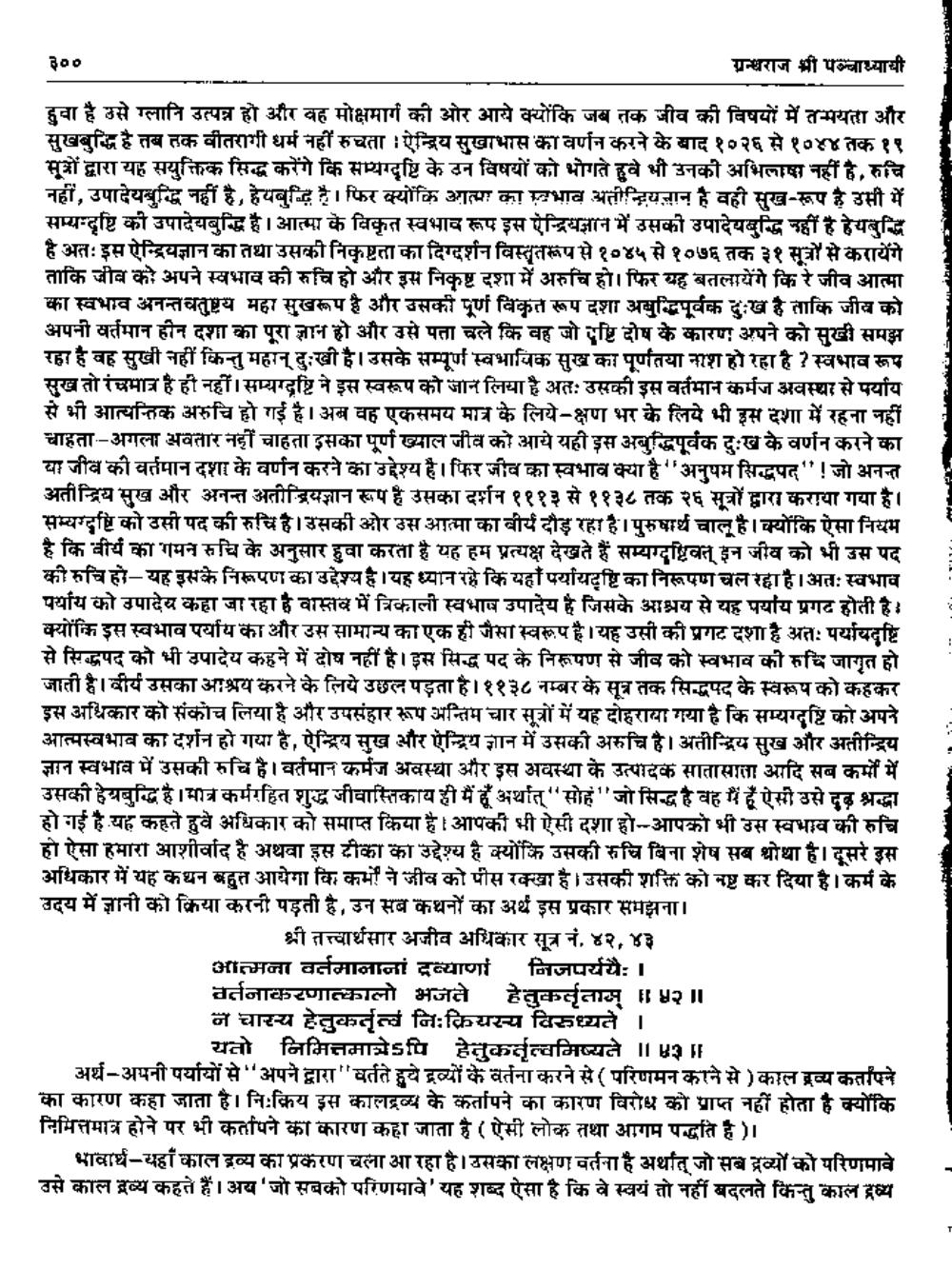________________
३००
ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी
हुवा है उसे ग्लानि उत्पन्न हो और वह मोक्षमार्ग की ओर आये क्योंकि जब तक जीव की विषयों में तन्मयता और सुखबुद्धि है तब तक वीतरागी धर्म नहीं रुचता । ऐन्द्रिय सुखाभास का वर्णन करने के बाद १०२६ से १०४४ तक १९ सूत्रों द्वारा यह सयुक्तिक सिद्ध करेंगे कि सम्यग्दृष्टि के उन विषयों को भोगते हुवे भी उनकी अभिलाषा नहीं है,रुचि नहीं, उपादेयबुद्धि नहीं है, हेयबुद्धि है। फिर क्योंकि आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रियजान है वही सुख-रूप है उसी में सम्यग्दृष्टि की उपादेयबुद्धि है। आत्मा के विकृत स्वभाव रूप इस ऐन्द्रियज्ञान में उसकी उपादेयबुद्धि नहीं है हेयबुद्धि है अतः इस ऐन्द्रियज्ञान का तथा उसकी निकृष्टता का दिग्दर्शन विस्तृतरूप से १०४५ से १०७६ तक ३१ सूत्रों से करायेंगे ताकि जीव को अपने स्वभाव की रुचि हो और इस निकष्ट दशा में अरुचि हो। फिर यह बतलायेंगे कि रे जीव आत्मा का स्वभाव अनन्तवतुष्टय महा सुखरूप है और उसकी पूर्ण विकृत रूप दशा अबुद्धिपूर्वक दुःख है ताकि जीव को अपनी वर्तमान हीन दशा का पूरा ज्ञान हो और उसे पता चले कि वह जो दृष्टि दोष के कारण अपने को सुखी समझ रहा है वह सुखी नहीं किन्तु महान् दुःखी है। उसके सम्पूर्ण स्वभाविक सुख का पूर्णतया नाश हो रहा है? स्वभाव रूप सुख तोरंचमात्र है ही नहीं।सम्यग्दृष्टि ने इस स्वरूप को जान लिया है अतः उसकी इस वर्तमान कर्मज अवस्था से पर्याय से भी आत्यन्तिक अरुचि हो गई है। अब वह एकसमय मात्र के लिये-क्षण भर के लिये भी इस दशा में रहना नहीं चाहता-अगला अवतार नहीं चाहता इसका पूर्ण ख्याल जीव को आये यही इस अबुद्धिपूर्वक दुःख के वर्णन करने का या जीव की वर्तमान दशा के वर्णन करने का उद्देश्य है। फिर जीव का स्वभाव क्या है "अनुपम सिद्धपद" ! जो अनन्त अतीन्द्रिय सुख और अनन्त अतीन्द्रियज्ञान रूप है उसका दर्शन १९१३ से ११३८ तक २६ सूत्रों द्वारा कराया गया है। सम्यग्दष्टि को उसी पद की रुचि है। उसकी ओर उस आत्मा का वीर्य दौड़ रहा है। पुरुषार्थ चालू है। क्योंकि ऐसा नियम है कि वीर्य का गमन रुचि के अनुसार हवा करता है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं सम्यग्दृष्टिवत् इन जीव को भी उस पद कीरुचि हो-यह नुसके निरूपणकाउद्देश्य है। यह ध्यान रहे कियहाँपर्यायष्टि का निरूपण पर्याय को उपादेय कहा जा रहा है वास्तव में त्रिकाली स्वभाष उपादेय है जिसके आश्रय से यह पर्याय प्रगट होती है। क्योंकि इस स्वभाव पर्याय का और उस सामान्य का एक ही जैसा स्वरूप है। यह उसी की प्रगट दशा है अतः पर्यायदृष्टि से सिद्धपद को भी उपादेय कहने में दोष नहीं है। इस सिद्ध पद के निरूपण से जीव को स्वभाव की रुचि जागत हो जाती है। वीर्य उसका आश्रय करने के लिये उछल पड़ता है।११३८ नम्बर के सूत्र तक सिद्धपद के स्वरूप को कहकर इस अधिकार को संकोच लिया है और उपसंहार रूप अन्तिम चार सूत्रों में यह दोहराया गया है कि सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मस्वभाव का दर्शन हो गया है,ऐन्ट्रिय सुख और ऐन्द्रिय ज्ञान में उसकी अरुचि है। अतीन्द्रिय सख और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में उसकी रुचि है। वर्तमान कर्मज अवस्था और इस अवस्था के उत्पादक सातासाता आदि सब कर्मों में उसकी हेयबुद्धि है। मात्र कर्मरहित शुद्ध जीवास्तिकाय ही मैं हूँ अर्थात् "सोहं"जो सिद्ध है वह मैं हूँ ऐसी उसे दुङ श्रद्धा हो गई है यह कहते हुवे अधिकार को समाप्त किया है। आपकी भी ऐसी दशा हो-आपको भी उस स्वभाव की रुचि हो ऐसा हमारा आशीर्वाद है अथवा इस टीका का उद्देश्य है क्योंकि उसकी रुचि बिना शेष सब थोथा है। दूसरे इस अधिकार में यह कथन बहुत आयेगा कि कर्मों ने जीव को पीस रक्खा है। उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। कर्म के उदय में ज्ञानी की क्रिया करनी पड़ती है, उन सब कथनों का अर्थ इस प्रकार समझना।
श्री तत्त्वार्थसार अजीव अधिकार सूत्र नं. ४२, ४३ आत्मना वर्तमानानां द्रव्याणां निजपर्ययैः । वर्तनाकरणात्कालो भजते हेतुकर्तृताम् ॥ ४२ ॥ न चारय हेतुकर्तृत्व नि:क्रियस्य विरुध्यते ।
यतो निमित्तमानेऽपि हेतुकर्तृत्वमिष्यते ॥ ३॥ अर्थ-अपनी पर्यायों से अपने द्वारा "वर्तते हुये द्रव्यों के वर्तना करने से (परिणमनकाने से)काल द्रव्य काफ्ने का कारण कहा जाता है। नि:क्रिय इस कालद्रव्य के कर्तापने का कारण विरोध को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि निमित्तमात्र होने पर भी कांपने का कारण कहा जाता है । ऐसी लोक तथा आगम पद्धति है)।
भावार्थ-यहाँकाल द्रव्य का प्रकरण चला आ रहा है। उसका लक्षण वर्तना है अर्थात् जो सब द्रव्यों को परिणमावे उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब 'जो सबको परिणमावे' यह शब्द ऐसा है कि वे स्वयं तो नहीं बदलते किन्तु काल ध्य