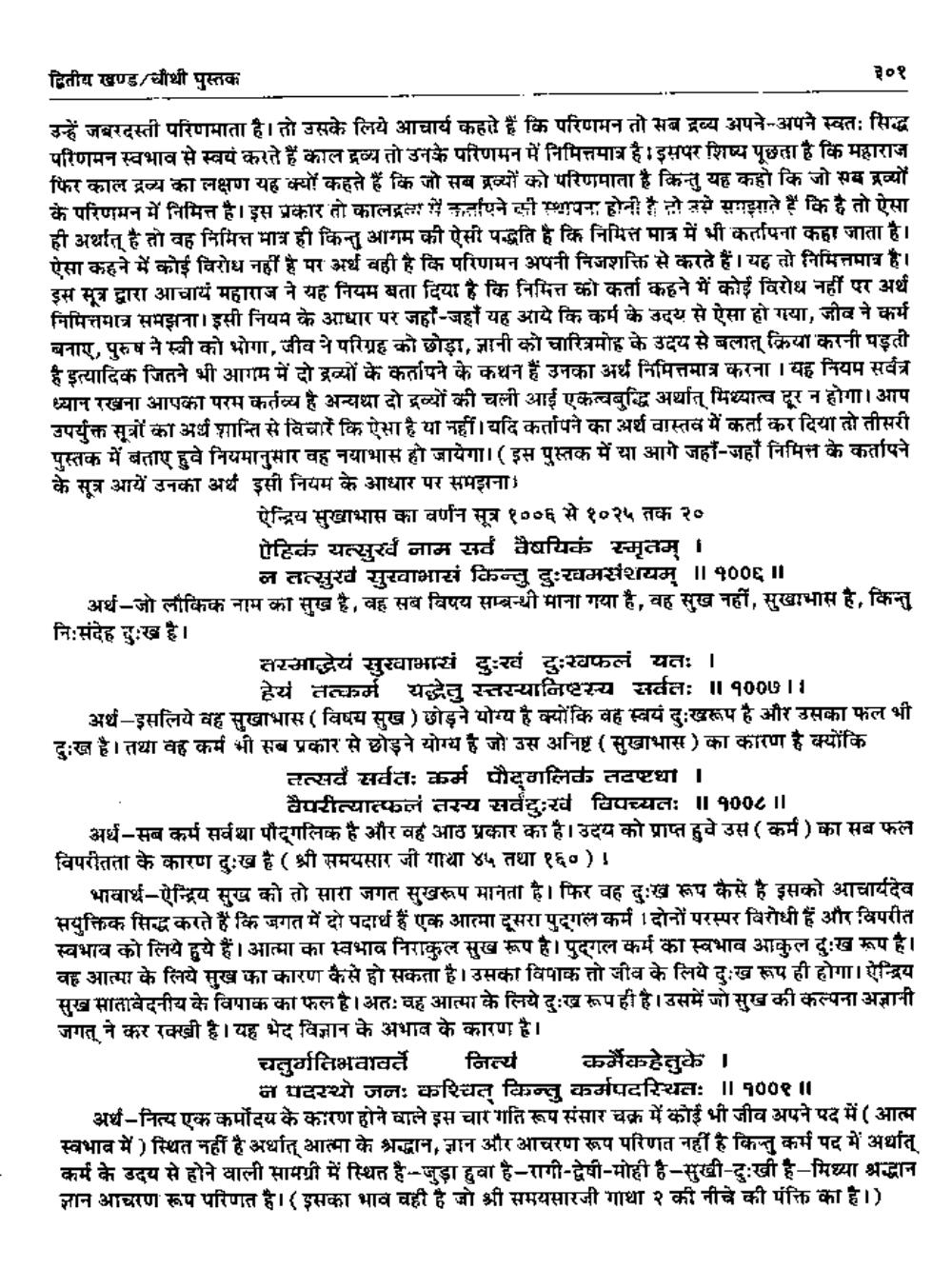________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
३०१
उन्हें जबरदस्ती परिणमाता है। तो उसके लिये आचार्य कहते हैं कि परिणमन तो सब द्रव्य अपने-अपने स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव से स्वयं करते हैं काल द्रव्य तो उनके परिणमन में निमित्तमात्र है। इसपर शिष्य पूछता है कि महाराज फिर काल द्रव्य का लक्षण यह क्यों कहते हैं कि जो सब द्रव्यों को परिणमाता है किन्तु यह कहो कि जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। इस प्रकार तो कालगता में कांपने सीमापना होनी है तो उसे साझाते हैं कि है तो ऐसा ही अर्थात है तो वह निमित्त मात्र ही किन्त आगम की ऐसी पद्धति है कि निमित्त मात्र में भी काफ्ना कहा जाता है। ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है पर अर्थ वही है कि परिणमन अपनी निजशक्ति से करते हैं। यह तो निमित्तमात्र है। इस सूत्र द्वारा आचार्य महाराज ने यह नियम बता दिया है कि निमित्त को कर्ता कहने में कोई विरोध नहीं पर अर्थ निमित्तमात्र समझना। इसी नियम के आधार पर जहाँ-जहाँ यह आये कि कर्म के उदय से ऐसा हो गया, जीव ने कर्म बनाए, पुरुष ने स्त्री को भोगा, जीव ने परिग्रह को छोड़ा, ज्ञानी को चारित्रमोह के उदय से बलात् क्रिया करनी पड़ती है इत्यादिक जितने भी आगम में दो द्रव्यों के कांपने के कथन हैं उनका अर्थ निमित्तमात्र करना । यह नियम सर्वत्र ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है अन्यथा दो द्रव्यों की चली आई एकत्वबुद्धि अर्थात् मिथ्यात्व दूर न होगा। आप उपर्युक्त सूत्रों का अर्थ शान्ति से विचारें कि ऐसा है या नहीं। यदि कर्तापने का अर्थ वास्तव में कर्ता कर दिया तो तीसरी पुस्तक में बताए हुवे नियमानुसार वह नयाभास हो जायेगा। (इस पुस्तक में या आगे जहाँ-जहाँ निमित्त के कर्तापने के सूत्र आयें उनका अर्थ इसी नियम के आधार पर समझना)
ऐन्द्रिय सुखाभास का वर्णन सूत्र १००६ से १०२५ तक २० ऐहिक यत्सुखं नाम सर्व वैषयिकं स्मृतम् ।
ल तत्सुरव सुरवाभासं किन्तु दुःरबमसंशयम् ॥ १००६ ॥ अर्थ-जो लौकिक नाम का सुख है, वह सब विषय सम्बन्धी माना गया है, वह सुख नहीं, सुखाभास है, किन्तु नि:संदेह दुःख है।
तरमादेयं सस्वाभासं दुःखं दाखफलं यतः ।
हेयं तत्कर्म यद्धेतु स्तरन्यानिष्टस्य सर्वतः ।। १००७ ।। अर्थ-इसलिये वह सुखाभास ( विषय सुख ) छोड़ने योग्य है क्योंकि वह स्वयं दुःखरूप है और उसका फल भी दुःख है। तथा वह कर्म भी सब प्रकार से छोड़ने योग्य है जो उस अनिष्ट (सुखाभास)का कारण है क्योंकि
तत्सर्वं सर्वतः कर्म पौगलिक तटष्टथा ।
वैपरीत्यात्फलं तस्य सर्वदुःख विपच्यतः ।। १००८ ॥ अर्थ-सब कर्म सर्वथा पौदगलिक है और वह आठ प्रकार का है। उदय को प्राप्त हवे उस (कर्म) का सब फल विपरीतता के कारण दःख है (श्री समयसार जी गाथा ४५ तथा १६०)!
भावार्थ-ऐन्द्रिय सुख को तो सारा जगत सुखरूप मानता है। फिर वह दुःख रूप कैसे है इसको आचार्यदेव सयुक्तिक सिद्ध करते हैं कि जगत में दो पदार्थ हैं एक आत्मा दूसरा पुद्गल कर्म दोनों परस्पर विरोधी हैं और विपरीत स्वभाव को लिये हुये हैं। आत्मा का स्वभाव निराकुल सुख रूप है। पुद्गल कर्म का स्वभाव आकुल दुःख रूप है। वह आत्मा के लिये सुख का कारण कैसे हो सकता है। उसका विपाक तो जीव के लिये दुःख रूप ही होगा। ऐन्द्रिय सुख सातावेदनीय के विपाक का फल है। अतः वह आत्मा के लिये दःखरूपही है। उसमें जो सुख की कल्पना अज्ञानी जगत् ने कर रक्खी है। यह भेद विज्ञान के अभाव के कारण है।
चतुर्गतिभवावर्ते नित्य कर्मैकहेतुके ।
न पदस्थो जनः कश्चित किन्तु कर्मपदस्थितः || 100९ ।। अर्थ-नित्य एक कर्मोदय के कारण होने वाले इस चार गति रूप संसार चक्र में कोई भी जीव अपने पद में (आत्म स्वभाव में ) स्थित नहीं है अर्थात् आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप परिणत नहीं है किन्तु कर्म पद में अर्थात् कर्म के उदय से होने वाली सामग्री में स्थित है-जुड़ा हुवा है-रागी-द्वेषी-मोही है-सुखी-दुःखी है-मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप परिणत है। (इसका भाव वही है जो श्री समयसारजी गाथा २ की नीचे की पंक्ति का है।)