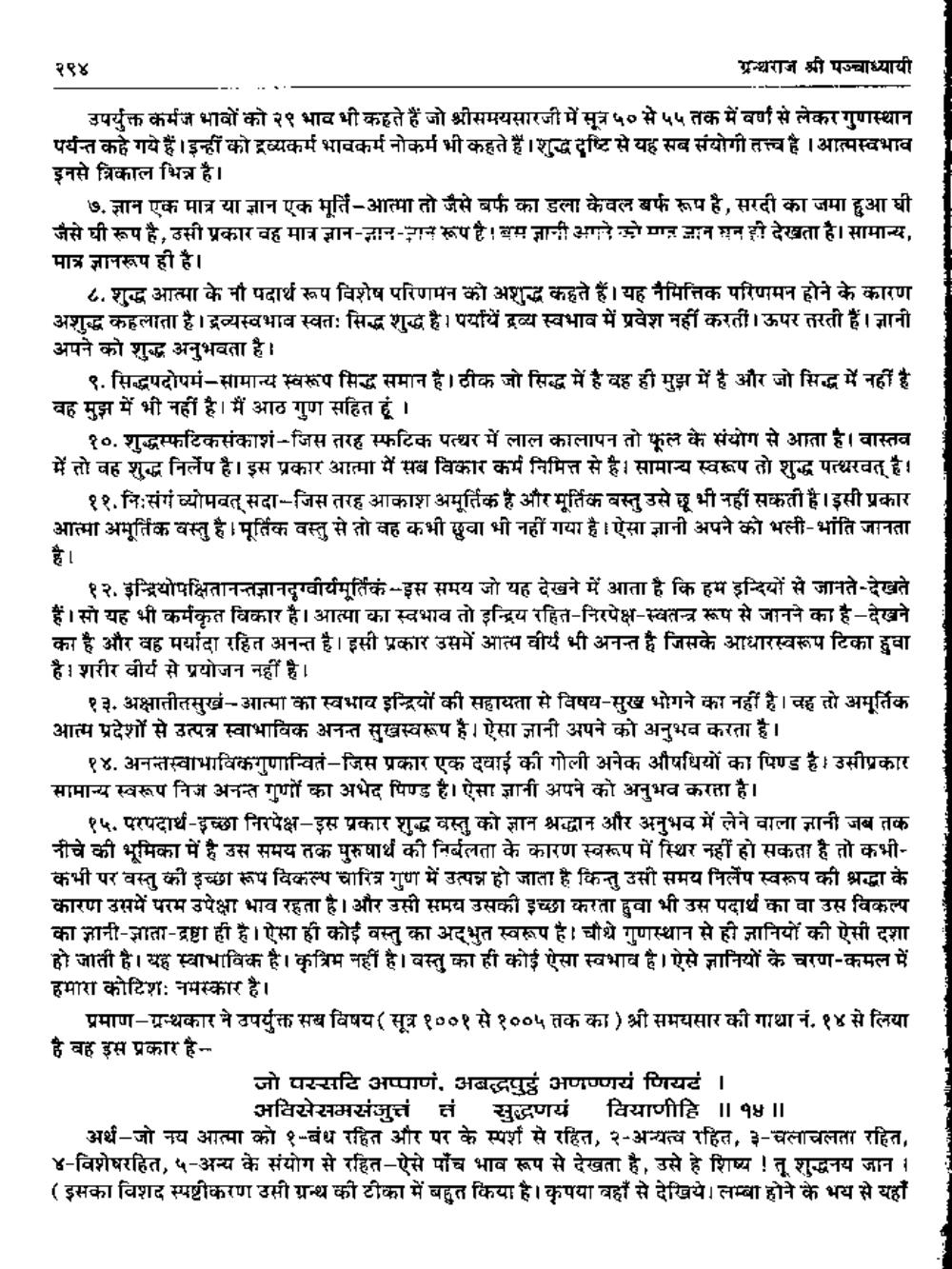________________
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
उपर्युक्त कर्मज भावों को २९ भाव भी कहते हैं जो श्रीसमयसारजी में सूत्र ५० से ५५ तक में वर्षों से लेकर गुणस्थान पर्यन्त कहे गये हैं। इन्हीं को द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म भी कहते हैं। शुद्ध दृष्टि से यह सब संयोगी तत्त्व है । आत्मस्वभाव इनसे त्रिकाल भिन्न हैं ।
२९४
७. ज्ञान एक मात्र या ज्ञान एक मूर्ति-आत्मा तो जैसे बर्फ का डला केवल बर्फ रूप है, सरदी का जमा हुआ घी जैसे घी रूप है, उसी प्रकार वह मात्र ज्ञान-ज्ञान-ज्ञान रूप है। बस ज्ञानी अपने को मार ज्ञान न हो देखता है। सामान्य, मात्र ज्ञानरूप ही हैं।
८. शुद्ध आत्मा के नौ पदार्थ रूप विशेष परिणमन को अशुद्ध कहते हैं। यह नैमित्तिक परिणमन होने के कारण अशुद्ध कहलाता है। द्रव्यस्वभाव स्वतः सिद्ध शुद्ध है। पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करतीं। ऊपर तरती हैं। ज्ञानी अपने को शुद्ध अनुभवता है।
९. सिद्धपदोपमं - सामान्य स्वरूप सिद्ध समान है। ठीक जो सिद्ध में है वह ही मुझ में है और जो सिद्ध में नहीं है वह मुझ में भी नहीं है। मैं आठ गुण सहित हूं ।
१०. शुद्धस्फटिकसंकाशं जिस तरह स्फटिक पत्थर में लाल कालापन तो फूल के संयोग से आता है। वास्तव में तो वह शुद्ध निर्लेप है । इस प्रकार आत्मा में सब विकार कर्म निमित्त से है। सामान्य स्वरूप तो शुद्ध पत्थरवत् है ।
११. निःसंगं व्योमवत् सदा-जिस तरह आकाश अमूर्तिक है और मूर्तिक वस्तु उसे छू भी नहीं सकती है। इसी प्रकार आत्मा अमूर्तिक वस्तु है। मूर्तिक वस्तु से तो वह कभी छुवा भी नहीं गया है। ऐसा ज्ञानी अपने को भली-भांति जानता है
१२. इन्द्रियोपक्षितानन्तज्ञानदृग्वीर्यमूर्तिकं - इस समय जो यह देखने में आता है कि हम इन्दियों से जानते-देखते हैं । सो यह भी कर्मकृत विकार है। आत्मा का स्वभाव तो इन्द्रिय रहित-निरपेक्ष - स्वतन्त्र रूप से जानने का है - देखने का है और वह मर्यादा रहित अनन्त है। इसी प्रकार उसमें आत्म वीर्य भी अनन्त है जिसके आधारस्वरूप टिका हुवा है । शरीर वीर्य से प्रयोजन नहीं है।
१३. अक्षातीतसुखं- आत्मा का स्वभाव इन्द्रियों की सहायता से विषय सुख भोगने का नहीं है। वह तो अमूर्तिक आत्म प्रदेशों से उत्पन्न स्वाभाविक अनन्त सुखस्वरूप है। ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता है ।
१४. अनन्तस्वाभाविकगुणान्वितं जिस प्रकार एक दवाई की गोली अनेक औषधियों का पिण्ड है। उसीप्रकार सामान्य स्वरूप निज अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड है। ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता है।
१५. परपदार्थ - इच्छा निरपेक्ष- इस प्रकार शुद्ध वस्तु को ज्ञान श्रद्धान और अनुभव में लेने वाला ज्ञानी जब तक नीचे की भूमिका में है उस समय तक पुरुषार्थं की निर्बलता के कारण स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है तो कभीकभी पर वस्तु की इच्छा रूप विकल्प चारित्र गुधा में उत्पन्न हो जाता है किन्तु उसी समय निर्लेप स्वरूप की श्रद्धा के कारण उसमें परम उपेक्षा भाव रहता है। और उसी समय उसकी इच्छा करता हुवा भी उस पदार्थ का वा उस विकल्प का ज्ञानी ज्ञाता द्रष्टा ही है। ऐसा ही कोई वस्तु का अद्भुत स्वरूप है। चौथे गुणस्थान से ही ज्ञानियों की ऐसी दशा हो जाती है। यह स्वाभाविक है। कृत्रिम नहीं है। वस्तु का ही कोई ऐसा स्वभाव है। ऐसे ज्ञानियों के चरण कमल में हमारा कोटिशः नमस्कार है।
प्रमाण-ग्रन्थकार ने उपर्युक्त सब विषय (सूत्र १००१ से १००५ तक का ) श्री समयसार की गाथा नं. १४ से लिया है वह इस प्रकार है
जो परसटि अप्पाणं. अबद्धटुं अणण्णयं जियटं । अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १४ ॥
अर्थ- जो नय आत्मा को १-बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, २- अन्यत्व रहित, ३-चलाचलता रहित, ४ - विशेषरहित, ५- अन्य के संयोग से रहित ऐसे पाँच भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य ! तू शुद्धनय जान । (इसका विशद स्पष्टीकरण उसी ग्रन्थ की टीका में बहुत किया है। कृपया वहाँ से देखिये। लम्बा होने के भय से यहाँ