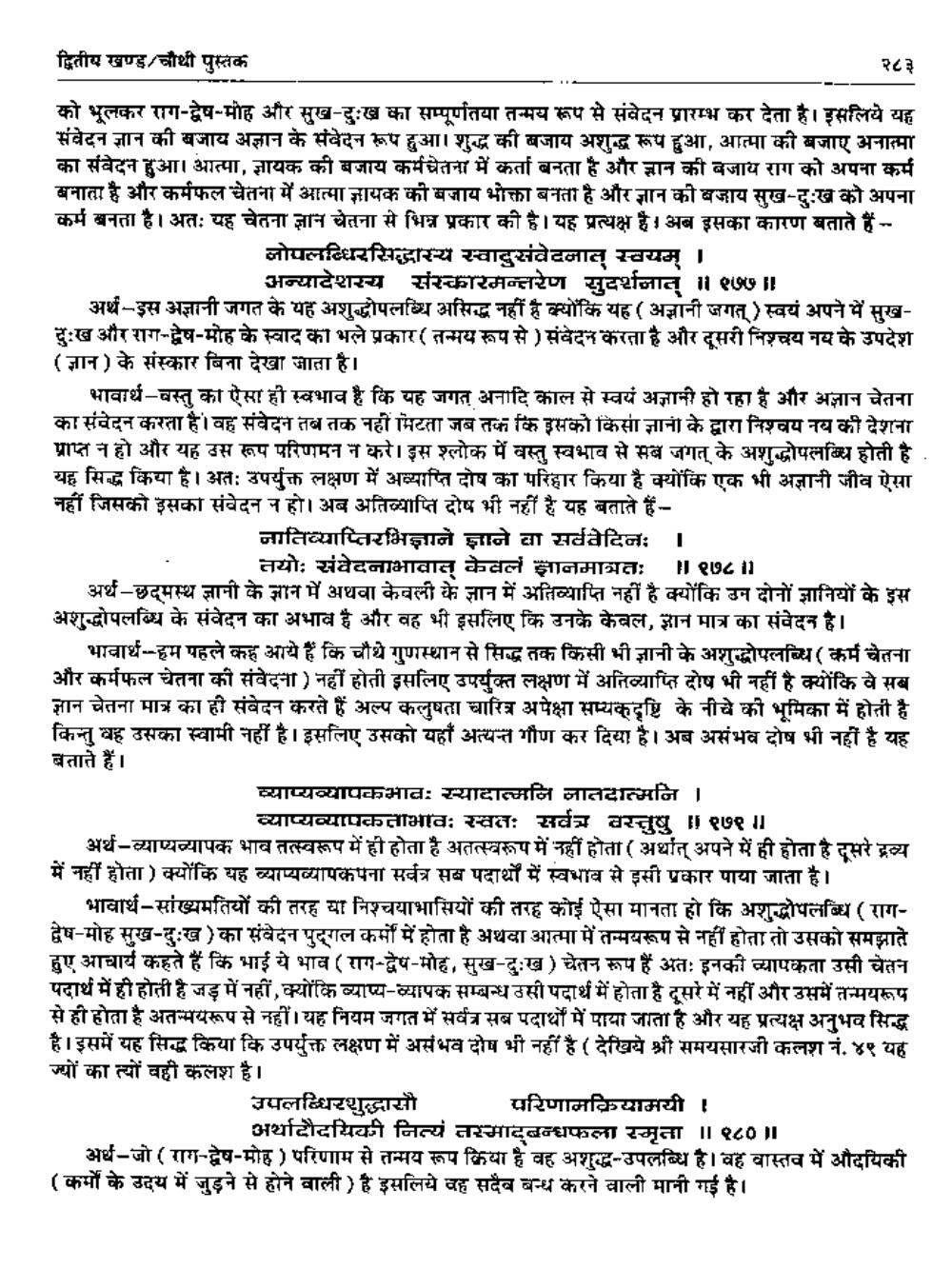________________
द्वितीय खण्ड /चौथी पुस्तक
२८३
को भूलकर राग-द्वेष-मोह और सुख-दुःख का सम्पूर्णतया तन्मय रूप से संवेदन प्रारम्भ कर देता है। इसलिये यह संवेदन ज्ञान की बजाय अज्ञान के संवेदन रूप हुआ। शुद्ध की बजाय अशुद्ध रूप हुआ, आत्मा की बजाए अनात्मा का संवेदन हुआ । आत्मा, ज्ञायक की बजाय कर्मचेतना में कर्ता बनता है और ज्ञान की बजाय राग को अपना कर्म बनाता है और कर्मफल चेतना में आत्मा ज्ञायक की बजाय भोक्ता बनता है और ज्ञान की बजाय सुख-दुःख को अपना कर्म बनता है। अतः यह चेतना ज्ञान चेतना से भिन्न प्रकार की है। यह प्रत्यक्ष है। अब इसका कारण बताते हैंलोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुसंवेदनात् स्वयम् ।
T
अन्यादेशस्य संस्कारमन्तरेण सुदर्शनात् ॥ ९७७ ॥
अर्थ- इस अज्ञानी जगत के यह अशुद्धोपलब्धि असिद्ध नहीं है क्योंकि यह ( अज्ञानी जगत् ) स्वयं अपने में सुखदुःख और राग-द्वेष-मोह के स्वाद का भले प्रकार (तन्मय रूप से) संवेदन करता है और दूसरी निश्चय नय के उपदेश (ज्ञान) के संस्कार बिना देखा जाता है।
भावार्थ- वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है कि यह जगत् अनादि काल से स्वयं अज्ञानी हो रहा है और अज्ञान चेतना का संवेदन करता है। वह संवेदन तब तक नहीं मिटता जब तक कि इसको किसी ज्ञानी के द्वारा निश्चय नय की देशना प्राप्त न हो और यह उस रूप परिणामन न करे। इस श्लोक में वस्तु स्वभाव से सब जगत् के अशुद्धोपलब्धि होती है यह सिद्ध किया है। अतः उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष का परिहार किया है क्योंकि एक भी अज्ञानी जीव ऐसा नहीं जिसको इसका संवेदन न हो। अब अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है यह बताते हैं
नातिव्याप्तिरभिज्ञाने ज्ञाने वा सर्ववेदिनः
I
तयोः संवेदनाभावात् केवलं ज्ञानमात्रतः
॥ ९७८ ॥
अर्थ - छद्मस्थ ज्ञानी के ज्ञान में अथवा केवली के ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि उन दोनों ज्ञानियों के इस अशुद्धोपलब्धि के संवेदन का अभाव है और वह भी इसलिए कि उनके केवल, ज्ञान मात्र का संवेदन है।
भावार्थ - हम पहले कह आये हैं कि चौथे गुणस्थान से सिद्ध तक किसी भी ज्ञानी के अशुद्धोपलब्धि (कर्म चेतना और कर्मफल चेतना की संवेदना ) नहीं होती इसलिए उपर्युक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है क्योंकि वे सब ज्ञान चेतना मात्र का ही संवेदन करते हैं अल्प कलुषता चारित्र अपेक्षा सम्यकदृष्टि के नीचे की भूमिका में होती है किन्तु वह उसका स्वामी नहीं है। इसलिए उसको यहाँ अत्यन्त गौण कर दिया है। अब असंभव दोष भी नहीं है यह बताते हैं ।
व्याप्यव्यापकभाव: स्थादात्मनि नातदात्मनि । व्याप्यव्यापकताभाव: स्वतः सर्वत्र वस्तुषु ॥ ९७९ ॥
अर्थ-व्याप्यव्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है अतत्स्वरूप में नहीं होता ( अर्थात् अपने में ही होता है दूसरे द्रव्य में नहीं होता) क्योंकि यह व्याप्यव्यापकपना सर्वत्र सब पदार्थों में स्वभाव से इसी प्रकार पाया जाता है।
भावार्थ- सांख्यमतियों की तरह या निश्चयाभासियों की तरह कोई ऐसा मानता हो कि अशुद्धोपलब्धि (रागद्वेष- मोह सुख - दु: ख ) का संवेदन पुद्गल कर्मों में होता है अथवा आत्मा में तन्मयरूप से नहीं होता तो उसको समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई ये भाव (राग-द्वेष-मोह, सुख-दुःख ) चेतन रूप हैं अतः इनकी व्यापकता उसी चेतन पदार्थ में ही होती है जड़ में नहीं, क्योंकि व्याप्य व्यापक सम्बन्ध उसी पदार्थ में होता है दूसरे में नहीं और उसमें तन्मयरूप से ही होता है अतन्मयरूप से नहीं। यह नियम जगत में सर्वत्र सब पदार्थों में पाया जाता है और यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है । इसमें यह सिद्ध किया कि उपर्युक्त लक्षण में असंभव दोष भी नहीं है (देखिये श्री समयसारजी कलश नं. ४९ यह ज्यों का त्यों वही कलश है।
उपलब्धिरशुद्धासौ
परिणामक्रियामयी !
अर्थादौदयिकी नित्यं तस्माद्बन्धफला स्मृता ॥ ९८० ॥
अर्ध-जो ( राग-द्वेष-मोह ) परिणाम से तन्मय रूप किया है वह अशुद्ध-उपलब्धि है। वह वास्तव में औदयिकी
( कर्मों के उदय में जुड़ने से होने वाली ) है इसलिये वह सदैव बन्ध करने वाली मानी गई है।