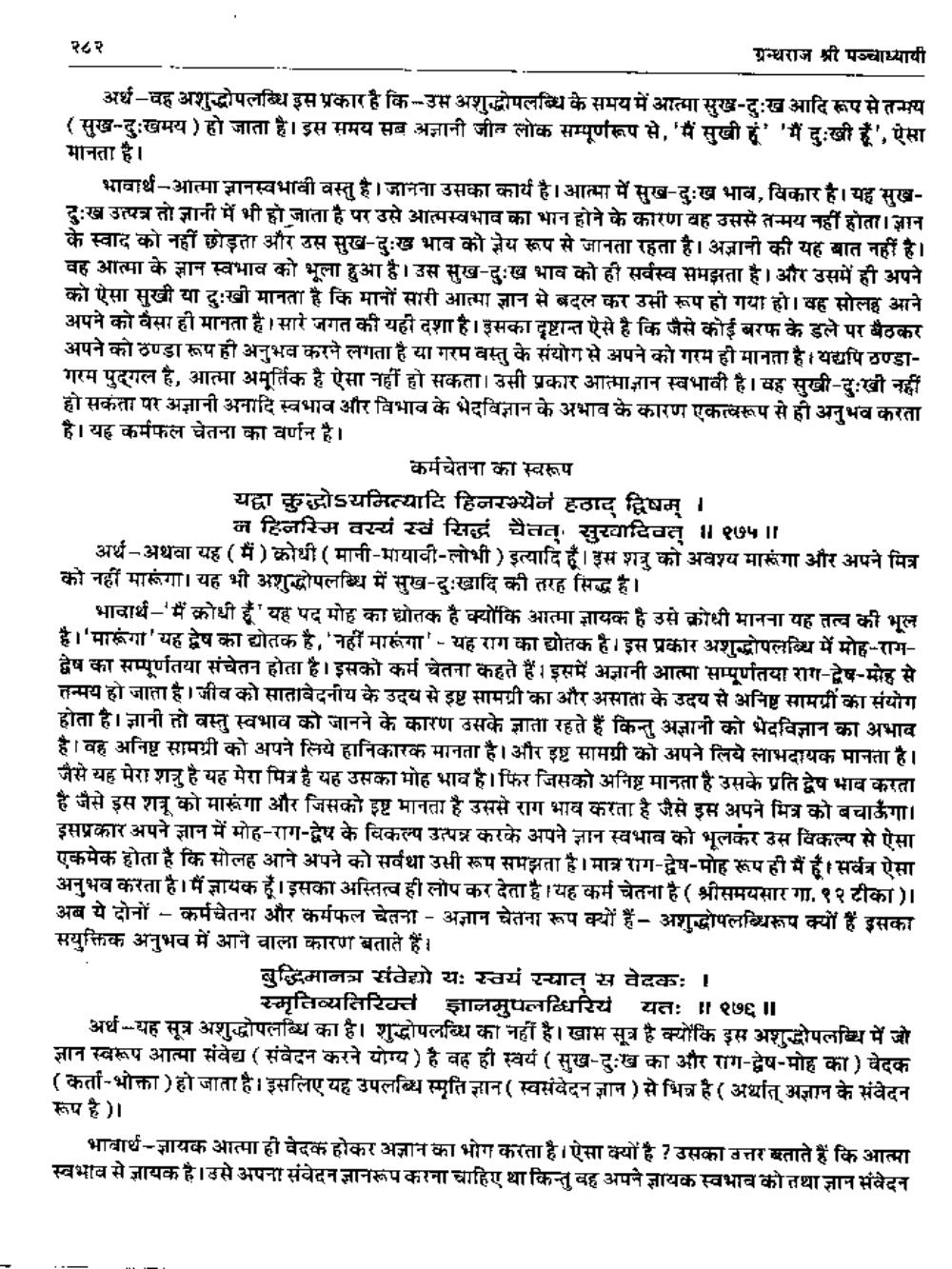________________
२८२
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
अर्थ-वह अशुद्धोपलब्धि इस प्रकार है कि-उस अशुद्धोपलब्धि के समय में आत्मा सुख-दुःख आदि रूप से तन्मय (सुख-दुःखमय ) हो जाता है। इस समय सब अज्ञानी जीत लोक सम्पूर्णरूप से, 'मैं सुखी हूं' 'मैं दुःखी हूँ', ऐस मानता है।
भावार्थ-आत्मा ज्ञानस्वभावी वस्तु है। जानना उसका कार्य है। आत्मा में सुख-दुःख भाव, विकार है। यह सुखदुःख उत्पन्न तो ज्ञानी में भी हो जाता है पर उसे आत्मस्वभाव का भान होने के कारण वह उससे तन्मय नहीं होता । ज्ञान के स्वाद को नहीं छोड़ता और उस सुख-दुःख भाव को ज्ञेय रूप से जानता रहता है। अज्ञानी की यह बात नहीं है। वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भूला हुआ है। उस सुख-दुःख भाव को ही सर्वस्व समझता है और उसमें ही अपने को ऐसा सुखी या दुःखी मानता है कि मानों सारी आत्मा ज्ञान से बदल कर उसी रूप हो गया हो। वह सोलह आने अपने को वैसा ही मानता है। सारे जगत की यही दशा है। इसका दृष्टान्त ऐसे है कि जैसे कोई बरफ के डले पर बैठकर अपने को ठण्डारूप ही अनुभव करने लगता है या गरम वस्तु के संयोग से अपने को गरम ही मानता है। यद्यपि ठण्डागरम पुद्गल है, आत्मा अमूर्तिक है ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्माज्ञान स्वभावी है। वह सुखी-दुःखी नहीं हो सकता पर अज्ञानी अनादि स्वभाव और विभाव के भेदविज्ञान के अभाव के कारण एकत्वरूप से ही अनुभव करता है। यह कर्मफल चेतना का वर्णन है।
कर्मचेतना का स्वरूप यद्वा कुन्द्धोऽयमित्यादि हिनरभ्येने हठाद् द्विषम् ।
न हिनरिम वस्यं रखें सिद्धं चैतत् सुरवादिवत् ॥ ९७५ ॥
यह (मैं) क्रोधी ( मानी-मायावी-लोभी) इत्यादि हैं। इस शव को अवश्य मारूंगा और अपने मित्र को नहीं मारूंगा। यह भी अशुद्धोपलब्धि में सुख-दुःखादि की तरह सिद्ध है।
भावार्थ-'मैं क्रोधी हूँ'यह पद मोह का द्योतक है क्योंकि आत्मा जायक है उसे क्रोधी मानना यह तत्व की भूल है। मारूंगा' यह द्वेष का द्योतक है, नहीं मारूंगा' - यह राग का द्योतक है। इस प्रकार अशुद्धोपलब्धि में मोह-रामद्वेष का सम्पूर्णतया संचेतन होता है। इसको कर्म चेतना कहते हैं। इसमें अज्ञानी आत्मा सम्पूर्णतया राग-द्वेष-मोह से तन्मय हो जाता है। जीव को सातावेदनीय के उदय से इष्ट सामग्री का और असाता के उदय से अनिष्ट सामग्री का संयोग होता है। ज्ञानी तो वस्तु स्वभाव को जानने के कारण उसके ज्ञाता रहते हैं किन्तु अज्ञानी को भेदविज्ञान का अभाव है। वह अनिष्ट सामग्री को अपने लिये हानिकारक मानता है। और इष्ट सामग्री को अपने लिये लाभदायक मानता है। जैसे यह मेरा शत्रु है यह मेरा मित्र है यह उसका मोह भाव है। फिर जिसको अनिष्ट मानता है उसके प्रति द्वेष भाव करता है जैसे इस शत्रू को मारूंगा और जिसको इष्ट मानता है उससे राग भाव करता है जैसे इस अपने मित्र को बचाऊँगा। इसप्रकार अपने ज्ञान में मोह-राग-द्वेष के विकल्प उत्पन्न करके अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर उस विकल्प से ऐसा एकमेक होता है कि सोलह आने अपने को सर्वथा उसी रूप समझता है। मात्र राग-द्वेष-मोह रूप ही मैं हूँ। सर्वत्र ऐसा अनुभव करता है। मैं ज्ञायक हूँ। इसका अस्तित्व ही लोप कर देता है। यह कर्म चेतना है ( श्रीसमयसार गा.१२ टीका)। अब ये दोनों - कर्मचेतना और कर्मफल चेतना - अज्ञान चेतना रूप क्यों हैं - अशुद्धोपलब्धिरूप क्यों हैं इसका सयुक्तिक अनुभव में आने वाला कारण बताते हैं।
बुद्धिमानन संवेद्यो यः स्वयं स्यात् स वेदकः ।
स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानमुपलब्धिरियं यतः १९७६॥ अर्ध-यह सूत्र अशुद्धोपलब्धि का है। शुद्धोपलब्धि का नहीं है। खास सूत्र है क्योंकि इस अशुद्धोपलब्धि में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा संवेद्य (संवेदन करने योग्य) है वह ही स्वयं ( सुख-दुःख का और राग-द्वेष-मोह का) वेदक (कर्ता-भोक्ता)हो जाता है। इसलिए यह उपलब्धि स्मृति ज्ञान ( स्वसंवेदन ज्ञान) से भिन्न है ( अर्थात् अज्ञान के संवेदन रूप है।
भावार्थ-ज्ञायक आत्मा ही वेदकहोकर अज्ञानका भोग करता है। ऐसा क्यों है? उसका उत्तर बताते हैं कि आत्मा स्वभाव से ज्ञायक है।उसे अपना संवेदन ज्ञानरूपकरना चाहिए था किन्तु वह अपने ज्ञायक स्वभाव को तथा ज्ञान संवेदन