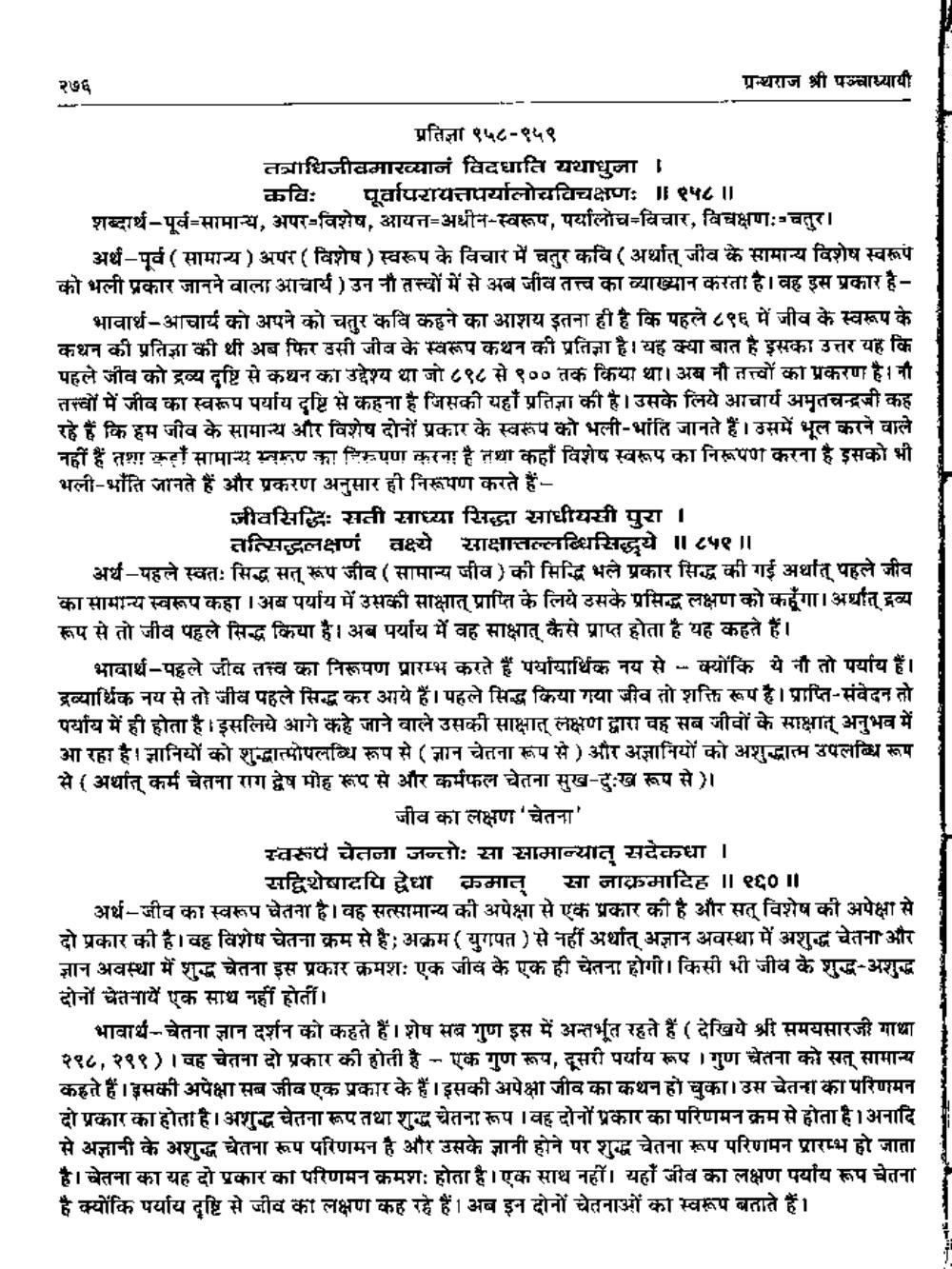________________
२७६
प्रतिज्ञा ९५८- ९५९
तत्राधिजीवमाख्यानं विदधाति यथाधुना ।
पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षणः ॥ ९५८ ॥
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
कविः
शब्दार्थ- पूर्व- सामान्य, अपर-विशेष, आयन- अधीन स्वरूप, पर्यालोच-विचार, विचक्षणः- चतुर ।
अर्थ - पूर्व (सामान्य) अपर (विशेष ) स्वरूप के विचार में चतुर कवि ( अर्थात् जीव के सामान्य विशेष स्वरूपं को भली प्रकार जानने वाला आचार्य ) उन नौ तत्वों में से अब जीव तत्त्व का व्याख्यान करता है। वह इस प्रकार है
-
भावार्थ- आचार्य को अपने को चतुर कवि कहने का आशय इतना ही है कि पहले ८९६ में जीव के स्वरूप के कथन की प्रतिज्ञा की थी अब फिर उसी जीव के स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा है। यह क्या बात है इसका उत्तर यह कि पहले जीव को द्रव्य दृष्टि से कथन का उद्देश्य था जो ८९८ से १०० तक किया था। अब नौ तत्त्वों का प्रकरण है। नौ तस्वों में जीव का स्वरूप पर्याय दृष्टि से कहना है जिसकी यहाँ प्रतिज्ञा की है । उसके लिये आचार्य अमृतचन्द्रजी कह रहे हैं कि हम जीव के सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के स्वरूप को भली-भांति जानते हैं। उसमें भूल करने वाले नहीं हैं तथा कहाँ सामान्य स्वरूप का निरूपण करना है तथा कहाँ विशेष स्वरूप का निरूपण करना है इसको भी भली-भाँति जानते हैं और प्रकरण अनुसार ही निरूपण करते हैं
जीवसिद्धिः सती साध्या सिद्धा साधीयसी पुरा । तत्सिद्धलक्षणं वक्ष्ये साक्षात्तल्लब्धिसिद्धये ॥ ८५९ ॥
अर्थ - पहले स्वतः सिद्ध सत् रूप जीव ( सामान्य जीव ) की सिद्धि भले प्रकार सिद्ध की गई अर्थात् पहले जीव का सामान्य स्वरूप कहा । अब पर्याय में उसकी साक्षात् प्राप्ति के लिये उसके प्रसिद्ध लक्षण को कहूँगा। अर्थात् द्रव्य रूप से तो जीव पहले सिद्ध किया है। अब पर्याय में वह साक्षात् कैसे प्राप्त होता है यह कहते हैं ।
भावार्थ- पहले जीव तत्त्व का निरूपण प्रारम्भ करते हैं पर्यायार्थिक नय से क्योंकि ये नौ तो पर्याय हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो जीव पहले सिद्ध कर आये हैं। पहले सिद्ध किया गया जीव तो शक्ति रूप है। प्राप्ति संवेदन तो पर्याय में ही होता है। इसलिये आगे कहे जाने वाले उसकी साक्षात् लक्षण द्वारा वह सब जीवों के साक्षात् अनुभव में आ रहा है । ज्ञानियों को शुद्धात्मोपलब्धि रूप से (ज्ञान चेतना रूप से) और अज्ञानियों को अशुद्धात्म उपलब्धि रूप से (अर्थात् कर्म चेतना राग द्वेष मोह रूप से और कर्मफल चेतना सुख-दुःख रूप से )।
जीव का लक्षण 'चेतना'
स्वरूपं चेतना जन्तोः सा सामान्यात् सदेकधा । सद्विशेषादपि द्वेधा क्रमात् सा नाक्रमादिह ॥ ९६० ॥
अर्थ- जीव का स्वरूप चेतना है। वह सत्सामान्य की अपेक्षा से एक प्रकार की है और सत् विशेष की अपेक्षा से दो प्रकार की है। वह विशेष चेतना क्रम से है; अक्रम (युगपत) से नहीं अर्थात् अज्ञान अवस्था में अशुद्ध चेतना और ज्ञान अवस्था में शुद्ध चेतना इस प्रकार क्रमशः एक जीव के एक ही चेतना होगी। किसी भी जीव के शुद्ध-अशुद्ध दोनों चेतनायें एक साथ नहीं होतीं ।
भावार्थ- चेतना ज्ञान दर्शन को कहते हैं। शेष सब गुण इस में अन्तर्भूत रहते हैं (देखिये श्री समयसारजी गाथा २९८, १९९ ) । वह चेतना दो प्रकार की होती है एक गुण रूप दूसरी पर्याय रूप गुण चेतना को सत् सामान्य कहते हैं। इसकी अपेक्षा सब जीव एक प्रकार के हैं। इसकी अपेक्षा जीव का कथन हो चुका। उस चेतना का परिणमन दो प्रकार का होता है। अशुद्ध चेतना रूप तथा शुद्ध चेतना रूप । वह दोनों प्रकार का परिणमन क्रम से होता है । अनादि से अज्ञानी के अशुद्ध चेतना रूप परिणमन है और उसके ज्ञानी होने पर शुद्ध चेतना रूप परिणमन प्रारम्भ हो जाता है। चेतना का यह दो प्रकार का परिणमन क्रमशः होता है। एक साथ नहीं। यहाँ जीव का लक्षण पर्याय रूप चेतना है क्योंकि पर्याय दृष्टि से जीव का लक्षण कह रहे हैं। अब इन दोनों चेतनाओं का स्वरूप बताते हैं ।