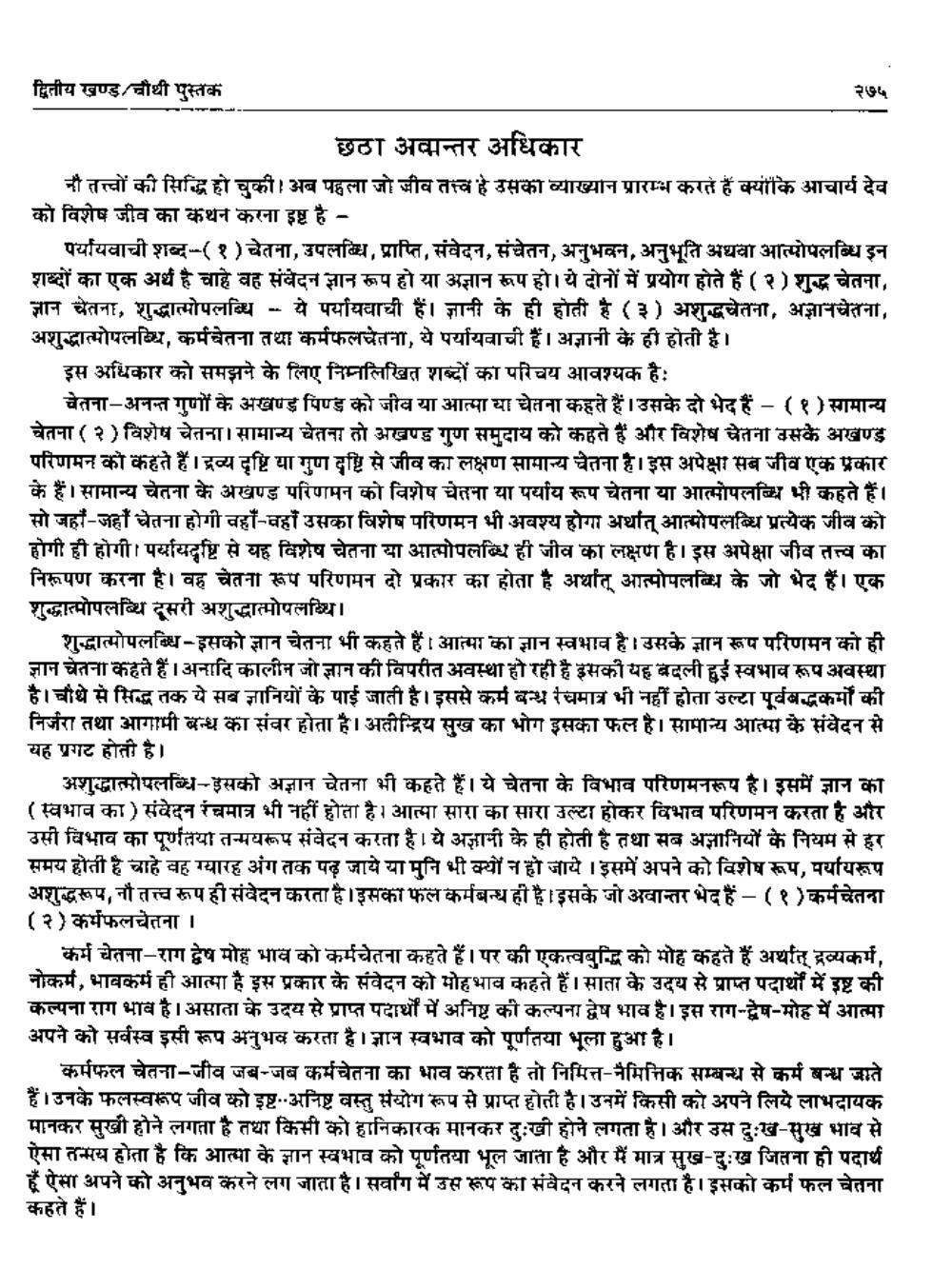________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
२७५
छठा अवान्तर अधिकार नौ तत्त्वों की सिद्धि हो चुकी। अब पहला जो जीव तत्व हे उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं क्योंकि आचार्य देव को विशेष जीव का कथन करना इष्ट है -
पर्यायवाची शब्द-(१)चेतना, उपलब्धि, प्राप्ति, संवेदन, संचेतन, अनुभवन, अनुभूति अथवा आत्मोपलब्धि इन शब्दों का एक अर्थ है चाहे वह संवेदन ज्ञान रूप हो या अज्ञान रूप हो। ये दोनों में प्रयोग होते हैं ( २)शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना, शुद्धात्मोपलब्धि -- ये पर्यायवाची हैं। ज्ञानी के ही होती है (३) अशुद्धचेतना, अज्ञानचेतना, अशुद्धात्मोपलब्धि, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना, ये पर्यायवाची हैं। अज्ञानी के ही होती है।
इस अधिकार को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों का परिचय आवश्यक है:
चेतना-अनन्त गुणों के अखण्ड पिण्ड को जीव या आत्मा या चेतना कहते हैं। उसके दो भेद हैं - (१)सामान्य चेतना (विशेष चेतना। सामान्य चेतना तो अखण्ड गण समदाय को कहते हैं और विशेष चेतना परिणमन को कहते हैं। द्रव्य दृष्टि या गुण दृष्टि से जीव का लक्षण सामान्य चेतना है। इस अपेक्षा सब जीव एक प्रकार के हैं। सामान्य चेतना के अखण्ड परिणमन को विशेष चेतना या पर्याय रूप चेतना या आत्मोपलब्धि भी कहते हैं। सो जहाँ-जहाँ चेतना होगी वहाँ-वहाँ उसका विशेष परिणमन भी अवश्य होगा अर्थात् आत्मोपलब्धि प्रत्येक जीव को होगी ही होगी। पर्यायदृष्टि से यह विशेष चेतना या आत्मोपलब्धि ही जीव का लक्षण है। इस अपेक्षा जीव तत्त्व का निरूपण करना है। वह चेतना रूप परिणमन दो प्रकार का होता है अर्थात् आत्मोपलब्धि के जो भेद हैं। एक शुद्धात्मोपलब्धि दूसरी अशुद्धास्मोपलब्धि।
शुद्धात्मोपलब्धि-इसको ज्ञान चेतना भी कहते हैं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। उसके ज्ञान रूप परिणमन को ही ज्ञान चेतना कहते हैं। अनादिकालीन जो ज्ञान की विपरीत अवस्था हो रही है इसकी यह बदली हुई स्वभावरूपअवस्था है। चौथे से सिद्ध तक ये सब ज्ञानियों के पाई जाती है। इससे कर्म बन्धरेचमात्र भी नहीं होता उल्टा पूर्वबद्धकर्मों की निर्जरा तथा आगामी बन्धका संवर होता है। अतीन्द्रिय सख का भोग इसका फल है। सामान्य आत्मा के संवेदन से यह प्रगट होती है।
अशुद्धात्मोपलब्धि-इसको अज्ञान चेतना भी कहते हैं। ये चेतना के विभाव परिणमनरूप है। इसमें ज्ञान का (स्वभाव का) संवेदन रंचमात्र भी नहीं होता है। आत्मा सारा का सारा उल्टा होकर विभाव परिणमन करता है और उसी विभाव का पूर्णतया तन्मयरूप संवेदन करता है। ये अज्ञानी के ही होती है तथा सब अज्ञानियों के नियम से हर समय होती है चाहे वह ग्यारह अंग तक पढ़ जाये या मुनि भी क्यों न हो जाये । इसमें अपने को विशेष रूप, पर्यायरूप अशुद्धरूप, नौ तत्त्व रूपही संवेदन करता है। इसका फल कर्मबन्ध ही है। इसके जो अवान्तर भेद हैं - (१)कर्मचेतना (२) कर्मफलचेतना ।। ___ कर्म चेतना-राग द्वेष मोह भाव को कर्मचेतना कहते हैं। पर की एकत्वबुद्धि को मोह कहते हैं अर्थात् द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकर्म ही आत्मा है इस प्रकार के संवेदन को मोहभाव कहते हैं। साता के उदय से प्राप्त पदार्थों में इष्ट की कल्पना राग भाव है। असाता के उदय से प्राप्त पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना द्वेष भाव है। इस राग-द्वेष-मोह में आत्मा अपने को सर्वस्व इसी रूप अनुभव करता है। ज्ञान स्वभाव को पूर्णतया भूला हुआ है।
कर्मफल चेतना-जीव जब-जब कर्मचेतना का भाव करता है तो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध से कर्म बन्ध जाते हैं। उनके फलस्वरूप जीव को इष्ट- अनिष्ट वस्तु संयोग रूप से प्राप्त होती है। उनमें किसी को अपने लिये लाभदायक मानकर सुखी होने लगता है तथा किसी को हानिकारक मानकर दुःखी होने लगता है। और उस दुःख-सुख भाव से ऐसा तन्मय होता है कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव को पूर्णतया भूल जाता है और मैं मात्र सुख-दुःख जितना ही पदार्थ हूँ ऐसा अपने को अनुभव करने लग जाता है। सर्वांग में उस रूप का संवेदन करने लगता है। इसको कर्म फल चेतना कहते हैं।