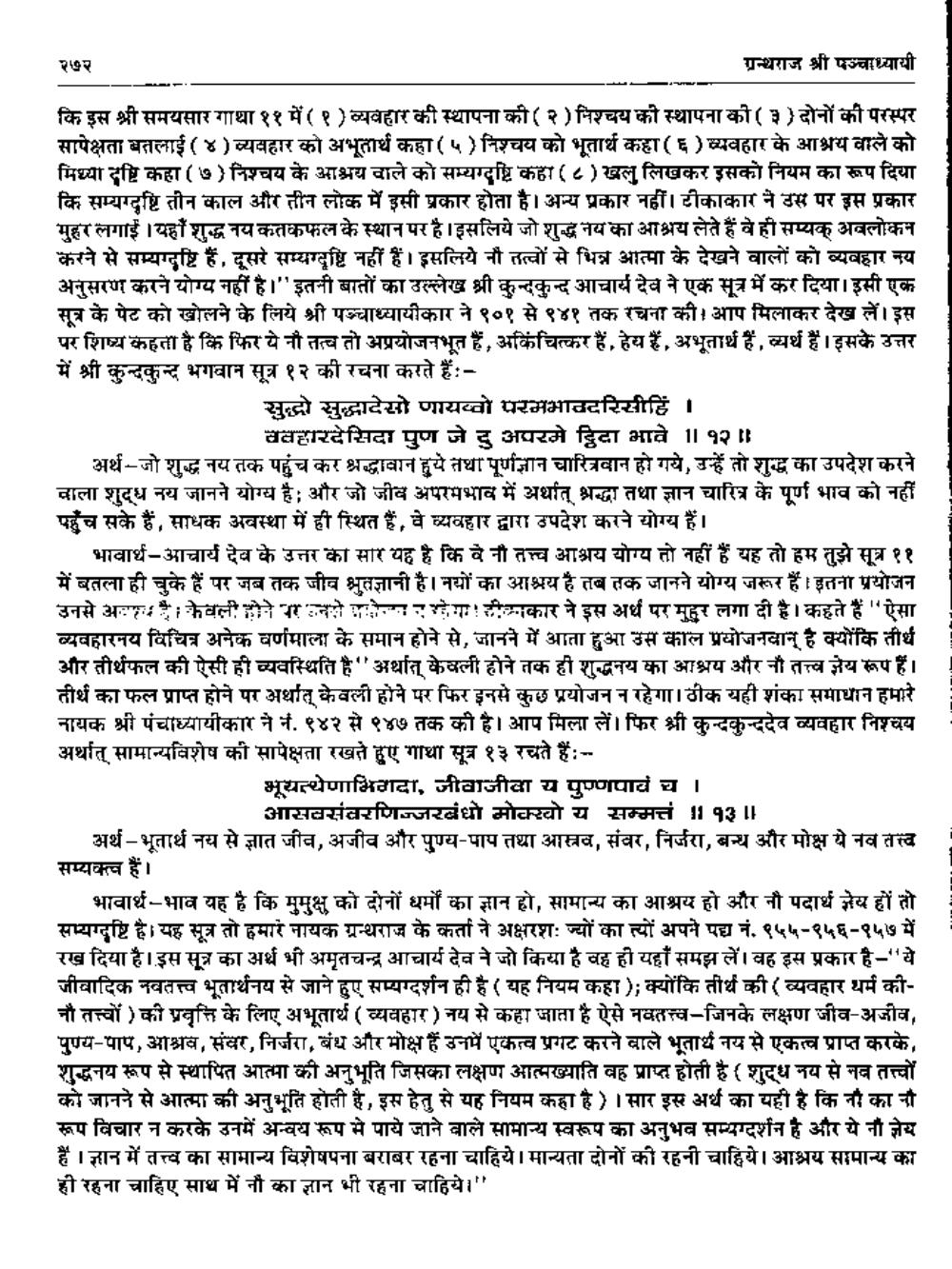________________
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
कि इस श्री समयसार गाथा ११ में ( ९ ) व्यवहार की स्थापना की ( २ ) निश्चय की स्थापना की (३) दोनों की परस्पर सापेक्षता बतलाई ( ४ ) व्यवहार को अभूतार्थ कहा ( ५ ) निश्चय को भूतार्थ कहा ( ६ ) व्यवहार के आश्रय वाले को मिध्यादृष्टि कहा ( ७ ) निश्चय के आश्रय वाले को सम्यग्दृष्टि कहा ( ८ ) खलु लिखकर इसको नियम का रूप दिया कि सम्यग्दृष्टि तीन काल और तीन लोक में इसी प्रकार होता है। अन्य प्रकार नहीं। टीकाकार ने उस पर इस प्रकार मुहर लगाईं । यहाँ शुद्ध नय कतकफल के स्थान पर है। इसलिये जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक् अवलोकन करने से सम्यग्दृष्टि हैं, दूसरे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं। इसलिये नौ तत्वों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है।" इतनी बातों का उल्लेख श्री कुन्दकुन्द आचार्य देव ने एक सूत्र में कर दिया। इसी एक सूत्र के पेट को खोलने के लिये श्री पञ्चाध्यायीकार ने ९०१ से १४१ तक रचना की। आप मिलाकर देख लें। इस पर शिष्य कहता है कि फिर ये नौ तत्व तो अप्रयोजनभूत हैं, अकिंचित्कर हैं, हेय हैं, अभूतार्थ हैं, व्यर्थ हैं। इसके उत्तर में श्री कुन्दकुन्द भगवान सूत्र १२ की रचना करते हैं:
-
२७२
सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरिसीहिं । ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥ १२ ॥
अर्थ- जो शुद्ध नय तक पहुंच कर श्रद्धावान हुये तथा पूर्णज्ञान चारित्रवान हो गये, उन्हें तो शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है; और जो जीव अपरमभाव में अर्थात् श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।
भावार्थ- आचार्य देव के उत्तर का सार यह है कि वे नौ तत्त्व आश्रय योग्य तो नहीं हैं यह तो हम तुझे सूत्र ११ में बतला ही चुके हैं पर जब तक जीव श्रुतज्ञानी है। नयों का आश्रय है तब तक जानने योग्य जरूर हैं। इतना प्रयोजन उनसे है। केवली होने पर कार ने इस अर्थ पर मुहर लगा दी है। कहते हैं " ऐसा व्यवहारनय विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से, जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान् है क्योंकि तीर्थं और तीर्थफल की ऐसी ही व्यवस्थिति है" अर्थात् केवली होने तक ही शुद्धनय का आश्रय और नौ तत्त्व ज्ञेय रूप हैं । तीर्थ का फल प्राप्त होने पर अर्थात् केवली होने पर फिर इनसे कुछ प्रयोजन न रहेगा। ठीक यही शंका समाधान हमारे नायक श्री पंचाध्यायीकार ने नं. ९४२ से ९४७ तक की है। आप मिला लें। फिर श्री कुन्दकुन्ददेव व्यवहार निश्चय अर्थात् सामान्यविशेष की सापेक्षता रखते हुए गाथा सूत्र १३ रचते हैं: --
भूयत्येणाभिगदा, जीवाजीवा य पुण्णपावं च । आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्स्खो य सम्मत्तं ॥ १३ ॥
अर्थ-भूतार्थ नय से ज्ञात जीव, अजीव और पुण्य पाप तथा आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नव तत्त्व सम्यक्त्व हैं।
भावार्थ - भाव यह है कि मुमुक्षु को दोनों धर्मों का ज्ञान हो, सामान्य का आश्रय हो और नौ पदार्थ ज्ञेय हों तो सम्यग्दृष्टि है। यह सूत्र तो हमारे नायक ग्रन्थराज के कर्ता ने अक्षरशः ज्यों का त्यों अपने पद्य नं. ९५५ - ९५६ - ९५७ में रख दिया है। इस सूत्र का अर्थ भी अमृतचन्द्र आचार्य देव ने जो किया है वह ही यहाँ समझ लें । वह इस प्रकार है-" ये जीवादिक नवतत्त्व भूतार्थनय से जाने हुए सम्यग्दर्शन ही है ( यह नियम कहा ); क्योंकि तीर्थ की ( व्यवहार धर्म कीनौ तत्त्वों) की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ (व्यवहार) नय से कहा जाता है ऐसे नवतत्त्व- जिनके लक्षण जीव- अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष हैं उनमें एकत्व प्रगट करने वाले भूतार्थं नय से एकत्व प्राप्त करके, शुद्धtय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण आत्मख्याति वह प्राप्त होती है ( शुद्ध नय से नव तत्त्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यह नियम कहा है ) । सार इस अर्थ का यही है कि नौ का नौ रूप विचार न करके उनमें अन्वय रूप मे पाये जाने वाले सामान्य स्वरूप का अनुभव सम्यग्दर्शन है और ये नौ ज्ञेय हैं। ज्ञान में तत्त्व का सामान्य विशेषपना बराबर रहना चाहिये। मान्यता दोनों की रहनी चाहिये। आश्रय सामान्य का ही रहना चाहिए साथ में नौ का ज्ञान भी रहना चाहिये।"