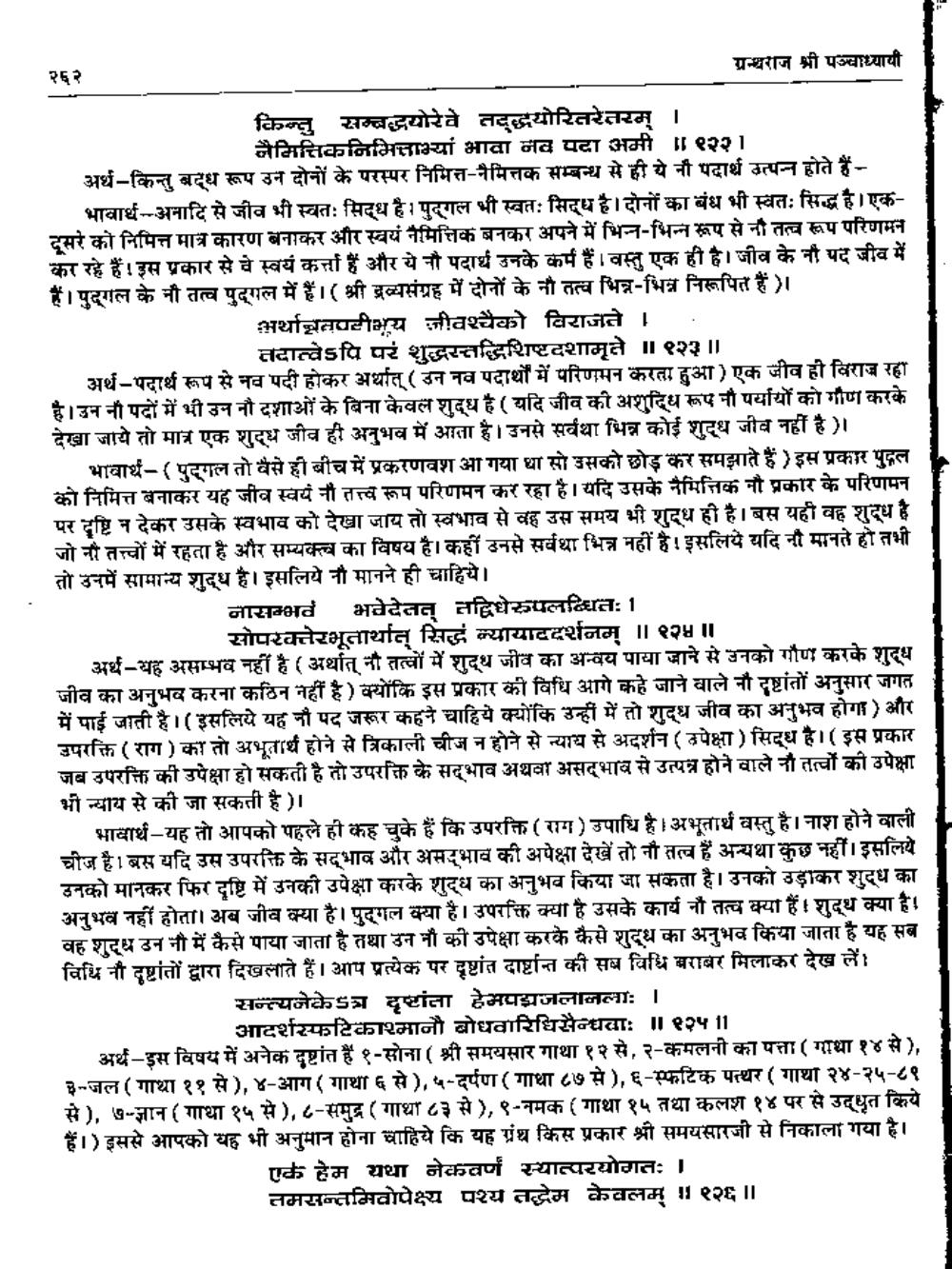________________
२६२
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
किन्तु सम्बद्धयोरेवे तद्द्वयोरितरेतरम् । नैमित्तिकनिमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ॥ ९२२ ॥ अर्थ-किन्तु बद्ध रूप उन दोनों के परस्पर निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध से ही ये नौ पदार्थ उत्पन्न होते हैं
भावार्थ -- अनादि से जीव भी स्वतः सिद्ध है। पुद्गल भी स्वतः सिद्ध है। दोनों का बंध भी स्वतः सिद्ध है। एकदूसरे को निमित्त मात्र कारण बनाकर और स्वयं नैमित्तिक बनकर अपने में भिन्न-भिन्न रूप से नौ तत्व रूप परिणमन कर रहे हैं। इस प्रकार से वे स्वयं कर्त्ता हैं और ये नौ पदार्थ उनके कर्म हैं। वस्तु एक ही है। जीव के नौ पद जीव में हैं । पुद्गल के नौ तत्व पुद्गल में हैं। (श्री द्रव्यसंग्रह में दोनों के नौ तत्व भिन्न-भिन्न निरूपित हैं ) ।
अर्थातपटीभूय जीवश्चैको विराजते ।
तदात्वेऽपि परं शुद्धस्तद्धिशिष्टदशामृते ॥ ९२३ ॥
अर्थ - पदार्थ रूप से नव पदी होकर अर्थात् (उन नव पदार्थों में परिणमन करता हुआ ) एक जीव ही विराज रहा है। उन नौ पदों में भी उन नौ दशाओं के बिना केवल शुद्ध है (यदि जीव की अशुद्धि रूप नौ पर्यायों को गौण करके देखा जाये तो मात्र एक शुद्ध जीव ही अनुभव में आता है। उनसे सर्वथा भिन्न कोई शुद्ध जीव नहीं है )।
भावार्थ - (पुद्गल तो वैसे ही बीच में प्रकरणवश आ गया था सो उसको छोड़ कर समझाते हैं ) इस प्रकार पुगल को निमित्त बनाकर यह जीव स्वयं नौ तत्त्व रूप परिणमन कर रहा है। यदि उसके नैमित्तिक नौ प्रकार के परिणमन पर दृष्टि न देकर उसके स्वभाव को देखा जाय तो स्वभाव से वह उस समय भी शुद्ध ही है। बस यही वह शुद्ध है जो नौ तत्त्वों में रहता है और सम्यक्त्व का विषय है। कहीं उनसे सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिये यदि नौ मानते हो तभी तो उनमें सामान्य शुद्ध है। इसलिये नौ मानने ही चाहिये।
नासम्भवं भवेदेतत् तद्विधेरुपलब्धितः । सोपरक्तेरभूतार्थात् सिद्धं न्यायाददर्शनम् ॥ २२४ ॥
अर्थ - यह असम्भव नहीं है (अर्थात् नौ तत्वों में शुद्ध जीव का अन्वय पाया जाने से उनको गौण करके शुद्ध जीव का अनुभव करना कठिन नहीं है) क्योंकि इस प्रकार की विधि आगे कहे जाने वाले नौ दृष्टांतों अनुसार जगत में पाई जाती है। (इसलिये यह नौ पद जरूर कहने चाहिये क्योंकि उन्हीं में तो शुद्ध जीव का अनुभव होगा ) और उपरक्ति (राग) का तो अभूतार्थं होने से त्रिकाली चीज न होने से न्याय से अदर्शन (उपेक्षा ) सिद्ध है। ( इस प्रकार जब उपरक्ति की उपेक्षा हो सकती है तो उपरक्ति के सद्भाव अथवा असद्भाव से उत्पन्न होने वाले नौ तत्वों की उपेक्षा भी न्याय से की जा सकती है ) ।
भावार्थ - यह तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि उपरक्ति (राग) उपाधि है। अभूतार्थं वस्तु है। नाश होने वाली चीज है। बस यदि उस उपरक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा देखें तो नौ तत्व हैं अन्यथा कुछ नहीं। इसलिये उनको मानकर फिर दृष्टि में उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया जा सकता है। उनको उड़ाकर शुद्ध का अनुभव नहीं होता। अब जीव क्या है। पुद्गल क्या है। उपरक्ति क्या है उसके कार्य नौ तत्व क्या हैं। शुद्ध क्या है! वह शुद्ध उन नौ में कैसे पाया जाता है तथा उन नौ की उपेक्षा करके कैसे शुद्ध का अनुभव किया जाता है यह सब विधि नौ दृष्टांतों द्वारा दिखलाते हैं। आप प्रत्येक पर दृष्टांत दाष्टान्त की सब विधि बराबर मिलाकर देख लें।
सन्त्यनेकेऽत्र दृष्टांता हेअपझजलानलाः । आदर्शस्फटिकाश्मानौ बोधवारिधिसैन्धवाः ॥ ९२५ ॥
अर्थ - इस विषय में अनेक दृष्टांत है १ - सोना ( श्री समयसार गाथा १२ से २- कमलनी का पत्ता ( गाथा १४ से ), ३- जल (गाथा ११ से ), ४- आग ( गाथा ६ से ), ५ - दर्पण ( गाथा ८७ से ), ६- स्फटिक पत्थर ( गाथा २४-२५-८९ किये से), ७ - ज्ञान ( गाथा १५ से ), ८ - समुद्र ( गाथा ८३ से ), ९ - नमक ( गाथा १५ तथा कलश १४ पर से उद्धृत हैं।) इससे आपको यह भी अनुमान होना चाहिये कि यह ग्रंथ किस प्रकार श्री समयसारजी से निकाला गया है। एक हेम यथा नेकवर्णं स्थात्परयोगतः । तमसन्तमिवोपेक्ष्य पश्य तद्धेम केवलम् ॥ ९२६ ॥