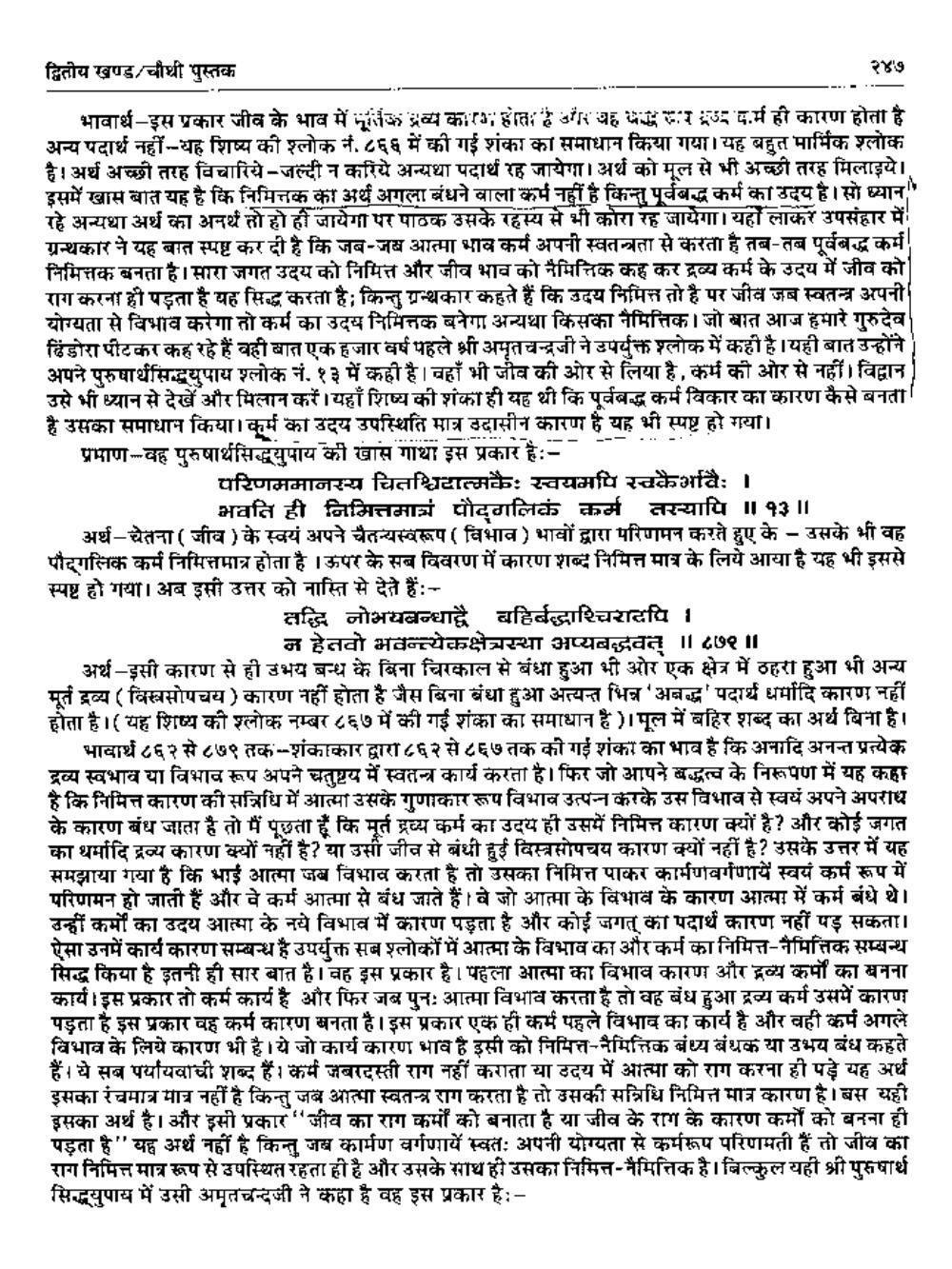________________
द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तक
भावार्थ - इस प्रकार जीव के भाव में मूर्तिक द्रव्य कारण होता है और यह
कर्म ही कारण होता है अन्य पदार्थ नहीं - यह शिष्य की श्लोक नं. ८६६ में की गई शंका का समाधान किया गया। यह बहुत मार्मिक श्लोक है | अर्थ अच्छी तरह विचारिये जल्दी न करिये अन्यथा पदार्थ रह जायेगा। अर्थ को मूल से भी अच्छी तरह मिलाइये। इसमें खास बात यह है कि निमित्तक का अर्थ अगला बंधने वाला कर्म नहीं है किन्तु पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। सो ध्यान रहे अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो हो हो जायेगा पर पाठक उसके रहस्य से भी कोरा रह जायेगा। यहाँ लाकर उपसंहार में ग्रन्थकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब-जब आत्मा भाव कर्म अपनी स्वतन्त्रता से करता है तब-तब पूर्वबद्ध कर्म निमित्तक बनता है । सारा जगत उदय को निमित्त और जीव भाव को नैमित्तिक कह कर द्रव्य कर्म के उदय में जीव को राग करना ही पड़ता है यह सिद्ध करता है; किन्तु ग्रन्थकार कहते हैं कि उदय निमित्त तो है पर जीव जब स्वतन्त्र अपनी योग्यता से विभाव करेगा तो कर्म का उदय निर्मित्तक बनेगा अन्यथा किसका नैमित्तिक । जो बात आज हमारे गुरुदेव छिंडोरा पीटकर कह रहे हैं वही बात एक हजार वर्ष पहले श्री अमृतचन्द्रजी ने उपर्युक्त श्लोक में कही है। यही बात उन्होंने अपने पुरुषार्थसिद्धयुपाय श्लोक नं. १३ में कही है। वहाँ भी जीव की ओर से लिया है, कर्म की ओर से नहीं। विद्वान उसे भी ध्यान से देखें और मिलान करें। यहाँ शिष्य की शंका ही यह थी कि पूर्वबद्ध कर्म विकार का कारण कैसे बनता है उसका समाधान किया। कूर्म का उदय उपस्थिति मात्र उदासीन कारण है यह भी स्पष्ट हो गया।
प्रमाण - वह पुरुषार्थसिद्धयुपाय की खास गाथा इस प्रकार है: -
२४७
परिणममानस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैअवैः ।
-
भवति ही निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥ अर्थ - चेतना (जीव ) के स्वयं अपने चैतन्यस्वरूप ( विभाव) भावों द्वारा परिणमन करते हुए के उसके भी वह पौद्गलिक कर्म निमित्तमात्र होता है । ऊपर के सब विवरण में कारण शब्द निमित्त मात्र के लिये आया है यह भी इससे स्पष्ट हो गया। अब इसी उत्तर को नास्ति से देते हैं:
तद्धि नोभयबन्धाद्वै
बहिर्बद्धाश्चिरादपि ।
न हेतवो भवन्त्येकक्षेत्रस्था अप्यबद्धवत् ॥ २७९ ॥
अर्थ - इसी कारण से | उभय बन्ध के बिना चिरकाल से बंधा हुआ भी ओर एक क्षेत्र में ठहरा हुआ भी अन्य मूर्त द्रव्य (विस्वसोपचय) कारण नहीं होता है जैस बिना बंधा हुआ अत्यन्त भिन्न 'अबद्ध ' पदार्थ धर्मादि कारण नहीं होता है। ( यह शिष्य की श्लोक नम्बर ८६७ में की गई शंका का समाधान हैं ) । मूल में बहिर शब्द का अर्थ बिना है।
भावार्थ ८६२ से ८७९ तक- शंकाकार द्वारा ८६२ से ८६७ तक की गई शंकर का भाव है कि अनादि अनन्त प्रत्येक द्रव्य स्वभाव या विभाव रूप अपने चतुष्टय में स्वतन्त्र कार्य करता है। फिर जो आपने बद्धत्व के निरूपण में यह कहा है कि निमित्त कारण की सन्निधि में आत्मा उसके गुणाकार रूप विभाव उत्पन्न करके उस विभाव से स्वयं अपने अपराध के कारण बंध जाता है तो मैं पूछता हूँ कि मूर्त द्रव्य कर्म का उदय ही उसमें निमित्त कारण क्यों है? और कोई जगत का धर्मादि द्रव्य कारण क्यों नहीं है? या उसी जीव से बंधी हुई विस्त्रसोपचय कारण क्यों नहीं है? उसके उत्तर में यह समझाया गया है कि भाई आत्मा जब विभाव करता है तो उसका निमित्त पाकर कार्मणवर्गणायें स्वयं कर्म रूप में परिणमन हो जाती हैं और वे कर्म आत्मा से बंध जाते हैं। वे जो आत्मा के विभाव के कारण आत्मा में कर्म बंधे थे। उन्हीं कर्मों का उदय आत्मा के नये विभाव में कारण पड़ता है और कोई जगत् का पदार्थ कारण नहीं पड़ सकता । ऐसा उनमें कार्य कारण सम्बन्ध है उपर्युक्त सब श्लोकों में आत्मा के विभाव का और कर्म का निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध सिद्ध किया है इतनी ही सार बात है। वह इस प्रकार है। पहला आत्मा का विभाव कारण और द्रव्य कर्मों का बनना कार्यं । इस प्रकार तो कर्म कार्य है और फिर जब पुनः आत्मा विभाव करता है तो वह बंध हुआ द्रव्य कर्म उसमें कारण पड़ता है इस प्रकार वह कर्म कारण बनता है। इस प्रकार एक ही कर्म पहले विभाव का कार्य है और वही कर्म अगले विभाव के लिये कारण भी है। ये जो कार्य कारण भाव है इसी को निमित्तनैमित्तिक बंध्य बंधक या उभय बंध कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। कर्म जबरदस्ती राग नहीं कराता या उदय में आत्मा को राग करना ही पड़े यह अर्थ इसका रंचमात्र मात्र नहीं है किन्तु जब आत्मा स्वतन्त्र राग करता है तो उसकी सन्निधि निमित्त मात्र कारण है। बस यही इसका अर्थ । और इसी प्रकार " जीव का राग कर्मों को बनाता है या जीव के राग के कारण कर्मों को बनना ही पड़ता है" यह अर्थ नहीं है किन्तु जब कार्मण वर्गणायें स्वतः अपनी योग्यता से कर्मरूप परिणमती हैं तो जीव का राग निमित्त मात्र रूप से उपस्थित रहता ही है और उसके साथ ही उसका निमित्त नैमित्तिक है। बिल्कुल यही श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में उसी अमृतचन्दजी ने कहा है वह इस प्रकार है: