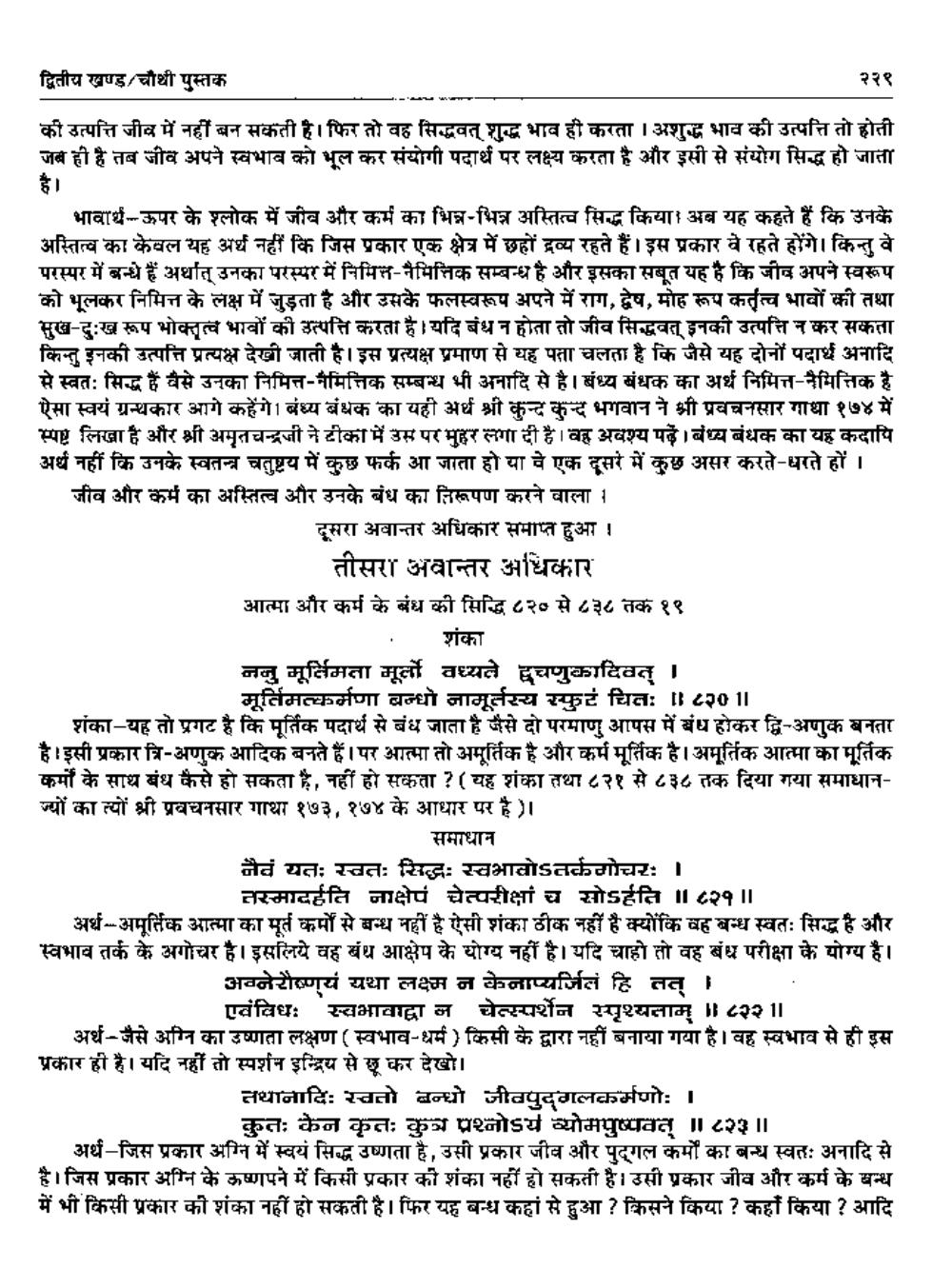________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
२२९
की उत्पत्ति जीव में नहीं बन सकती है। फिर तो वह सिद्धवत् शुद्ध भाव ही करता । अशुद्ध भाव की उत्पत्ति तो होती जब ही है तब जीव अपने स्वभाव को भूल कर संयोगी पदार्थ पर लक्ष्य करता है और इसी से संयोग सिद्ध हो जाता
भावार्थ-ऊपर के श्लोक में जीव और कर्म का भिन्न-भिन्न अस्तित्व सिद्ध किया। अब यह कहते हैं कि उनके अस्तित्व का केवल यह अर्थ नहीं कि जिस प्रकार एक क्षेत्र में छहों द्रव्य रहते हैं। इस प्रकार वे रहते होंगे। किन्तु वे परस्पर में बन्धे हैं अर्थात् उनका परस्पर में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है और इसका सबूत यह है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर निमित्त के लक्ष में जुड़ता है और उसके फलस्वरूप अपने में राग, द्वेष, मोह रूप कर्तृत्त्व भावों की तथा सुख-दुःख रूप भोक्तृत्व भावों की उत्पत्ति करता है। यदि बंधन होता तो जीव सिद्धवत् इनकी उत्पत्ति न कर सकता किन्तु इनकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से यह पता चलता है कि जैसे यह दोनों पदार्थ अनादि से स्वत: सिद्ध हैं वैसे उनका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी अनादि से है। बंध्य बंधक का अर्थ निमित्त-नैमित्तिक है ऐसा स्वयं ग्रन्थकार आगे कहेंगे1 बंध्य बंधक का यही अर्थ श्री कुन्द कुन्द भगवान ने श्री प्रबचनसार गाथा १७४ में स्पष्ट लिखा है और श्री अमृतचन्द्रजी नेटीका में उस पर मुहर लगा दी है। वह अवश्य पढ़ें। बंध्य बंधक का यह कदापि अर्थ नहीं कि उनके स्वतन्त्र चतुष्टय में कुछ फर्क आ जाता हो या वे एक दूसरे में कुछ अ जीव और कर्म का अस्तित्व और उनके बंध का निरूपण करने वाला ।
दूसरा अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ ।
तीसरा अवान्तर अधिकार आत्मा और कर्म के बंध की सिद्धि ८२० से ८३८ तक १९
शंका ननु मूर्तिमता मूर्लो वध्यते द्वचणुकादिवत् ।
मूर्तिमत्कर्मणा बन्धो नामूर्तस्य स्फुट चितः ॥ ८२० ॥ शंका-यह तो प्रगट है कि मूर्तिक पदार्थ से बंध जाता है जैसे दो परमाणु आपस में बंध होकर द्वि-अणुक बनता है। इसी प्रकार त्रि-अणक आदिक बनते हैं। पर आत्मा तो अमर्तिक है और कर्म मर्तिक है। अम कर्मों के साथ बंध कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता?(यह शंका तथा ८२१ से ८३८ तक दिया गया समाधानज्यों का त्यों श्री प्रवचनसार गाथा १७३.१७४ के आधार पर है।
समाधान नैवं यतः स्वतः सिद्धः स्वभावोऽतर्कगोचरः ।
तस्मादर्हति नाक्षेपं चेत्परीक्षां च सोऽहति ॥ ८२१॥ अर्थ-अमूर्तिक आत्मा का मूर्त कर्मों से बन्ध नहीं है ऐसी शंका ठीक नहीं है क्योंकि वह बन्ध स्वतः सिद्ध है और स्वभाव तर्क के अगोचर है। इसलिये वह बंध आक्षेप के योग्य नहीं है। यदि चाहो तो वह बंध परीक्षा के योग्य है।
अवनेरौष्ण्यं यथा लक्ष्म न केनाप्यर्जितं हि तत् ।
एवंविधः स्वभावाद्वा न चेत्स्पर्शेन स्पृश्यताम् ॥ ८२२ ॥ अर्थ-जैसे अग्नि का उष्णता लक्षण (स्वभाव-धर्म ) किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। वह स्वभाव से ही इस प्रकार ही है। यदि नहीं तो स्पर्शन इन्द्रिय से छू कर देखो।
तथानादिः ततो बन्यो जीतपुदगलकर्मणोः ।
कुतः केन कतः कुत्र प्रश्नोऽय व्योमपुष्पावत ॥ ८२३ ॥ अर्थ-जिस प्रकार अग्नि में स्वयं सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्मों का बन्ध स्वतः अनादि से है। जिस प्रकार अग्नि के ऊष्णपने में किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जीव और कर्म के बन्ध में भी किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती है। फिर यह बन्ध कहां से हुआ? किसने किया? कहाँ किया ? आदि