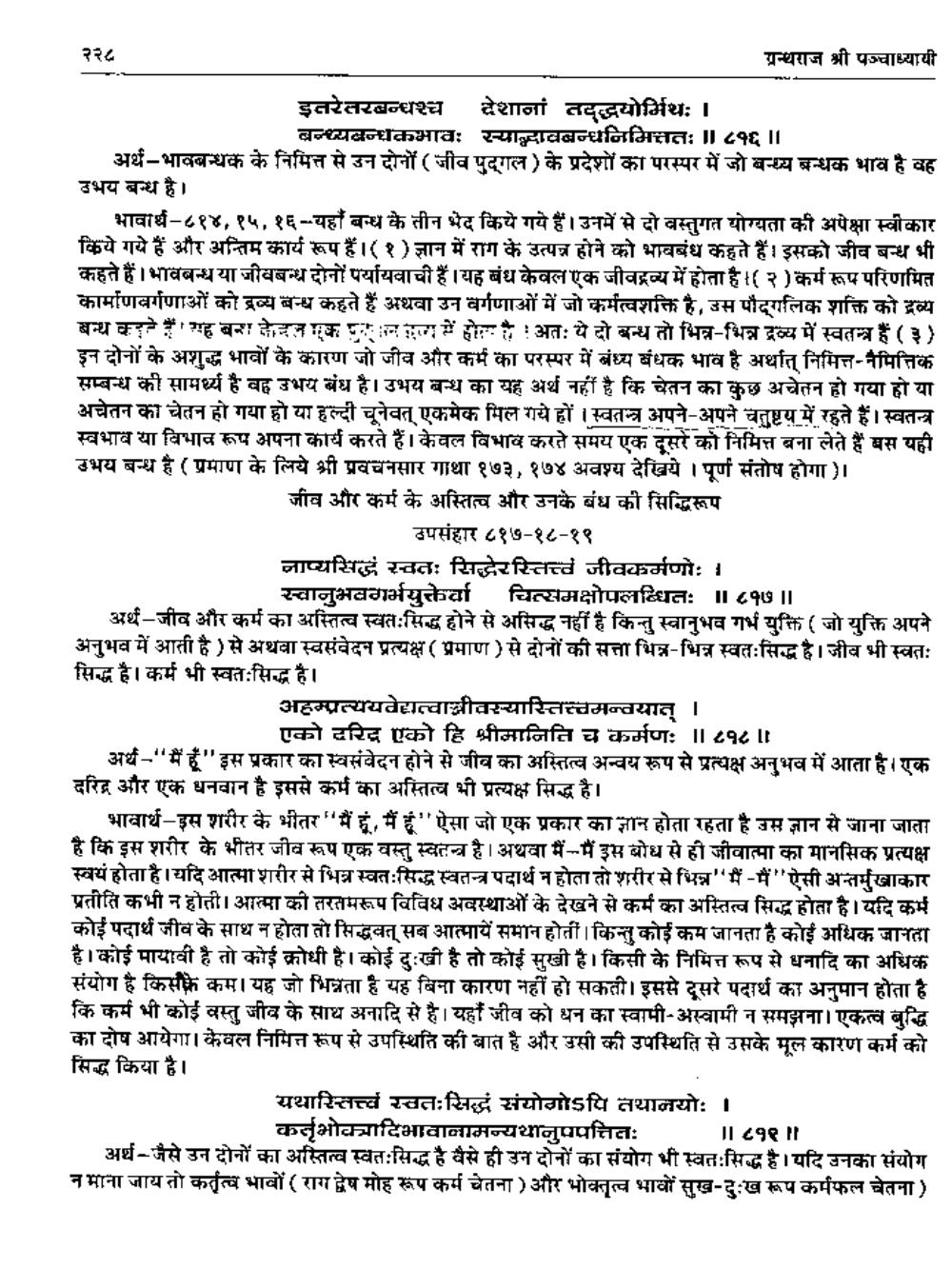________________
२२८
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
इतरेतरबन्धश्च देशानां तद्द्वयोर्मिथः ।
बन्ध्यबन्धकभावः स्याद्भावबन्धनिमित्ततः ॥ ८१६ ॥
अर्थ - भावबन्धक के निमित्त से उन दोनों (जीव पुद्गल ) के प्रदेशों का परस्पर में जो बन्ध्य बन्धक भाव है वह उभय बन्ध है ।
भावार्थ - ८१४, १५, १६ - यहाँ बन्ध के तीन भेद किये गये हैं। उनमें से दो वस्तुगत योग्यता की अपेक्षा स्वीकार किये गये हैं और अन्तिम कार्य रूप हैं । ( १ ) ज्ञान में राग के उत्पन्न होने को भावबंध कहते हैं। इसको जीव बन्ध भी कहते हैं । भावबन्ध या जीवबन्ध दोनों पर्यायवाची हैं। यह बंध केवल एक जीवद्रव्य में होता है । ( २ ) कर्म रूप परिणमित कार्माणवर्गणाओं को द्रव्य बन्ध कहते हैं अथवा उन वर्गणाओं में जो कर्मत्वशक्ति है, उस पौद्गलिक शक्ति को द्रव्य बन्ध करते हैं। यह बस केवल एक में होता है अतः ये दो बन्ध तो भिन्न-भिन्न द्रव्य में स्वतन्त्र हैं ( ३ ) इन दोनों के अशुद्ध भावों के कारण जो जीव और कर्म का परस्पर में बंध्य बंधक भाव है अर्थात् निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध की सामर्थ्य है वह उभय बंध है । उभय बन्ध का यह अर्थ नहीं है कि चेतन का कुछ अचेतन हो गया हो या अचेतन का चेतन हो गया हो या हल्दी चूनेवत् एकमेक मिल गये हों । स्वतन्त्र अपने-अपने चतुष्टय में रहते हैं । स्वतन्त्र स्वभाव या विभावरूप अपना कार्य करते हैं। केवल विभाव करते समय एक दूसरे को निमित्त बना लेते हैं बस यही उभय बन्ध है ( प्रमाण के लिये श्री प्रवचनसार गाथा १७३, १७४ अवश्य देखिये । पूर्ण संतोष होगा ) । जीव और कर्म के अस्तित्व और उनके बंध की सिद्धिरूप उपसंहार ८१७-१८-१९
नाप्यसिद्धं स्वतः सिद्धेरस्तित्त्वं जीवकर्मणोः । स्वानुभवगर्भयुक्तेर्वा चित्समक्षोपलब्धितः ॥ ८१७ ॥
अर्थ-जीव और कर्म का अस्तित्व स्वतः सिद्ध होने से असिद्ध नहीं है किन्तु स्वानुभव गर्भ युक्ति (जो युक्ति अपने अनुभव में आती है) से अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष (प्रमाण ) से दोनों की सत्ता भिन्न-भिन्न स्वतः सिद्ध है। जीव भी स्वतः सिद्ध है। कर्म भी स्वतः सिद्ध है।
अहम्प्रत्ययवेद्यत्वाञ्जीवस्यास्तित्त्वमन्वयात् ।
एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कर्मणः ॥ ८१८
अर्थ - " मैं हूँ" इस प्रकार का स्वसंवेदन होने से जीव का अस्तित्व अन्वय रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। एक दरिद्र और एक धनवान है इससे कर्म का अस्तित्व भी प्रत्यक्ष सिद्ध है।
भावार्थ - इस शरीर के भीतर "मैं हूं, मैं हूं" ऐसा जो एक प्रकार का ज्ञान होता रहता है उस ज्ञान से जाना जाता है कि इस शरीर के भीतर जीव रूप एक वस्तु स्वतन्त्र है। अथवा मैं-मैं इस बोध से ही जीवात्मा का मानसिक प्रत्यक्ष स्वयं होता है। यदि आत्मा शरीर से भिन्न स्वतः सिद्ध स्वतन्त्र पदार्थ न होता तो शरीर से भिन्न " मैं मैं ऐसी अन्तर्मुखाकार प्रतीति कभी न होती । आत्मा की तरतमरूप विविध अवस्थाओं के देखने से कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि कर्म कोई पदार्थ जीव के साथ न होता तो सिद्धवत् सब आत्मायें समान होतीं । किन्तु कोई कम जानता है कोई अधिक जानता है। कोई मायावी है तो कोई क्रोधी है। कोई दुःखी है तो कोई सुखी है। किसी के निमित्त रूप से धनादि का अधिक संयोग है किसीके कम । यह जो भिन्नता है यह बिना कारण नहीं हो सकती। इससे दूसरे पदार्थ का अनुमान होता है कि कर्म भी कोई वस्तु जीव के साथ अनादि से है। यहाँ जीव को धन का स्वामी- अस्वामी न समझना एकत्व बुद्धि का दोष आयेगा । केवल निमित्त रूप से उपस्थिति की बात है और उसी की उपस्थिति से उसके मूल कारण कर्म को सिद्ध किया है।
यथारितत्त्वं स्वतः सिद्धं संयोगोऽपि तथानयोः । कर्तृभोक्त्रादिभावानामन्यथानुपपत्तितः
|| ८१९ ॥
अर्थ- जैसे उन दोनों का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है वैसे ही उन दोनों का संयोग भी स्वतः सिद्ध है। यदि उनका संयोग न माना जाय तो कर्तृत्व भावों (राग द्वेष मोह रूप कर्म चेतना) और भोक्तृत्व भावों सुख-दुःख रूप कर्मफल चेतना)