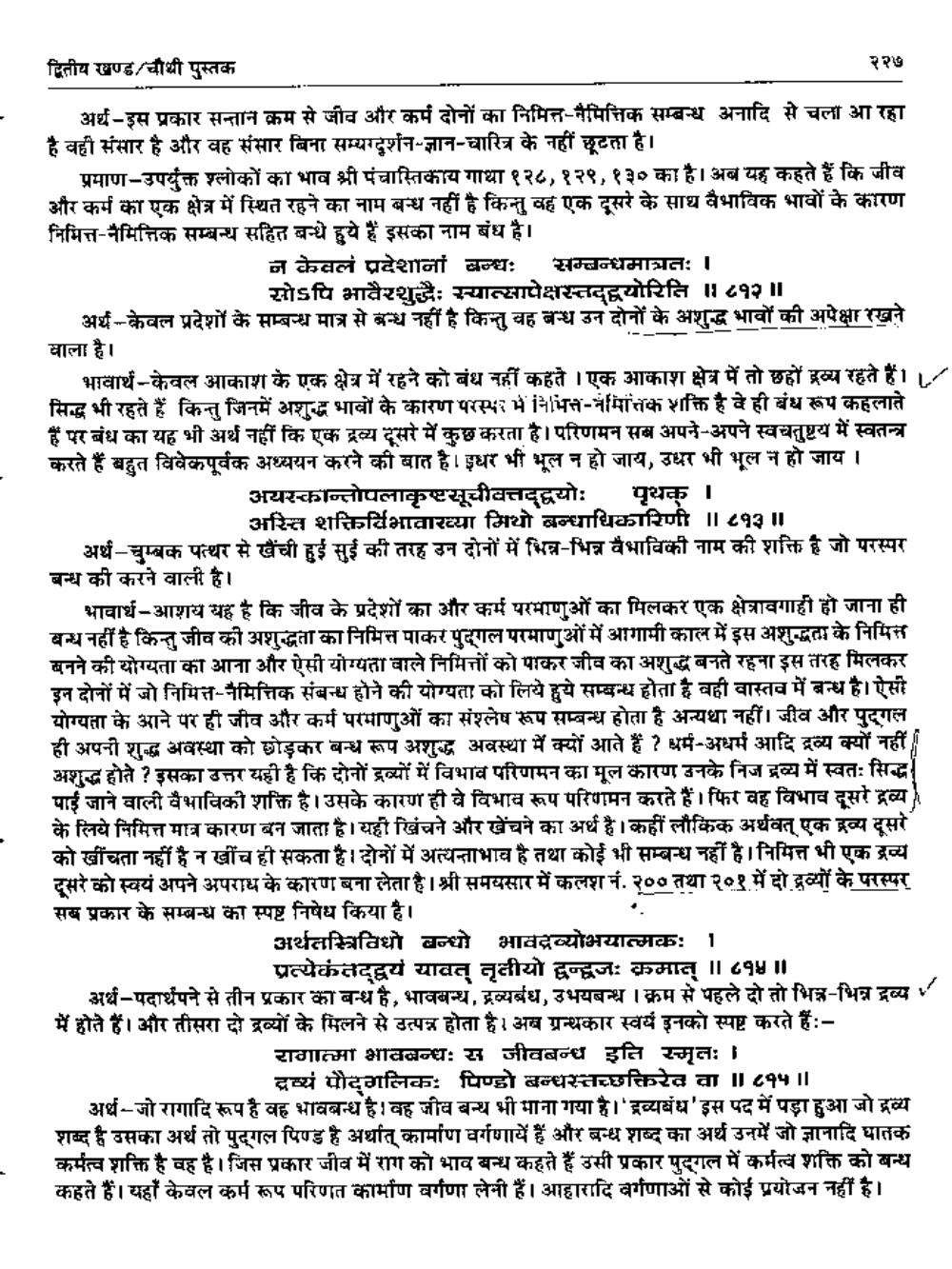________________
द्वितीय खण्ड /चौथी पुस्तक
२२७
अर्थ - इस प्रकार सन्तान क्रम से जीव और कर्म दोनों का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अनादि से चला आ रहा है वही संसार है और वह संसार बिना सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र के नहीं छूटता है।
प्रमाण - उपर्युक्त श्लोकों का भाव श्री पंचास्तिकाय गाथा १२८, १२९, १३० का है। अब यह कहते हैं कि जीव और कर्म का एक क्षेत्र में स्थित रहने का नाम बन्ध नहीं है किन्तु वह एक दूसरे के साथ वैभाविक भावों के कारण निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध सहित बन्धे हुये हैं इसका नाम बंध है।
न केवलं प्रदेशानां बन्धः
'सम्बन्धमात्रतः ।
सोऽपि भावैरशुद्धः स्यात्सापेक्षस्तद्द्वयोरिति ॥ ८१२ ॥ अर्थ- केवल प्रदेशों के सम्बन्ध मात्र से बन्ध नहीं है किन्तु वह बन्ध उन दोनों के अशुद्ध भावों की अपेक्षा रखने वाला है ।
भावार्थ - केवल आकाश के एक क्षेत्र में रहने को बंध नहीं कहते। एक आकाश क्षेत्र में तो छहों द्रव्य रहते हैं। L सिद्ध भी रहते हैं किन्तु जिनमें अशुद्ध भावों के कारण परस्पर में नितिन शक्ति है वे ही बंध रूप कहलाते हैं पर बंध का यह भी अर्थ नहीं कि एक द्रव्य दूसरे में कुछ करता है। परिणमन सब अपने-अपने स्वचतुष्टय में स्वतन्त्र करते हैं बहुत विवेकपूर्वक अध्ययन करने की बात है। इधर भी भूल न हो जाय, उधर भी भूल न हो जाय ।
अयस्कान्तोपलाकृष्टसूचीवत्तद्द्वयोः
पृथक् ।
अस्ति शक्तिर्विभावाख्या मिथो बन्धाधिकारिणी ॥ ८१३ ॥ अर्थ- चुम्बक पत्थर से खैंची हुई सुई की तरह उन दोनों में भिन्न-भिन्न वैभाविकी नाम की शक्ति है जो परस्पर बन्ध की करने वाली है।
भावार्थ- आशय यह है कि जीव के प्रदेशों का और कर्म परमाणुओं का मिलकर एक क्षेत्रावगाही हो जाना ही बन्ध नहीं है किन्तु जीव की अशुद्धता का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणुओं में आगामी काल में इस अशुद्धता के निमित्त बनने की योग्यता का आना और ऐसी योग्यता वाले निमित्तों को पाकर जीव का अशुद्ध बनते रहना इस तरह मिलकर इन दोनों में जो निमित्तनैमित्तिक संबन्ध होने की योग्यता को लिये हुये सम्बन्ध होता है वही वास्तव में बन्ध है। ऐसी योग्यता के आने पर ही जीव और कर्म परमाणुओं का संश्लेष रूप सम्बन्ध होता है अन्यथा नहीं जीव और पुद्गल ही अपनी शुद्ध अवस्था को छोड़कर बन्ध रूप अशुद्ध अवस्था में क्यों आते हैं ? धर्म-अधर्म आदि द्रव्य क्यों नहीं ।। अशुद्ध होते ? इसका उत्तर यही है कि दोनों द्रव्यों में विभाव परिणमन का मूल कारण उनके निज द्रव्य में स्वतः सिद्ध पाई जाने वाली वैभाविकी शक्ति है। उसके कारण ही वे विभाव रूप परिणमन करते हैं। फिर वह विभाव दूसरे द्रव्य के लिये निमित्त मात्र कारण बन जाता है। यही खिंचने और खेंचने का अर्थ है। कहीं लौकिक अर्थवत् एक द्रव्य दूसरे को खींचता नहीं है न खींच ही सकता है। दोनों में अत्यन्ताभाव है तथा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। निमित्त भी एक द्रव्य दूसरे को स्वयं अपने अपराध के कारण बना लेता है। श्री समयसार में कलश नं. २०० तथा २०१ में दो द्रव्यों के परस्पर सब प्रकार के सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध किया है।
अर्थतस्त्रिविधो बन्धो भावद्रव्योभयात्मकः 1
प्रत्येकंतद्द्द्वयं यावत् तृतीयो द्वन्द्वजः क्रमात् ॥ ८१४ ॥
अर्थ - पदार्थपने से तीन प्रकार का बन्ध है, भावबन्ध, द्रव्यबंध, उभयबन्ध । क्रम से पहले दो तो भिन्न-भिन्न द्रव्य में होते हैं। और तीसरा दो द्रव्यों के मिलने से उत्पन्न होता है। अब ग्रन्थकार स्वयं इनको स्पष्ट करते हैं:
रागात्मा भातबन्धः स जीवबन्ध इति स्मृतः ।
द्रव्यं मौद्गलिकः पिण्डो बन्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ८१५ ॥
अर्थ - जो रागादि रूप है वह भावबन्ध है। वह जीव बन्ध भी माना गया है। ' द्रव्यबंध' इस पद में पड़ा हुआ जो द्रव्य शब्द है उसका अर्थ तो पुद्गल पिण्ड है अर्थात् कार्माण वर्गणायें हैं और बन्ध शब्द का अर्थ उनमें जो ज्ञानादि घातक कर्मत्व शक्ति है वह है । जिस प्रकार जीव में राग को भाव बन्ध कहते हैं उसी प्रकार मुद्गल में कर्मत्व शक्ति को बन्ध कहते हैं । यहाँ केवल कर्म रूप परिणत कार्माण वर्गणा लेनी हैं। आहारादि वर्गणाओं से कोई प्रयोजन नहीं है ।