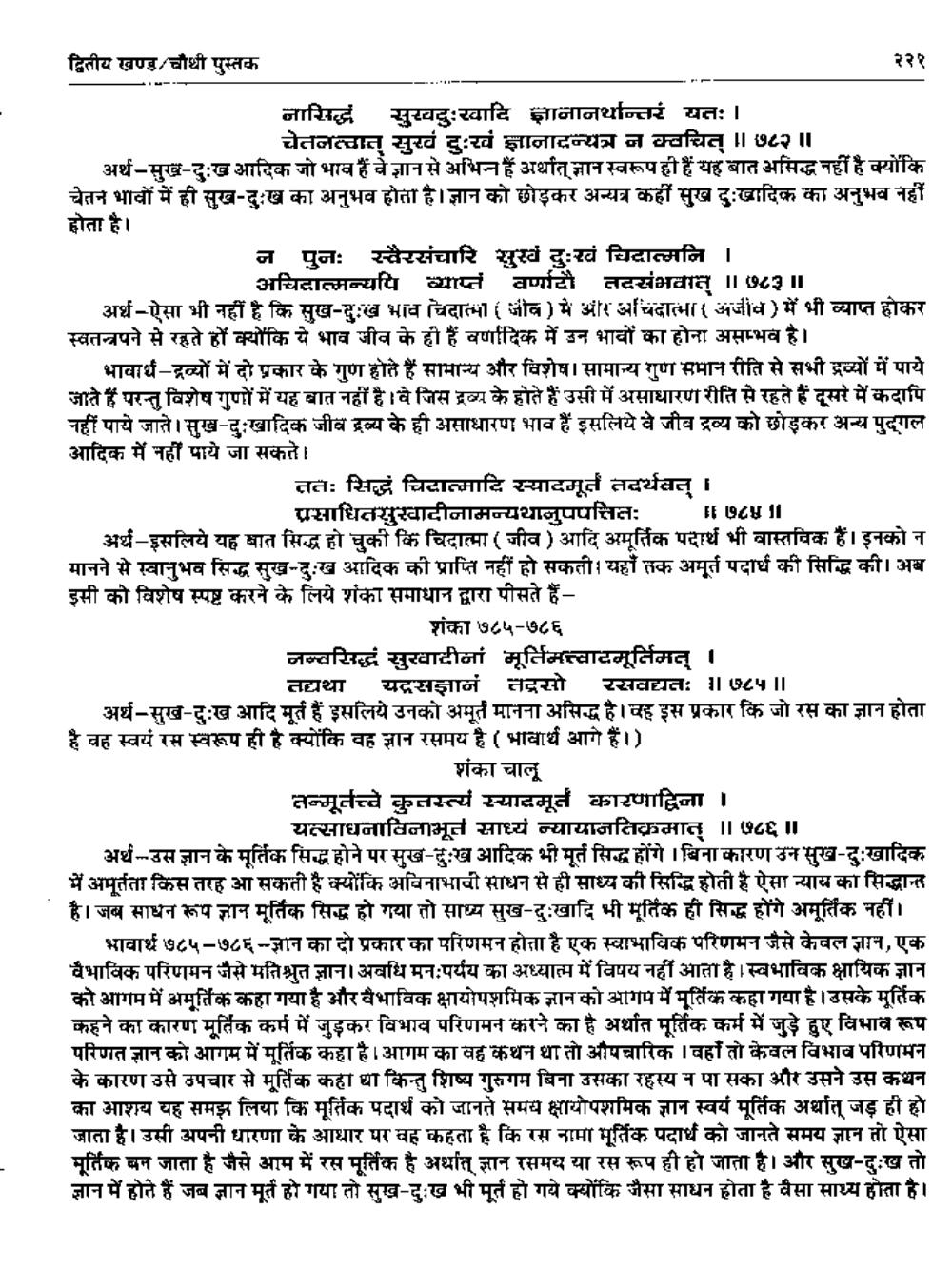________________
द्वितीय खण्ड /चौथी
पुस्तक
नासिद्धं सुखदुःखादि ज्ञानानर्थान्तरं यतः । चेतनत्वात् सुखं दुःखं ज्ञानादन्यत्र न क्वचित् ॥ ७८२ ॥ अर्थ- सुख-दुःख आदिक जो भाव हैं वे ज्ञान से अभिन्न हैं अर्थात् ज्ञान स्वरूप ही हैं यह बात असिद्ध नहीं है क्योंकि चेतन भावों में ही सुख-दुःख का अनुभव होता है। ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र कहीं सुख दुःखादिक का अनुभव नहीं होता है।
पुनः स्वैरसंचारि सुखं दुःखं चिदात्मनि । अचिदात्मन्यपि व्याप्तं वर्णादौ तदसंभवात् ॥ ७८३ ॥
२२१
न
अर्थ - ऐसा भी नहीं है कि सुख-दुःख भाव चिदात्मा (जीव) में और अचिदात्मा (अजीव) में भी व्याप्त होकर स्वतन्त्रपने से रहते हों क्योंकि ये भाव जीव के ही हैं वर्णादिक में उन भावों का होना असम्भव है।
भावार्थ- द्रव्यों में दो प्रकार के गुण होते हैं सामान्य और विशेष । सामान्य गुण समान रीति से सभी द्रव्यों में पाये जाते हैं परन्तु विशेष गुणों में यह बात नहीं है। वे जिस द्रव्य के होते हैं उसी में असाधारण रीति से रहते हैं दूसरे में कदापि नहीं पाये जाते । सुख-दुःखादिक जीव द्रव्य के ही असाधारण भाव हैं इसलिये वे जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य पुद्गल आदिक में नहीं पाये जा सकते।
ततः सिद्धं चिदात्मादि स्यादमूर्तं तदर्थवत् । प्रसाधितसुखादीनामन्यथानुपपत्तित:
७८४ 11
अर्थ - इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि चिदात्मा (जीव ) आदि अमूर्तिक पदार्थ भी वास्तविक हैं। इनको न मानने से स्वानुभव सिद्ध सुख-दुःख आदिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक अमूर्त पदार्थ की सिद्धि की। अब इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिये शंका समाधान द्वारा पीसते हैं
शंका ७८५-७८६
नवसिद्धं सुरवादीनां मूर्तिमत्त्वादमूर्तिमत् ।
तद्यथा यद्रसज्ञानं तद्रसो रसवद्यतः ॥ ७८५ ॥
अर्थ- सुख-दुःख आदि मूर्त हैं इसलिये उनको अमूर्त मानना असिद्ध है। वह इस प्रकार कि जो रस का ज्ञान होता है वह स्वयं रस स्वरूप ही है क्योंकि वह ज्ञान रसमय है ( भावार्थ आगे हैं। )
शंका चालू
तन्मूर्तच्वे कुतस्त्यं स्यादमूर्त कारणाद्विना । यत्साधनाविनाभूतं साध्यं न्यायानतिक्रमात् ॥ ७८६ ॥
अर्थ -- उस ज्ञान के मूर्तिक सिद्ध होने पर सुख-दुःख आदिक भी मूर्त सिद्ध होंगे। बिना कारण उन सुख-दुःखादिक मैं अमूर्तता किस तरह आ सकती है क्योंकि अविनाभावी साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है ऐसा न्याय का सिद्धान्त है। जब साधन रूप ज्ञान मूर्तिक सिद्ध हो गया तो साध्य सुख-दुःखादि भी मूर्तिक ही सिद्ध होंगे अमूर्तिक नहीं।
भावार्थ ७८५ - ७८६ - ज्ञान का दो प्रकार का परिणमन होता है एक स्वाभाविक परिणमन जैसे केवल ज्ञान, एक वैभाविक परिणमन जैसे मतिश्रुत ज्ञान । अवधि मन:पर्यय का अध्यात्म में विषय नहीं आता है। स्वभाविक क्षायिक ज्ञान को आगम में अमूर्तिक कहा गया है और वैभाविक क्षायोपशमिक ज्ञान को आगम में मूर्तिक कहा गया है। उसके मूर्तिक कहने का कारण मूर्तिक कर्म में जुड़कर विभाव परिणमन करने का है अर्थात मूर्तिक कर्म में जुड़े हुए विभाव रूप परिणत ज्ञान को आगम में मूर्तिक कहा है। आगम का वह कथन था तो औपचारिक । वहाँ तो केवल विभाव परिणमन के कारण उसे उपचार से मूर्तिक कहा था किन्तु शिष्य गुरुगम बिना उसका रहस्य न पा सका और उसने उस कथन का आशय यह समझ लिया कि मूर्तिक पदार्थ को जानते समय क्षायोपशमिक ज्ञान स्वयं मूर्तिक अर्थात् जड़ ही हो जाता है। उसी अपनी धारणा के आधार पर वह कहता है कि रस नामा मूर्तिक पदार्थ को जानते समय ज्ञान तो ऐसा मूर्तिक बन जाता है जैसे आम में रस मूर्तिक है अर्थात् ज्ञान रसमय या रस रूप ही हो जाता है। और सुख-दुःख तो ज्ञान में होते हैं जब ज्ञान मूर्त हो गया तो सुख-दुःख भी मूर्त हो गये क्योंकि जैसा साधन होता है वैसा साध्य होता है।