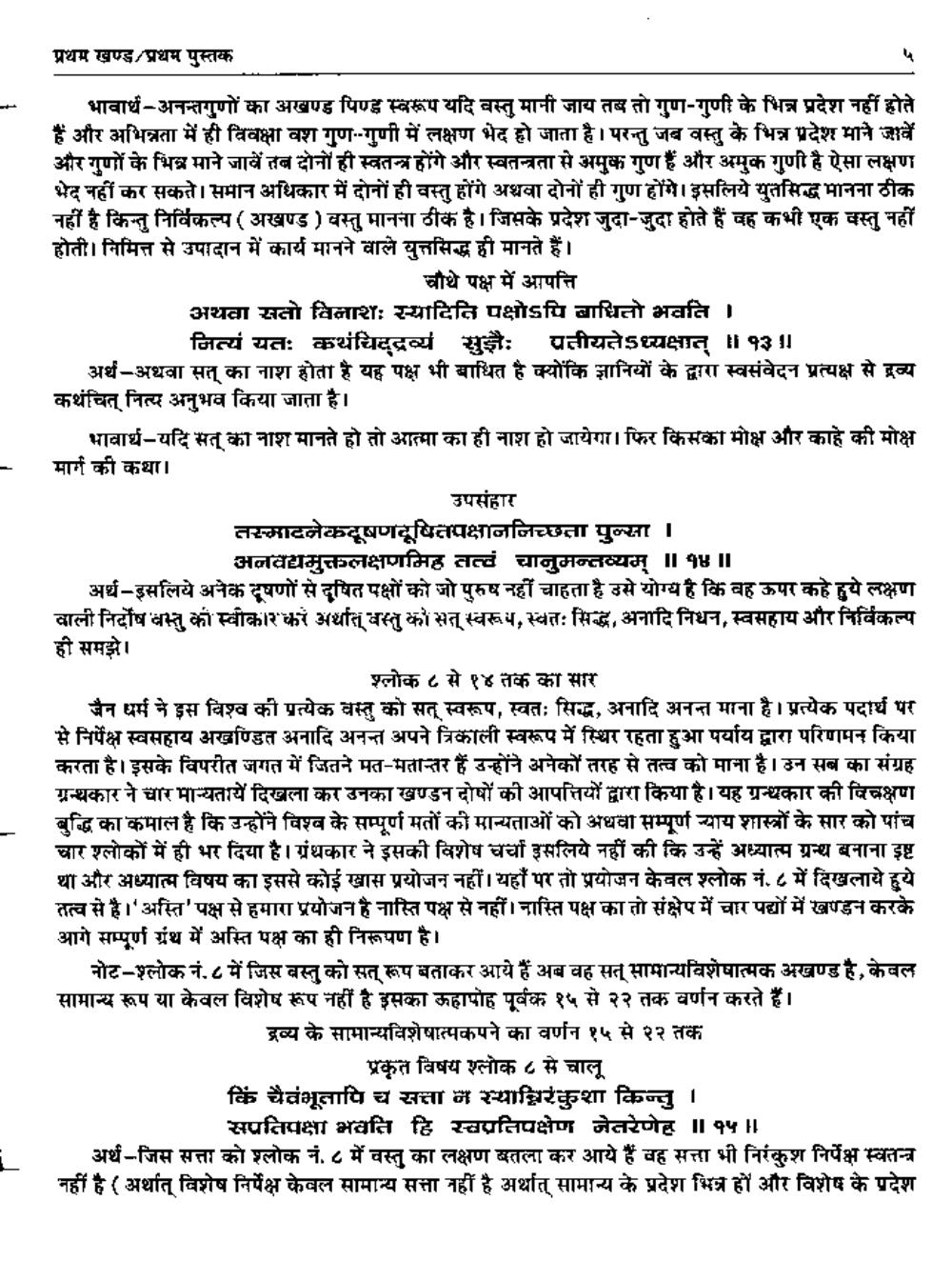________________
प्रथम खण्ड/प्रथम पुस्तक
भावार्थ-अनन्तगुणों का अखण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी जाय तब तो गुण-गुणी के भिन्न प्रदेश नहीं होते हैं और अभिन्नता में ही विवक्षा वश गुण-गुणी में लक्षण भेद हो जाता है। परन्तु जब वस्तु के भिन्न प्रदेश माने जावें और गुणों के भित्र माने जावें तब दोनों ही स्वतन्त्र होंगे और स्वतन्त्रता से अमुक गुण हैं और अमुक गुणी है ऐसा लक्षण भेद नहीं कर सकते। समान अधिकार में दोनों ही वस्तु होंगे अथवा दोनों ही गुण होंगे। इसलिये युतसिद्ध मानना ठीक नहीं है किन्तु निर्विकल्प ( अखण्ड ) वस्तु मानना ठीक है। जिसके प्रदेश जुदा-जुदा होते हैं वह कभी एक वस्तु नहीं होती। निमित्त से उपादान में कार्य मानने वाले युत्तसिद्ध ही मानते हैं।
चौथे पक्ष में आपत्ति अथवा सतो विलाश: स्यादिति पक्षोऽपि बाधितो भवति ।
नित्यं यतः कथंचिद्रव्यं सुझैः पतीयतेऽध्यक्षात् ॥ १३॥ अर्थ-अथवा सत् का नाश होता है यह पक्ष भी बाधित है क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से द्रव्य कथंचित् नित्य अनुभव किया जाता है।
भावार्थ-यदि सत्का नाश मानते हो तो आत्मा का ही नाश हो जायेगा। फिर किसका मोक्ष और काहे की मोक्ष मार्ग की कथा।
उपसंहार तस्माटनेकदूषणदूषितपक्षाननिच्छता पुल्सा ।
अनवद्यमुक्तलक्षणमिह तत्वं चानुमन्तव्यम् ॥ १४ ॥ अर्थ-इसलिये अनेक दूषणों से दृषित पक्षों को जो पुरुष नहीं चाहता है उसे योग्य है कि वह ऊपर कहे हुये लक्षण वाली निर्दोष वस्तु की स्वीकार कर अर्थात् वस्तु को सत् स्वरूप, स्वत: सिद्ध, अनादि निधन, स्वसहाय और निर्विकल्प ही समझे।
श्लोक८ से १४ तक का सार जैन धर्म ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को सत् स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि अनन्त माना है। प्रत्येक पदार्थ पर से निर्पेक्ष स्वसहाय अखण्डित अनादि अनन्त अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ पर्याय द्वारा परिणमन किया करता है। इसके विपरीत जगत में जितने मत-मतान्तर हैं उन्होंने अनेकों तरह से तत्व को माना है। उन सब का संग्रह ग्रन्थकार ने चार मान्यतायें दिखला कर उनका खण्डन दोषों की आपत्तियों द्वारा किया है। यह ग्रन्थकार की विचक्षण बुद्धि का कमाल है कि उन्होंने विश्व के सम्पूर्ण मतों की मान्यताओं को अधवा सम्पूर्ण व्याय शास्त्रों के सार को पांच चार श्लोकों में ही भर दिया है। ग्रंथकार ने इसकी विशेष चर्चा इसलिये नहीं की कि उन्हें अध्यात्म ग्रन्थ बनाना इष्ट था और अध्यात्म विषय का इससे कोई खास प्रयोजन नहीं। यहाँ पर तो प्रयोजन केवल श्लोक नं.८ में दिखलाये हुये तत्व से है। अस्ति' पक्ष से हमारा प्रयोजन है नास्ति पक्ष से नहीं। नास्ति पक्ष का तो संक्षेप में चार पद्यों में खण्डन करके आगे सम्पूर्ण ग्रंथ में अस्ति पक्ष का ही निरूपण है।
नोट-श्लोक नं.८ में जिस वस्तु को सत् रूप बताकर आये हैं अब वह सत् सामान्यविशेषात्मक अखण्ड है, केवल सामान्य रूप या केवल विशेष रूप नहीं है इसका ऊहापोह पूर्वक १५ से २२ तक वर्णन करते हैं।
द्रव्य के सामान्यविशेषात्मकपने का वर्णन १५ से २२ तक
प्रकृत विषय श्लोक ८ से चालू किं चैवंभूतापि च सत्ता न स्थानिरंकुशा किन्तु ।
सपतिपक्षा भवति हि स्वप्रतिपक्षेण जेतरेणेह ॥ १५ ॥ अर्थ-जिस सत्ता को श्लोक नं.८ में वस्तु का लक्षण बतला कर आये हैं वह सत्ता भी निरंकुश निर्पेक्ष स्वतन्त्र नहीं है ( अर्थात् विशेष निर्पेक्ष केवल सामान्य सत्ता नहीं है अर्थात् सामान्य के प्रदेश भित्र हों और विशेष के प्रदेश