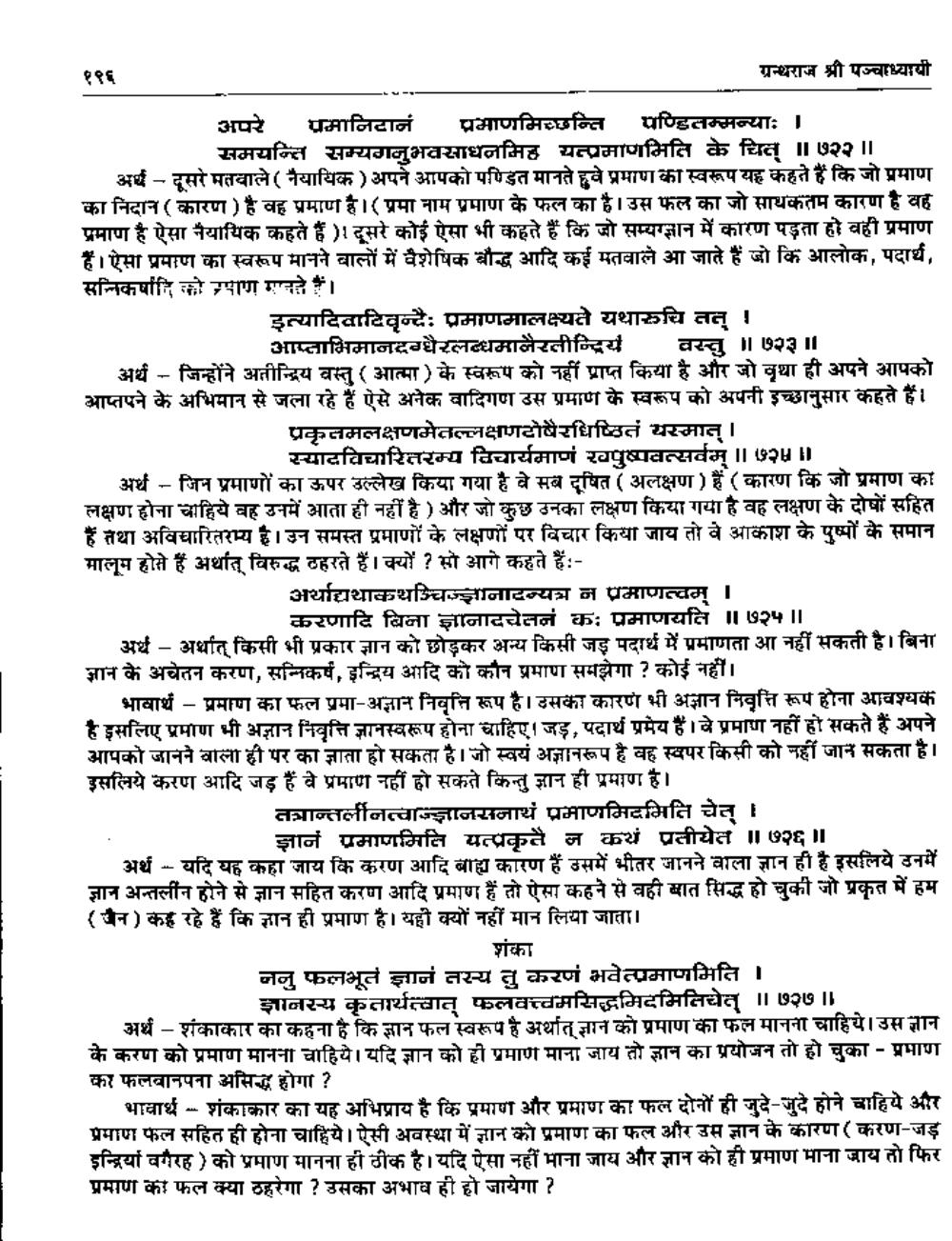________________
१९६
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
अपरे
प्रमानिदानं प्रभाणमिच्छन्ति पण्डितम्मन्याः । समयन्ति सम्यगनुभवसाधनमिह यत्प्रमाणमिति के चित् ॥ ७२२ ॥ अर्थ- दूसरे मतवाले ( नैयायिक) अपने आपको पण्डित मानते हुवे प्रमाण का स्वरूप यह कहते हैं कि जो प्रमाण का निदान (कारण) है वह प्रमाण है। (प्रमा नाम प्रमाण के फल का है। उस फल का जो साधकतम कारण है वह प्रमाण है ऐसा नैयायिक कहते हैं ) दूसरे कोई ऐसा भी कहते हैं कि जो सम्यग्ज्ञान में कारण पड़ता हो वही प्रमाण हैं। ऐसा प्रमाण का स्वरूप मानने वालों में वैशेषिक बौद्ध आदि कई मतवाले आ जाते हैं जो कि आलोक, पदार्थ, सन्निकर्षादि कोणते हैं।
इत्यादिवादिवृन्दैः प्रमाणमालक्ष्यते यथारुचि तत् ।
आप्ताभिमानदग्धैरलब्धमानैरतीन्द्रियं
वस्तु ॥ ७२३ ॥
अर्थ- जिन्होंने अतीन्द्रिय वस्तु (आत्मा) के स्वरूप को नहीं प्राप्त किया है और जो वृथा ही अपने आपको आप्तपने के अभिमान से जला रहे हैं ऐसे अनेक वादिगण उस प्रमाण के स्वरूप को अपनी इच्छानुसार कहते हैं । प्रकृतमलक्षणमेतल्लक्षणदोषैरधिष्ठितं यस्मात् ।
स्यादविचारितरम्य विचार्यमाणं वपुष्पवत्सर्वम् ॥ ७२॥ ॥
अर्थ - जिन प्रमाणों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे सब दूषित (अलक्षण ) हैं ( कारण कि जो प्रमाण का लक्षण होना चाहिये वह उनमें आता ही नहीं है) और जो कुछ उनका लक्षण किया गया है वह लक्षण के दोषों सहित हैं तथा अविचारितरम्य है। उन समस्त प्रमाणों के लक्षणों पर विचार किया जाय तो वे आकाश के पुष्पों के समान मालूम होते हैं अर्थात् विरुद्ध ठहरते हैं। क्यों ? सो आगे कहते हैं:
अर्थाद्यथाकथञ्चिज्ज्ञानादन्यत्र न प्रमाणत्वम् I
करणादि बिना ज्ञानादचेतनं कः प्रमाणयति ॥ ७२५ ॥
अर्थ - अर्थात् किसी भी प्रकार ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी जड़ पदार्थ में प्रमाणता आ नहीं सकती है। बिना ज्ञान के अचेतन करण, सन्निकर्ष, इन्द्रिय आदि को कौन प्रमाण समझेगा ? कोई नहीं ।
भावार्थं 1- प्रमाण का फल प्रमा-अज्ञान निवृत्ति रूप है। उसका कारण भी अज्ञान निवृत्ति रूप होना आवश्यक है इसलिए प्रमाण भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप होना चाहिए। जड़, पदार्थ प्रमेय हैं। वे प्रमाण नहीं हो सकते हैं अपने आपको जानने वाला ही पर का ज्ञाता हो सकता है। जो स्वयं अज्ञानरूप है वह स्वपर किसी को नहीं जान सकता है। इसलिये करण आदि जड़ हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है।
तत्रान्तर्लीनत्वाज्ज्ञानसनाथं प्रमाणमिदमिति चेत् ।
ज्ञानं प्रमाणमिति यत्प्रकृतै न कथं प्रतीयेत ॥ ७२६ ॥
अर्थ - यदि यह कहा जाय कि करण आदि बाह्य कारण हैं उसमें भीतर जानने वाला ज्ञान ही है इसलिये उनमें ज्ञान अन्तलींन होने से ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण हैं तो ऐसा कहने से वही बात सिद्ध हो चुकी जो प्रकृत में हम (जैन) कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रमाण है। यही क्यों नहीं मान लिया जाता।
शंका
ननु फलभूतं ज्ञानं तस्य तु करणं भवेत्प्रमाणमिति ।
ज्ञानस्य कृतार्थत्वात् फलवत्त्वमसिद्धमिदमितिचेत् ॥ ७२७ ॥
अर्थ - शंकाकार का कहना है कि ज्ञान फल स्वरूप है अर्थात् ज्ञान को प्रमाण का फल मानना चाहिये। उस ज्ञान के करण को प्रमाण मानना चाहिये। यदि ज्ञान को ही प्रमाण माना जाय तो ज्ञान का प्रयोजन तो हो चुका प्रमाण कर फलवानपना असिद्ध होगा ?
-
भावार्थ - शंकाकार का यह अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाण का फल दोनों ही जुदे जुदे होने चाहिये और प्रमाण फल सहित ही होना चाहिये। ऐसी अवस्था में ज्ञान को प्रमाण का फल और उस ज्ञान के कारण (करण - जड़ इन्द्रिय वगैरह ) को प्रमाण मानना ही ठीक है। यदि ऐसा नहीं माना जाय और ज्ञान को ही प्रमाण माना जाय तो फिर प्रमाण का फल क्या ठहरेगा ? उसका अभाव ही हो जायेगा ?