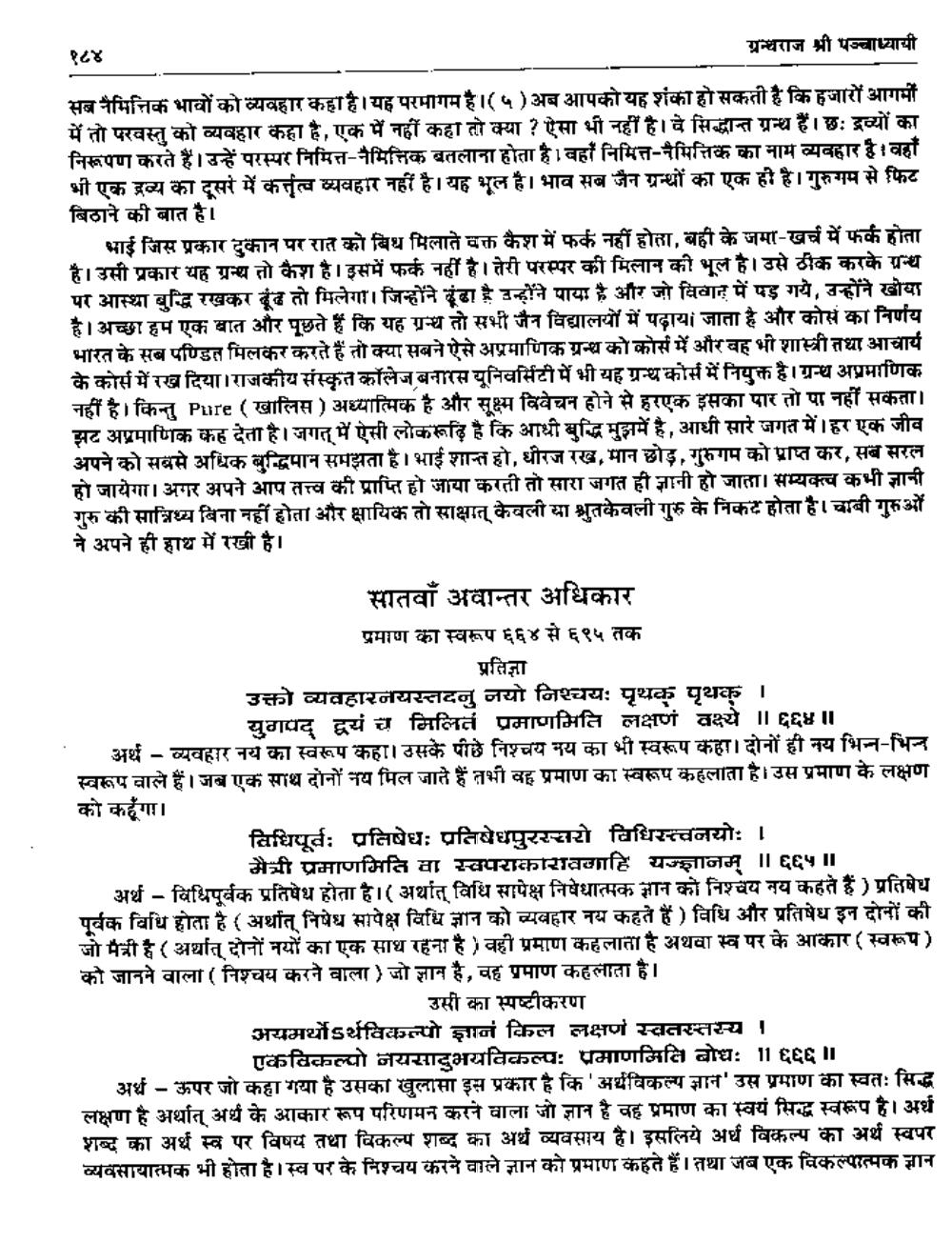________________
१८४
ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी
सब नैमित्तिक भावों को व्यवहार कहा है। यह परमागम है।(५) अब आपको यह शंका हो सकती है कि हजारों आगमों में तो परवस्तु को व्यवहार कहा है, एक में नहीं कहा तो क्या? ऐसा भी नहीं है। वे सिद्धान्त ग्रन्थ हैं। छः द्रव्यों का निरूपण करते हैं। उन्हें परस्पर निमित्त-नैमित्तिक बतलाना होता है। वहाँ निमित्त-नैमित्तिक का माम व्यवहार है। वहाँ भी एक द्रव्य का दूसरे में कर्तृत्व व्यवहार नहीं है। यह भूल है। भाव सब जैन ग्रन्थों का एक ही है। गुरुगम से फिट बिठाने की बात है।
भाई जिस प्रकार दुकान पर रात को बिध मिलाते वक्त कैश में फर्क नहीं होता, बही के जमा-खर्च में फर्क होता है। उसी प्रकार यह ग्रन्थ तो कैश है। इसमें फर्क नहीं है। तेरी परस्पर की मिलान की भूल है। उसे ठीक करके ग्रन्थ पर आस्था बुद्धि रखकर दूंट तो मिलेगा। जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने पाया है और जो विवाद में पड़ गये, उन्होंने खोया है। अच्छा हम एक बात और पूछते हैं कि यह ग्रन्थ तो सभी जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और कोसे का निर्णय भारत के सब पण्डित मिलकर करते हैं तो क्या सबने ऐसे अप्रमाणिक ग्रन्धको कोर्स में और वह भी शास्त्री तथा आचार्य के कोर्स में रख दिया।राजकीय संस्कृत कॉलेज बनारस यूनिवर्सिटी में भी यह ग्रन्थ कोर्स में नियुक्त है। ग्रन्थ अप्रमाणिक नहीं है। किन्तु Pure (खालिस) अध्यात्मिक है और सूक्ष्म विवेचन होने से हरएक इसका पार तो पा नहीं सकता। झट अप्रमाणिक कह देता है। जगत् में ऐसी लोकरूढ़ि है कि आधी बुद्धि मुझमें है, आधी सारे जगत में। हर एक जीव अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है। भाई शान्त हो, धीरज रख,मान छोड़, गुरुगम को प्राप्त कर, सब सरल हो जायेगा। अगर अपने आप तत्त्व की प्राप्ति हो जाया करती तो सारा जगत ही ज्ञानी हो जाता। सम्यक्त्व कभी ज्ञानी गुरु की सानिध्य बिना नहीं होता और क्षायिक तो साक्षात् केबली या श्रुतकेवली गुरु के निकट होता है। चाबी गुरुओं ने अपने ही हाथ में रखी है।
सातवाँ अवान्तर अधिकार प्रमाण का स्वरूप ६६४ से ६९५ तक
प्रतिज्ञा उक्तो व्यवहारनयस्तदनु जयो निश्चयः पृथक पृथक ।
युगपद् द्वयं च मिलितं प्रमाणमिति लक्षणं वक्ष्ये ॥ ६६४ ।। अर्थ - व्यवहार नय का स्वरूप कहा। उसके पीछे निश्चय नय का भी स्वरूप कहा। दोनों ही नय भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले हैं। जब एक साथ दोनों नय मिल जाते हैं तभी वह प्रमाण का स्वरूप कहलाता है। उस प्रमाण के लक्षण को कहूँगा।
विधिपूर्वः प्रतिषेधः प्रतिषेधपुररसरो विधिस्स्वनयोः ।
मैत्री प्रमाणमिति वा स्वपराकारावगाहि यज्ज्ञानम् ॥ ६६५ ॥ अर्थ - विधिपूर्वक प्रतिषेध होता है। ( अर्थात् विधि सापेक्ष निषेधात्मक ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं) प्रतिषेध पूर्वक विधि होता है ( अर्थात् निषेध सापेक्ष विधि ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं ) विधि और प्रतिषेध इन दोनों की जो मैत्री है (अर्थात् दोनों नयों का एक साथ रहना है वही प्रमाण कहलाता है अथवा स्व पर के आकार (स्वरूप) को जानने वाला (निश्चय करने वाला) जो ज्ञान है, वह प्रमाण कहलाता है।
उसी का स्पष्टीकरण अयमर्थोऽर्थविकल्पो ज्ञानं किल लक्षणं स्वतस्तस्य ।
एकविकल्पो नयसाभयविकल्पः प्रमाणमिति बोधः 11 Ece| अर्थ - ऊपर जो कहा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है कि 'अर्थविकल्प ज्ञान' उस प्रमाण का स्वतः सिद्ध लक्षण है अर्थात् अर्थ के आकार रूप परिणमन करने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण का स्वयं सिद्ध स्वरूप है। अर्थ शब्द का अर्थ स्व पर विषय तथा विकल्प शब्द का अर्थ व्यवसाय है। इसलिये अर्थ विकल्प का अर्थ स्वपर व्यवसायात्मक भी होता है। स्व पर के निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तथा जब एक विकल्पात्मक ज्ञान