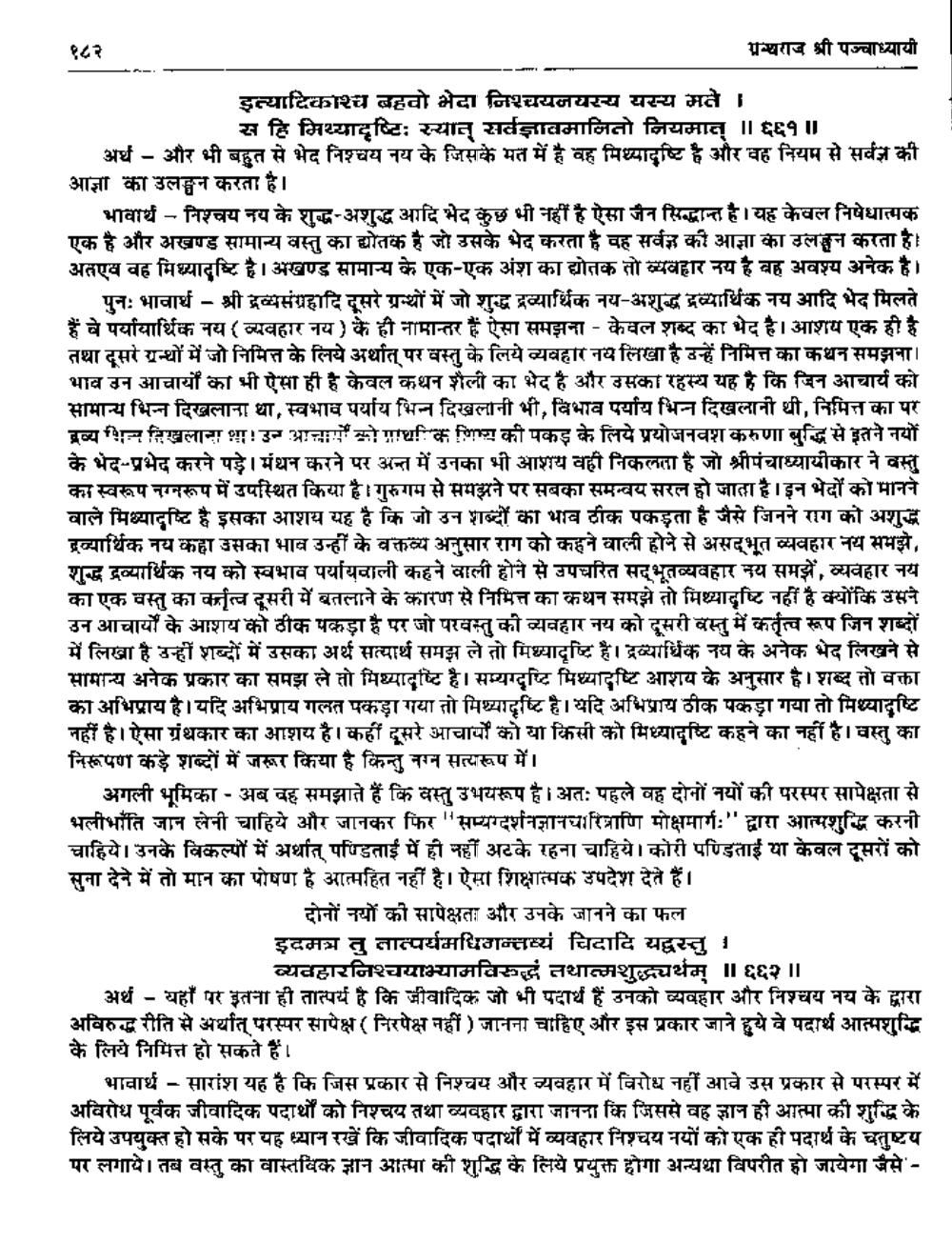________________
प्रस्थराज श्री पञ्चाध्यायी
इत्यादिकाश्च बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मते ।
स हि मिथ्यादष्टिः स्यात सर्वज्ञावमानितो नियमात ||६९१॥ अर्थ - और भी बहुत से भेद निश्चय नय के जिसके मत में है वह मिथ्यादृष्टि है और वह नियम से सर्वज्ञ की आज्ञा का उलङ्घन करता है।
भावार्थ-निश्चय नय के शुद्ध-अशुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं है ऐसा जैन सिद्धान्त है। यह केवल निषेधात्मक एक है और अखण्ड सामान्य वस्तु का द्योतक है जो उसके भेद करता है वह सर्वज्ञ की आज्ञा का उलान करता है। अतएव वह मिध्यादृष्टि है। अखण्ड सामान्य के एक-एक अंश का द्योतक तो व्यवहार नय है वह अवश्य अनेक है।
पुनः भावार्थ - श्री द्रव्यसंग्रहादि दूसरे ग्रन्थों में जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय-अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय आदि भेद मिलते हैं वे पर्यायार्थिक नय ( व्यवहार नय) के ही नामान्तर हैं ऐसा समझना - केवल शब्द का भेद है। आशय एक ही है तथा दूसरे ग्रन्थों में जो निमित्त के लिये अर्थात् पर वस्तु के लिये व्यवहार नय लिखा है उन्हें निमित्त का कथन समझना। भाव उन आचार्यों का भी ऐसा ही है केवल कथन शैली का भेद है और उसका रहस्य यह है कि जिन आचार्य को सामान्य भिन्न दिखलाना था,स्वभाव पर्याय भिन दिखलानी भी, विभाव पर्याय भिन दिखलानी थी, निमित्त का पर द्रव्य पिन दिखलाना शा! उन आया कोपाकिणिय की पकड़ के लिये प्रयोजनवशकरुणा बुद्धि से इतने नयों के भेद-प्रभेद करने पड़े। मंथन करने पर अन्त में उनका भी आशय वही निकलता है जो श्रीपंचाध्यायीकार ने वस्तु का स्वरूप नग्नरूप में उपस्थित किया है। गुरुगम से समझने पर सबका समन्वय सरल हो जाता है। इन भेदों को मानने वाले मिथ्यावृष्टि है इसका आशय यह है कि जो उन शब्दों का भाव ठीक पकड़ता है जैसे जिनने राग को अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा उसका भाव उन्हीं के वक्तव्य अनुसार राग को कहने वाली होने से असद्भुत व्यवहार नय समझे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को स्वभाव पर्यायवाली कहने वाली होने से उपचरित सद्भूतव्यवहार नय समझें, व्यवहार नय का एक वस्तु का कर्तत्व दूसरी में बतलाने के कारण से निमित्त का कथन समझे तो मिथ्यादष्टि नहीं है क्योंकि उसने उन आचार्यों के आशय को ठीक पकड़ा है पर जो परवस्तु की व्यवहार नय को दूसरी वस्तु में कर्तृत्व रूप जिन शब्दों में लिखा है उन्हीं शब्दों में उसका अर्थ सत्यार्थ समझ ले तो मिथ्यादृष्टि है। द्रव्यार्थिक नय के अनेक भेद लिखने से सामान्य अनेक प्रकार का समझ ले तो मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि आशय के अनुसार है। शब्द तो वक्ता का अभिप्राय है। यदि अभिप्राय गलत पकड़ा गया तो मिथ्याष्टि है। यदि अभिप्राय ठीक पकड़ा गया तो मिथ्याष्टि नहीं है। ऐसा ग्रंथकार का आशय है। कहीं दूसरे आचार्यों को या किसी को मिध्यादृष्टि कहने का नहीं है। वस्तु का निरूपण कड़े शब्दों में जरूर किया है किन्तु नग्न सत्यारूप में। __अगली भूमिका - अब वह समझाते हैं कि वस्तु उभयरूप है। अत: पहले वह दोनों नयों की परस्पर सापेक्षता से भलीभाँति जान लेनी चाहिये और जानकर फिर "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" द्वारा आत्मशुद्धि करनी चाहिये। उनके विकल्पों में अर्थात् पण्डिताई में ही नहीं अटके रहना चाहिये। कोरी पण्डिताई या केवल दूसरों को सुना देने में तो मान का पोषण है आत्महित नहीं है। ऐसा शिक्षात्मक उपदेश देते हैं।
दोनों नयों की सापेक्षता और उनके जानने का फल इदमन तु तात्पर्यमधिगन्तव्यं चिदादि यद्वस्तु ।
व्यवहारनिश्चयाभ्यामविरुद्धं तथात्मशुद्धयर्थम् ॥ ६६२॥ अर्थ - यहाँ पर इतना ही तात्पर्य है कि जीवादिक जो भी पदार्थ हैं उनको व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा अविरुद्ध रीति से अर्थात् परस्पर सापेक्ष (निरपेक्ष नहीं) जानना चाहिए और इस प्रकार जाने हुये वे पदार्थ आत्मशुद्धि के लिये निमित्त हो सकते हैं।
भावार्थ - सारांश यह है कि जिस प्रकार से निश्चय और व्यवहार में विरोध नहीं आवे उस प्रकार से परस्पर में अविरोध पूर्वक जीवादिक पदार्थों को निश्चय तथा व्यवहार द्वारा जानना कि जिससे वह ज्ञान ही आत्मा की शुद्धि के लिये उपयुक्त हो सके पर यह ध्यान रखें कि जीवादिक पदार्थों में व्यवहार निश्चय नयों को एक ही पदार्थ के चतुष्टय पर लगाये। तब वस्तु का वास्तविक ज्ञान आत्मा की शद्धि के लिये प्रयुक्त होगा अन्यथा विपरीत हो जायेगा जैसे