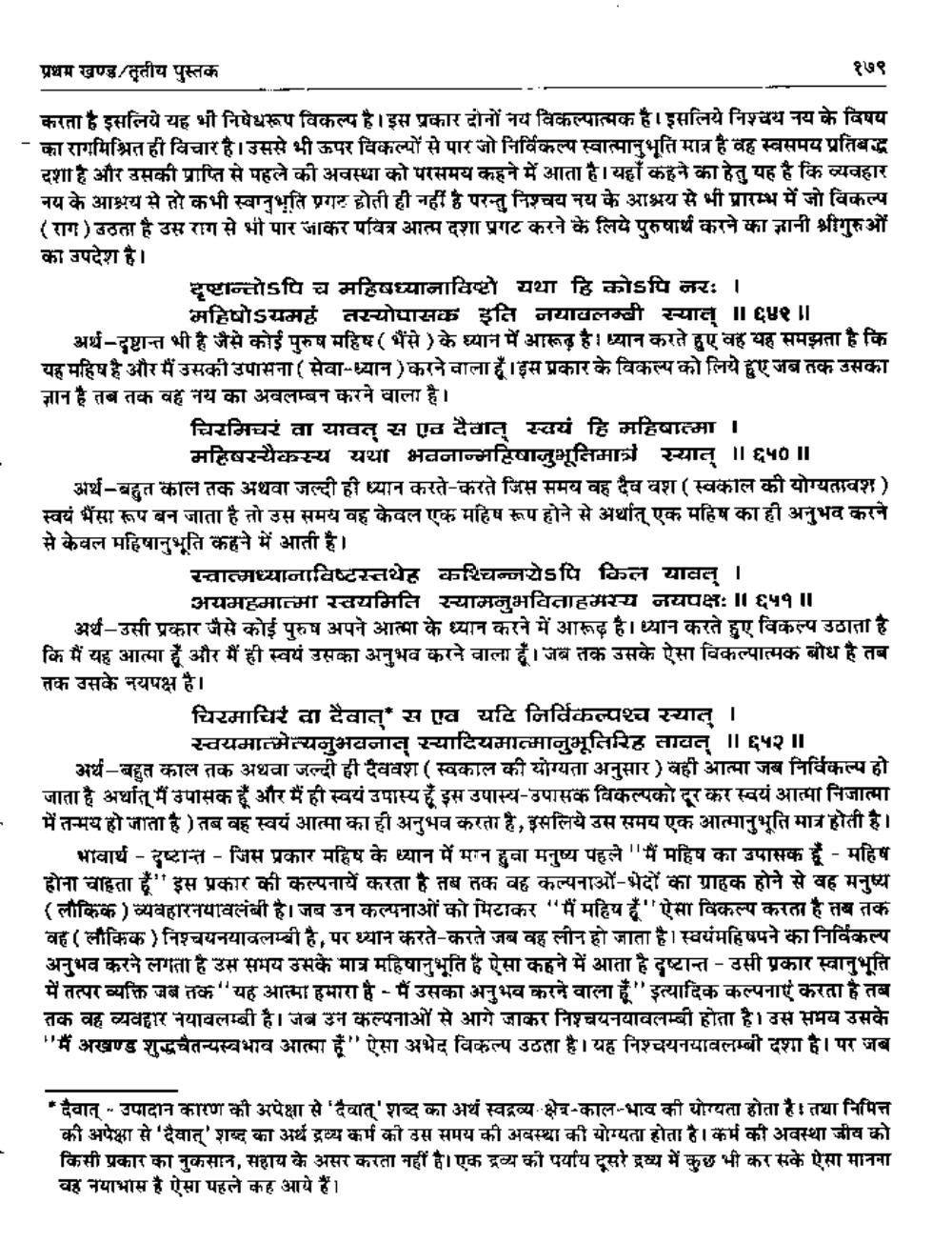________________
प्रथम खण्ड/तृतीय पुस्तक
१७९
करता है इसलिये यह भी निषेधरूप विकल्प है। इस प्रकार दोनों नय विकल्पात्मक है। इसलिये निश्चय नय के विषय का रागमिश्रितही विचार है। उससे भी ऊपर विकल्पों से पार जो निर्विकल्प स्वात्मानुभूति मात्र है वह स्वसमय प्रतिबद्ध दशा है और उसकी प्राप्ति से पहले की अवस्था को परसमय कहने में आता है। यहाँ कहने का हेतु यह है कि व्यवहार नय के आभय से तो कभी स्वानुभति प्रगट होती ही नहीं है परन्तु निश्चय नय के आश्रय से भी प्रारम्भ में जो विकल्प (राग) उठता है उस राग से भी पार जाकर पवित्र आत्म दशा प्रगट करने के लिये पुरुषार्थ करने का ज्ञानी श्रीगुरूओं का उपदेश है।
दृष्टान्तोऽपि च महिषध्यानाविष्टो यथा हि कोऽपि नरः ।
महिषोऽयमहं तस्योपासक इति नयावलम्बी स्यात् ॥ ६५९॥ अर्थ-दृष्टान्त भी है जैसे कोई पुरुष महिष (भैंसे ) के ध्यान में आरूढ़ है। ध्यान करते हुए वह यह समझता है कि यह महिष है और मैं उसकी उपासना ( सेवा-ध्यान ) करने वाला हूँ। इस प्रकार के विकल्प को लिये हुए जब तक उसका ज्ञान है तब तक वह नय का अवलम्बन करने वाला है।
चिरमिचरं ता यावत् स एन दैवात् स्वयं हि महिषात्मा ।
महिषस्यैकस्य यथा भवनान्महिषानुभूतिमात्र स्यात् ॥६५० ॥ अर्थ-बहुत काल तक अथवा जल्दी ही ध्यान करते-करते जिस समय वह देव वश (स्वकाल की योग्यतावश) स्वयं भैंसा रूप बन जाता है तो उस समय वह केवल एक महिष रूप होने से अर्थात् एक महिष काही अनुभव करने से केवल महिषानुभूति कहने में आती है।
रत्रात्मध्यानाविष्टस्तथेह कश्चिन्नरोऽपि किल यावत् ।
अयमहमात्मा रतयमिति स्यामनुभविताहमरय नयपक्षः।। ६५१।। अर्थ-उसी प्रकार जैसे कोई पुरुष अपने आत्मा के ध्यान करने में आरूढ़ है। ध्यान करते हुए विकल्प उठाता है कि मैं यह आत्मा हूँ और मैं ही स्वयं उसका अनुभव करने वाला हूँ। जब तक उसके ऐसा विकल्पात्मक बोध है तब तक उसके नयपक्ष है।
चिरमाचिर वा दैवात् स एव यदि निर्विकल्पश्च स्यात् ।
स्वयमात्मेत्यनुभवनात् स्यादियमात्मानुभूतिरिह तावत् ॥ ६५२ ॥
काल तक अथवा जल्दी ही दैववश (स्वकाल की योग्यता अनुसार) वही आत्मा जब निर्विकल्प हो जाता है अर्थात् मैं उपासक हैं और मैं ही स्वयं उपास्य हूँ इस उपास्य-उपासक विकल्पको दूर कर स्वयं आत्मा निजात्मा में तन्मय हो जाता है ) तब वह स्वयं आत्मा का ही अनुभव करता है, इसलिये उस समय एक आत्मानुभूति मात्र होती है।
भावार्थ - दृष्टान्त - जिस प्रकार महिष के ध्यान में मान हुवा मनुष्य पहले "मैं महिष का उपासक हूँ - महिष होना चाहता हैं" इस प्रकार की कल्पनायें करता है तब तक वह कल्पनाओं-भेदों का ग्राहक होने से वह मनुष्य (लौकिक) व्यवहारनयावलंबी है। जब उन कल्पनाओं को मिटाकर "मैं महिय हूँ"ऐसा विकल्प करता है तब तक वह ( लौकिक )निश्चयनयावलम्बी है, पर ध्यान करते-करते जब वह लीन हो जाता है। स्वयंमहिषपने का निर्विकल्प अनुभव करने लगता है उस समय उसके मात्र महिषानुभूति है ऐसा कहने में आता है दृष्टान्त - उसी प्रकार स्वानुभूति में तत्पर व्यक्ति जब तक "यह आत्मा हमारा है - मैं उसका अनुभव करने वाला हूँ" इत्यादिक कल्पनाएं करता है तब तक वह व्यवहार नयावलम्बी है। जब उन कल्पनाओं से आगे जाकर निश्चयनयावलम्बी होता है। उस समय उसके "मैं अखण्ड शुद्धचैतन्यस्वभाव आत्मा हूँ" ऐसा अभेद विकल्प उठता है। यह निश्चयनयावलम्बी दशा है। पर जब
*दैवात् - उपादान कारण की अपेक्षा से 'दैवात्'शब्द का अर्थ स्वगव्य क्षेत्र-काल-भाव की योग्यता होता है। तथा निमित्त
की अपेक्षा से 'दैवात्' शब्द का अर्थ द्रव्य कर्म की उस समय की अवस्था की योग्यता होता है। कर्म की अवस्था जीव को किसी प्रकार का नुकसान, सहाय के असर करता नहीं है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रष्य में कुछ भी कर सके ऐसा मानना वह नयाभास है ऐसा पहले कह आये हैं।