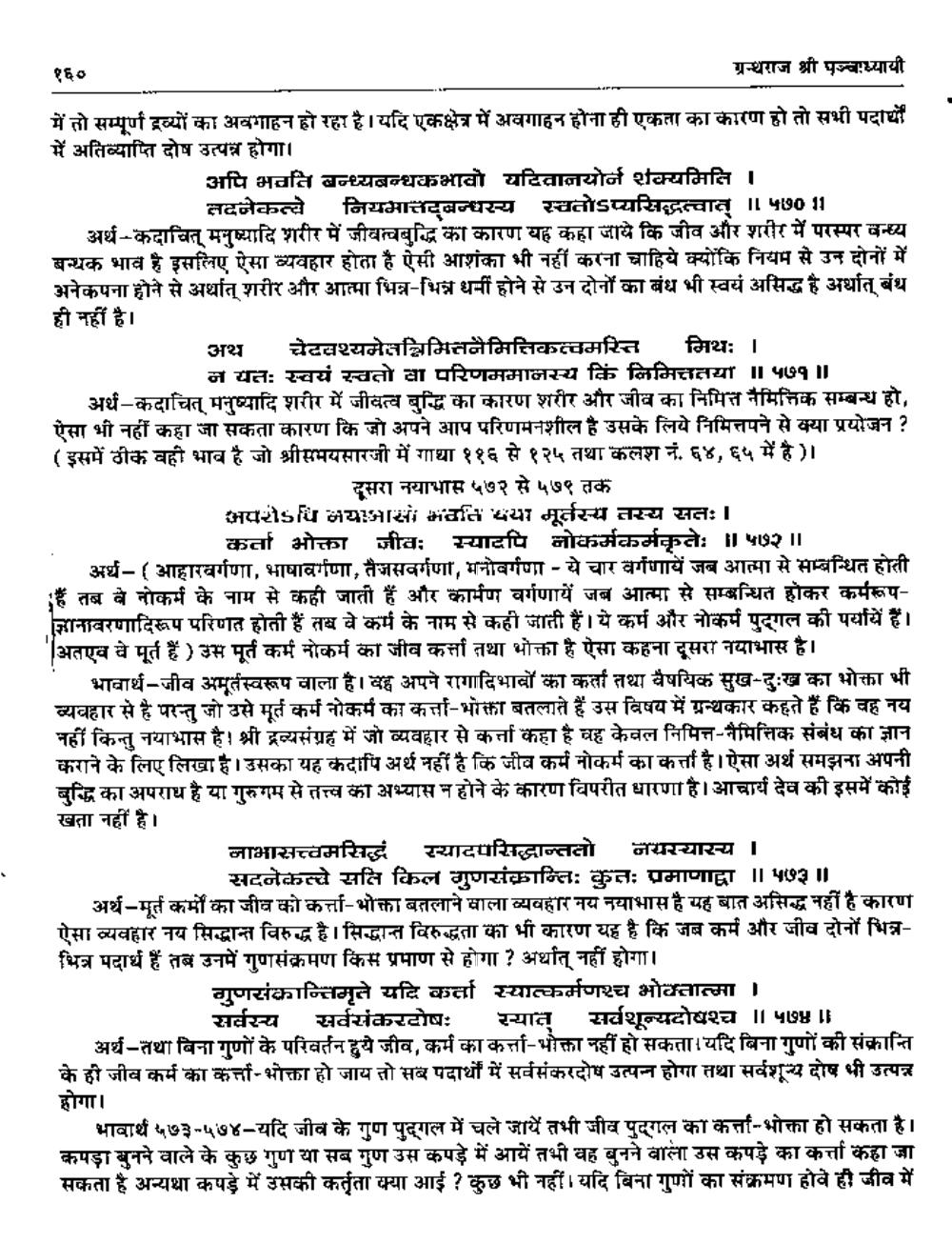________________
१६०
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
में तो सम्पूर्ण द्रव्यों का अवगाहन हो रहा है। यदि एकक्षेत्र में अवगाहन होना ही एकता का कारण हो तो सभी पदार्थों में अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा।
अपि भवति बन्ध्यबन्धकभावो यटितानयोर्न शक्यमिति ।
तदनेकत्वे नियमात्तबन्धस्य स्वतोऽप्यसिद्धत्वात् ॥ ५७011 अर्थ-कदाचित मनुष्यादि शरीर में जीवत्वबुद्धि का कारण यह कहा जाये कि जीव और शरीर में परस्पर बन्ध्य बन्धक भाव है इसलिए ऐसा व्यवहार होता है ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि नियम से उन दोनों में अनेकपना होने से अर्थात शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न धर्म होने से उन दोनों का बंध भी स्वयं असिद्ध है अर्थात बंध ही नहीं है।
अथ चेदवश्यमेतन्निमितनैमित्तिकत्वमस्ति मिथः ।
न यत: स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य किं लिमित्ततया ॥ ५७१॥ अर्थ-कदाचित् मनुष्यादि शरीर में जीवत्व बुद्धि का कारण शरीर और जीव का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कारण कि जो अपने आप परिणमनशील है उसके लिये निमित्तपने से क्या प्रयोजन? (इसमें ठीक वही भाव है जो श्रीसमयसारजी में गाथा ११६ से १२५ तथा कलश नं. ६४,६५ में है)।
दूसरा नयाभास ५७२ से ५७९ तक अपरोऽधि जयामास मावति या मूर्तस्य तस्य सतः।
कर्ता भोक्ता जीवः स्यादपि नोकर्मकर्मकृतेः ॥ ५७२ ।। अर्थ-(आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा - ये चार वर्गणायें जब आत्मा से सम्बन्धित होती हैं तब वे नोकर्म के नाम से कही जाती हैं और कार्मण वर्गणायें जब आत्मा से सम्बन्धित होकर कर्मरूपज्ञानावरणादिरूप परिणत होती हैं तब वे कर्म के नाम से कही जाती हैं। ये कर्म और नोकर्म पदगल की पर्यायें हैं। "अतएव वे मूर्त हैं) उस मूर्त कर्म नोकर्म का जीव कर्ता तथा भोक्ता है ऐसा कहना दूसरा नयाभास है।
भावार्थ-जीव अमूर्तस्वरूप वाला है। वह अपने रागादिभावों का कर्ता तथा वैषयिक सुख-दुःख का भोक्ता भी व्यवहार से है परन्तु जो उसे मूर्त कर्म नोकर्म का कर्ता-भोक्ता बतलाते हैं उस विषय में ग्रन्थकार कहते हैं कि वह नय नहीं किन्तु नयाभास है। श्री द्रव्यसंग्रह में जो व्यवहार से कर्ता कहा है वह केवल निमित्त-नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए लिखा है। उसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि जीव कर्म नोकर्म का कर्ता है। ऐसा अर्थ समझना अपनी बुद्धि का अपराध है या गुरुगम से तत्त्व का अभ्यास न होने के कारण विपरीत धारणा है। आचार्य देव की इसमें कोई खता नहीं है।
नाभासत्त्वमसिद्धं स्यादपसिद्धान्ततो जयस्यास्य ।
सदनेकत्चे सलि किल गुणसंक्रान्तिः कुतः प्रमाणाद्वा ॥ ५७३॥ अर्थ-मूर्त कर्मों का जीव कोका -भोक्ता बतलाने वाला व्यवहार नय नयाभास है यह बात असिद्ध नहीं है कारण ऐसा व्यवहार नय सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता का भी कारण यह है कि जब कर्म और जीव दोनों भिन्नभित्र पदार्थ हैं तब उनमें गुणसंक्रमण किस प्रमाण से होगा ? अर्थात् नहीं होगा।
गुणसंकान्तिमृते यदि कर्ता स्यात्कर्मणश्च भोक्तात्मा ।
सर्वस्य सर्वसंकरटोषः स्यात् सर्वशून्यदोषश्च || ५७४ ।। अर्थ-तथा बिना गुणों के परिवर्तन हुये जीव, कर्म का कर्ता-भोक्ता नहीं हो सकता। यदि बिना गुणों की संक्रान्ति के ही जीव कर्म का कर्ता-भोक्ता हो जाय तो सब पदार्थों में सर्वसंकरदोष उत्पन्न होगा तथा सर्वशून्य दोष भी उत्पन्न होगा।
भावार्थ ५७३-५७४-यदि जीव के गुण पुद्गल में चले जायें तभी जीव पुद्गल का कर्ता-भोक्ता हो सकता है। कपड़ा बुनने वाले के कुछ गुण या सब गुण उस कपड़े में आयें तभी वह बुनने वाला उस कपड़े का कर्ता कहा जा सकता है अन्यथा कपड़े में उसकी कर्तृता क्या आई? कुछ भी नहीं। यदि बिना गुणों का संक्रमण होवे ही जीव में