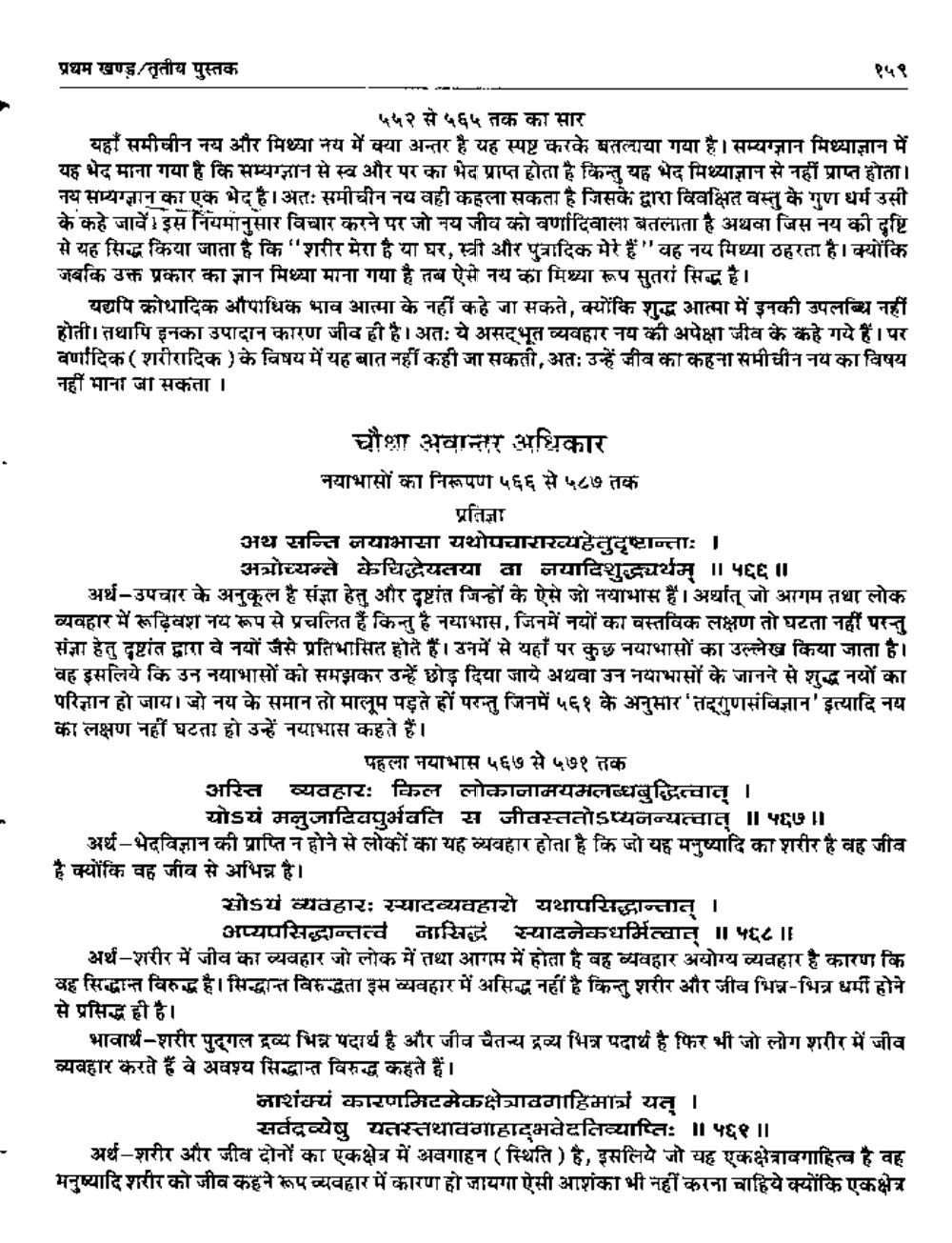________________
प्रथम खण्ड/तृतीय पुस्तक
५५२ से ५६५ तक का सार यहाँ समीचीन नय और मिथ्या नय में क्या अन्तर है यह स्पष्ट करके बतलाया गया है। सम्यग्जान मि यह भेद माना गया है कि सम्यग्ज्ञान से स्व और पर का भेद प्राप्त होता है किन्तु यह भेद मिथ्याज्ञान से नहीं प्राप्त होता। नय सम्यग्ज्ञान का एक भेद है। अतः समीचीन नय वही कहला सकता है जिसके द्वारा विवक्षित वस्तु के गुण धर्म उसी के कहे जावें। इस नियमानुसार विचार करने पर जो नय जीव को वर्णादिवाला बतलाता है अथवा जिस नय की दृष्टि से यह सिद्ध किया जाता है कि "शरीर मेरा है या घर, स्त्री और पत्रादिक मेरे हैं"वह नय मिथ्या ठहरता है। क्योंकि जबकि उक्त प्रकार का ज्ञान मिथ्या माना गया है तब ऐसे नय का मिथ्या रुप सुतरां सिद्ध है। । यद्यपि क्रोधादिक औपाधिक भाव आत्मा के नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शुद्ध आत्मा में इनकी उपलब्धि नहीं होती। तथापि इनका उपादान कारण जीव ही है। अतः ये असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा जीव के कहे गये हैं। पर वर्णादिक (शरीरादिक)के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, अत: उन्हें जीव का कहना समीचीन नय का विषय नहीं माना जा सकता ।
चौक्षा अवान्तर अधिकार नयाभासों का निरूपण ५६६ से ५८७ तक
प्रतिज्ञा अथ सन्ति नयाभासा यथोपचाराव्यहेतुदृष्टान्ताः ।
अनोच्यम्ले केचिद्धेयतया वा जयादिशुद्धयर्थम् ॥ ६ ॥ अर्थ-उपचार के अनुकूल है संज्ञा हेतु और दृष्टांत जिन्हों के ऐसे जो नयाभास हैं। अर्थात् जो आगम तथा लोक व्यवहार में रूढ़िवश नय रूप से प्रचलित हैं किन्तु है नयाभास, जिनमें नयों का वस्तविक लक्षण तो घरता नहीं परन्तु संज्ञा हेतु दृष्टांत द्वारा वे नयों जैसे प्रतिभासित होते हैं। उनमें से यहाँ पर कुछ नयाभासों का उल्लेख किया जाता है। वह इसलिये कि उन नयाभासों को समझकर उन्हें छोड़ दिया जाये अथवा उन नयाभासों के जानने से शुद्ध नयों का परिज्ञान हो जाय। जो नय के समान तो मालूम पड़ते हों परन्तु जिनमें ५६१के अनुसार 'तद्गुणसंविज्ञान' इत्यादि नय का लक्षण नहीं घटता हो उन्हें नयाभास कहते हैं।
पहला नयाभास ५६७ से ५७१ तक अस्ति व्यवहारः किल लोकानामयमलब्धबुद्रित्वात् ।
योऽयं मनुजादिवपुर्भवति स जीतस्ततोऽप्यनन्यत्वात् ॥ ५६७ ॥ अर्थ-भेदविज्ञान की प्राप्ति न होने से लोकों का यह व्यवहार होता है कि जो यह मनुष्यादि का शरीर है वह जीव है क्योंकि वह जीव से अभिन्न है।
सोऽयं व्यवहारः स्यादव्यवहारो यथापसिद्धान्तात् ।
अप्यपसिद्धान्तत्वं नासिद्धं स्यादनेकधर्मित्वात ॥ ५६८॥ अर्थ-शरीर में जीव का व्यवहार जो लोक में तथा आगम में होता है वह व्यवहार अयोग्य व्यवहार है कारण कि वह सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता इस व्यवहार में असिद्ध नहीं है किन्तु शरीर और जीव भिन्न-भिन्न धर्मी होने से प्रसिद्ध ही है।
भावार्थ-शरीर पुद्गल द्रव्य भिन्न पदार्थ है और जीव चैतन्य द्रव्य भिन्न पदार्थ है फिर भी जो लोग शरीर में जीव व्यवहार करते हैं वे अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते हैं।
नाशक्यं कारणमिटमेकक्षेत्रावगाहिमानं यत् ।
सर्वद्रव्येषु यतस्तथावगाहाद्भवेदलिव्याप्तिः ॥ ५६९ ॥ अर्थ-शरीर और जीव दोनों का एकक्षेत्र में अवगाहन (स्थिति) है, इसलिये जो यह एकक्षेत्रावगाहित्व है वह मनुष्यादि शरीर को जीव कहने रूप व्यवहार में कारण हो जायगा ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि एक क्षेत्र