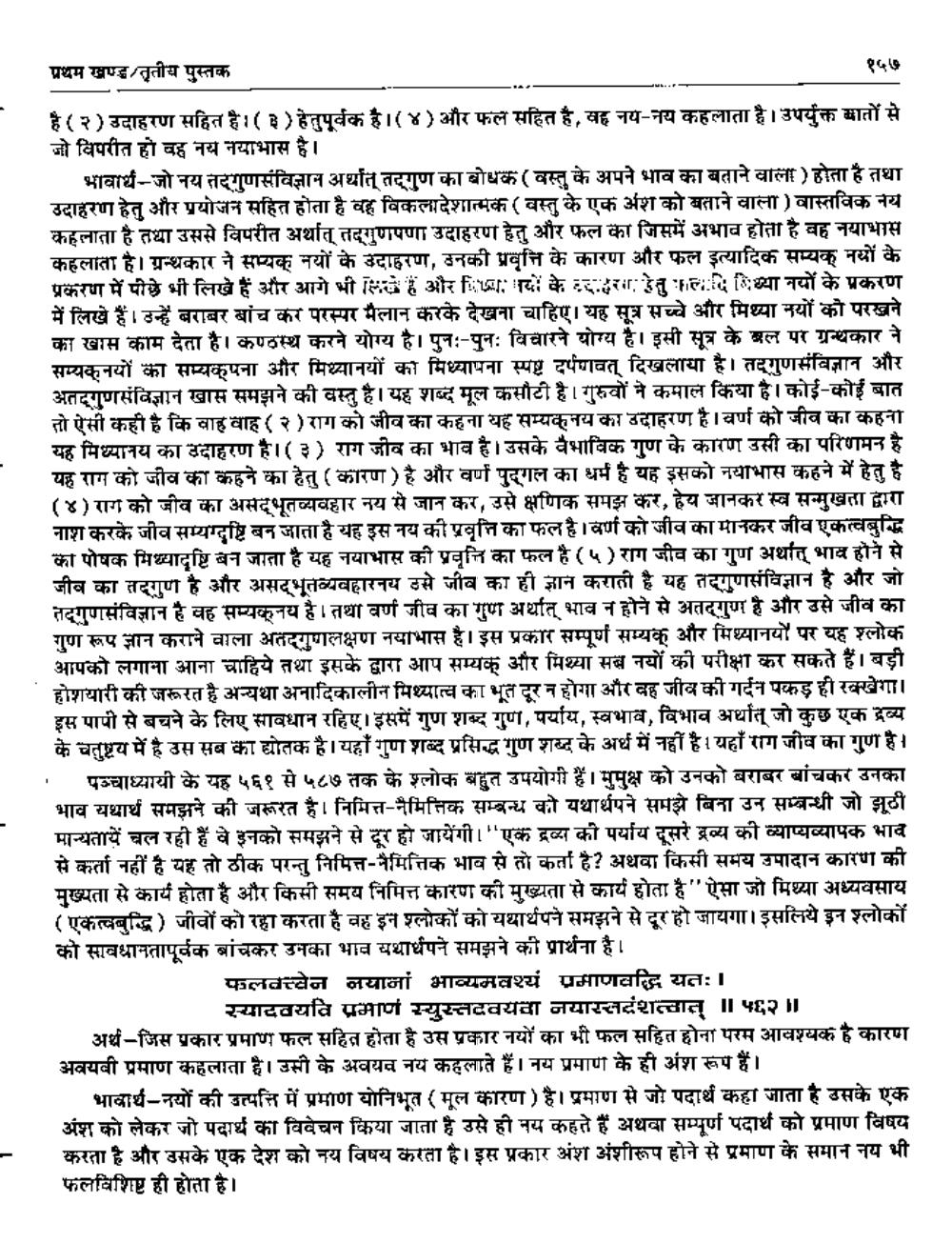________________
प्रथम खण्ड/तृतीय पुस्तक
१५७
है (२) उदाहरण सहित है। (३) हेतुपूर्वक है। (४) और फल सहित है, यह नय-नय कहलाता है। उपर्युक्त बातों से जो विपरीत हो वह नय नयाभास है।
भावार्थ-जो नय तद्गुणसंविज्ञान अर्थात् तद्गुण का बोधक (वस्तु के अपने भाव का बताने वाला) होता है तथा उदाहरण हेतु और प्रयोजन सहित होता है वह विकलादेशात्मक (वस्तु के एक अंश को बताने वाला) वास्तविक नय कहलाता है तथा उससे विपरीत अर्थात् तद्गुणपणा उदाहरण हेतु और फल का जिसमें अभाव होता है वह नयाभास कहलाता है। ग्रन्थकार ने सम्यक् नयों के उदाहरण, उनकी प्रवृत्ति के कारण और फल इत्यादिक सम्यक् नयों के प्रकरण में पीछे भी लिखे हैं और आगे भी लिखें हैं और मियाः पदों के दादरसा हेतु कालादिमिथ्या नयों के प्रकरण में लिखे हैं। उन्हें बराबर बांच कर परस्पर मैलान करके देखना चाहिए। यह सूत्र सच्चे और मिथ्या नयों को परखने का खास काम देता है। कण्ठस्थ करने योग्य है। पुन:-पुनः विचारने योग्य है। इसी सूत्र के बल पर ग्रन्थकार ने सम्यक्नयों का सम्यक्पना और मिथ्यानयों का मिथ्यापना स्पष्ट दर्पणवत् दिखलाया है। तद्गुणसंविज्ञान और अतद्गुणसंविज्ञान खास समझने की वस्तु है। यह शब्द मूल कसौटी है। गुरुवों ने कमाल किया है। कोई-कोई बात तो ऐसी कही है कि वाह वाह (२)राग को जीव का कहना यह सम्मानय का उदाहरण है। वर्ण को जीव का कहना यह मिथ्यानय का उदाहरण है।(३) राग जीव का भाव है। उसके वैभाविक गुण के कारण उसी का परिणमन है यह राम को जीव का कहने का हेतु (कारण) है और वर्ण पुद्गल का धर्म है यह इसको नयाभास कहने में हेतु है (४) राग को जीव का असद्भूतव्यवहार नय से जान कर, उसे क्षणिक समझ कर, हेय जानकर स्व सन्मुखता द्वारा नाश करके जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है यह इस नय की प्रवृत्ति का फल है। वर्णको जीव का मानकर जीव एकत्वबुद्धि का पोषक मिथ्यादृष्टि बन जाता है यह नयाभास की प्रवृत्ति का फल है (५) राग जीव का गुण अर्थात् भाव होने से जीव का तद्गुण है और असद्भुतव्यवहारनय उसे जीव का ही ज्ञान कराती है यह तद्गुणसंविज्ञान है और जो तद्गुणसंविज्ञान है वह सम्यनय है। तथा वर्ण जीव का गुण अर्थात् भाव न होने से अतद्गुण है और उसे जीव का गुण रूप ज्ञान कराने वाला अतद्गुणलक्षण नयाभास है। इस प्रकार सम्पूर्ण सम्यक् और मिथ्यानयों पर यह श्लोक आपको लगाना आना चाहिये तथा इसके द्वारा आप सम्यक् और मिथ्या सब नयों की परीक्षा कर सकते हैं। बड़ी होशयारी की जरूरत है अन्यथा अनादिकालीन मिथ्यात्व का भूत दूर न होगा और वह जीव की गर्दन पकड़ ही रक्खेगा। इस पापी से बचने के लिए सावधान रहिए। इसमें गुण शब्द गुण, पर्याय, स्वभाव, विभाव अर्थात् जो कुछ एक द्रव्य
के चतुष्टय में है उस सब का द्योतक है। यहाँ गुण शब्द प्रसिद्ध गुण शब्द के अर्थ में नहीं है। यहाँ राग जीव का गुण है। । पञ्चाध्यायी के यह ५६१ से ५८७ तक के श्लोक बहुत उपयोगी हैं। ममक्ष को उनको बराबर बांचकर उनका भाव यथार्थ समझने की जरूरत है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध को यथार्थपने समझे बिना उन सम्बन्धी जो झूठी मान्यतायें चल रही हैं वे इनको समझने से दूर हो जायेंगी। "एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की व्याप्यव्यापक भाव से कर्ता नहीं है यह तो ठीक परन्तु निमित्त-नैमित्तिक भाव से तो कर्ता है? अथवा किसी समय उपादान कारण की मख्यता से कार्य होता है और किसी समय निमित्त कारण की मख्यता से कार्य होता है"ऐसा जो मिथ्या अध्यवसाय (एकत्वबुद्धि) जीवों को रहा करता है वह इन श्लोकों को यथार्थपने समझने से दूर हो जायगा। इसलिये इन श्लोकों को सावधानतापूर्वक बांचकर उनका भाव यथार्थपने समझने की प्रार्थना है।
फलतत्वेन लयानां भाव्यमवश्यं प्रमाणवद्धि यतः।
स्यादवयवि प्रमाण स्युस्तटवयवा नयारसदंशत्वात् ॥ ५६२॥ अर्थ-जिस प्रकार प्रमाण फल सहित होता है उस प्रकार नयों का भी फल सहित होना परम आवश्यक है कारण अवयवी प्रमाण कहलाता है। उसी के अवयव नय कहलाते हैं। नय प्रमाण के ही अंश रूप हैं।
भावार्थ-नयों की उत्पत्ति में प्रमाण योनिभूत (मूल कारण ) है। प्रमाण से जो पदार्थ कहा जाता है उसके एक अंश को लेकर जो पदार्थ का विवेचन किया जाता है उसे ही नय कहते हैं अथवा सम्पूर्ण पदार्थ को प्रमाण विषय करता है और उसके एक देश को नय विषय करता है। इस प्रकार अंश अंशीरूप होने से प्रमाण के समान नय भी फलविशिष्ट ही होता है।