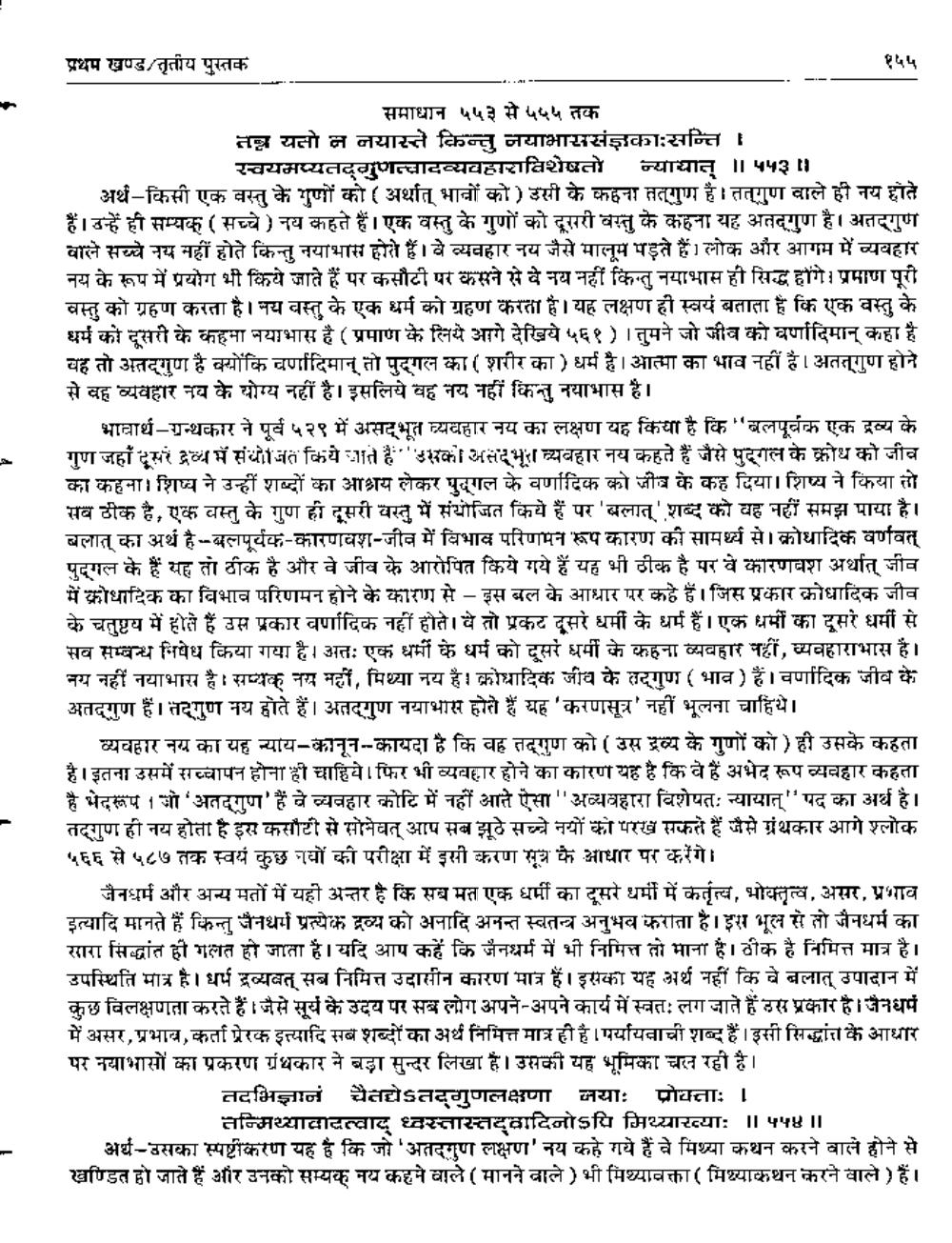________________
प्रथम खण्ड/ तृतीय पुस्तक
समाधान ५५३ से ५५५ तक
तन्न यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति ।
१५५
स्वयमप्यतद्गुणत्वादव्यवहाराविशेषतो
न्यायात् ॥ ५५३ ॥
अर्थ- किसी एक वस्तु के गुणों को (अर्थात् भावों को) उसी के कहना तत्गुण है। तत्गुण वाले ही नय होते हैं। उन्हें ही सम्यक् (सच्चे ) नय कहते हैं। एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु के कहना यह अतद्गुण है । अतद्गुण वाले सच्चे नय नहीं होते किन्तु नयाभास होते हैं। वे व्यवहार नय जैसे मालूम पड़ते हैं। लोक और आगम में व्यवहार नय के रूप में प्रयोग भी किये जाते हैं पर कसौटी पर कसने से वे नय नहीं किन्तु नयाभास ही सिद्ध होंगे। प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है। नय वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करता है। यह लक्षण ही स्वयं बताता है कि एक वस्तु के धर्म को दूसरी के कहना नयाभास है ( प्रमाण के लिये आगे देखिये ५६१ ) । तुमने जो जीव को वर्णादिमान् कहा है यह तो अतद्गुण है क्योंकि वर्णादिमान् तो पुद्गल का ( शरीर का ) धर्म है। आत्मा का भाव नहीं है। अतत्गुण होने से वह व्यवहार नय के योग्य नहीं है। इसलिये वह नय नहीं किन्तु नयाभास है।
भावार्थ- ग्रन्थकार ने पूर्व ५२९ में असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण यह किया है कि "बलपूर्वक एक द्रव्य के गुण जहाँ दूसरे द्रव्य में संयोजित किये जाते हैं उसको असभूत व्यवहार नय कहते हैं जैसे पुद्गल के क्रोध को जीव का कहना। शिष्य ने उन्हीं शब्दों का आश्रय लेकर पुद्गल के वर्णादिक को जीब के कह दिया। शिष्य ने किया तो सब ठीक है, एक वस्तु के गुण ही दूसरी वस्तु में संयोजित किये हैं पर 'बलात्' शब्द को वह नहीं समझ पाया है। बलात् का अर्थ है - बलपूर्वक कारणवश जीव में विभाव परिणमन रूप कारण की सामर्थ्य से । क्रोधादिक वर्णवत् पुद्गल के हैं यह तो ठीक है और वे जीव के आरोपित किये गये हैं यह भी ठीक है पर वे कारणवश अर्थात् जीव में क्रोधादिक का विभाव परिणमन होने के कारण से इस बल के आधार पर कहे हैं। जिस प्रकार क्रोधादिक जीव के चतुष्टय में होते हैं उस प्रकार वर्णादिक नहीं होते। वे तो प्रकट दूसरे धर्मों के धर्म हैं। एक धर्मों का दूसरे धर्मी से सब सम्बन्ध निषेध किया गया है। अतः एक धर्मों के धर्म को दूसरे धर्मी के कहना व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। नय नहीं नयाभास है। सम्यक् नय नहीं मिथ्या नय है। क्रोधादिक जीव के तद्गुण (भाव) हैं। वर्णादिक जीव के अतद्गुण हैं । तद्गुण नय होते हैं। अतद्गुण नयाभास होते हैं यह 'करणसूत्र' नहीं भूलना चाहिये ।
1
1
व्यवहार नय का यह न्याय कानून कायदा है कि वह तद्गुण को ( उस द्रव्य के गुणों को ) ही उसके कहता है । इतना उसमें सच्चापन होना ही चाहिये। फिर भी व्यवहार होने का कारण यह है कि वे हैं अभेद रूप व्यवहार कहता है भेदरूप 1 जो 'अतद्गुण' हैं वे व्यवहार कोटि में नहीं आते ऐसा " अव्यवहारा विशेषतः न्यायात् " पद का अर्थ है । तद्गुण ही नय होता है इस कसौटी से सोमेवत् आप सब झूठे सच्चे नयों को परख सकते हैं जैसे ग्रंथकार आगे श्लोक ५६६ से ५८७ तक स्वयं कुछ नयों की परीक्षा में इसी करण सूत्र के आधार पर करेंगे।
जैनधर्म और अन्य मतों में यही अन्तर है कि सब मत एक धर्मी का दूसरे धर्मी में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर, प्रभाव इत्यादि मानते हैं किन्तु जैनधर्म प्रत्येक द्रव्य को अनादि अनन्त स्वतन्त्र अनुभव कराता है। इस भूल से तो जैनधर्म का सारा सिद्धांत ही गलत हो जाता है। यदि आप कहें कि जैनधर्म में भी निमित्त तो माना है। ठीक है निमित्त मात्र है। उपस्थिति मात्र है । धर्म द्रव्यवत् सब निमित्त उदासीन कारण मात्र हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि वे बलात् उपादान में कुछ विलक्षणता करते हैं। जैसे सूर्य के उदय पर सब लोग अपने-अपने कार्य में स्वतः लग जाते हैं उस प्रकार है। जैनधर्म में असर, प्रभाव, कर्ता प्रेरक इत्यादि सब शब्दों का अर्थ निमित्त मात्र ही है। पर्यायवाची शब्द हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर नयाभासों का प्रकरण ग्रंथकार ने बड़ा सुन्दर लिखा है। उसकी यह भूमिका चल रही है।
तदभिज्ञानं चैतद्येऽतद्गुणलक्षणा जयाः प्रोक्ताः ।
तन्मिथ्यावादत्वाद् ध्वस्तास्तद्वादिनोऽयि मिथ्याख्याः ॥ ५५४ ॥
अर्थ-उसका स्पष्टीकरण यह है कि जो 'अतद्गुण लक्षण' नय कहे गये हैं वे मिथ्या कथन करने वाले होने से खण्डित हो जाते हैं और उनको सम्यक् नय कहने वाले (मानने वाले ) भी मिथ्यावक्ता ( मिथ्याकथन करने वाले ) हैं ।