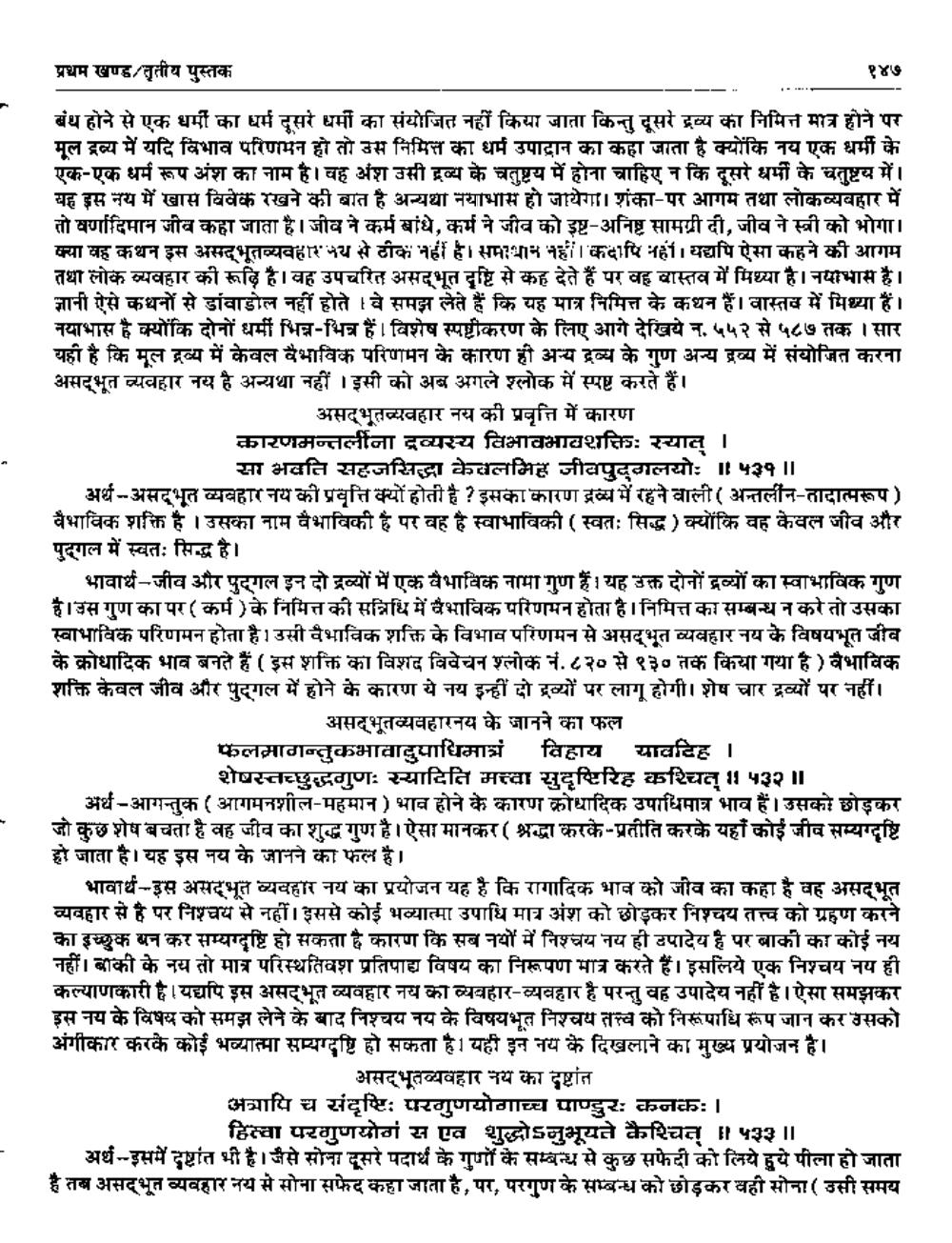________________
प्रथम खण्ड/तृतीय पुस्तक
१४७
बंध होने से एक धर्मी का धर्म दूसरे धर्मी का संयोजित नहीं किया जाता किन्तु दूसरे द्रव्य का निमिन मात्र होने पर मूल द्रव्य में यदि विभाव परिणमन हो तो उस निमित्त का धर्म उपादान का कहा जाता है क्योंकि नय एक धर्मी के एक-एक धर्म रूप अंश का नाम है। वह अंश उसी द्रव्य के चतुष्टय में होना चाहिए न कि दूसरे धर्मी के चतुष्टय में। यह इस नय में खास विवेक रखने की बात है अन्यथा नयाभास हो जायेगा। शंका-पर आगम तथा लोकव्यवहार में तो वर्णादिमान जीव कहा जाता है। जीव ने कर्म बांधे, कर्म ने जीव को इट-अनिष्ट सामग्री दी, जीव ने स्त्री को भोगा। क्या वह कथन इस असद्भूतव्यवहारमय से ठीक नहीं है। समाधान नहीं। कदापि नहीं। यद्यपि ऐसा कहने की आगम तथा लोक व्यवहार की रूढ़ि है। वह उपचरित असद्भुत दृष्टि से कह देते हैं पर वह वास्तव में मिथ्या है। नयाभास है। ज्ञानी ऐसे कथनों से डांवाडोल नहीं होते । वे समझ लेते हैं कि यह मात्र निमित्त के कथन हैं। वास्तव में मिथ्या हैं। नयाभास है क्योंकि दोनों धर्मी भिन्न-भित्र हैं। विशेष स्पष्टीकरण के लिए आगे देखिये न.५५२ से ५८७ तक । सार यही है कि मूल द्रव्य में केवल वैभाविक परिणमन के कारण ही अन्य द्रव्य के गण अन्य द्रव्य में संयोजित करना असद्भुत च्यवहार नय है अन्यथा नहीं । इसी को अब अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं।
असद्धृतव्यवहार नय की प्रवृत्ति में कारण कारणमन्तीना द्रव्यस्य विभावभावशक्तिः स्यात ।
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुदगलयोः ॥ ५३१॥ पदभत व्यवहार नय की प्रवत्तिक्यों होती है? इसका कारण द्रव्य में रहने वाली अन्तलीन-तादात्मरूप) वैभाविक शक्ति है। उसका नाम वैभाविकी है पर वह है स्वाभाविकी (स्वतः सिद्ध क्योंकि वह केवल जीव और पुद्गल में स्वतः सिद्ध है।
भावार्थ-जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में एक वैभाविक नामा गुण हैं। यह उक्त दोनों द्रव्यों का स्वाभाविक गुण है। उस गुण कापर (कर्म)के निमित्त की सन्निधि में वैभाविक परिणमन होता है। निमित्त का सम्बन्ध न करे तो उसका स्वाभाविक परिणमन होता है। उसी वैभाविक शक्ति के विभाव परिणमन से असद्भुत व्यवहार नय के विषयभूत जीव के क्रोधादिक भाव बनते हैं ( इस शक्ति का विशद विवेचन श्लोक नं.८२० से १३० तक किया गया है) वैभाविक शक्ति केवल जीव और पुदगल में होने के कारण ये नय इन्हीं दो द्रव्यों पर लागू होगी। शेष चार द्रव्यों पर नहीं।
असद्भुतव्यवहारनय के जानने का फल फलमागन्तुकभावानुपाधिमानं विहाय यावदिह ।
शेषस्तच्छुद्धगुणः स्यादिति मत्वा सुदृष्टिरिह कश्चित् ।। ५३२॥ अर्थ-आगन्तुक (आगमनशील-महमान) भाव होने के कारण क्रोधादिक उपाधिमात्र भाव हैं। उसको छोड़कर जो कुछ शेष बचता है वह जीव का शुद्ध गुण है। ऐसा मानकर ( श्रद्धा करके-प्रतीति करके यहाँ कोई जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है। यह इस नय के जानने का फल है।
भावार्थ-इस असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोजन यह है कि रागादिक भाव को जीव का कहा है वह असद्भुत व्यवहार से है पर निश्चय से नहीं। इससे कोई भव्यात्मा उपाधि मात्र अंश को छोड़कर निश्चय तत्त्व को ग्रहण करने का इच्छुक बन कर सम्यग्दृष्टि हो सकता है कारण कि सब नयों में निश्चय नय ही उपादेय है पर बाकी का कोई नय नहीं। बाकी के नय तो मात्र परिस्थतिवश प्रतिपाद्य विषय का निरूपण मात्र करते हैं। इसलिये एक नि कल्याणकारी है। यद्यपि इस असद्भुत व्यवहार नय का व्यवहार-व्यवहार है परन्तु वह उपादेय नहीं है। ऐसा समझकर इस नय के विषय को समझ लेने के बाद निश्चय नय के विषयभूत निश्चय तत्त्वको निरूपाधि रूप जान कर उसको अंगीकार करके कोई भव्यात्मा सम्यग्दष्टि हो सकता है। यही इन नय के दिखलाने का मुख्य प्रयोजन है।
असद्भूतव्यवहार नय का दृष्टांत अनापि च संदष्टिः परगणयोगाच्च पाण्डर: कनकः।
हिस्वा परगुणयोग स एव शुद्धोऽनुभूयते कैश्चित् ॥ ५३३ ।। अर्थ-इसमें दृष्टांत भी है। जैसे सोना दूसरे पदार्थ के गुणों के सम्बन्ध से कुछ सफेदी को लिये हुये पीला हो जाता है तब असद्भूत व्यवहार नय से सोना सफेद कहा जाता है, पर, परगण के सम्बन्ध को छोड़कर वही सोना( उसी समय