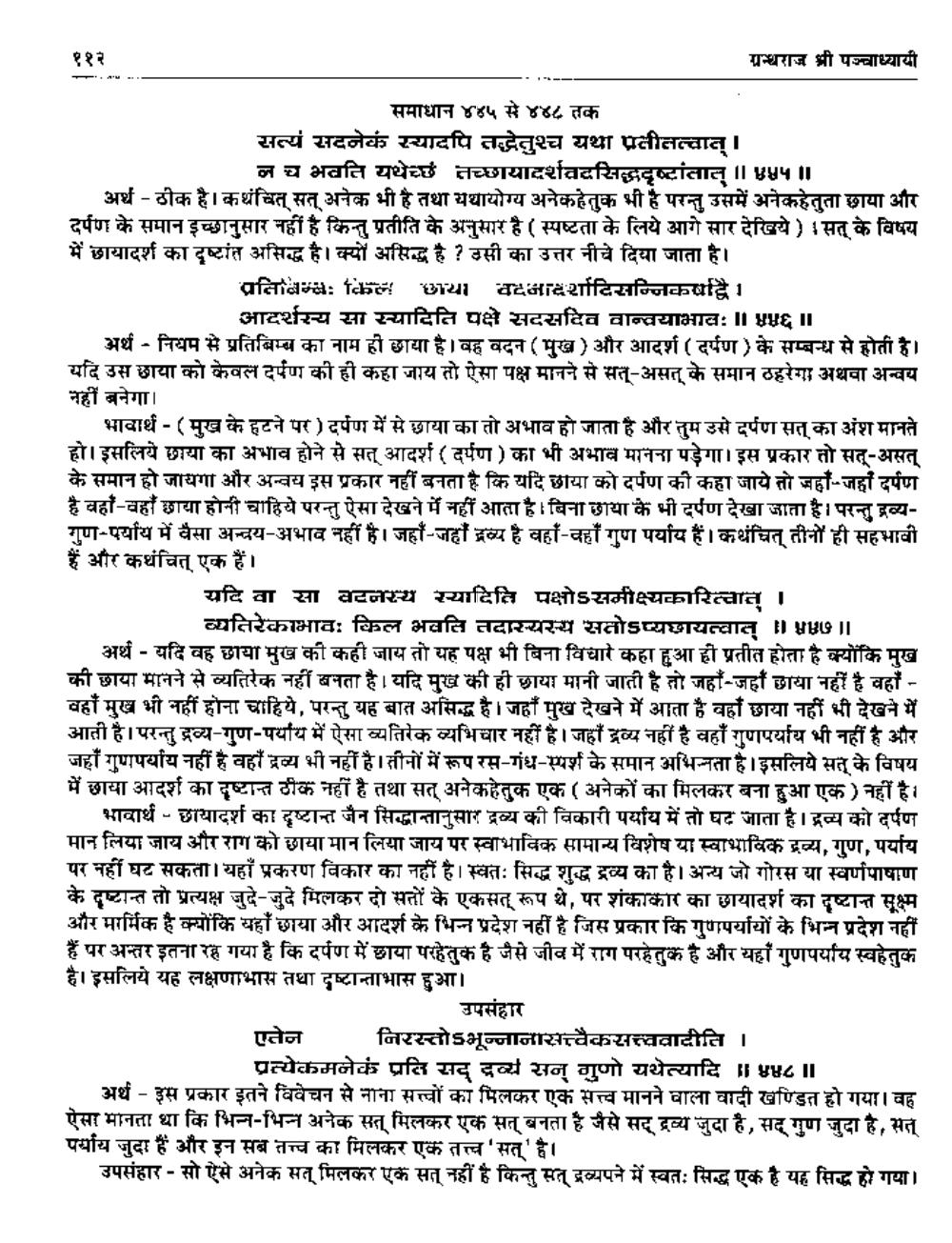________________
११२
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
समाधान ४४५ से ४४८ तक
सत्यं सदनेकं स्यादपि तद्धेतुश्च यथा प्रतीतत्वात् ।
न च भवति यथेच्छं तच्छायादर्शवदसिद्धदृष्टांतात् ॥ ४४५ ॥
अर्थ - ठीक है । कथंचित् सत् अनेक भी है तथा यथायोग्य अनेकहेतुक भी है परन्तु उसमें अनेकहेतुता छाया और दर्पण के समान इच्छानुसार नहीं है किन्तु प्रतीति के अनुसार है ( स्पष्टता के लिये आगे सार देखिये) । सत् के विषय में छायादर्श का दृष्टांत असिद्ध है। क्यों असिद्ध है ? उसी का उत्तर नीचे दिया जाता है।
प्रतिविम्बः किल छाया
वदनादर्शादिसन्निकर्षाद्वै ।
आदर्शस्य सा स्यादिति पक्षे सदसदिव वान्वयाभावः ॥ ४४६ ॥
अर्थ- नियम से प्रतिबिम्ब का नाम ही छाया है। वह वदन (मुख) और आदर्श (दर्पण) के सम्बन्ध से होती है। यदि उस छाया को केवल दर्पण की ही कहा जाय तो ऐसा पक्ष मानने से सत्-असत् के समान ठहरेगा अथवा अन्वय नहीं बनेगा।
भावार्थ (मुख के हटने पर ) दर्पण में से छाया का तो अभाव हो जाता है और तुम उसे दर्पण सत् का अंश मानते हो। इसलिये छाया का अभाव होने से सत् आदर्श (दर्पण) का भी अभाव मानना पड़ेगा। इस प्रकार तो सत्-असत् के समान हो जायगा और अन्वय इस प्रकार नहीं बनता है कि यदि छाया को दर्पण को कहा जाये तो जहाँ-जहाँ दर्पण है वहाँ वहाँ छाया होनी चाहिये परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता है। बिना छाया के भी दर्पण देखा जाता है। परन्तु द्रव्यगुण- पर्याय में वैसा अन्वय-अभाव नहीं है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ गुण पर्याय हैं। कथंचित् तीनों ही सहभावी हैं और कथंचित् एक हैं।
यदि वा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोऽसमीक्ष्यकारित्वात् ।
व्यतिरेकाभावः किल भवति तदास्यस्य सतोऽप्यछायत्वात् ॥ ४४७ ॥
अर्थ यदि वह छाया मुख की कही जाय तो यह पक्ष भी बिना विचारे कहा हुआ ही प्रतीत होता है क्योंकि मुख की छाया मानने से व्यतिरेक नहीं बनता है। यदि मुख की ही छाया मानी जाती है तो जहाँ-जहाँ छाया नहीं है वहाँ - वहाँ मुख भी नहीं होना चाहिये, परन्तु यह बात असिद्ध है। जहाँ मुख देखने में आता है वहाँ छाया नहीं भी देखने में आती है । परन्तु द्रव्य-गुण- पर्याय में ऐसा व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। जहाँ द्रव्य नहीं है वहाँ गुणपर्याय भी नहीं है और जहाँ गुणपर्याय नहीं है वहाँ द्रव्य भी नहीं है। तीनों में रूप रस-गंध-स्पर्श के समान अभिन्नता है। इसलिये सत् के विषय में छाया आदर्श का दृष्टान्त ठीक नहीं है तथा सत् अनेकहेतुक एक ( अनेकों का मिलकर बना हुआ एक ) नहीं है। भावार्थ - छायादर्श का दृष्टान्त जैन सिद्धान्तानुसार द्रव्य की विकारी पर्याय में तो घट जाता है । द्रव्य को दर्पण मान लिया जाय और राग को छाया मान लिया जाय पर स्वाभाविक सामान्य विशेष या स्वाभाविक द्रव्य, गुण, पर्याय पर नहीं घट सकता। यहाँ प्रकरण विकार का नहीं है। स्वतः सिद्ध शुद्ध द्रव्य का है। अन्य जो गोरस या स्वर्णपाषाण के दृष्टान्त तो प्रत्यक्ष जुदे-जुदे मिलकर दो सतों के एकसत् रूप थे, पर शंकाकार का छायादर्श का दृष्टान्त सूक्ष्म और मार्मिक है क्योंकि यहाँ छाया और आदर्श के भिन्न प्रदेश नहीं है जिस प्रकार कि गुणपर्यायों के भिन्न प्रदेश नहीं हैं पर अन्तर इतना रह गया है कि दर्पण में छाया परहेतुक है जैसे जीव में राग परहेतुक है और यहाँ गुणपर्याय स्वहेतुक है । इसलिये यह लक्षणाभास तथा दृष्टान्ताभास हुआ।
उपसंहार
-
एतेन
निरस्तोऽभून्नानासत्त्वैकसत्ववादीति ।
प्रत्येकमनेकं प्रति सद् द्रव्यं सन् गुणो यथेत्यादि ॥ ४४८ ॥
अर्थ - इस प्रकार इतने विवेचन से नाना सत्त्वों का मिलकर एक सत्त्व मानने वाला वादी खण्डित हो गया। वह ऐसा मानता था कि भिन्न-भिन्न अनेक सत् मिलकर एक सत् बनता है जैसे सद् द्रव्य जुदा है, सद् गुण जुदा है, सत् पर्याय जुदा हैं और इन सब तत्त्व का मिलकर एक तत्त्व 'सत् ' है ।
उपसंहार - सो ऐसे अनेक सत् मिलकर एक सत् नहीं है किन्तु सत् द्रव्यपने में स्वतः सिद्ध एक है यह सिद्ध हो गया।