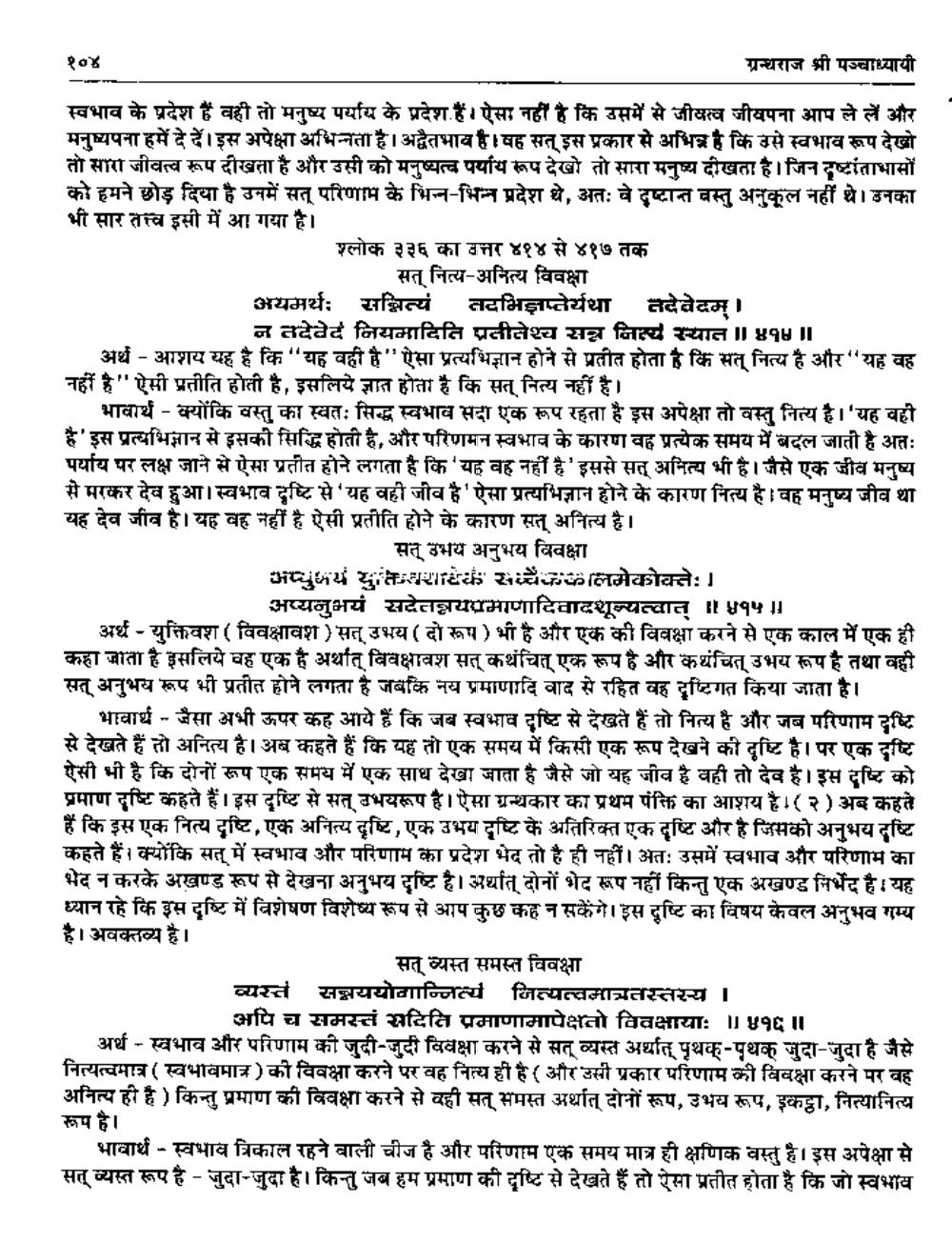________________
१०४
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
स्वभाव के प्रदेश हैं वहीं तो मनुष्य पर्याय के प्रदेश हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें से जीवत्व जीवपना आप ले लें और मनुष्यपना हमें दे दें। इस अपेक्षा अभिन्नता है। अद्वैतभाव है। वह सत् इस प्रकार से अभित्र है कि उसे स्वभाव रूप देखो तो सारा जीवत्व रूप दीखता है और उसी को मनुष्यत्व पर्याय रूप देखो तो सारा मनुष्य दीखता है। जिन दृष्टांताभासों को हमने छोड़ दिया है उनमें सत् परिणाम के भिन्न-भिन्न प्रदेश थे, अतः वे दृष्टान्त वस्तु अनुकूल नहीं थे। उनका भी सार तत्व इसी में आ गया है।
श्लोक ३३६ का उत्तर ४१४ से ४१७ तक
सत् नित्य-अनित्य विवक्षा अयमर्थः सन्नित्यं तदभिज्ञप्तेर्यथा तदेवेटम्।
न तदेवेदं नियमादिति प्रतीतेश्च सन्न लिस्य स्यात ॥ ४१४ ॥ अर्थ - आशय यह है कि "यह वही है" ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से प्रतीत होता है कि सत् नित्य है और"यह वह नहीं है" ऐसी प्रतीति होती है, इसलिये ज्ञात होता है कि सत् नित्य नहीं है।
भावार्थ- क्योंकि वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव सदा एक रूप रहता है इस अपेक्षा तो वस्तु नित्य है। यह वही है' इस प्रत्यभिज्ञान से इसकी सिद्धि होती है, और परिणमन स्वभाव के कारण वह प्रत्येक समय में बदल जाती है अतः पर्याय पर लक्ष जाने से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि 'यह वह नहीं है' इससे सत् अनित्य भी है। जैसे एक जीव मनुष्य से परकर देव हुआ। स्वभाव दृष्टि से यह वही जीव है। ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने के कारण नित्य है। वह मनुष्य जीव था यह देव जीव है। यह वह नहीं है ऐसी प्रतीति होने के कारण सत् अनित्य है।
सत् उभय अनुभय विवक्षा अग्युभयं युक्तिवाटेवं सम्मालमेकोक्तेः।
अप्यनुभयं सटेतन्नयप्रमाणादिवादशूज्यत्वात् ।।१५।। अर्थ-यक्तिवश (विवक्षावश) सत उभय(दो रूप) भी है और एक की विवक्षा करने से एक काल में कहा जाता है इसलिये वह एक है अर्थात् विवक्षावश सत् कथंचित् एक रूप है और कथंचित् उभय रूप है तथा वही सत् अनुभव रूप भी प्रतीत होने लगता है जबकि नय प्रमाणादि वाद से रहित वह दृष्टिगत किया जाता है।
भावार्थ - जैसा अभी ऊपर कह आये हैं कि जब स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो नित्य है और जब परिणाम दृष्टि से देखते हैं तो अनित्य है। अब कहते हैं कि यह तो एक समय में किसी एक रूप देखने की दृष्टि है। पर एक दृष्टि ऐसी भी है कि दोनों रूप एक समय में एक साथ देखा जाता है जैसे जो यह जीव है वही तो देव है। इस दृष्टि को प्रमाण दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से सत् उभयरूप है। ऐसा ग्रन्थकार का प्रथम पंक्ति का आशय है। (२) अब कहते हैं कि इस एक नित्य दृष्टि,एक अनित्य दृष्टि, एक उभय दृष्टि के अतिरिक्त एक दृष्टि और है जिसको अनुभय दृष्टि कहते हैं। क्योंकि सत् में स्वभाव और परिणाम का प्रदेश भेद तो है ही नहीं। अत: उसमें स्वभाव और परिणाम का भेद न करके अखण्ड रूप से देखना अनुभय दृष्टि है। अर्थात् दोनों भेद रूप नहीं किन्तु एक अखण्ड निर्भेद है। यह ध्यान रहे कि इस दृष्टि में विशेषण विशेष्य रूप से आप कुछ कह न सकेंगे। इस दृष्टि का विषय केवल अनुभव गम्य है। अवक्तव्य है।
सत् व्यस्त समस्त विवक्षा व्यरतं सन्नययोगान्नित्य जित्यत्तमात्रतस्तस्य ।
अपि च समस्तं सदिति प्रमाणामापेक्षतो विवक्षायाः ॥ ४१६ ।। अर्थ-स्वभाव और परिणाम की जदी-जुदी विवक्षा करने से सत् व्यस्त अर्थात् पृथक्-पृथक् जुदा-जुदा है जैसे नित्यत्वमात्र ( स्वभावमात्र)की विवक्षा करने पर वह नित्य ही है (और उसी प्रकार परिणाम की विवक्षा करने पर वह अनित्य ही है किन्तु प्रमाण की विवक्षा करने से वही सत् समस्त अर्थात् दोनों रूप, उभय रूप, इकट्ठा, नित्यानित्य रूप है। ___ भावार्थ - स्वभाव त्रिकाल रहने वाली चीज है और परिणाम एक समय मात्र ही क्षणिक वस्तु है। इस अपेक्षा से सत् व्यस्त रूप है - जुदा-जुदा है। किन्तु जब हम प्रमाण की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्वभाव