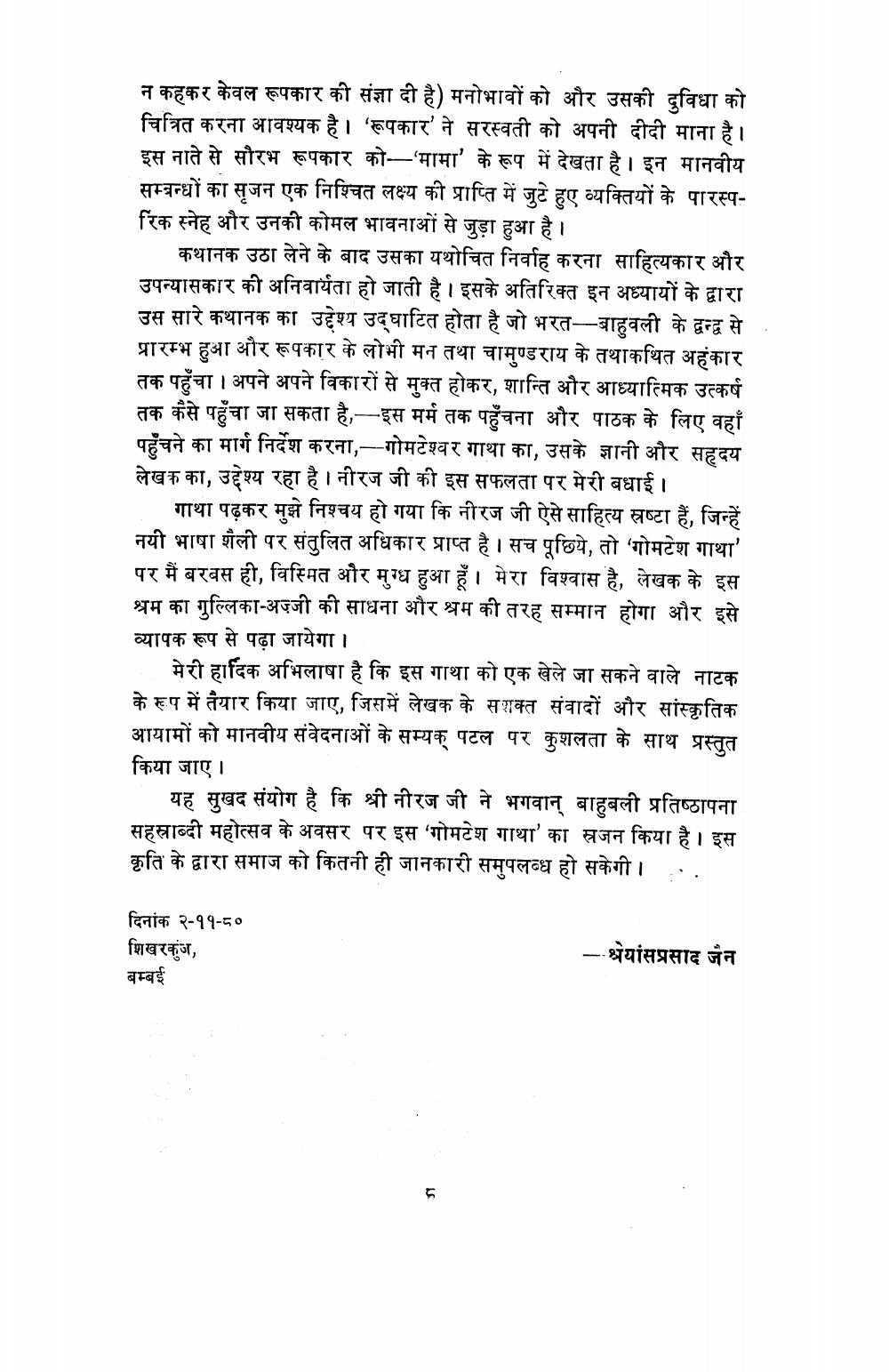________________
न कहकर केवल रूपकार की संज्ञा दी है) मनोभावों को और उसकी दुविधा को चित्रित करना आवश्यक है । 'रूपकार' ने सरस्वती को अपनी दीदी माना है । इस नाते से सौरभ रूपकार को — 'मामा' के रूप में देखता है । इन मानवीय सम्बन्धों का सृजन एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे हुए व्यक्तियों के पारस्परिक स्नेह और उनकी कोमल भावनाओं से जुड़ा हुआ है ।
कथानक उठा लेने के बाद उसका यथोचित निर्वाह करना साहित्यकार और उपन्यासकार की अनिवार्यता हो जाती है । इसके अतिरिक्त इन अध्यायों के द्वारा उस सारे कथानक का उद्देश्य उद्घाटित होता है जो भरत - बाहुवली के द्वन्द्व से प्रारम्भ हुआ और रूपकार के लोभी मन तथा चामुण्डराय के तथाकथित अहंकार तक पहुँचा । अपने अपने विकारों से मुक्त होकर, शान्ति और आध्यात्मिक उत्कर्ष तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इस मर्म तक पहुँचना और पाठक के लिए वहाँ पहुँचने का मार्ग निर्देश करना, — गोमटेश्वर गाथा का, उसके ज्ञानी और सहृदय लेखक का, उद्देश्य रहा है। नीरज जी की इस सफलता पर मेरी बधाई |
गाथा पढ़कर मुझे निश्चय हो गया कि नीरज जी ऐसे साहित्य स्रष्टा हैं, जिन्हें नयी भाषा शैली पर संतुलित अधिकार प्राप्त है। सच पूछिये, तो 'गोमटेश गाथा' पर मैं बरबस ही, विस्मित और मुग्ध हुआ हूँ । मेरा विश्वास है, लेखक के इस श्रम का गुल्लिका - अज्जी की साधना और श्रम की तरह सम्मान होगा और इसे व्यापक रूप से पढ़ा जायेगा ।
मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि इस गाथा को एक खेले जा सकने वाले नाटक के रूप में तैयार किया जाए, जिसमें लेखक के सशक्त संवादों और सांस्कृतिक आयामों को मानवीय संवेदनाओं के सम्यक् पटल पर कुशलता के साथ प्रस्तुत किया जाए ।
यह सुखद संयोग है कि श्री नीरज जी ने भगवान् बाहुबली प्रतिष्ठापना सहस्राब्दी महोत्सव के अवसर पर इस 'गोमटेश गाथा' का स्रजन किया है । इस कृति के द्वारा समाज को कितनी ही जानकारी समुपलब्ध हो सकेगी ।
दिनांक २-११-८०
शिखरकुंज,
बम्बई
८
- श्रेयांसप्रसाद जैन