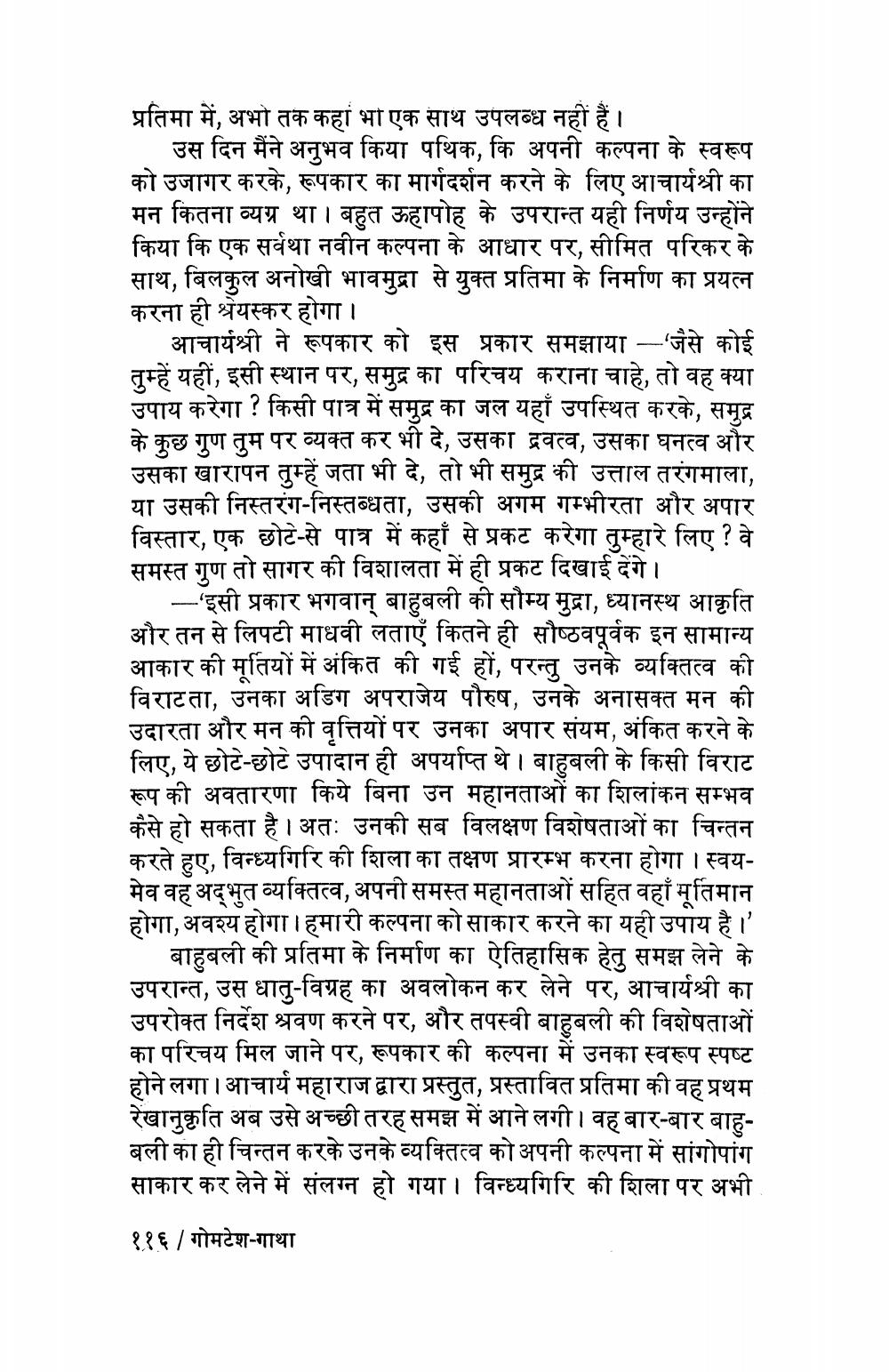________________
प्रतिमा में, अभी तक कहां भी एक साथ उपलब्ध नहीं हैं।
उस दिन मैंने अनुभव किया पथिक, कि अपनी कल्पना के स्वरूप को उजागर करके, रूपकार का मार्गदर्शन करने के लिए आचार्यश्री का मन कितना व्यग्र था। बहुत ऊहापोह के उपरान्त यही निर्णय उन्होंने किया कि एक सर्वथा नवीन कल्पना के आधार पर, सीमित परिकर के साथ, बिलकुल अनोखी भावमुद्रा से युक्त प्रतिमा के निर्माण का प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर होगा।
आचार्यश्री ने रूपकार को इस प्रकार समझाया - 'जैसे कोई तुम्हें यहीं, इसी स्थान पर, समुद्र का परिचय कराना चाहे, तो वह क्या उपाय करेगा? किसी पात्र में समुद्र का जल यहाँ उपस्थित करके, समुद्र के कुछ गुण तुम पर व्यक्त कर भी दे, उसका द्रवत्व, उसका घनत्व और उसका खारापन तुम्हें जता भी दे, तो भी समुद्र की उत्ताल तरंगमाला, या उसकी निस्तरंग-निस्तब्धता, उसकी अगम गम्भीरता और अपार विस्तार, एक छोटे-से पात्र में कहाँ से प्रकट करेगा तुम्हारे लिए? वे समस्त गुण तो सागर की विशालता में ही प्रकट दिखाई देंगे।
-इसी प्रकार भगवान् बाहुबली की सौम्य मुद्रा, ध्यानस्थ आकृति और तन से लिपटी माधवी लताएँ कितने ही सौष्ठवपूर्वक इन सामान्य आकार की मूर्तियों में अंकित की गई हों, परन्तु उनके व्यक्तित्व की विराटता, उनका अडिग अपराजेय पौरुष, उनके अनासक्त मन की उदारता और मन की वृत्तियों पर उनका अपार संयम, अंकित करने के लिए, ये छोटे-छोटे उपादान ही अपर्याप्त थे। बाहुबली के किसी विराट रूप की अवतारणा किये बिना उन महानताओं का शिलांकन सम्भव कैसे हो सकता है। अतः उनकी सब विलक्षण विशेषताओं का चिन्तन करते हुए, विन्ध्यगिरि की शिला का तक्षण प्रारम्भ करना होगा । स्वयमेव वह अद्भुत व्यक्तित्व, अपनी समस्त महानताओं सहित वहाँ मूर्तिमान होगा, अवश्य होगा। हमारी कल्पना को साकार करने का यही उपाय है।'
बाहुबली की प्रतिमा के निर्माण का ऐतिहासिक हेतु समझ लेने के उपरान्त, उस धातु-विग्रह का अवलोकन कर लेने पर, आचार्यश्री का उपरोक्त निर्देश श्रवण करने पर, और तपस्वी बाहुबली की विशेषताओं का परिचय मिल जाने पर, रूपकार की कल्पना में उनका स्वरूप स्पष्ट होने लगा। आचार्य महाराज द्वारा प्रस्तुत, प्रस्तावित प्रतिमा की वह प्रथम रेखानुकृति अब उसे अच्छी तरह समझ में आने लगी। वह बार-बार बाहबली का ही चिन्तन करके उनके व्यक्तित्व को अपनी कल्पना में सांगोपांग साकार कर लेने में संलग्न हो गया। विन्ध्यगिरि की शिला पर अभी
११६ / गोमटेश-गाथा