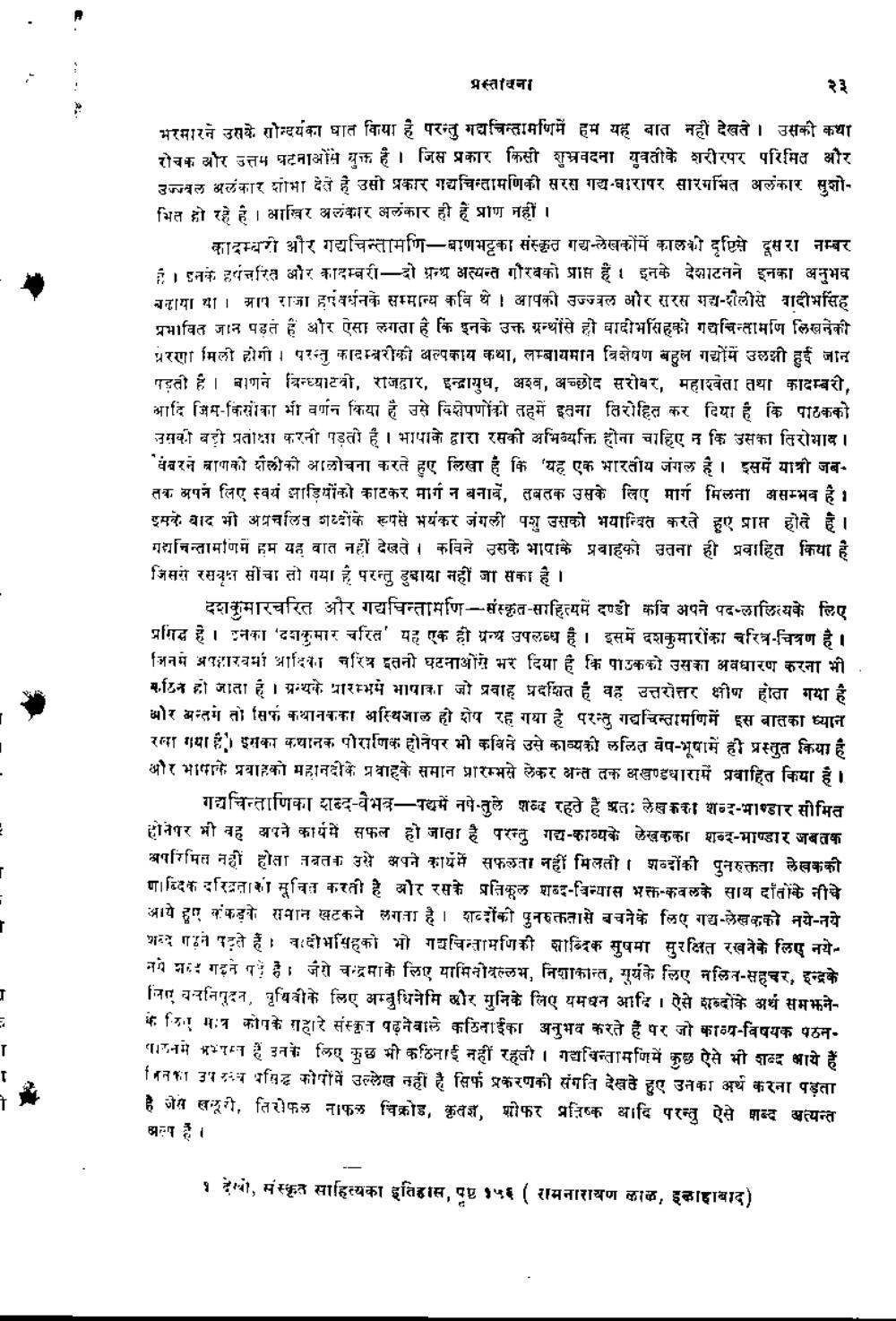________________
प्रस्तावना
भरमारने उसके सौन्दर्यका घात विया है परन्तु गद्यचिन्तामणिमें हम यह बात नहीं देखते। उसकी कथा सोचक और उत्तम घटनाओंसे युक्त है। जिस प्रकार किसी शुभ्रवदना युवतीके शरीरपर परिमित और उज्जवल अलंकार शोभा देते है उसी प्रकार गद्यचिन्तामणिकी सरस गद्य-धारापर सारगर्भित अलंकार सुशोभित हो रहे है । आखिर अलंकार अलंकार ही है प्राण नहीं ।
कादम्बरी और गद्यचिन्तामणि-बाणभट्टका संस्कृत गद्य-लेखकोंमें कालको दृष्टिसे दूसरा नम्बर
नक हपंचरित और कादम्बरी-दो अन्ध अत्यन्त गौरबको प्राप्त है। इनके देशाटनने इनका अनुभव बनाया था। मा राजा हरवर्धनके सम्मान्य कवि थे। आपकी उज्ज्वल और सरस गद्य-दौलीसे वादीसिंह प्रभावित जान पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इनके उक्त ग्रन्थोंसे ही बादीभसिंहको गद्यचिन्तामणि लिखनेकी प्ररणा मिली होगी। परन्तु कादम्बरीकी बल्पकाय कथा, लम्बायमान विशेषण बहुल गद्योंमें उलझी हुई जान पड़ती है। बाणने बिन्ध्याटवी, राजद्वार, इन्द्रायुध, अश्व, अच्छोद सरोबर, महारवेता तथा कादम्बरी, आदि जिम-किसका भी वर्णन किया है उसे विशेपणोंकी तहमें इतना तिरोहित कर दिया है कि पाठकको जसकी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । भाषाके द्वारा रसको अभिव्यक्ति होना चाहिए न कि उसका तिरोभाव । 'वंबरने बाणको शैली को आलोचना करते हुए लिखा है कि 'यह एक भारतीय जंगल है। इसमें यात्री जब. तक अपन लिए स्वयं झाड़ियों को काटकर मार्ग न बनावें, तबतक उसके लिए मार्ग मिलना असम्भव है। इसके बाद भी अप्रचलित शब्दोंके रूपसे भयंकर जंगली पशु उसको भयान्वित करते हुए प्राप्त होते है। गनिन्तामणिम हम यह बात नहीं देखते। कविने उसके भापाके प्रवाहको उतना ही प्रवाहित किया है जिससे रसवक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुबाया नहीं जा सका है।
दशकुमारचरित और गद्यचिन्तामणि-संस्कृत-साहित्यमें दण्डी कवि अपने पद-लालित्यके लिए प्रसिद्ध है। इनका 'दशकुमार चरित' यह एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें दशकुमारोंका चरित्र-चित्रण है। जिनमे अपहारवा आदिवा चरित्र इतनी घटनाओंगे भर दिया है कि पाठकको उसका अवधारण करना भी कठिन हो जाता है । ग्रन्थके प्रारम्भमे भाषाका जो प्रवाह प्रदर्शित है वह उत्तरोत्तर क्षीण होता गया है और अन्तम तो सिर्फ कथानका अस्थिजाल हो शेष रह गया है परन्तु गद्यचिन्तामणिमें इस बातका ध्यान रखा गया है। इसका कथानक पौराणिक होनेपर भी कविने उसे काव्यको ललित वेष-भूषामें ही प्रस्तुत किया है और भापाके प्रवाहको महानदीके प्रवाहके समान प्रारम्भसे लेकर अन्त तक अखण्डधारामें प्रवाहित किया है।
गद्यचिन्ताणिका शब्द-वैभव-पद्यमें नपे-तुले शब्द रहते हैं अतः लेखकका शब्द-भाण्डार सीमित होनेपर भी वह अपने कार्य में सफल हो जाता है परन्तु गद्य-काव्यके लेखकका शब्द-माण्डार जबतक अपरिमित नहीं होता तबतक उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। शब्दोंकी पुनरुक्तता लेखककी ण। ब्दिक दरिद्रताका मूचित करती है और रसके प्रतिकूल शब्द-विन्यास भक्त-कवलके साथ दाँतोंके नीचे आये हुए कंकड़ो समान खटकने लगता है। शब्दोंकी पुनरुक्ततासे बचने के लिए गद्य-लेखकको नये-नये शब्द पने पढ़ते हैं। वादीमिहको भो गचितामणिकी शाब्दिक सुषमा सुरक्षित रखने के लिए नयेनये शाः गढ़ने पड़े हैं। जैसे चन्द्रमाके लिए यामिनीवल्लभ, निशाकान्त, गुर्य के लिए नलिन-सहचर, इन्द्रके लिए चरनिदन, पृथिवीके लिए अम्बुधिनेमि और मुनिके लिए यमधन आदि । ऐसे शब्दोंके अर्थ समझनेकमिा मात्र कोपके सहारे संस्कृत पढ़नेवाले कठिनाईका अनुभव करते हैं पर जो काव्य-विषयक पठनपारनमे अपम्न हैं उनके लिए कुछ भी कठिनाई नहीं रहती। गद्यचिन्तामणिमें कुछ ऐसे भी शब्द आये हैं जिनका उपरत्र सिद्ध कोपों में उल्लेख नहीं है सिर्फ प्रकरणकी संगति देखते हुए उनका अर्थ करना पड़ता है जेस खलूग, तिरोफल नाफल चिक्रोड, कृतज्ञ, शोफर प्रतिष्क आदि परन्तु ऐसे शब्द अत्यन्त
1
-
-
-
१ देवी, संस्कृत साहित्यका इतिहास, पृष्ट १५६ ( रामनारायण काल, इलाहाबाद)