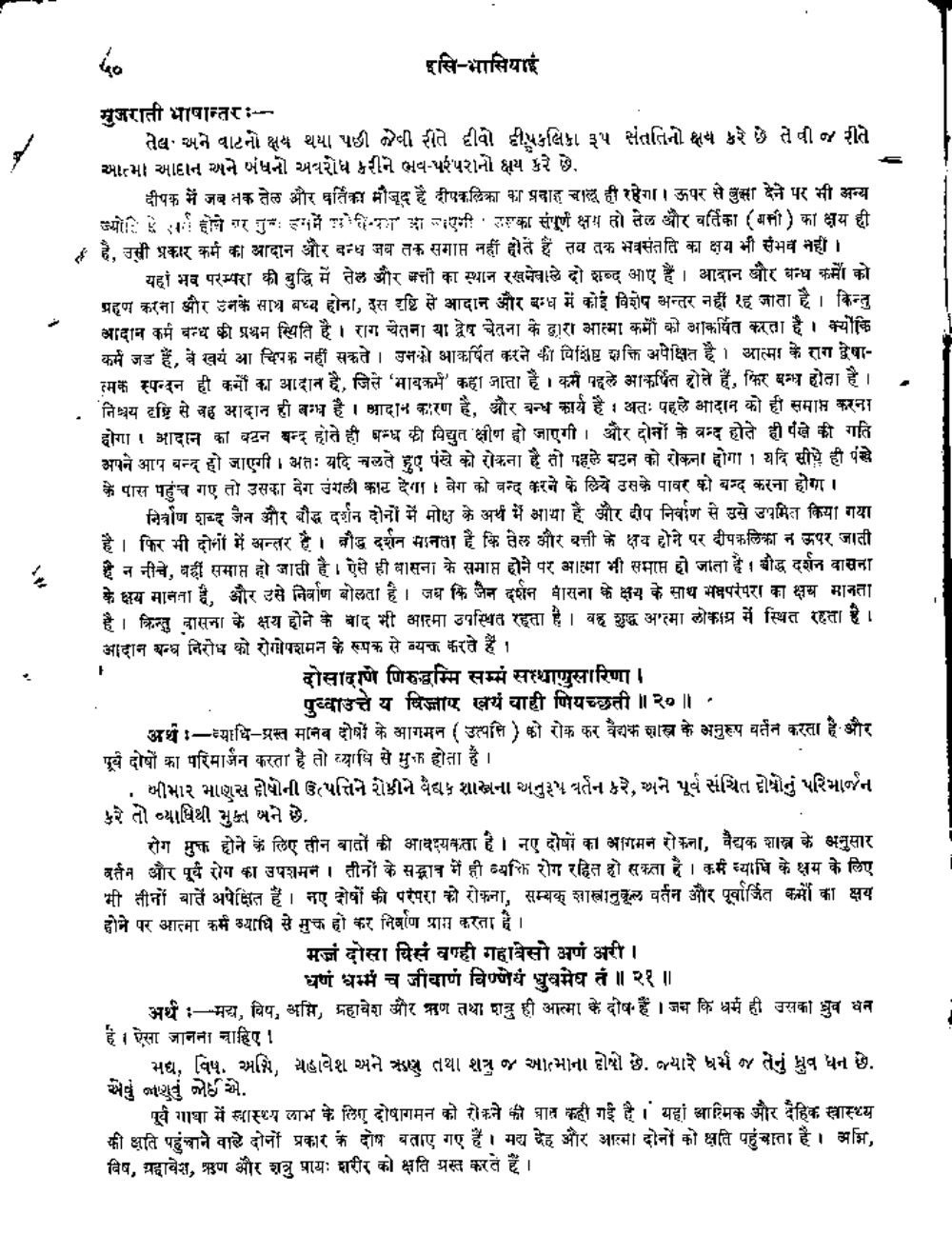________________
10
गुजराती भाषान्तर:
તેલ અને વાટનો ક્ષય થયા પછી જેવી રીતે દીવો દીપકલિકા રૂપ સંતતિનો ક્ષય કરે છે તેવી જ રીતે આત્મા આદાન અને બંધનો અવરોધ કરીને ભવ-પરંપરાનો હ્રાય કરે છે.
दीपक में जब तक तेल और वर्तिका मौजूद हैं दीपकलिका का प्रवाह चालू ही रहेगा। ऊपर से बुझा देने पर भी अन्य ज्योति होने पर आएगी उसका संपूर्ण क्षय तो तेल और वर्तिका (गती) का क्षय ही है, उसी प्रकार कर्म का आदान और बन्ध जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक भवसंतति का क्षय भी संभव नहीं ।
इसि - भासियाई
यहाँ भव परम्परा की बुद्धि में तेल और बत्ती का स्थान रखनेवाले दो शब्द आए हैं। आदान और बन्ध कर्मों को ग्रहण करना और उनके साथ बध्य होना, इस दृष्टि से आदान और बन्ध में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता है। किन्तु आदान कर्म बन्ध की प्रथम स्थिति है। राग चेतना या द्वेष चेतना के द्वारा आत्मा कर्मों को आकर्षित करता है। क्योंकि कर्म जड हैं, वे खर्य आ चिपक नहीं सकते। उनको आकर्षित करने की विशिष्ट शक्ति अपेक्षित है। आत्मा के राग द्वेषात्मक स्पन्दन ही कर्मों का आदान है, जिसे 'भावकर्म' कहा जाता है। कर्म पहले आकर्षित होते हैं, फिर बन्ध होता है। निश्चय दृष्टि से वह आदान ही बन्ध है | आदान कारण है, और बन्ध कार्य है । अतः पहले आदान को ही समाप्त करना होगा | आदान का बटन बन्द होते ही धन्ध की विद्युत क्षीण हो जाएगी। और दोनों के बन्द होते ही पंखे की गति अपने आप बन्द हो जाएगी। अतः यदि चलते हुए पंखे को रोकना है तो पहले बटन को रोकना होगा । यदि सीधे ही पंखे के पास पहुंच गए तो उसका वेग जंगली काट देगा । वेग को बन्द करने के लिये उसके पावर को बन्द करना होगा ।
निर्वाण शब्द जैन और बौद्ध दर्शन दोनों में मोक्ष के अर्थ में आया हैं और दीप निर्वाण से उसे उयमित किया गया है। फिर भी दोनों में अन्तर है। बौद्ध दर्शन मानता है कि तेल और बत्ती के क्षय होने पर दीपकलिका न ऊपर जाती है न नीचे, वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वासना के समाप्त होने पर आत्मा भी समाप्त हो जाता है। बौद्ध दर्शन वासना जब कि जैन दर्शन वासना के क्षय के साथ भयपरंपरा का क्षय मानता आत्मा उपस्थित रहता है। वह शुद्ध अत्मा लोकाग्र में स्थित रहता है । व्यक्त करते हैं ।
के क्षय मानता हैं, और उसे निर्माण बोलता है। है। किन्तु वासना के क्षय होने के बाद भी आदान घन्ध विरोध को रोगोपशमन के रूपक से
दोलादणे णिरुम्मि सम्मं सस्थागुसारिणा । पुव्वाउत्ते य विज्ञाय खयं चाही नियच्छती ॥ २० ॥
अर्थ-व्याधि- प्रस्त मानव दोषों के आगमन ( उत्पति) को रोक कर वैद्यक शास्त्र के अनुरूप वर्तन करता है और पूर्व दोषों का परिमार्जन करता है तो व्याधि से मुक्त होता है।
બીમાર માણસ દોષોની ઉત્પત્તિને રોકીને વૈદ્યક શાસ્ત્રના અનુરૂપ વર્તન કરે, અને પૂર્વ સંચિત દોષોનું પરિમાર્જન કરે તો ન્યાધિથી મુક્ત બને છે.
रोग मुक्त होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। नए दोषों का आगमन रोकना, वैद्यक शास्त्र के अनुसार वर्तन और पूर्व रोग का उपशमन । तीनों के सद्भाव में ही व्यक्ति रोग रहित हो सकता है। कर्म व्याधि के श्रम के लिए भी तीनों बातें अपेक्षित हैं। नए शेषों की परंपरा को रोकना, सम्यक् शास्त्रानुकूल वर्तन और पूर्वार्जित कर्मों का क्षय होने पर आत्मा कर्म व्याधि से मुक्त हो कर निर्माण प्राम करता है I
मज्जं दोसा यिसं वही गहावेसो अणं अरी ।
घणं धम्मं च जीवाणं विण्जेय धुवमेध तं ॥ २१ ॥
अर्थ :-मय, विष, अग्नि, महावेश और ऋण तथा शत्रु ही आत्मा के दोष हैं। जब कि धर्म ही उसका ध्रुव वन हैं । ऐसा जानना चाहिए 1
મદ્ય, વિધ. અગ્નિ, ચહાવેશ અને ઋણુ તથા શત્રુ જ આત્માના દોષો છે. જ્યારે ધર્મ જ તેનું ધ્રુવ ધન છે. એવું જાણવું જોઈ એ.
पूर्व गाथा में स्वास्थ्य लाभ के लिए दोषागमन को रोकने की बात कही गई है। यहां आत्मिक और दैहिक स्वास्थ्य की क्षति पहुंचाने वाले दोनों प्रकार के दोष बताए गए हैं। मद्य देह और आत्मा दोनों को क्षति पहुंचाता है। अभि विष, ग्रहावेश, ऋण और शत्रु प्रायः शरीर को क्षति ग्रस्त करते हैं।