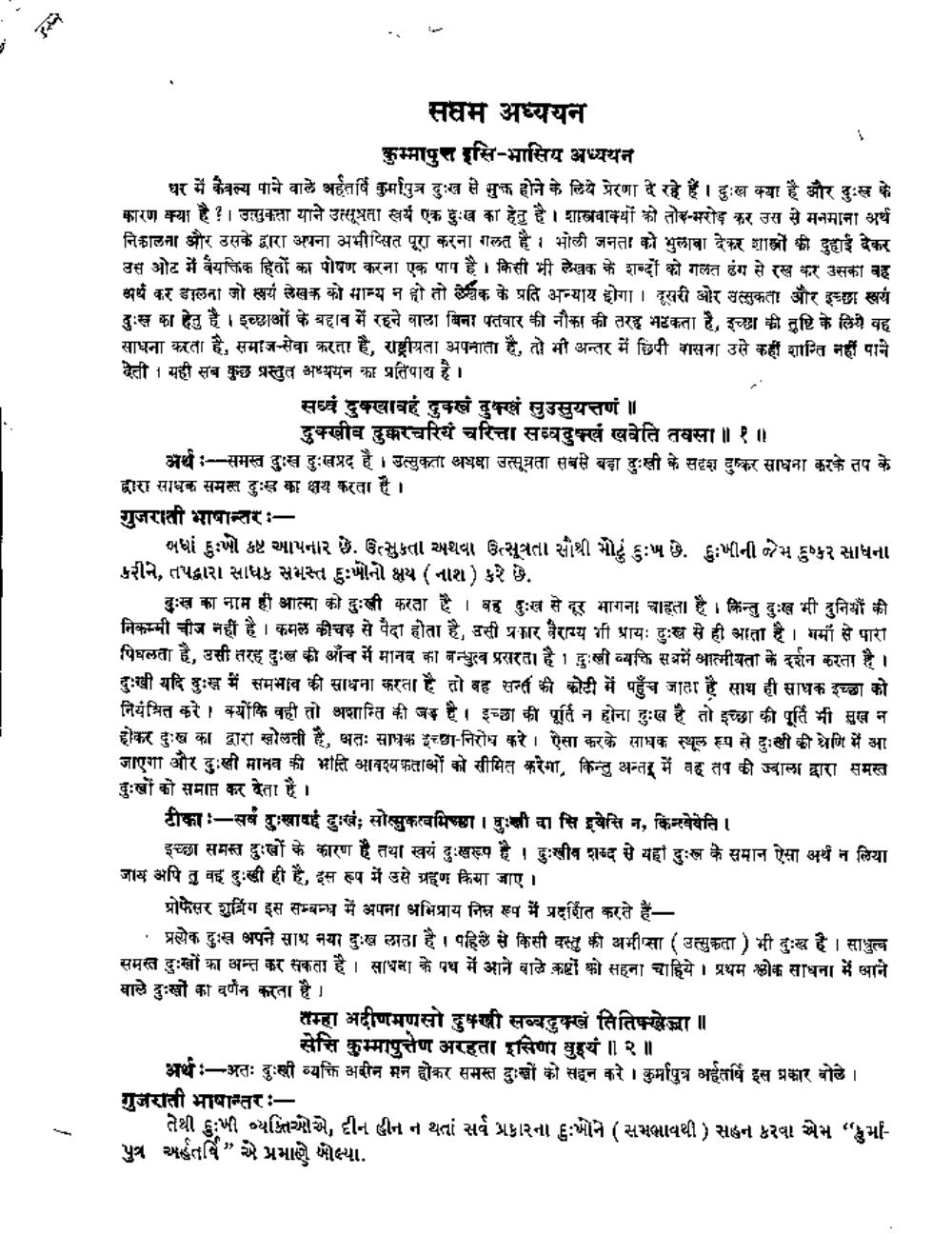________________
सक्षम अध्ययन
कुम्मापुस इसि-भासिय अध्ययन घर में कैवल्य पाने वाले अर्हतर्षि कुर्मापुत्र दुःख से मुक्त होने के लिये प्रेरणा दे रहे हैं। दुःख क्या है और दुःख के कारण क्या है ? । उत्सुकता याने उत्सूत्रता खर्य एक दुःख का हेतु है। शास्त्रवाक्यों को तोड़-मरोड़ कर उस से मनमाना अर्थ निकालना और उसके द्वारा अपना अभीप्सित पूरा करना गलत है। भोली जनता को भुलावा देकर शास्त्रों की दुहाई देकर उस ओट में वैयक्तिक हितों का पोषण करना एक पाप है। किसी भी लेखक के शब्दों को गलत ढंग से रख कर उसका वह अर्थ कर डालना जो स्वयं लेखक को मान्य न हो तो लेखक के प्रति अन्याय होगा। दूसरी ओर उत्सुकता और इच्छा स्वयं दुःस का हेतु है । इच्छाओं के बहाव में रहने वाला बिना पतवार की नौका की तरह भटकता है, इच्छा की तुष्टि के लिये वह साधना करता है, समाज-सेवा करता है, राष्ट्रीयता अपनाता है, तो भी अन्तर में छिपी गसना उसे कहीं शान्ति नहीं पाने देती । यही सब कुछ प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिपाद्य है।
सध्यं दुक्खावहं दुक्खं दुक्खं सुउसुयत्तणं ॥
दुक्खीव ठुकरचरियं चरित्ता सव्वदुक्खं खवेति तवसा ॥१॥ अर्थ:--समस्त दुःख दुःखप्रद है। उत्सुकता अथवा उत्सूत्रता सबसे बड़ा दुःखी के सदृश दुष्कर साधना करके तप के द्वारा साधक समस्त दुःस का क्षय करता है। गुजराती भाषान्तर:
બધાં દુઃખે કષ્ટ આપનાર છે. ઉત્સુકતા અથવા સૂત્રતા સૌથી મોટું દુ:ખ છે. દુઃખીની જેમ દુષ્કર સાધના કરીને, તપદ્વારા સાધક સમસ્ત દુઃખોનો ક્ષય (નાશ) કરે છે.
दुःख का नाम ही आत्मा को दुःखी करता है । वह दुःख से दूर भागना चाहता है। किन्तु दुःख भी दुनियों की निकम्मी चीज नहीं है । कमल कीचड़ से पैदा होता है, उसी प्रकार वैराग्य भी प्रायः दुःख से ही आता है। गर्मी से पारा पिघलता है, उसी तरह दुःख की आँच में मानव का बन्धुत्व प्रसरता है। दुःस्त्री व्यक्ति सत्रमें आत्मीयता के दर्शन करता है। दुःखी यदि दुःख में समभाव की साधना करता है तो वह सनत की कोटी में पहुँच जाता है साथ ही साधक इच्छा को नियंत्रित करे। क्योंकि वही तो अशान्ति की जड़ है। इच्छा की पूर्ति न होना दुःख है तो इच्छा की पूर्ति भी सुख न होकर दुःख का द्वारा खोलती है, अतः साधक इच्छा-निरोध करे। ऐसा करके साधक स्थूल रूप से दुःखी की श्रेणि में आ जाएगा और दुःखी मानव की भांति आवश्यकताओं को सीमित करेगा, किन्तु अन्तर में वह तप की ज्वाला द्वारा समस्त दुःखों को समाप्त कर देता है।
टीका:-सर्व दुःखापई दुःखं; सोत्सुकरवमिच्छा । घुःखी वा सि इवेसि न, किन्दवेवेति ।
इच्छा समस्त दुःखों के कारण है तथा खयं दुःखरूप है। दुःखीव शब्द से यहां दुःख के समान ऐसा अर्थ न लिया जाय अपि तु वह दुःखी ही है, इस रूप में उसे ग्रहण किया जाए।
प्रोफेसर शुर्बिग इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं• प्रत्येक दुःस अपने साथ नया दुःख लाता है। पहिले से किसी वस्तु की अभीप्सा ( उत्सुकता) भी दुःख है। साधुत्व समस्त दुःखों का अन्त कर सकता है। साधना के पथ में आने वाले कष्टों को सहना चाहिये। प्रथम श्लोक साधना में आने वाले दुःखों का वर्णन करता है।
तम्हा अदीणमणसो दुक्खी सब्बदुक्खं तितिखेजा ॥
सेसि कुम्मापुत्तेण अरहता इसिणा वुइयं ॥ २॥ अर्थ:-अतः दुःखी व्यक्ति अदीन मन होकर समस्त दुःखों को सहन करे । कुर्मापुत्र अर्हतर्षि इस प्रकार बोले । गुजराती भाषान्तर:
તેથી દુખી વ્યક્તિઓએ, દીન હીન ન થતાં સર્વ પ્રકારના દુઓને (સમભાવથી સહન કરવા એમ “કુમપુત્ર અહંતર્વિ” એ પ્રમાણે ઓલ્યા.