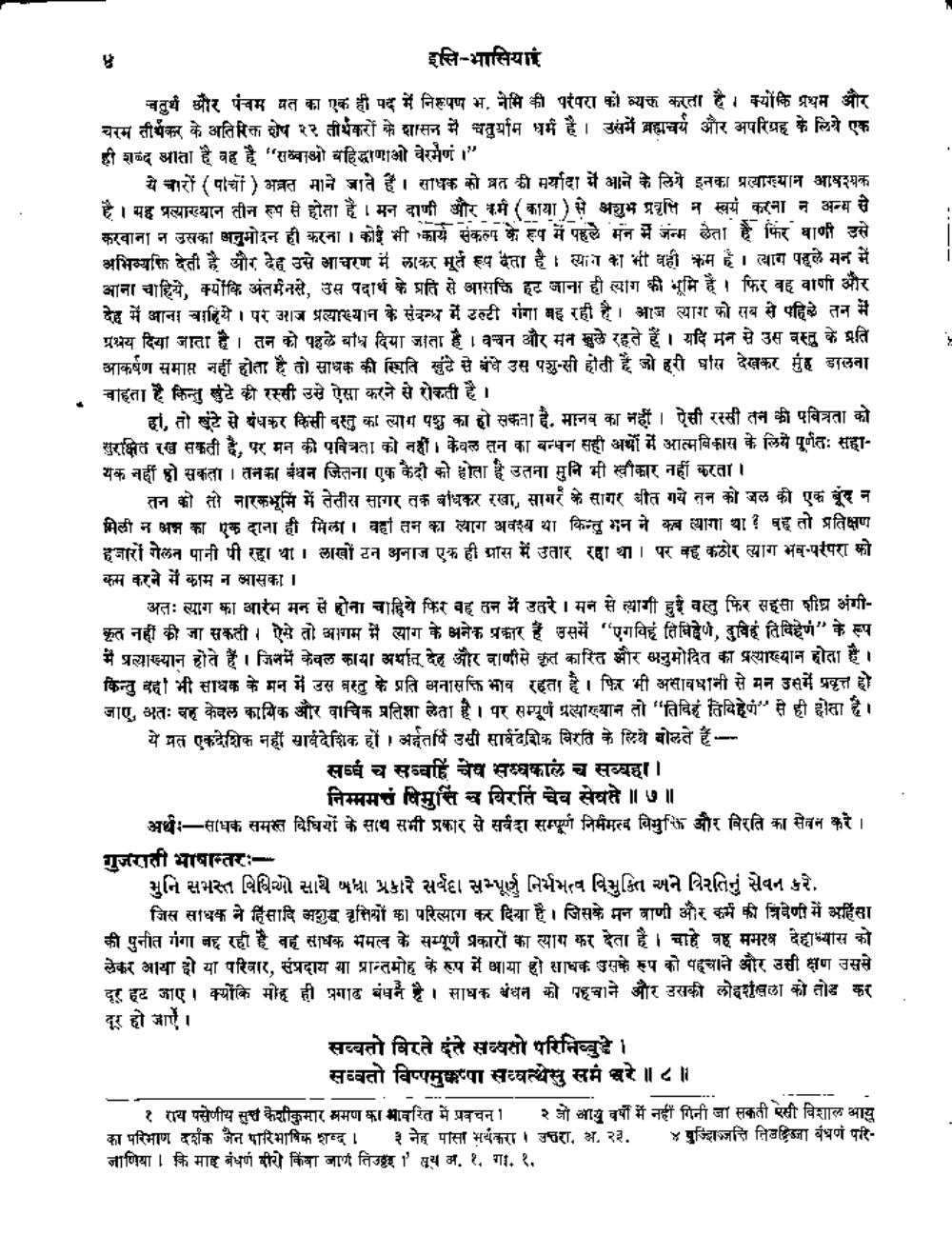________________
इसि-भासिया
चतुर्थ और पंचम यत का एक ही पद में निरूपण भ, नेमि की परंपरा को व्यक्त करता है। क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थकर के अतिरिक्त शेष २२ तीर्थकरों के शासन में चतुर्याम धर्म है। उसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के लिये एक ही शब्द आता है वह है "राठवाओ बहिद्धाणाओ बेरमैणं ।"
ये चारों (पांचा) अव्रत माने जाते हैं। साधक को व्रत की मर्यादा में आने के लिये इनका प्रत्याख्यान आवश्यक है। यह प्रत्याख्यान तीन रूप से होता है । मन दाणी और कर्म (काया) से अशुभ प्रवृत्ति म स्वयं करना न अन्य से करवाना न उसका अनुमोदन ही करना । कोई भी कार्य संकल्प के रूप में पहले मन में जन्म लेता है फिर पाणी उसे अभिव्यक्ति देती है और देह उसे आचरण में लाकर मूर्त रूप देता है। स्याग का भी वही क्रम है। त्याग पहले मन में आना चाहिये, क्योंकि अंतर्मनसे, उस पदार्थ के प्रति से आसकि हट जाना ही त्याग की भूमि हैं। फिर वह वाणी और देह में आना चाहिये। पर आज प्रत्यास्यान के संबन्ध में उल्टी गंगा बह रही है। आज त्याग को सब से पहिले तन में प्रश्रय दिया जाता है। तन को पहले बांध दिया जाता है। वचन और मन खुले रहते हैं। यदि मन से उस वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं होता है तो साधक की स्थिति खंदे से बंधे उस पशु-सी होती हैं जो हरी घास देखकर मुंह डालना चाहता है किन्तु खुंटे की रस्सी उसे ऐसा करने से रोकती है।
हो, तो खंटे से बंधकर किसी वस्तु का त्याग पश का हो सकता है. मानव का नहीं। ऐसी रस्सी तन की पवित्रता को सुरक्षित रख सकती है, पर मन की पवित्रता को नहीं। केवल तन का बन्धन सही अर्थों में आत्मविकास के लिये पूर्णतः सहायक नहीं हो सकता । तनका बंधन जितना एक कैदी को होता है उतना मुनि भी स्वीकार नहीं करता।
तन को तो नारकभूमि में तेतीस सागर तक बांधकर रखा, सागर के सागर बीत गये तन को जल की एक बूंद न मिली न अन्न का एक दाना ही मिला। वहाँ तन का त्याग अवश्य था किन्तु मन ने कब त्यागा था। वह तो प्रतिक्षण हजारों गेलन पानी पी रहा था। लाखों टन अनाज एक ही ग्रास में उतार रहा था। पर वह कठोर त्याग भव-परंपरा को कम करने में काम न आसका।
अतः त्याग का आरंभ मन से होना चाहिये फिर वह तन में उतरे। मन से त्यागी हुई वस्तु फिर सहसा शीघ्र अंगीकृत नहीं की जा सकती। ऐसे तो आगम में त्याग के अनेक प्रकार हैं उसमें “एगविहं ति बिदेणे, दुविहं तिविहेण" के रूप मैं प्रत्याख्यान होते हैं। जिनमें केवल काया अर्थात देह और वाणीसे कृत कारित और अनुमोदित का प्रत्याख्यान होता है। किन्तु यह भी साधक के मन में उस वस्तु के प्रति अनासक्ति भाव रहता है। फिर भी असावधानी से मन उसमें प्रवृत्त हो जाए, अतः वह केवल कायिक और वाचिक प्रतिज्ञा लेता है। पर सम्पूर्ण प्रत्याख्यान तो "तिविहं तिविहेण" से ही होता है। ये प्रत एकदेशिक नहीं सार्वदेशिक हो । अतिर्षि उसी सार्वदेशिक विरति के लिये बोलते हैं---
सधं च सम्वहि चेव सयकाल च सव्यहा।
निम्ममत्तं विमुसिं च विरतिं चेव सेवते ॥७॥ अर्थः-साधक समस्त विधियों के साथ सभी प्रकार से सर्वदा सम्पूर्ण निर्ममत्व विमुक्ति और विरति का सेवन करें। गुजराती भाषान्तरः
મુનિ સમસ્ત વિધિઓ સાથે બધા પ્રકારે સર્વદા સપૂર્ણ નિર્મમત્વ વિમુક્તિ અને વિરતિનું સેવન કરે,
जिस साधक ने हिंसादि अशुद्ध वृसियों का परित्याग कर दिया है। जिसके मन वाणी और कर्म की त्रिवेणी में अहिंसा की पुनीत गंगा नद्द रही है वह साधक ममल के सम्पूर्ण प्रकारों का त्याग कर देता है। चाहे वह ममरव देहाच्यास को लेकर आया हो या परिवार, संप्रदाय या प्रान्तमोह के रूप में आया हो साधक उसके रूप को पहचाने और उसी क्षण उससे दूर हट जाए। क्योंकि मोह ही प्रगाढ बंधन है। साधक बंधन को पहचाने और उसकी लोदशंखला को तोड कर दूर हो जाएँ।
सब्बतो बिरते दंते सव्यतो परिनिब्बुद्ध।
सवतो विप्पमुक्कप्पा सव्यस्थेसु समं बरे ॥ ८ ॥ १ राय पसेणीय सुस्त केशीकुमार प्रमण का भावरित में प्रवचन। जो आय वर्षों में नहीं गिनी जा सकती ऐसी विशाल आयु का परिमाण दर्शक जैन पारिभाषिक शब्द। ३ नेह पासा भयंकरा । उत्तरा, अ. २३. पुद्धिाजत्ति तिबहिजा बंधणं परिनाणिया । कि माह बंधर्ण वीरो किंवा जाणं तिउछ । सूर्य म. १, गा. १,