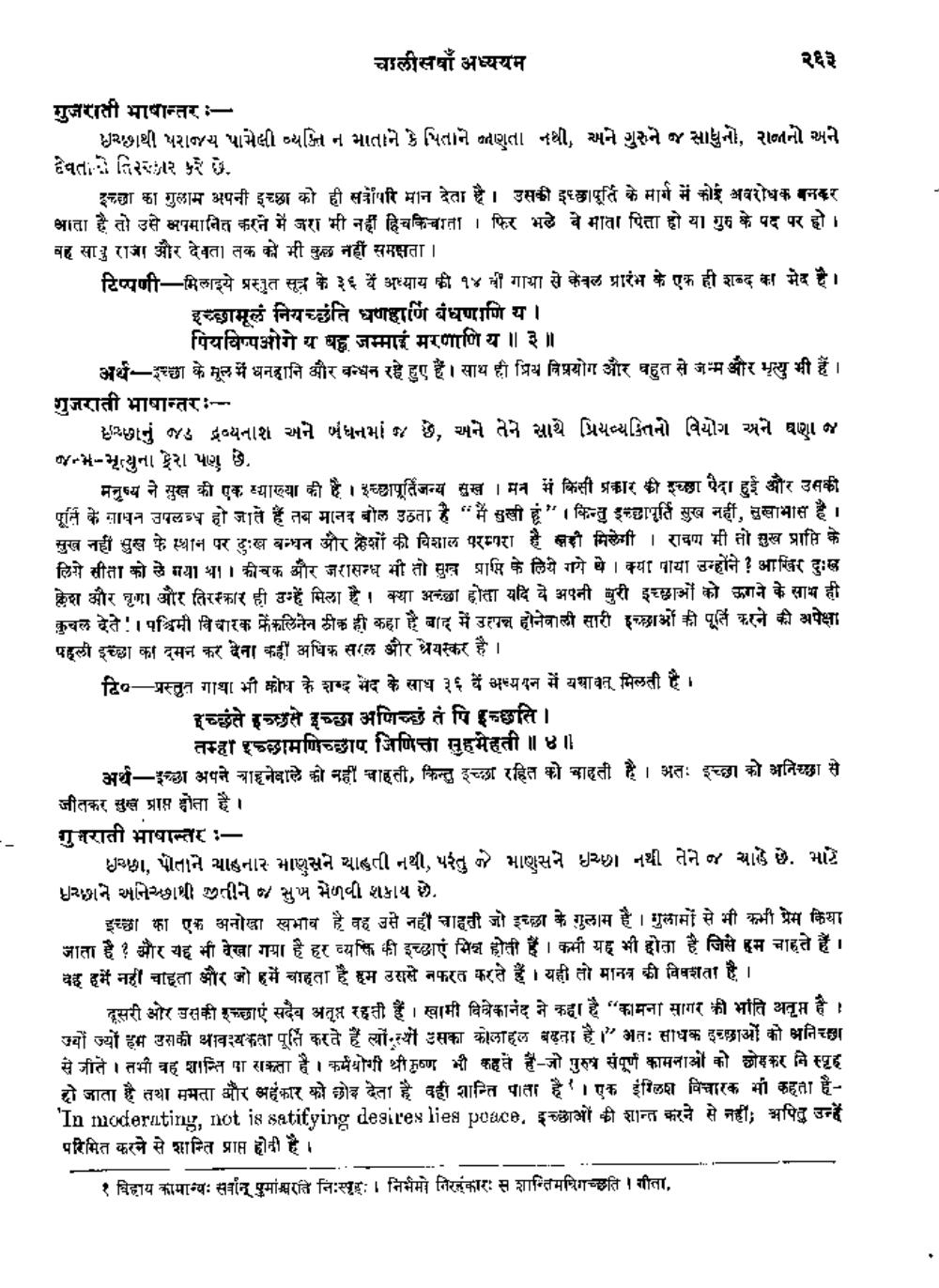________________
चालीसवाँ अध्ययन
२६३
गुजराती भाषान्तर:
ઇચ્છાથી પરાજય પામેલી વ્યક્તિ ન માતાને કે પિતાને જાણતા નથી, અને ગુરુને જ સાધુને, રાજાનો અને દેવતો વિરહાર કરે છે,
इच्छा का गुलाम अपनी इच्छा को ही सापरि मान देता है। उसकी इच्छापूर्ति के मार्ग में कोई अवरोधक बनकर आता है तो उसे अपमानित करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता । फिर भले वे माता पिता हो या गुरु के पद पर हो। वह साधु राजा और देवता तक को भी कुछ नहीं समझता । टिप्पणी-मिलाइये प्रस्तुत सूत्र के ३६ वें अध्याय की १४ वीं गाया से केवल प्रारंभ के एक ही शब्द का भेद है।
इच्छामूलं नियच्छति धणहाणि बंधणाणि य ।
पियविपओगे य बल जम्माई मरणाणि य ॥ ३॥ अर्थ-इच्छा के मूल में धनहानि और बन्धन रहे हुए हैं। साथ ही प्रिय विप्रयोग और बहुत से जन्म और मृत्यु भी हैं। गुजराती भाषान्तर:--
ઇચ્છાનું જડ દ્રવ્યનાશ અને બંધનમાં જ છે, અને તેને સાથે પ્રિયવ્યકિતને વિયોગ અને ઘણા જ -मृत्युना ३१ प .
मनुष्य ने सुख की एक व्याख्या की है। इच्छापूर्तिजन्य सुख । मन में किसी प्रकार की इच्छा पैदा हुई और उसकी पूर्ति के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तब मानद बोल उठता है "मैं सुखी हूं"। किन्तु इच्छापूर्ति सुख नहीं, सुखाभास है। मुख नहीं सुख के स्थान पर दुःख बन्धन और केशों की विशाल परम्परा है सही मिलेगी । रावण मी तो सुख प्राप्ति के लिये सीता को ले गया था। कीचक और जरासन्ध भी तो सुख प्राप्ति के लिये गये थे । क्या पाया उन्होंने ? आखिर दुःख क्लेश और चूगा और तिरस्कार ही उन्हें मिला है। क्या अच्छा होता यदि वे अपनी बुरी इच्छाओं को ऊगने के साथ ही कुचल देते । पश्चिमी विचारक फ्रेंकलिनेन ठीक ही कहा है बाद में उत्पन्न होनेवाली सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की अपेक्षा पहली इच्छा का दमन कर देना कहीं अधिक साल और श्रेयस्कर है। टिष-प्रस्तुत गाथा भी क्रोध के शम्द मेद के साध ३६ में अध्ययन में यथाक्त मिलती है।
इच्छते इच्छसे इच्छा अणिच्छं ते पि इच्छति ।
तम्हा इच्छामणिच्छाप जिणित्ता सुहमेहती ॥ ४॥ अर्थ-इच्छा अपने चाहनेवाले को नहीं चाहती, किन्तु इच्छा रहित को चाहती है। अतः इच्छा को अनिच्छा से जीतकर सुख प्राप्त होता है। गुजराती भाषान्तर:
ઈચ્છા, પોતાને ચાહનાર માણસને ચાહતી નથી, પરંતુ જે માણસને ઈચ્છા નથી તેને જ ચાહે છે. માટે ઈચ્છાને અનિચ્છાથી જીતીને જ સુખ મેળવી શકાય છે.
इच्छा का एक अनोखा स्वभाव है वह उसे नहीं चाहती जो इच्छा के गुलाम है । गुलामों से भी कभी प्रेम किया जाता है ? और यह भी देखा गया है हर व्यक्ति की इच्छाएं मिन्न होती हैं। की यह भी होता है जिसे हम चाहते हैं। वह हमें नहीं चाहता और जो हमें चाहता है हम उससे नफरत करते हैं। यही तो मानत्र की विवशता है।
दूसरी ओर उसकी इच्छाएं सदैव अतृप्त रहती हैं । स्वामी विवेकानंद ने कहा है “कामना सागर की भांति अतृप्त है। ज्यों ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं यो त्यो उसका कोलाहल बढ़ता है। अतः साधक इच्छाओं को अनिच्छा से जीते। तभी वह शान्ति पा सकता है। कर्मयोगी श्री कृष्ण भी कहते है-जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर नि स्पृह हो जाता है तथा ममता और अहंकार को छोड़ देता है वही शान्ति पाता है। एक इंग्लिश विचारक भी कहता हैIn moderutiny, not is satifying desires lies peace, इच्छाओं की शान्त करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शान्ति प्राप्त होती है।
१ विहाय कामान्यः सर्वान् एमांश्चरति निःस्पृहः । निर्भमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । गीता,