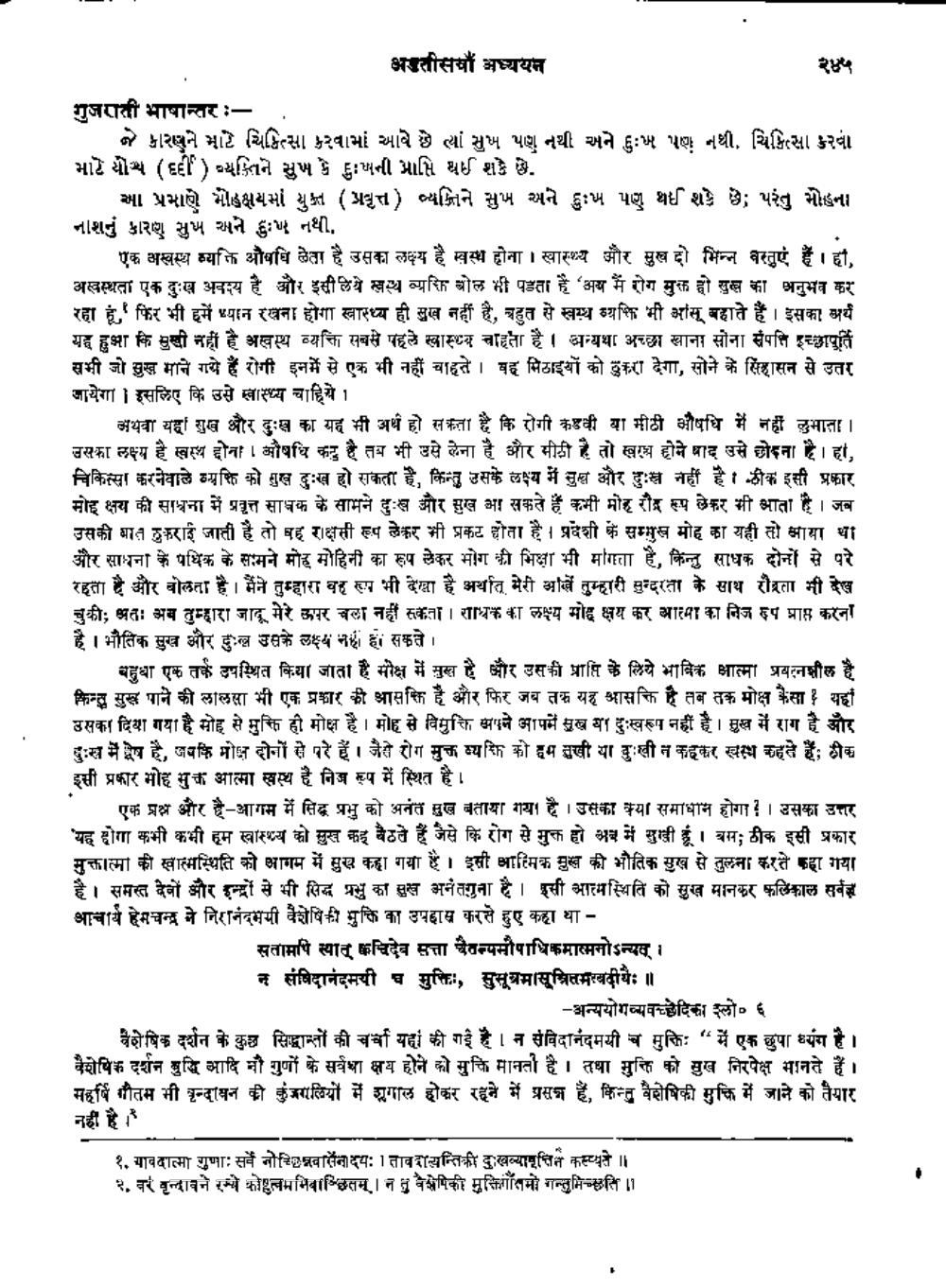________________
अडतीसवाँ अध्ययन
२४५ गुजराती भाषान्तर:
જે કારણને માટે ચિકિત્સા કરવામાં આવે છે ત્યાં સુખ પણ નથી અને દુઃખ પણ નથી, ચિકિત્સા કરવા માટે યોગ્ય (દદ) વ્યક્તિને સુખ કે દુઃખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
આ પ્રમાણે મહાયમાં યુક્ત (પ્રવૃત્ત) વ્યક્તિને સુખ અને દુઃખ પણ થઈ શકે છે, પરંતુ મોહના નાશનું કારણ સુખ અને દુઃખ નથી,
एक अस्वस्थ व्यक्ति औषधि लेता है उसका लक्ष्य है स्वस्थ होना । खास्थ्य और सुख दो भिन्न वस्तुएं हैं। हां, अखस्थता एक दुःख अवश्य है और इसीलिये स्वस्थ व्यक्ति बोल भी पड़ता है 'अब मैं रोग मुक्त हो सुख का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी हमें ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य ही सुख नहीं है, बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी आंसू बहाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुखी नहीं है अखस्थ व्यक्ति सबसे पहले स्वास्थ्य चाहता है। अन्यथा अच्छा स्वाना सोना संपत्ति इच्छापूर्ति सभी जो सुख माने गये हैं रोगी इनमें से एक भी नहीं चाहते। वह मिठाइयों को करा देगा, सोने के सिंहासन से उत्तर जायेगा। इसलिए कि उसे स्वास्थ्य चाहिये।
____ अथवा यहा सुख और दुःख का यह भी अर्थ हो सकता है कि रोगी कडवी या मीठी औषधि में नहीं लुभाता। उसका लक्ष्य है स्वस्थ होना । औषधि कटु है तब भी उसे लेना है और मीठी है तो वरच होने बाद उसे छोड़ना है। हा, चिकित्सा करनेवाले व्यक्ति को सुख दुःख हो सकता है, किन्तु उसके लक्ष्य में सुख और दुःस्त्र नहीं है। ठीक इसी प्रकार मोह क्षय की साधना में प्रवृत्त साधक के सामने दुःख और सुख आ सकते हैं कभी मोह रौद्र रूप लेकर भी आता है। जब उसकी बात कराई जाती है तो वह राक्षसी रूप लेकर भी प्रकट होता है। प्रदेश के सम्मुख मोह का यही तो भाया था
और साधना के पधिक के सामने मोह मोहिनी का रूप लेकर भोग की भिक्षा भी मांगता है, किन्तु साधक दोनों से परे रहता है और बोलता है। मैंने तुम्हारा वह रूप भी देखा है अर्थात मेरी आखें तुम्हारी सुन्दरता के साथ रौद्रता मी देख चुकी; अत: अब तुम्हारा जादू मेरे ऊपर चला नहीं सकता। साधक का लक्ष्य मोह क्षय कर आत्मा का निजरूप प्राप्त है । भौतिक सुख और दुःन्त्र उसके लक्ष्य नहीं हो सकते।
एक तर्क उपस्थित किया जाता है मोक्ष में मुस्त है और उसकी प्राप्ति के लिये भाविक आत्मा प्रयत्नशील है किन्तु सुख पाने की लालसा भी एक प्रकार की आसक्ति है और फिर जब तक यह आसक्ति है तब तक मोक्ष कैसा है यहाँ उसका दिया गया है मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। मोह से विमुक्ति अपने आपमें सुख या दुःस्वरूप नहीं है। मुख में राग है और दुःस में शेष है, जबकि मोक्ष दोनों से परे हैं। जैसे रोग मुक्त व्यक्ति को हम सुखी या दुःखी न कहकर स्वस्थ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मोह मुक आत्मा स्वस्थ है निज रूप में स्थित है।
एक प्रश्न और है-आगम में सिद्ध प्रभु को अनंत मुख बताया गया है । उसका क्या समाधान होगा! । उसका उत्तर 'यह होगा कभी कभी हम स्वास्थ्य को सुख कड् बैठते हैं जैसे कि रोग से मुक्त हो अब में सुखी हूं। बम ठीक इसी प्रकार मुक्तात्मा की खात्मस्थिति को आगम में सुख कहा गया है। इसी आस्मिक मुख की भौतिक सुख से तुलना करते कहा गया है। समस्त देनों और इन्द्रों से भी सिद्ध प्रभु का सुख अनंतगुना है। इसी आत्मस्थिति को सुख मानकर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने निरानंदमयी वैशेषिकी मुक्ति का उपहास करते हुए कहा था -
सतामपि स्यात् कचिदेव सत्ता चैतन्पमोपाधिकमात्मनोऽन्यत् । न संचिदानंदमयी घ मुक्तिः, सुसूत्रमासूनितमरखदीयैः ॥
-अन्ययोगव्यवच्छेदिका इलो०६ वैशेषिक दर्शन के कुछ सिद्धान्तों की चर्चा यहां की गई है । न संविदानंदमयी च मुक्तिः " में एक छुपा ध्यंग है।
आदि नौ गुणों के सर्वथा क्षय होने को मुक्ति मानती है। तथा मुक्ति को सुख निरपेक्ष मानते हैं। महर्षि गौतम भी वृन्दावन की कुंजगलियों में शूगाल होकर रहने में प्रसन्न है, किन्तु वैशेषिकी मुक्ति में जाने को तैयार नही है।
बहुध
वैशेषिक दर्शन बुद्धि आदि चौ गुण
१. यावदात्मा गुणाः सर्वे नोटिनवासेनादयः । तावदास्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिन कस्स्थते ।। २. वर वृन्दावने रम्ये कोष्ठत्वमभिवाचितम् । न तु वैश्ौमिकी मुक्तिगाँतमो गन्तुमिच्छति ।।