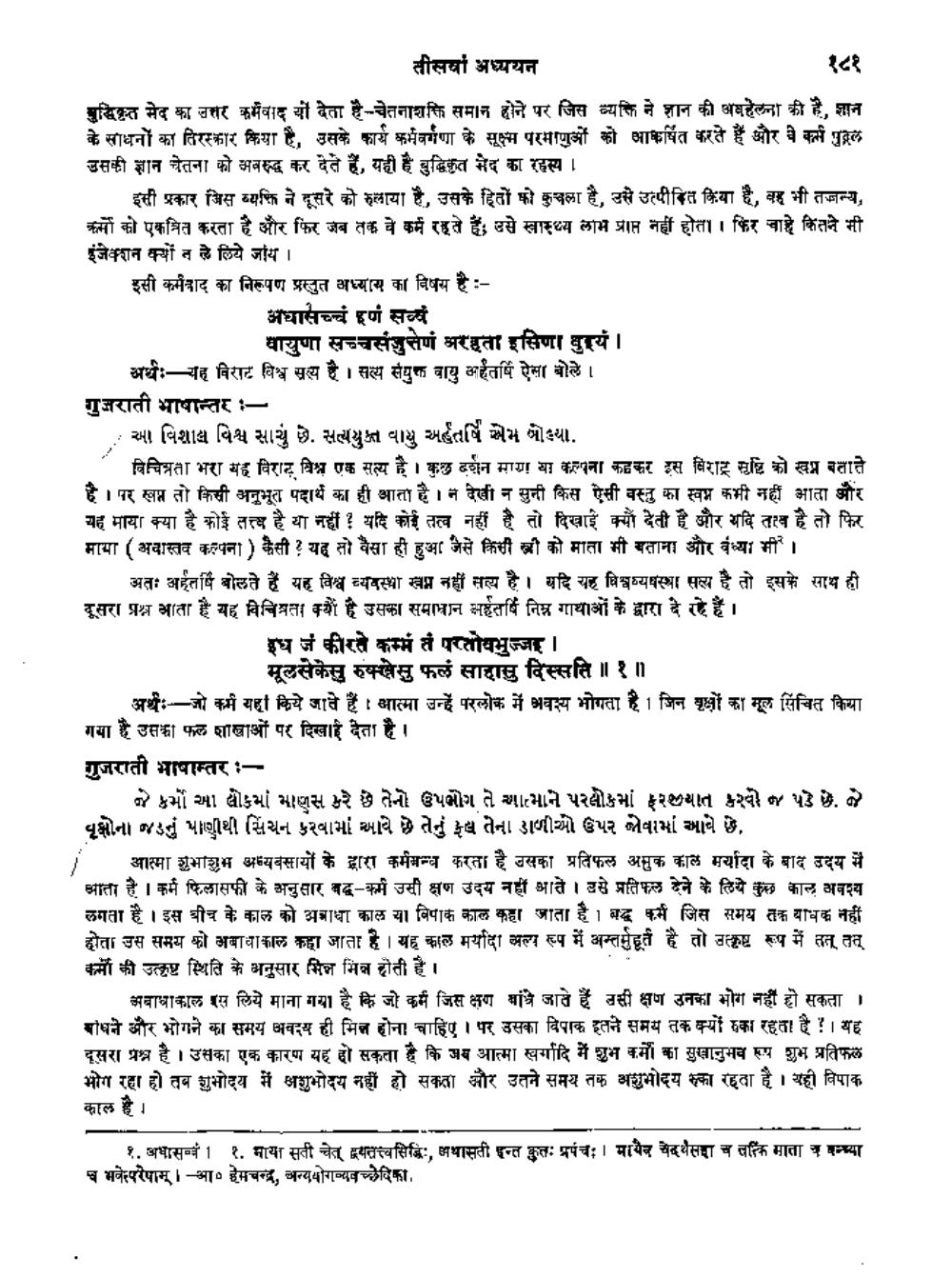________________
१८१
सीसा अध्ययन बुद्धिकृत मेद का उत्तर कर्मवाद यो देता है-चेतनाशक्ति समान होने पर जिस व्यक्ति ने ज्ञान की अवहेलना की है, ज्ञान के साधनों का तिरस्कार किया है, उसके कार्य कर्मवर्गणा के सूक्ष्म परमाणुओं को आकर्षित करते हैं और वे कर्म पुद्रल उसकी ज्ञान चेतना को अवरुद्ध कर देते हैं, यही है बुद्धिकृत मेद का रहस्य ।।
___ इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने दूसरे को रुलाया है, उसके हितों को कुचला है, उसे उत्पीरित किया है, वह भी तजन्य, ऋर्मों को एकत्रित करता है और फिर जब तक वे कर्म रहते हैं। उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं होता । फिर चाहे कितने भी इंजेक्शन क्यों न ले लिये जाय । इसी कर्मवाद का निरूपण प्रस्तुत अध्याय का विषय है :
अधासच्चं इणं सवं
वायुणा सच्चसंजुसेणं अरहता इसिणा वुइयं । अर्थः—यह विराट विश्व सत्य है । सत्य संयुक्त वायु अहंतर्षि ऐसा बोले । गुजराती भाषान्तर:
આ વિશાલ વિશ્વ સાચું છે. સત્યયુક્ત વાયુ અહંતર્ષિ એમ બેલ્યા.
विचित्रता भरा यह विराट विश्न एक सत्य है। कुछ दान मागा या कल्पना कहकर इस बिराट्र मुष्टि को खप्न बताते है। पर स्वप्न तो किसी अनुभूत पदार्थ का ही आता है। न देखी न सुनी किस ऐसी वस्तु का स्वप्न कभी नहीं आता और यह माया क्या है कोई तत्त्व है या नहीं ? यदि कोई तत्व नहीं है तो दिखाई क्यों देती है और यदि तत्व है तो फिर माया (अवास्तव कल्पना) कैसी? यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी स्त्री को माता भी बताना और वंध्या मी।
___ अतः अर्हतर्षि बोलते हैं यह विश्व व्यवस्था खप्न नहीं सत्य है। यदि यह विश्वव्यवस्था सत्य है तो इसके साथ ही दूसरा प्रश्न आता है यह विचित्रता क्यों है उसका समाधान महतर्षि निम्न गाथाओं के द्वारा दे रहे हैं।
इध ज कीरते कम्मं तं परतोषभुजह । ,
मूलसेकेसु रुक्लेसु फलं साहासु दिस्ससि ॥१॥ अर्थ:-जो कर्म यहां किये जाते हैं। आत्मा उन्हें परलोक में अवश्य भोगता है। जिन वृक्षों का मूल सिंचित किया गया है उसका फल शाखाओं पर दिखाई देता है। गुजराती भाषान्तर:
જે કમ આ લોકમાં માણસ કરે છે તેનો ઉપભોગ તે આત્માને પરલોકમાં ફરજીયાત કરવું જ પડે છે. જે વૃક્ષોના જડનું પાણીથી સિંચન કરવામાં આવે છે તેનું ફલ તેના ડાળીઓ ઉપર જોવામાં આવે છે,
आत्मा शुभाशुभ अध्यबसायों के द्वारा कर्मबन्ध करता है उसका प्रतिफल अमुक काल मर्यादा के बाद उदय में आता है । कर्म फिलासफी के अनुसार बद्ध-कर्म उसी क्षण उदय नहीं आते। उसे प्रतिफल देने के लिये कुछ काल अवश्य लगता है। इस बीच के काल को अबाधा काल या विपाक काल कहा जाता है। बद्ध कर्म जिस समय तक बाधक नहीं होता उस समय को अबाधाकाल कहा जाता है । यह काल मर्यादा अल्प रूप में अन्तर्मुहूर्त है तो उत्कृष्ट रूप में तत् तत् कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार मिन मिन्न होती है।
अबाधाकाल इस लिये माना गया है कि जो कर्म जिस क्षण बांधे जाते हैं उसी क्षण उनका भोग नहीं हो सकता । बोधने और भोगने का समय अवश्य ही भिन्न होना चाहिए । पर उसका विपाक इतने समय तक क्यों रुका रहता है । यह दूसरा प्रश्न है। उसका एक कारण यह हो सकता है कि अब आत्मा स्वर्गादि में शुभ कर्मों का सुखानुभव रूप शुभ प्रतिफल भोग रहा हो तब शुभोदय में अशुभोदय नहीं हो सकता और उतने समय तक अशुमोदय का रहता है । यही विपाक काल है।
१. अधासन्न । १. माया सती चेत् यतत्वसिद्धिः, अथासती इन्त कुतः प्रपंच: । मायैर चेदर्थसहा च चक्कि माता व पन्ध्या च भवेरपरेपाम् । -आ० हेमचन्द्र, अन्ययोगव्यवच्छेविका,