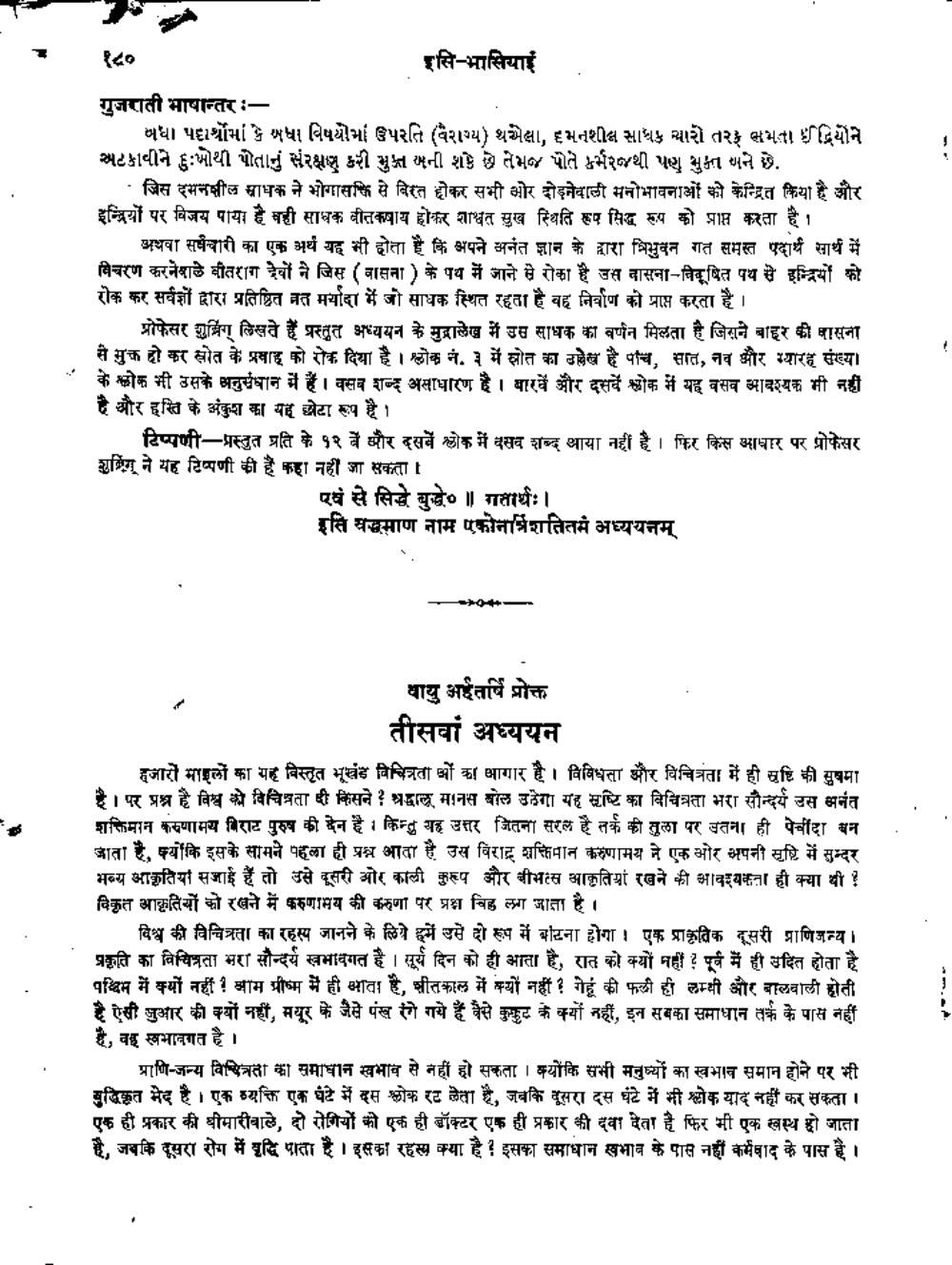________________
इस भासियाई
१८०
गुजराती भाषान्तर :
બધા પદાર્થોમાં કે અધા વિષયોમાં ઉપરતિ (વૈરાગ્ય) થએલા, દમનશીલ સાધક ચારો તરફ ભ્રમતા ઈદ્રિયોન અટકાવીને દુ:ખોથી પોતાનું સંરક્ષણુ કરી મુક્ત અની શકે છે તેમજ પોતે કર્મરજથી પણ મુક્ત બને છે.
जिस दमनशील साधक ने भोगासति से विरत होकर सभी और दोड़नेवाली मनोभावनाओं को केन्द्रित किया है और इन्द्रियों पर विजय पाया है वही साधक वीतकषाय होकर शाश्वत सुख स्थिति रूप सिद्ध रूप को प्राप्त करता है ।
अथवा सवारी का एक अर्थ यह भी होता है कि अपने अनंत ज्ञान के द्वारा त्रिभुवन गत समस्त पदार्थ सार्थ में विचरण करनेवाले वीतराग देवों ने जिस (वासना) के पथ में जाने से रोका है उस वासना- चिदूषित पथ से इन्द्रियों को रोक कर सर्वज्ञों द्वारा प्रतिष्ठित व्रत मर्यादा में जो साधक स्थित रहता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है ।
प्रोफेसर शुमिंग् लिखते हैं प्रस्तुत अध्ययन के मुद्रालेख में उस साधक का वर्णन मिलता है जिसने बाहर की वासना से मुक्त हो कर स्रोत के प्रवाह को रोक दिया है। लोक नं. ३ में स्रोत का उल्लेख है पाँच, सात, नव और ग्यारह संख्य के श्लोक भी उसके अनुसंधान में हैं। वसव शब्द असाधारण है । बारवें और दसवें श्लोक में यह वसव आवश्यक भी नहीं है और हस्ति के अंकुश का यह छोटा रूप है ।
टिप्पणी- प्रस्तुत प्रति के १२ वें और दसवें श्लोक में दसव शब्द आया नहीं है। फिर किस आधार पर प्रोफेसर शुटिंग ने यह टिप्पणी की है कहा नहीं जा सकता
एवं से सिद्धे बुद्धे० ॥ गतार्थः ।
इति वद्धमाण नाम एकोनत्रिंशतितमं अध्ययनम्
वायु अतर्षि प्रोक्त तीसवां अध्ययन
हजारों माइलों का यह विस्तृत भूखंड विचित्रताओं का आगार है । विविधता और विचित्रता में ही सृष्टि की सुषमा है। पर प्रश्न है विश्व को विचित्रता दी किसने ? श्रद्धालू, मानस बोल उठेगा यह सृष्टि का विचित्रता भरा सौन्दर्य उस अनंत शक्तिमान करुणामय विराट पुरुष की देन हैं । किन्तु यह उत्तर जितना सरल है तर्क की तुला पर उतना ही पेचीदा बन जाता है, क्योंकि इसके सामने पहला ही प्रश्न आता है उस विराद शक्तिमान करुणामय ने एक ओर अपनी सृष्टि में सुन्दर भव्य आकृतियां सजाई हैं तो उसे दूसरी ओर काली कुरूप और बीभत्स आकृतियां रखने की आवश्यकता ही क्या थी ? विकृत आकृतियों को रखने में करुणामय की करुणा पर प्रश्न चिह्न लग जाता है।
विश्व की विचित्रता का रहस्य जानने के लिये हमें उसे दो रूप में बांटना होगा। एक प्राकृतिक दूसरी प्राणिजन्य । प्रकृति का विचित्रता भरा सौन्दर्य स्वभावगत है । सूर्य दिन को ही आता है, रात को क्यों नहीं ? पूर्व में ही उदित होता है पश्चिम में क्यों नहीं ? आम ग्रीष्म में ही आता है, शीतकाल में क्यों नहीं ? गेहूं की फली ही लम्बी और बालवाली होती है ऐसी जुआर की क्यों नहीं, मथुर के जैसे पंख रंगे गये हैं वैसे कुक्कुट के क्यों नहीं, इन सबका समाधान तर्क के पास नहीं है, वह स्वभावगत है ।
प्राणिजन्य विचित्रता का समाधान स्वभाव से नहीं हो सकता। क्योंकि सभी मनुष्यों का स्वभाव समान होने पर भी बुद्धिकृत भेद हैं । एक व्यक्ति एक घंटे में दस श्लोक रट लेता है, जबकि दूसरा दस घंटे में भी श्लोक याद नहीं कर सकता । एक ही प्रकार की बीमारीवाले, दो रोगियों को एक ही डॉक्टर एक ही प्रकार की दवा देता है फिर भी एक स्वस्थ हो जाता है, जबकि दूसरा रोग में वृद्धि पाता है। इसका रहस्य क्या है ? इसका समाधान खभाव के पास नहीं कर्मवाद के पास है ।
1
1