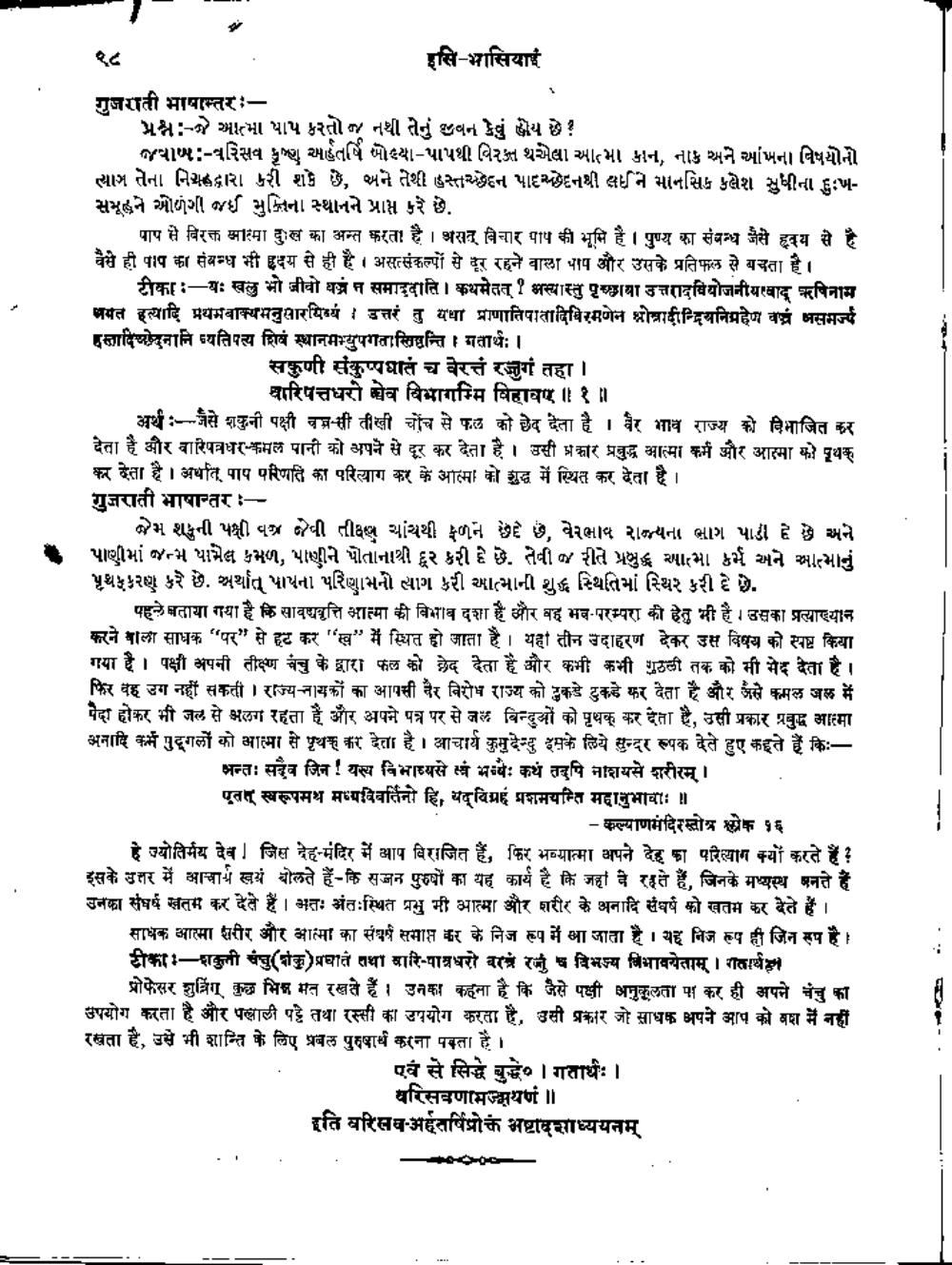________________
इसि-भासियाई
गुजराती भाषान्तर:
પ્રશ્ન:-જે આત્મા પાપ કરતો જ નથી તેનું જીવન કેવું હોય છે?
જવાબ:-વરિસવ કૃષ્ણ અહેતર્ષિ બોલ્યા-પાપથી વિરકત થએલા આત્મા કાન, નાક અને આંખના વિષયોનો યાગ તેના નિરહદ્રારા કરી શકે છે, અને તેથી હસ્તદન પાદ છેદનથી લઈને માનસિક કલેશ સુધીના દુઃખસમૂહને ઓળગી જઈ મુક્તિના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.
पाप से विरक्त मारमा दुख का अन्त करता है । असत् विचार पाप की भूमि है । पुण्य का संबन्ध जैसे हृदय से है वैसे ही पाप का संबन्ध भी हृदय से ही है । असत्संकल्पों से दूर रहने वाला पाप और उसके प्रतिफल से बरता है।
टीका:-यः खलु भो जीवो धनं न समाइदाति । कथमेतत् । अस्यास्तु पृछाया उत्तरादवियोजनीयवाद् ऋषिनाम भयत इत्यादि प्रथमवाक्यमनुसारयिव्यं । उत्तरं तु यथा प्राणातिपातादिविरमणेन श्रोत्रादीन्द्रियनिग्रहेण वनं असमर्म इस्लादियदनानि व्यतिपत्य शिवं स्थानमभ्युपगतास्तिष्ठन्ति । मतार्थः ।
सकुणी संकुप्पघातं च वेरत्तं रज्जुगं तहा।
वारिपत्तधरो श्वेव विभागम्मि विहावए ॥१॥ अर्थ:-जैसे शकुनी पक्षी वन-सी तीखी चोंच से फल को छेद देता है । वैर भाव राज्य को विभाजित कर देता है और वारिपत्रधर-कमल पानी को अपने से दूर कर देता है। उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा कर्म और आत्मा को पृथक कर देता है। अर्थात् पाप परिणति का परित्याग कर के आत्मा को शुद्ध में स्थित कर देता है। गुजराती भाषान्तर:
જેમ શકુની પક્ષી વક્ર જેવી તીવણ ચાંચથી ફળને છેદે છે, વેરભાવ રાજ્યના ભાગ પાડી દે છે અને
જન્મ પામેલ કમળ, પાણીને પોતાનાથી દૂર કરી દે છે. તેવી જ રીતે પ્રબુદ્ધ આત્મા કર્મ અને આત્માનું પૃથકકરણ કરે છે. અર્થાત્ પાપના પરિણામને ત્યાગ કરી આત્માની શુદ્ધ સ્થિતિમાં સ્થિર કરી દે છે.
पहले बताया गया है कि सावधवृत्ति भात्मा की विभाव दशा है और वह भव-परम्परा की हेतु भी है । उसका प्रत्याख्यान करने वाला साधक "पर" से हट कर "ख" में स्थित हो जाता है। यहा तीन उदाहरण देकर उस विषय को स्पष्ट किया गया है। पक्षी अपनी तीक्ष्ण चंचु के द्वारा फल को छेद देता है और कभी कभी गुठली तक को मी मेद देता है। फिर वह उग नहीं सकती । राज्य-नायकों का आपसी वैर विरोध राज्य को टुकडे टुकड़े कर देता है और जैसे कमल जल में पैदा होकर भी जल से अलग रहता है और अपने पत्र पर से जल बिन्दुओं को पृथक् कर देता है, उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा अनादि कर्म पुद्गलों को आत्मा से पृथक् कर देता है। आचार्य कुमुदेन्दु इसके लिये सुन्दर रूपक देते हुए कहते हैं कि:
अन्तः सदेव जिन! यस्य विभाध्यसे स्त्र भन्यः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् । एतत् स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि, यदविग्रह प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥
-कल्याणमंदिरस्तोत्र श्ोक १६ हे ज्योतिर्मय देव| जिस देहन्मंदिर में आप विराजित हैं, फिर भव्यात्मा अपने देह का परित्याग क्यों करते हैं? इसके उत्तर में आचार्य स्वयं बोलते हैं-कि सज्जन पुरुषों का यह कार्य है कि जहां वे रहते हैं, जिनके मध्यस्थ बनते हैं उनका संघर्ष खतम कर देते हैं। अतः अंतःस्थित प्रभु मी आत्मा और शरीर के अनादि संघर्ष को खतम कर देते हैं।
साधक आत्मा शरीर और आत्मा का संघर्ष समाप्त कर के निज रूप में आ जाता है। यह निज रूपही जिन रूप है। टीका-शकुनी संचु(कु)प्रघात तथा बारि-पानधरो बरनं रस्तुं व विभज्य विभावयेताम् । गतार्थ
प्रोफेसर शुत्रिंग कुछ भिन्न मत रखते हैं। उनका कहना है कि जैसे पक्षी अनुकूलता पा कर ही अपने चंच का उपयोग करता है और पखाली पट्टे तथा रस्सी का उपयोग करता है, उसी प्रकार जो साधक अपने आप को वश में नहीं रखता है, उसे भी शान्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है।
एवं से सिद्ध बुद्धे । गतार्थः।
परिसवणामज्झयणं॥ इति वरिसव-अर्हतर्षिप्रोक्तं अष्टादशाध्ययनम्