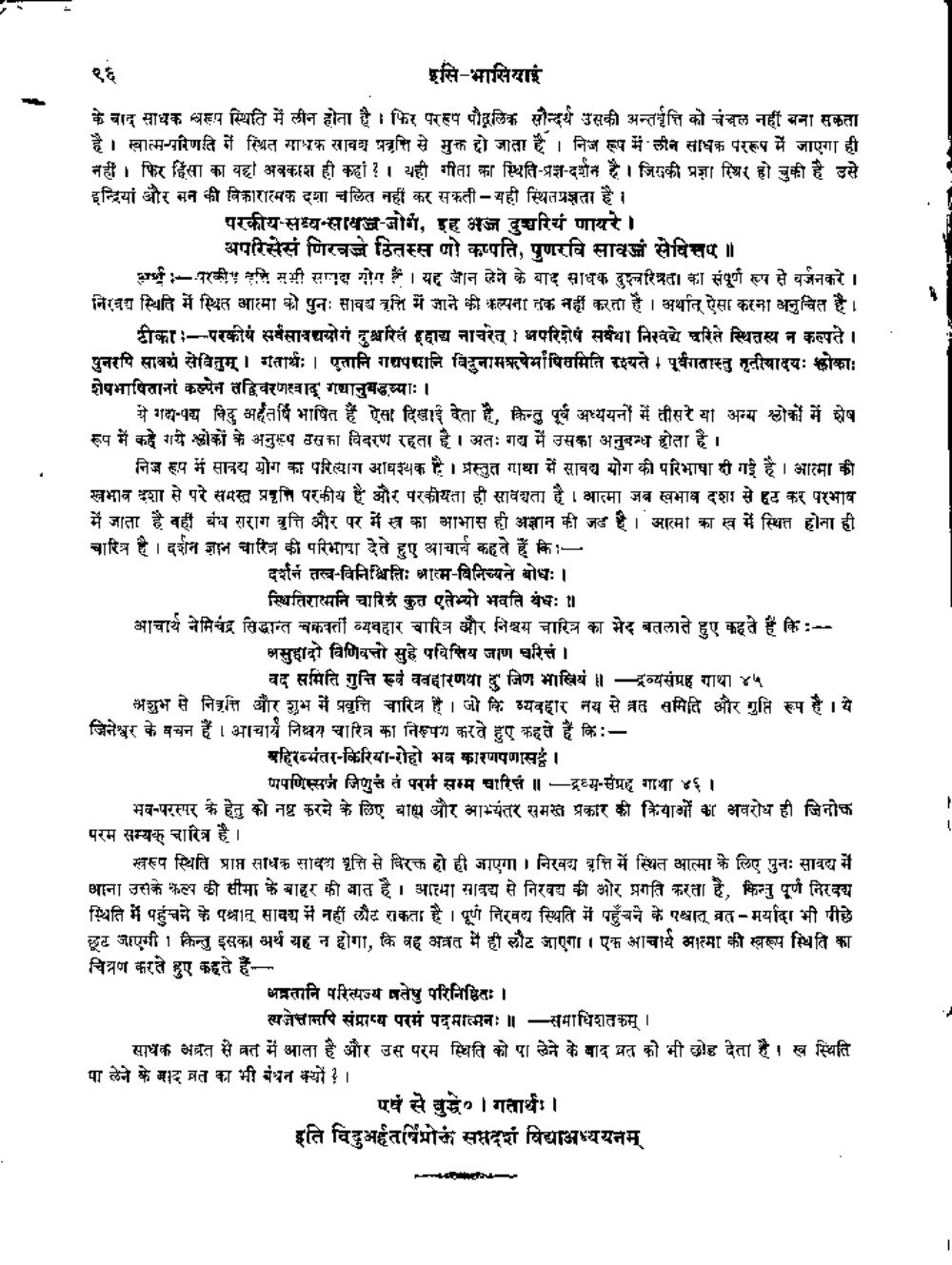________________
-
---
-
-
एसि-भासियाई के बाद साधक बरूप स्थिति में लीन होता है। फिर पररूप पौलिक सौन्दर्य उसकी अन्तर्वृत्ति को चंचल नहीं बना सकता है। खात्म-परिणति में स्थित गाधक सावध प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है । निज रूप में लीन साधक पररूप में जाएगा ही नहीं। फिर हिंसा का वह अक्काश ही कहां? । यही गीता का स्थिति-प्रज्ञ-दर्शन है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है उसे इन्द्रियां और मन की विकारात्मक दशा चलित नहीं कर सकती- यही स्थितप्रज्ञता है।
परकीय-सभ्य-सावज-जोग, इह अज दुश्चरियं णायरे।
अपरिसेसं णिरचज्जे ठितस्स णो कप्पति, पूणरवि सावज सेवित्तए॥ अर्थ:-परकी इति सभी सदा योग है । यह जान लेने के बाद साधक दुश्चरित्रता का संपूर्ण रूप से वर्जनकरे । निरनद्य स्थिति में स्थित आत्मा को पुनः सावध वृत्ति में जाने की कल्पना तक नहीं करता है । अर्थात ऐसा करना अनुचित है।
टीका:--परकीय सर्वसावधयोगं दुश्चरित इदाद्य नाचरेत् । अपरिशेष सर्वथा निरवये घरि स्थितस्य न कल्पते। . पुनरपि सावयं सेवितुम् । गत्तार्थः । एतानि गग्रपयानि विदुनामऋषेर्माधिसमिति रश्यते । पूर्वगतास्तु तृतीयादयः कोकाः शेषभाषितानां कल्पेन तद्विवरणवाद' गधानुबद्धव्याः ।
ये गदा-पय चिदु भईतर्षि भाषित हैं ऐसा दिखाई देता है, किन्तु पूर्व अध्ययनों में तीसरे या अन्य श्लोकों में शेष रूप में कहे गये श्लोकों के अनुरूप उसका विवरण रहता है । अतः गद्य में उसका अनुबन्ध होता है।
निज रूप में सानद्य योग का परित्याग आवश्यक है। प्रस्तुत गाथा में सावद्य योग की परिभाषा दी गई है । आत्मा की खभाव दशा से परे समस्त प्रवृति परकीय है और परकीयता ही सावधता है । आत्मा जब स्वभाव दशा से हट कर परभाष में जाता है वहीं बंध गराग बुत्ति और पर में स्त्र का आभास ही अज्ञान की जद है। आत्मा का स्त्र में स्थित्त होना ही चारित्र है । दर्शन जान चारित्र की परिभाषा देते हुए आचार्च कहते हैं कि
दर्शन तस्व-विनिश्चितिः आत्म-विनिच्यने बोधः।
स्थितिरात्मनि चावि कुत एतेभ्यो भवति बंधः ।। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र का भेद बतलाते हुए कहते हैं कि :
असुहादो विणिवत्तो सुहे पवित्तिय जाण चरितं ।
बद समिति गुत्ति स्वं ववहारणया दु जिण भाखियं ॥ द्रव्यसंग्रह गाथा ४५ अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है। जो कि व्यवहार नय से बात समिति और गुप्ति रूप है । ये जिनेश्वर के वचन हैं । आचार्य निश्चय चारित्र का निरूपग करते हुए कहते हैं कि :
पहिरमंतर-किरिया-रोहो भव कारणपणासहूँ।
पणिस्सजे जिणु तं परमं सम्म चारितं ॥ -द्रध्य-संग्रह गाथा ४६ । भव-परस्पर के हेतु को नष्ट करने के लिए बाध और आभ्यंतर समस्त प्रकार की क्रियाओं का अवरोध ही जिनोक परम सम्यक् चारित्र है।
स्वरूप स्थिति प्राप्त साधक सादा वृत्ति से विरक्त हो ही जाएगा। निरखद्य बृत्ति में स्थित आत्मा के लिए पुनः सावध में भाना उसके कल्य की सीमा के बाहर की बात है। आत्मा सावध से निरवद्य की ओर प्रगति करता है, किन्नु पूर्ण निरवद्य स्थिति में पहुंचने के पश्चात् साक्य में नहीं लौट सकता है । पूर्ण निरवद्य स्थिति में पहुँचने के पश्चात् व्रत-मर्यादा भी पीछे छूट जाएगी। किन्तु इसका अर्थ यह न होगा, कि वह अत्रत में ही लौट जाएगा। एक आचार्य आत्मा की स्वरूप स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं
अवतानि परित्यज्य तेषु परिनिष्ठितः।
स्वजेत्तामपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः॥ -समाधिशतकम् । साधक अव्रत से व्रत में आता है और उस परम स्थिति को पा लेने के बाद व्रत को भी छोड़ देता है। ख स्थिति पा लेने के बाद व्रत का भी धन क्यों है।
पर्व से बुद्धे । गताः । इति विदुअर्हतर्षिमोकं सप्तदर्श विद्याअध्ययनम्