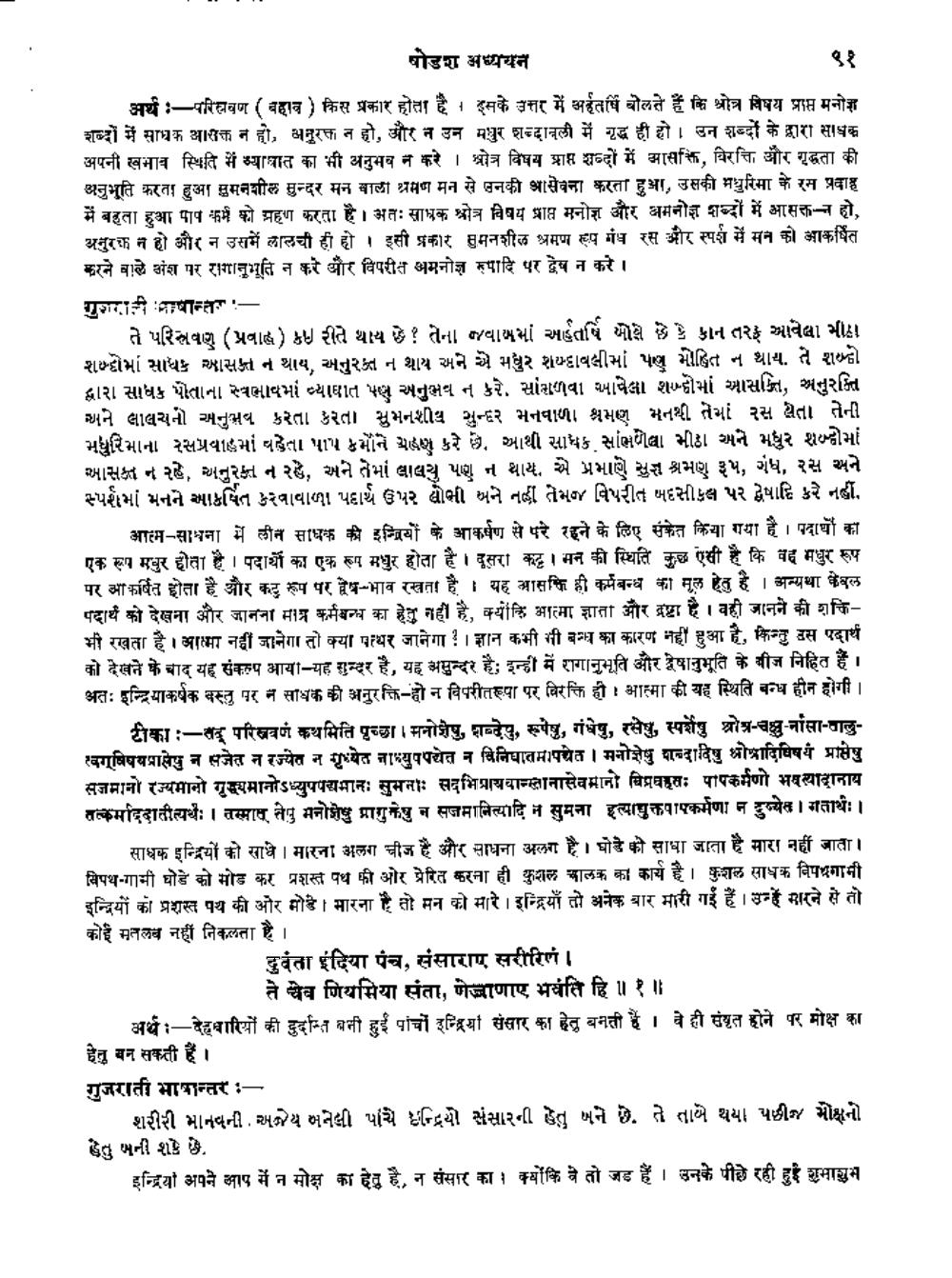________________
षोडश अध्ययन
अर्थ:-परित्रवण (बहाव) किस प्रकार होता है। इसके उत्तर में अतिर्षि बोलते हैं कि श्रोत्र विषय प्राप्त मनोज्ञ शब्दों में साधक आसक्त न हो, अनुरक्त न हो, और न उन मधुर शब्दावली में गृद्ध ही हो। उन शब्दों के द्वारा साधक अपनी खभाव स्थिति में व्याघात का भी अनुभव न करे । श्रोत्र विषय प्राप्त शब्दों में आसक्ति, विरत्ति और गृद्धता की अनुभूति करता हुआ सुमनशील सुन्दर मन बाला श्रमण मन से उनकी श्रासेवना करता हुआ, उसकी मधुरिमा के रम प्रवाह में बहता हुआ पाप कर्म को ग्रहण करता है। अतः साधक श्रोत्र विषय प्राप्त मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में आसक्त-न हो, अनुरक न हो और न उसमें लालची ही हो । इसी प्रकार सुमनशील श्रमण रूप गंध रस और स्पर्श में मन को आकर्षित करने वाले अंश पर रागानुभूति न करे और विपरीत अमनोज्ञ रूपादि पर द्वेष न करे। गुशहाली भाषान्त':
તે પરિભ્રવણ (પ્રવાહ) કઈ રીતે થાય છે? તેના જવાબમાં અહર્ષિ ઓલે છે કે કાન તરફ આવેલા મીઠા શબ્દોમાં સાધક આસક્ત ન થાય, અનુરક્ત ન થાય અને એ મધુર શબ્દાવલીમાં પણ મોહિત ન થાય. તે શબ્દો દ્વારા સાધક પોતાના સ્વભાવમાં વ્યાઘાત પડ્યું અનુભવ ન કરે. સાંભળવા આવેલા શબ્દોમાં આસક્તિ, અસુરક્તિ અને લાલચનો અનુભવ કરતા કરતા સુમન શીવ સુન્દર મનવાળા શ્રમણ મનથી તેમાં રસ લેતા તેની મધુરિમાના રસપ્રવાહમાં વહેતા પાપ કર્મોને ગ્રહણ કરે છે, આથી સાધક સાંભળેલા મીઠા અને મધુર શબ્દોમાં આસક્ત ન રહે, અનુરક્ત ન રહે, અને તેમાં લાલચુ પણ ન થાય. એ પ્રમાણે સુજ્ઞ શ્રમણ રૂપ, ગંધ, રસ અને પશેમાં મનને આકર્ષિત કરવાવાળા પદાર્થ ઉપર લોભી બને નહીં તેમજ વિપરીત બદસકલ પર છેષાદિ કરે નહીં,
आत्म-साधना में लीन साधक की इन्द्रियों के आकर्षण से परे रहने के लिए संकेत किया गया है । पदार्थों का एक रूप मधुर होता है। पदार्थों का एक रूप मधुर होता है। दूसरा कटु । मन की स्थिति कुछ ऐसी है कि वह मधुर रूप पर आकर्षित होता है और कटु रूप पर वेष-भाव रखता है । यह आसक्ति ही कर्मबन्ध का मूल हेतु है । अन्यथा केवल पदार्थ को देखना और जानना मात्र कर्मबन्ध का हेतु नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा है। वही जानने की शक्तिभी रखता है। आत्मा नहीं जानेगा तो क्या पत्थर जानेगा? । ज्ञान कभी भी बन्ध का कारण नहीं हुआ है, किन्तु उस पदार्थ को देखने के बाद यह संकल्प आया-यह सुन्दर है, यह असुन्दर है। इन्ही में रागानुभूति और देषानुभूति के बीज निहित हैं। अतः इन्द्रियाकर्षक वस्तु पर न साधक की अनुरक्ति-हो न विपरीतरूपा पर विरक्ति ही । आत्मा की यह स्थिति बन्ध हीन होगी ।
टीका:-तद् परिस्रवणं कथमिति पृच्छा । मनोज्ञेषु, शब्देषु, रूपेषु, गंधेषु, रसेषु, स्पर्शेषु श्रोत्र-चक्षु-नांसा-तालुस्वविषयमालेषु न सजेत न रज्येत न गृध्येत नाण्युपपद्यत न विनिधातमापयेत । मनोज्ञेषु चान्दादिषु श्रोत्रादिषिषयं प्रासेषु सजमानो रज्यमानो गृस्यमानोऽध्युपपद्यमानः सुमना सदभिप्रायवानस्तानासेवमानो विप्रवाहसः पापकर्मणो भवस्यादानाय तत्कर्माददातीत्यर्थः । तस्मात तेनु मनोज्ञेषु प्रागुकेषु न सजमानित्यादि न सुमना हत्याधुक्तपापकर्मणा न दुष्येत । गतार्थः ।
साधक इन्द्रियों को साधे । मारना अलग चीज है और साधना अलग है। घोडे को साधा जाता है मारा नहीं जाता। विपथ-गामी घोडे को मोड कर प्रशस्त पथ की ओर प्रेरित करना ही कुशल बालक का कार्य है। कुशल साधक विपथगामी इन्द्रियों को प्रशस्त पथ की ओर मोडे। मारना है तो मन को मारे । इन्द्रियाँ तो अनेक बार मारी गई हैं। उन्हें मारने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है।
दुवंता इंदिया पंच, संसाराए सरीरिणं ।
ते चेव णियमिया संता, णेजाणाए भवति हि ॥१॥ अर्थ:-देहधारियों की दुर्दान्त बनी हुई पांचों इन्द्रियाँ संसार का हेतु बनती हैं। वे ही संवृत होने पर मोक्ष का हेतु बन सकती है। गुजराती भाषान्तर:
શરીરી માનવની અજેય બનેલી પાંચ ઇન્દ્રિયો સંસારની હેતુ બને છે. તે તાબે થયા પછી જ મોક્ષનો હેતુ બની શકે છે.
इन्द्रियो अपने आप में न मोक्ष का हेतु है, न संसार का। क्योंकि वे तो जड हैं। उनके पीछे रही हुई शुभाशुभ