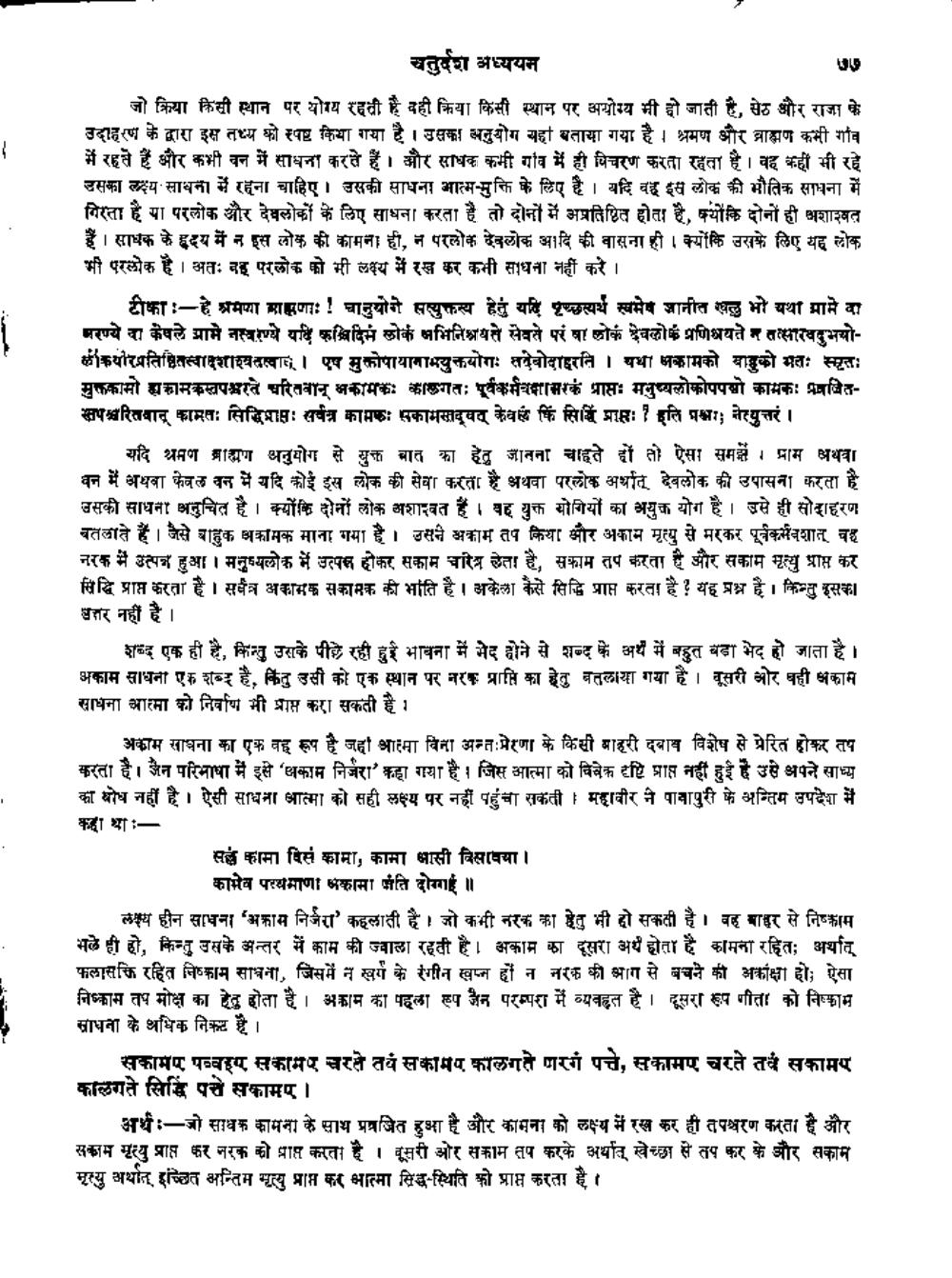________________
७७
चतुर्दश अध्ययन जो क्रिया किसी स्थान पर योग्य रहती है वही क्रिया किसी स्थान पर अयोग्य भी हो जाती है, सेठ और राजा के उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। उसका अनुयोग यहां बताया गया है। श्रमण और ब्राह्मण कभी गांव में रहते हैं और कभी वन में साधना करते हैं। और साधक कमी गांव में ही विचरण करता रहता है। वह कहीं भी रहे उसका लक्ष्य साधना में रहना चाहिए। उसकी साधना मात्म-मुक्ति के लिए है। यदि वह इस लोक की भौतिक साधना में गिरता है या परलोक और देवलोकों के लिए साधना करता है तो दोनों में अप्रतिष्ठित होता है, क्योंकि दोनों ही अशाश्वत हैं। साधक के हृदय में न इस लोक की कामना ही, न परलोक देवलोक आदि की वासना ही । क्योंकि उसके लिए यह लोक मी परलोक है । अतः नइ परलोक को मी लक्ष्य में रख कर कभी साधना नहीं करे ।
टीका:-हे श्रमप्या मालणाः! चानुयोगे सत्युक्तस्य हेतु यदि पृच्छत्यर्थ स्वमेव जानीत खलु भो यथा मामे वा भरण्ये वा केषले ग्रामे नस्वरण्ये यदि कनिदिन लोक अभिनिश्चय सेवते परं षा लोक देवलोक प्रणिश्रयते तसारवदुभयोलोकयोरप्रतिश्चितस्वादशाश्वतवार । एष मुक्कोपायामामयुक्तयोगः तदेवोदाहरति । यथा अकामको बाबुको मतः स्मृतः मुक्तकामो झकामकस्वपश्वरते चरितवान् भकामकः कालगतः पूर्वकर्मरामरकं प्राप्तः मनुष्यलोकोपपत्रो कामकः प्रवजितसपश्चरितवान् कामतः सिद्धिप्रासः सर्वत्र कामकः सकामसावत् केवल किं सिविं प्रातः इति प्रश्न अत्युत्तरं ।
यदि श्रमण ब्राह्मण अनुयोग से युक्त बात का हेतु जानना चाहते हो तो ऐसा समझें। प्राम अथवा वन में अथवा केवल वन में यदि कोई इस लोक की सेवा करता है अथवा परलोक अर्थात देवलोक की उपासना करता है उसकी साधना अनुचित है। क्योंकि दोनों लोक अशाश्वत है। यह युक्त योगियों का अयुक्त योग है। उसे ही सोदाहरण बतलाते हैं। जैसे बाहुक अकामक माना गया है। उसने अकाम तप किया और अकाम मृत्यु से मरकर पूर्व कर्मवशात् वह नरक में उत्पन्न हुआ। मनुष्यलोक में उत्पन होकर सकाम चरित्र लेता है, सकाम तप करता है और सकाम मृत्यु प्राप्त कर विद्धि प्राप्त करता है। सर्वत्र अकामक सकामक की भांति है। अकेला कैसे सिद्धि प्राप्त करता है ? यह प्रश्न है। किन्तु इसका उत्तर नहीं है।
शब्द एक ही है, किन्तु उसके पीछे रही हुई भावना में भेद होने से शन्द के अर्थ में बहुत बड़ा भेद हो जाता है। अकाम साधना एक शब्द है, किंतु उसी को एक स्थान पर नरक प्राप्ति का हेतु बतलाया गया है। दूसरी ओर वही अकाम साधना आत्मा को निर्वाण मी प्राप्त करा सकती है।
अकाम साधना का एक वह रूप है जहाँ आत्मा विना अन्तःप्रेरणा के किसी बाहरी दबाव विशेष से प्रेरित होकर तप करता है। जैन परिभाषा में इसे “अकाम निर्जरा कहा गया है। जिस आत्मा को विबेक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उसे अपने साध्य का बोध नहीं है। ऐसी साधना आत्मा को सही लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकती । महावीर ने पावापुरी के अन्तिम उपदेश में कहा था:
सल्लकामा विसं कामा, कामा पासी विसावया ।
कामेव परयमाणा अकामा ति दोगाई॥ लक्ष्य हीन साधना 'अकाम निर्जरा' कहलाती है। जो कभी नरक का हेतु भी हो सकती है। वह बाहर से निष्काम भले ही हो, किन्तु उसके अन्तर में काम की ज्वाला रहती है। अकाम का दूसरा अर्थ होता है कामना रहित; अर्थात् फलासक्ति रहित निष्काम साधना, जिसमें न खर्ग के रंगीन स्वप्न हो न नरक की आग से बचने की अकांक्षा हो; ऐसा निष्काम तप मोक्ष का हेतु होता है। अकाम का पहला रूप जैन परम्परा में व्यवहृत है। दूसरा रूप गीता को निष्काम साधना के अधिक निकट है।
सकामयः पन्चाइए सकामए चरते तवं सकामय कालगते णरगं पत्ते, सकामए चरते तवं सकामय कालगते सिद्धि पसे सकामए ।
अर्थ:-जो साधक कामना के साथ प्रप्रजित हुभा है और कामना को लक्ष्य में रख कर ही तपश्चरण करता है और सकाम मृत्यु प्राप्त कर नरक को प्राप्त करता है। दूसरी ओर सकाम तप करके अर्थात् खेच्छा से तप कर के और सकाम मृत्यु अथोत् इच्छित अन्तिम मूत्यु प्राप्त कर भात्मा सिद्ध-स्थिति को प्राप्त करता है।
-