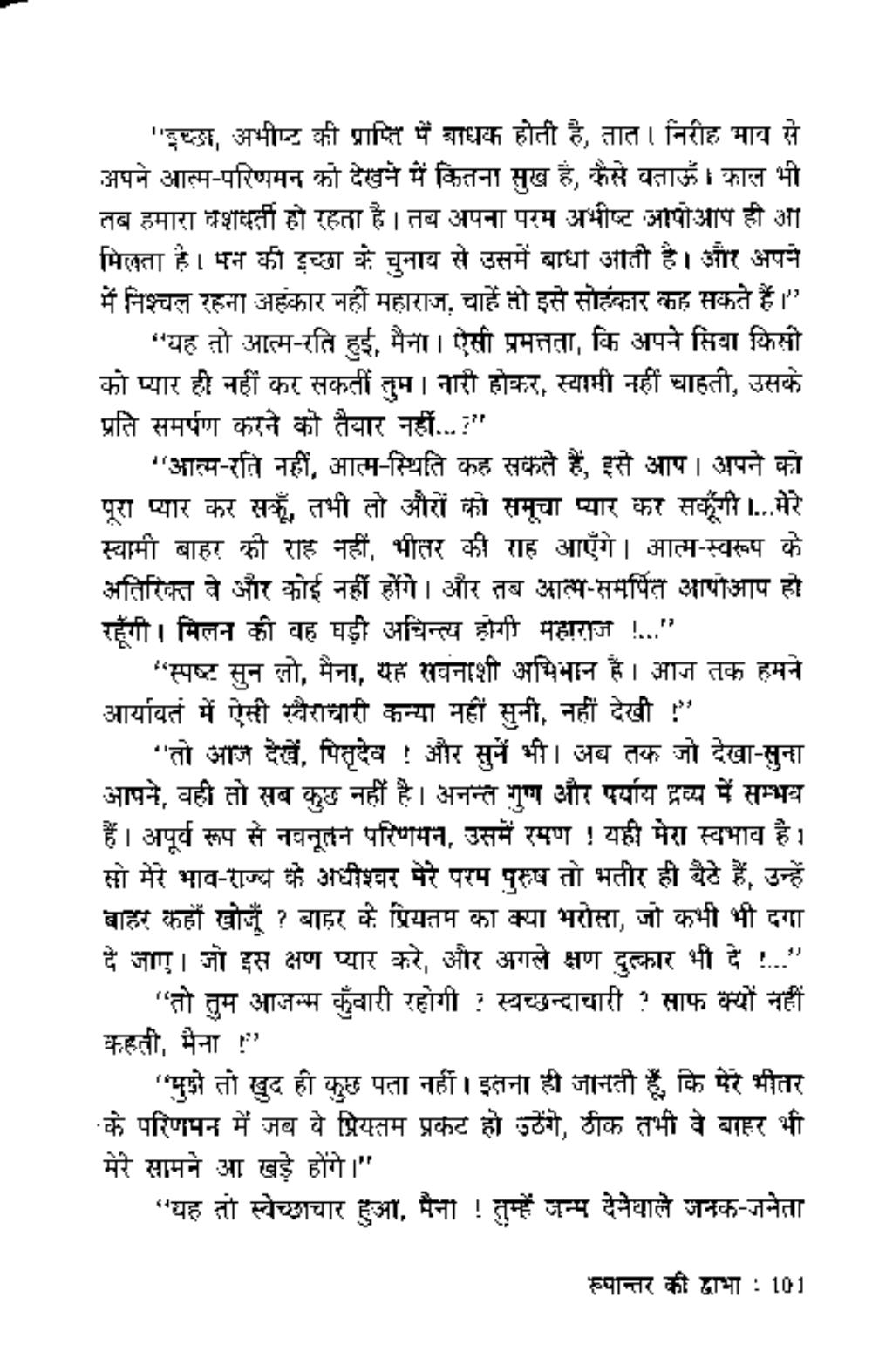________________
'इच्छा, अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक होती है, तात। निरीह भाव से अपने आत्म-परिणमन को देखने में कितना सुख हैं, कैसे बताऊँ । काल भी तब हमारा प्रशवर्ती हो रहता है । तब अपना परम अभीष्ट आपोआप ही आ मिलता है। मन की इच्छा के चुनाव से उसमें बाधा आती है। और अपने में निश्चल रहना अहंकार नहीं महाराज, चाहें तो इसे सोहंकार कह सकते हैं।" ___ "यह तो आत्म-रति हुई, मैना । ऐसी प्रमत्तता, कि अपने सिया किसी को प्यार ही नहीं कर सकतीं तुम । नारी होकर, स्वामी नहीं चाहती, उसके प्रति समर्पण करने को तैयार नहीं..."
"आत्म-रति नहीं, आत्म-स्थिति कह सकते हैं, इसे आप । अपने को पूरा प्यार कर सकूँ, तभी तो औरों को समूचा प्यार कर सकूँगी।...मेरे स्वामी बाहर की राह नहीं, भीतर की राह आएँगे। आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त वे और कोई नहीं होंगे। और तब आत्म-समर्पित आपोआप हो रहूँगी। मिलन की वह घड़ी अचिन्त्य होगी महाराज !..."
__“स्पष्ट सुन लो, मैना, यह सर्वनाशी अभिभान हैं। आज तक हमने आर्यावतं में ऐसी स्वैराचारी कन्या नहीं सुनी, नहीं देखी !" ___"तो आज देखें, पितृदेव ! और सुनें भी। अब तक जो देखा-सुना आपने, वही तो सब कुछ नहीं है। अनन्त गुण और पर्याय द्रव्य में सम्भव हैं । अपूर्व रूप से नवनूतन परिणमन, उसमें रपण ! यही मेरा स्वभाव है। सो मेरे भाव-राज्य के अधीश्वर मेरे परम पुरुष तो भतीर ही बैठे हैं, उन्हें बाहर कहाँ खोजें ? बाहर के प्रियतम का क्या भरोसा, जो कभी भी दगा दे जाए। जो इस क्षण प्यार करे, और अगले क्षण दुत्कार भी दे !.."
"तो तुम आजम्म कुँवारी रहोगी : स्वच्छन्दाचारी : साफ क्यों नहीं कहती, मैना ।" __"पुछो तो खुद ही कुछ पता नहीं। इतना ही जानती हूँ, कि मेरे भीतर के परिणपन में जब वे प्रियतम प्रकट हो उठेंगे, ठीक तभी वे बाहर भी मेरे सामने आ खड़े होंगे।"
"यह तो स्वेच्छाचार हुआ, मैना ! तुम्हें जन्म देनेवाले जनक-जनेता
रूपान्तर की द्वाभा : 101