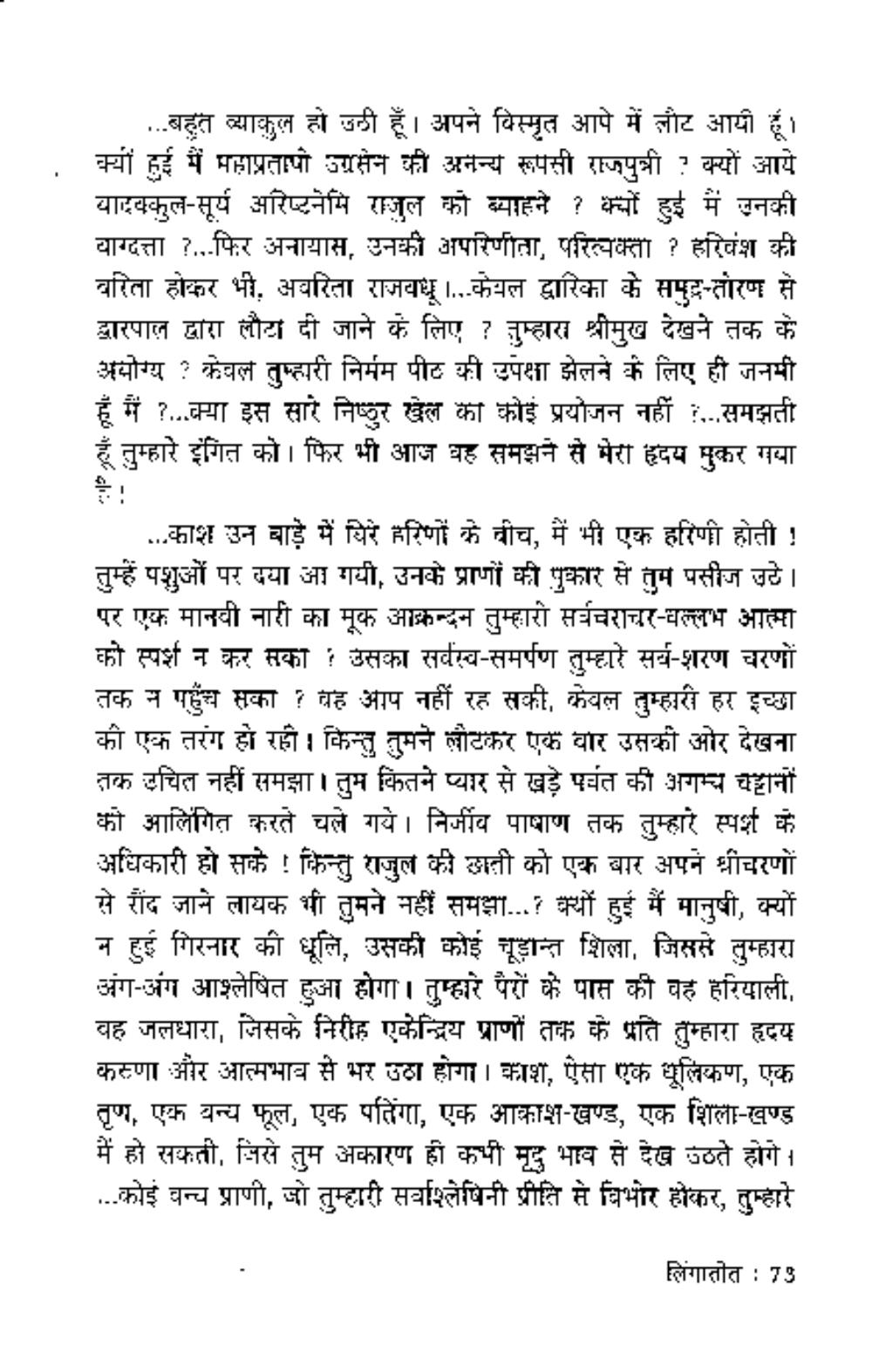________________
..बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। अपने विस्मृत आपे में लौट आयी हूँ। क्यों हुई मैं महाप्रतापी उग्रसेन की अनन्य रूपसी राजपुत्री ? क्यों आये यादवकुल-सूर्य अरिष्टनेमि राजुल को व्याहने ? क्यों हुई मैं उनकी वाग्दत्ता ?... फिर अनायास, उनकी अपरिणीता, परित्यक्ता ? हरिवंश की वरिता होकर भी, अवरिता राजवधू ।... केवल द्वारिका के समुद्र-तोरण से द्वारपाल द्वारा लौटा दी जाने के लिए ? तुम्हारा श्रीमुख देखने तक के अयोग्य ? केवल तुम्हारी निर्मम पीट की उपेक्षा झेलने के लिए ही जनमी हूँ मैं ?... क्या इस सारे निष्ठुर खेल का कोई प्रयोजन नहीं : ... समझती हूँ तुम्हारे इंगित को । फिर भी आज वह समझने से मेरा हृदय मुकर गया
... काश उन बाड़े में घिरे हरिणों के बीच, मैं भी एक हरिणी होती ! तुम्हें पशुओं पर दया आ गयी, उनके प्राणों की पुकार से तुम पसीज उठे । पर एक मानवी नारी का मूक आक्रन्दन तुम्हारी सर्वचराचर - वल्लभ आत्मा को स्पर्श न कर सका उसका सर्वस्व समर्पण तुम्हारे सर्व-शरण चरणों तक न पहुँच सका? वह आप नहीं रह सकी, केवल तुम्हारी हर इच्छा की एक तरंग हो रही। किन्तु तुमने लौटकर एक बार उसकी ओर देखना तक उचित नहीं समझा। तुम कितने प्यार से खड़े पर्वत की अगम्य चट्टानों को आलिंगित करते चले गये। निर्जीव पाषाण तक तुम्हारे स्पर्श के अधिकारी हो सके ! किन्तु राजुल की छाती को एक बार अपने श्रीचरणों से रौंद जाने लायक भी तुमने नहीं समझा...? क्यों हुई मैं मानुषी, क्यों न हुई गिरनार की धूलि, उसकी कोई चूड़ान्त शिला, जिससे तुम्हारा अंग-अंग आश्लेषित हुआ होगा। तुम्हारे पैरों के पास की वह हरियाली, वह जलधारा, जिसके निरीह एकेन्द्रिय प्राणों तक के प्रति तुम्हारा हृदय करुणा और आत्मभाव से भर उठा होगा। काश, ऐसा एक धूलिकण, एक तृण, एक अन्य फूल, एक पतिंगा, एक आकाश खण्ड, एक शिला खण्ड मैं हो सकती, जिसे तुम अकारण ही कभी मृदु भाव से देख उठते होगे । ....कोई वन्य प्राणी, जो तुम्हारी सर्वाश्लेषिनी प्रीति से विभोर होकर, तुम्हारे
लिंगातीत 73