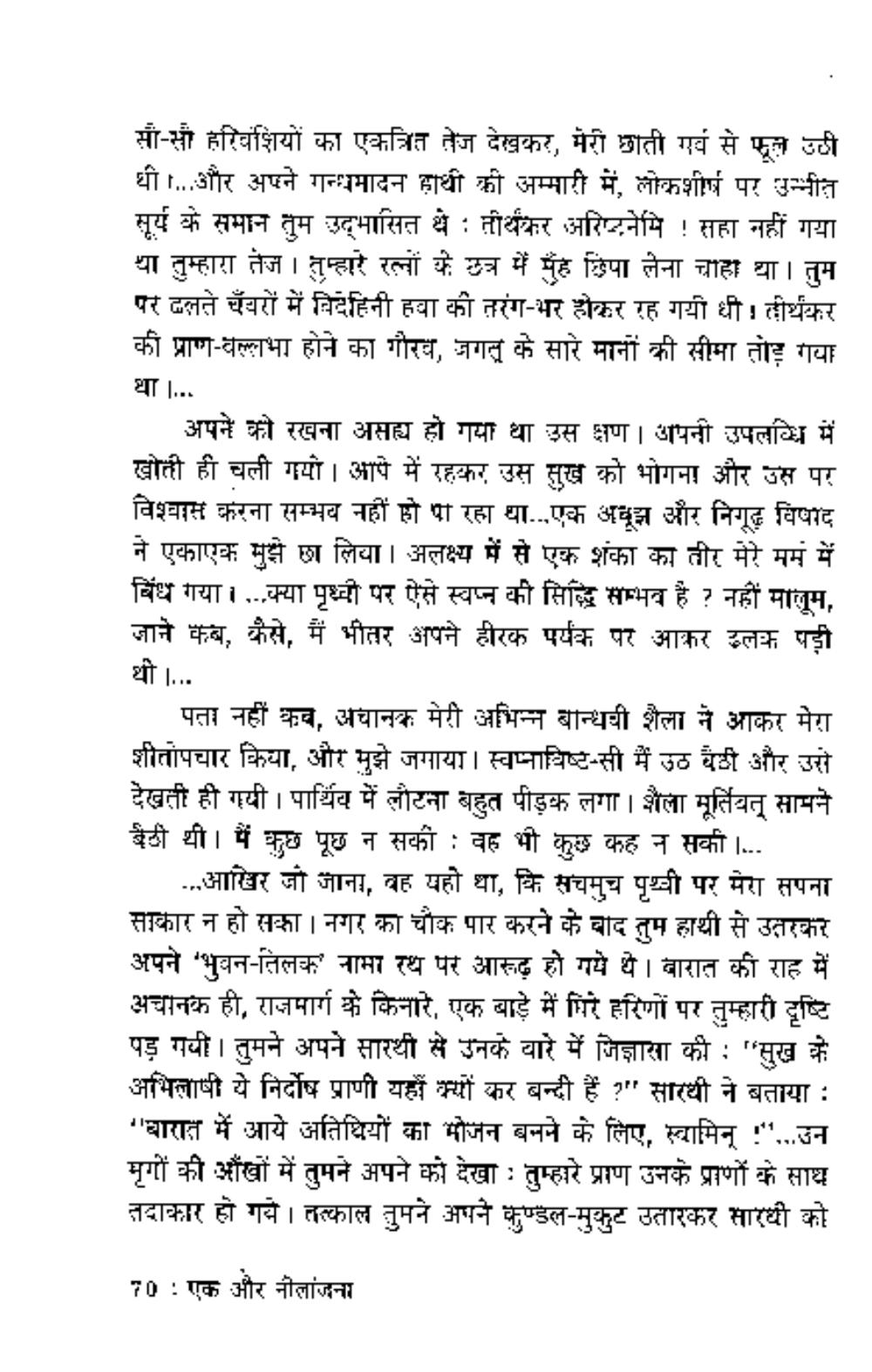________________
सौ-सौ हरिवंशियों का एकत्रित तेज देखकर, मेरी छाती गर्व से फूल उठी थी।...और अपने गन्धमादन हाथी की अम्मारी में, लोकशीर्ष पर उन्भीत सूर्य के समान तुम उद्भासित थे : तीर्थंकर अरिष्टनेमि ! सहा नहीं गया था तुम्हारा तेज । तुम्हारे रत्नों के छत्र में मुंह छिपा लेना चाहा था। तुम पर ढलते चैंबरों में विहिनी हवा की तरंग-भर होकर रह गयी थी। हीर्थंकर की प्राण-वल्लाभा होने का गौरव, जगत के सारे मानों की सीमा तोड़ गया था ।...
अपने को रखना असह्य हो गया था उस क्षण। अपनी उपलब्धि में खोती ही चली गयो। आपे में रहकर उस सुख को भोगना और उस पर विश्वास करना सम्भव नहीं हो पा रहा था...एक अबूझ और निगूढ विषाद ने एकाएक मुझे छा लिया। अलक्ष्य में से एक शंका का तीर मेरे ममं में बिंध गया। ...क्या पृथ्वी पर ऐसे स्वप्न की सिद्धि सम्भव है ? नहीं मालूम, जाने कब, कैसे, मैं भीतर अपने हीरक पर्यक पर आकर इलक पड़ी
थी।...
पता नहीं कब, अचानक मेरी अभिन्न बान्धवी शैला ने आकर मेरा शीतोपचार किया, और मुझे जगाया। स्वप्नाविष्ट-सी मैं उठ बैठी और उसे देखती ही गयी। पार्थिव में लौटना बहुत पीड़क लगा। शैला मूर्तियत् सामने बैठी थी। मैं कछ पूछ न सकी : वह भी कछ कह न सकी।...
...आखिर जो जाना, वह यहो था, कि सचमुच पृथ्वी पर मेरा सपना साकार न हो सका। नगर का चौक पार करने के बाद तुम हाथी से उतरकर अपने 'भुवन-तिलक' नामा रथ पर आरूढ़ हो गये थे। बारात की राह में अचानक ही, राजमार्ग के किनारे, एक बाड़े में घिरे हरिणों पर तुम्हारी दृष्टि पड़ गयी। तुमने अपने सारथी से उनके बारे में जिज्ञासा की : "सुख के अभिलाषी ये निर्दोष प्राणी यहाँ क्यों कर बन्दी हैं ?" सारथी ने बताया : "बारात में आये अतिथियों का भोजन बनने के लिए, स्वामिन् !"...उन मृगों की आँखों में तुमने अपने को देखा : तुम्हारे प्राण उनके प्राणों के साथ तदाकार हो गये। तत्काल तुमने अपने कुण्डल-मुकुट उतारकर सारथी को
70 : एक और नीलांजना